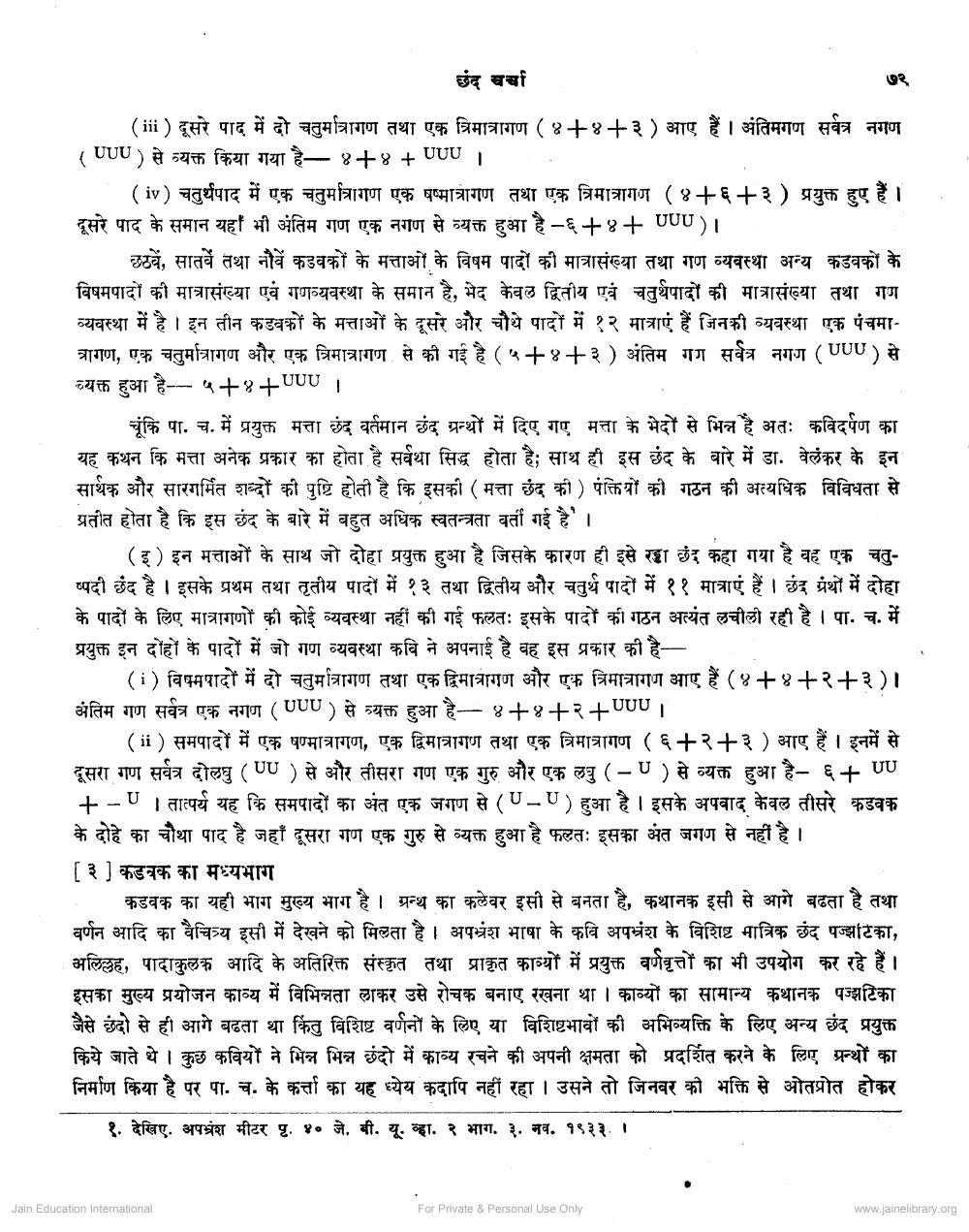________________
छंद चर्चा
(iii) दूसरे पाद में दो चतुर्मात्रागण तथा एक त्रिमात्रागण ( ४+४+३ ) आए हैं। अंतिमगण सर्वत्र नगण ( UUU ) से व्यक्त किया गया है— ४+४+ UUU 1
(iv) चतुर्थपाद में एक चतुर्मात्रागण एक षष्मात्रागण तथा एक त्रिमात्रागण ( ४+६+ ३ ) प्रयुक्त हुए हैं। दूसरे पाद के समान यहाँ भी अंतिम गण एक नगण से व्यक्त हुआ है - ६+४+ UUU)।
७१
छठवें, सातवें तथा नौवें कडवकों के मत्ताओं के विषम पादों की मात्रासंख्या तथा गण व्यवस्था अन्य कडवकों के विषमपादों की मात्रासंख्या एवं गणव्यवस्था के समान है, भेद केवल द्वितीय एवं चतुर्थपादों की मात्रासंख्या तथा गण व्यवस्था में है । इन तीन कडवकों के मत्ताओं के दूसरे और चौथे पादों में १२ मात्राएं हैं जिनकी व्यवस्था एक पंचमात्रागण, एक चतुर्मात्रागण और एक त्रिमात्रागण से की गई है ( ५+४+३ ) अंतिम गग सर्वत्र नगग ( UUU ) से व्यक्त हुआ है-- -- ५+४+ UUU 1
चूंकि पा. च. में प्रयुक्त मत्ता छंद वर्तमान छंद ग्रन्थों में दिए गए मत्ता के भेदों से भिन्न है अतः कविदर्पण का यह कथन कि मत्ता अनेक प्रकार का होता है सर्वथा सिद्ध होता है; साथ ही इस छंद के बारे में डा. वेलंकर के इन सार्थक और सारगर्मित शब्दों की पुष्टि होती है कि इसकी ( मत्ता छंद की ) पंक्तियों की गठन की अत्यधिक विविधता से प्रतीत होता है कि इस छंद के बारे में बहुत अधिक स्वतन्त्रता वर्ती गई है' ।
(इ) इन मत्ताओं के साथ जो दोहा प्रयुक्त हुआ है जिसके कारण ही इसे रड्डा छंद कहा गया है वह एक चतुपदी छंद है । इसके प्रथम तथा तृतीय पादों में १३ तथा द्वितीय और चतुर्थ पादों में ११ मात्राएं हैं । छंद ग्रंथों में दोहा के पादों के लिए मात्रागणों की कोई व्यवस्था नहीं की गई फलतः इसके पादों की गठन अत्यंत लचीली रही है । पा. च. में प्रयुक्त इन दोहों के पादों में जो गण व्यवस्था कवि ने अपनाई है वह इस प्रकार की है—
(i) विषमपादों में दो चतुर्मात्रागण तथा एक द्विमात्रागण और एक त्रिमात्रागण आए हैं (४+४+२+३)। अंतिम गण सर्वत्र एक नगण ( UUU ) से व्यक्त हुआ है — ४+४+२+ UUU|
(ii) समपादों में एक षण्मात्रागण, एक द्विमात्रागण तथा एक त्रिमात्रागण ( ६+२+३) आए हैं । इनमें से दूसरा गण सर्वत्र दोलघु (UU ) से और तीसरा गण एक गुरु और एक लघु ( ) से व्यक्त हुआ है- ६ + UU U ) हुआ है। इसके अपवाद केवल तीसरे कडवक
1
+ - । तात्पर्य यह कि समपादों का अंत एक जगण से (
=
के दोहे का चौथा पाद है जहाँ दूसरा गण एक गुरु से व्यक्त हुआ है फलतः इसका अंत जगण से नहीं है ।
[३] कडवक का मध्यभाग
कवक का यही भाग मुख्य भाग है । ग्रन्थ का कलेवर इसी से बनता है, कथानक इसी से आगे बढता है तथा वर्णन आदि का वैचित्र्य इसी में देखने को मिलता है । अपभ्रंश भाषा के कवि अपभ्रंश के विशिष्ट मात्रिक छंद पज्झटिका, अलिल्लह, पादाकुलक आदि के अतिरिक्त संस्कृत तथा प्राकृत काव्यों में प्रयुक्त वर्णवृत्तों का भी उपयोग कर रहे हैं । इसका मुख्य प्रयोजन काव्य में विभिन्नता लाकर उसे रोचक बनाए रखना था । काव्यों का सामान्य कथानक पज्झटिका जैसे छंदो से ही आगे बढता था किंतु विशिष्ट वर्णनों के लिए या विशिष्टभावों की अभिव्यक्ति के लिए अन्य छंद प्रयुक्त किये जाते थे । कुछ कवियों ने भिन्न भिन्न छंदो में काव्य रचने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए ग्रन्थों का निर्माण किया है पर पा. च. के कर्त्ता का यह ध्येय कदापि नहीं रहा । उसने तो जिनवर की भक्ति से ओतप्रोत होकर
१. देखिए अपभ्रंश मीटर पृ. ४० जे. बी. यू. व्हा. २ भाग. ३. नव. १९३३. ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org