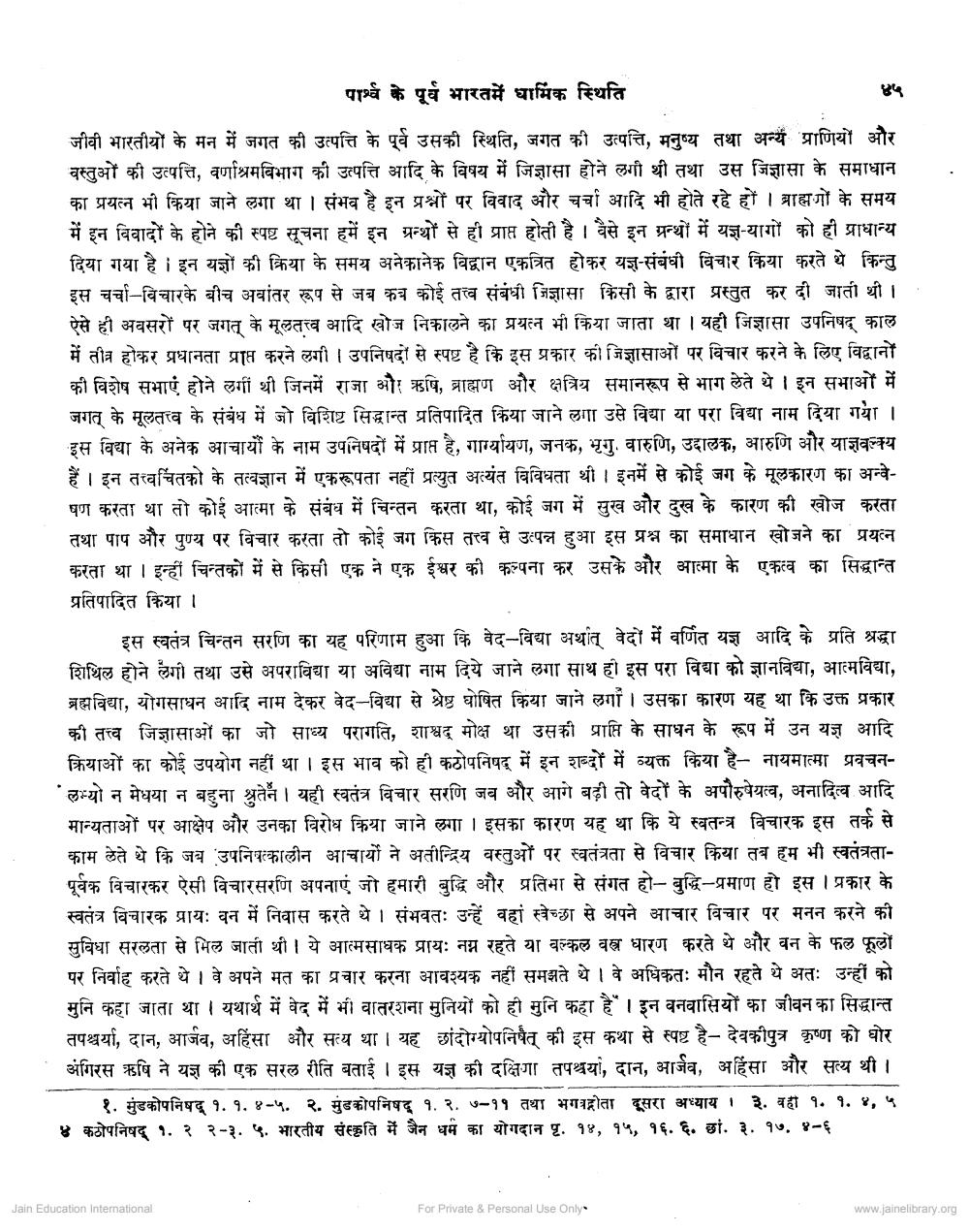________________
पार्श्व के पूर्व भारतमें धार्मिक स्थिति
जीवी भारतीयों के मन में जगत की उत्पत्ति के पूर्व उसकी स्थिति, जगत की उत्पत्ति, मनुष्य तथा अन्य प्राणियों और वस्तुओं की उत्पत्ति, वर्णाश्रमविभाग की उत्पत्ति आदि के विषय में जिज्ञासा होने लगी थी तथा उस जिज्ञासा के समाधान का प्रयत्न भी किया जाने लगा था। संभव है इन प्रश्नों पर विवाद और चर्चा आदि भी होते रहे हों । ब्राह्मणों के समय में इन विवादों के होने की स्पष्ट सूचना हमें इन ग्रन्थों से ही प्राप्त होती है। वैसे इन ग्रन्थों में यज्ञ-यागों को ही प्राधान्य दिया गया है। इन यज्ञों की क्रिया के समय अनेकानेक विद्वान एकत्रित होकर यज्ञ-संबंधी विचार किया करते थे किन्तु इस चर्चा - विचार के बीच अवांतर रूप से जब कब कोई तत्त्व संबंधी जिज्ञासा किसी के द्वारा प्रस्तुत कर दी जाती थी । ऐसे ही अवसरों पर जगत् के मूलतत्त्व आदि खोज निकालने का प्रयत्न भी किया जाता था । यही जिज्ञासा उपनिषद् काल में तीव्र होकर प्रधानता प्राप्त करने लगी । उपनिषदों से स्पष्ट है कि इस प्रकार की जिज्ञासाओं पर विचार करने के लिए विद्वानों की विशेष सभाएं होने लगीं थी जिनमें राजा और ऋषि, ब्राह्मण और क्षत्रिय समानरूप भाग लेते थे । इन सभाओं में जगत् के मूलतत्व के संबंध में जो विशिष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया जाने लगा उसे विद्या या परा विद्या नाम दिया गया । इस विद्या के अनेक आचार्यों के नाम उपनिषदों में प्राप्त है, गार्ग्यायण, जनक, भृगु वारुणि, उद्दालक, आरुणि और याज्ञवल्क्य हैं । इन तत्वचितको के तत्वज्ञान में एकरूपता नहीं प्रत्युत अत्यंत विविधता थी। इनमें से कोई जग के मूलकारण का अन्वे
करता था तो कोई आत्मा के संबंध में चिन्तन करता था, कोई जग में सुख और दुख के कारण की खोज करता तथा पाप और पुण्य पर विचार करता तो कोई जग किस तत्व से उत्पन्न हुआ इस प्रश्न का समाधान खोजने का प्रयत्न करता था । इन्हीं चिन्तकों में से किसी एक ने एक ईश्वर की कल्पना कर उसके और आत्मा के एकत्व का सिद्धान्त प्रतिपादित किया ।
इस स्वतंत्र चिन्तन सरणि का यह परिणाम हुआ कि वेद-विद्या अर्थात् वेदों में वर्णित यज्ञ आदि के प्रति श्रद्धा शिथिल होने लगी तथा उसे अपराविद्या या अविद्या नाम दिये जाने लगा साथ ही इस परा विद्या को ज्ञानविद्या, आत्मविद्या, ब्रह्मविद्या, योगसाधन आदि नाम देकर वेद-विद्या से श्रेष्ठ घोषित किया जाने लगा। उसका कारण यह था कि उक्त प्रकार की तत्त्व जिज्ञासाओं का जो साध्य परागति, शाश्वद् मोक्ष था उसकी प्राप्ति के साधन के रूप में उन यज्ञ आदि क्रियाओं का कोई उपयोग नहीं था । इस भाव को ही कठोपनिषद् में इन शब्दों में व्यक्त किया है- नायमात्मा प्रवचन• लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते । यही स्वतंत्र विचार सरणि जब और आगे बढ़ी तो वेदों के अपौरुषेयत्व, अनादित्व आदि मान्यताओं पर आक्षेप और उनका विरोध किया जाने लगा । इसका कारण यह था कि ये स्वतन्त्र विचारक इस तर्क से काम लेते थे कि जब उपनिषत्कालीन आचार्यों ने अतीन्द्रिय वस्तुओं पर स्वतंत्रता से विचार किया तब हम भी स्वतंत्रतापूर्वक विचारकर ऐसी विचारसरणि अपनाएं जो हमारी बुद्धि और प्रतिभा से संगत हो - बुद्धि-प्रमाण हो इस प्रकार के स्वतंत्र विचारक प्रायः वन में निवास करते थे । संभवतः उन्हें वहां स्वेच्छा से अपने आचार विचार पर मनन करने की सुविधा सरलता से मिल जाती थी । ये आत्मसाधक प्रायः नग्न रहते या वल्कल वस्त्र धारण करते थे और वन के फल फूलों पर निर्वाह करते थे । वे अपने मत का प्रचार करना आवश्यक नहीं समझते थे । वे अधिकतः मौन रहते थे अतः उन्हीं को मुनि कहा जाता था । यथार्थ में वेद में भी वातरशना मुनियों को ही मुनि कहा है। इन वनवासियों का जीवन का सिद्धान्त तपश्चर्या, दान, आर्जव, अहिंसा और सत्य था । यह छांदोग्योपनिषत् की इस कथा से स्पष्ट है- देवकीपुत्र कृष्ण को घोर अंगिरस ऋषि ने यज्ञ की एक सरल रीति बताई । इस यज्ञ की दक्षिणा तपश्रयां, दान, आर्जव, अहिंसा और सत्य थी ।
४५
१. मुंडकोपनिषद् १.१.४-५ २. मुंडकोपनिषद् १२ ७-११ तथा भगवद्गीता दूसरा अध्याय । ३. वही १.१.४, ५ ४ कठोपनिषद् १ २ २ ३. ५. भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान पृ. १४, १५, १६.६. छां. ३. १७, ४-६
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org