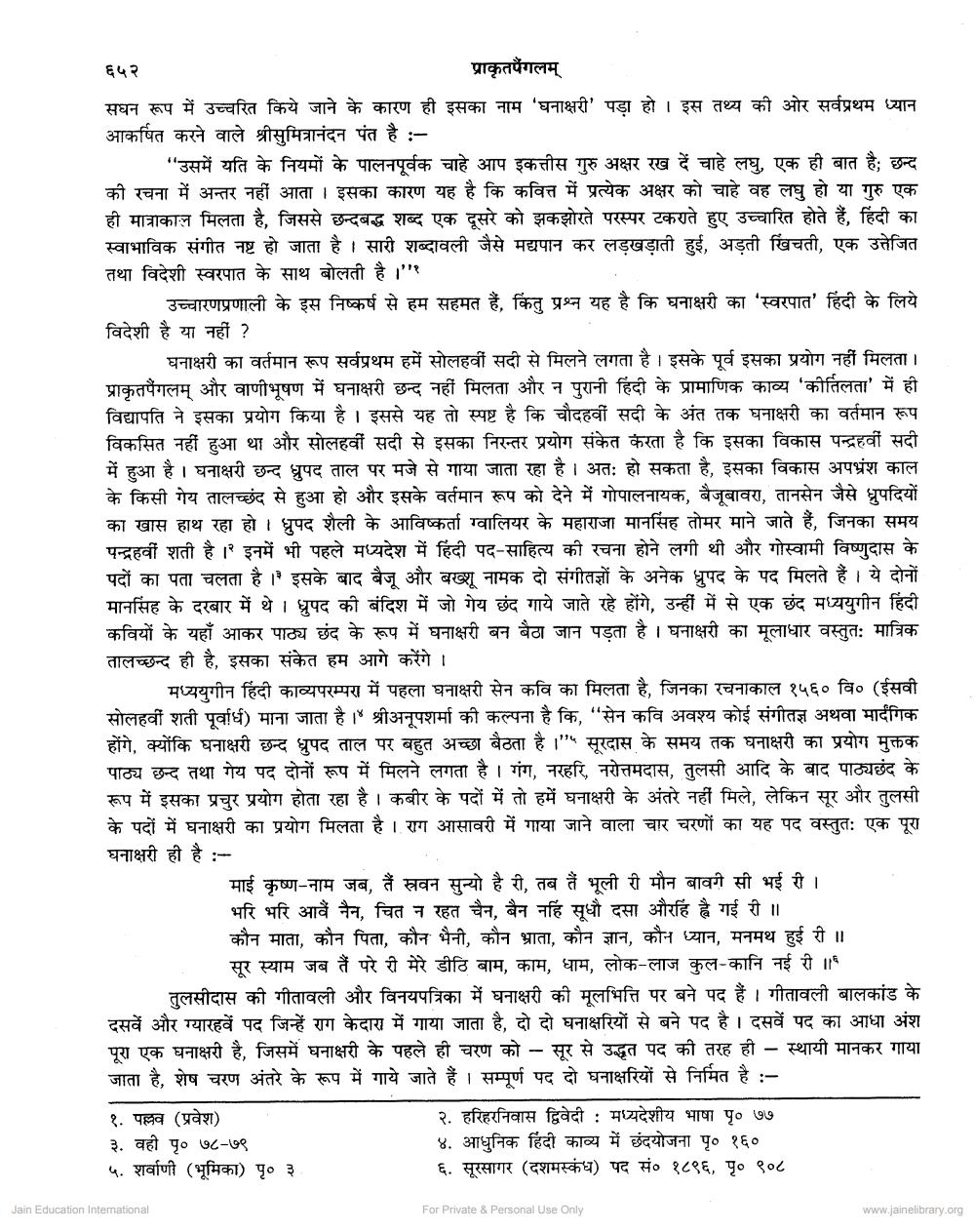________________
६५२
प्राकृतपैंगलम्
सघन रूप में उच्चरित किये जाने के कारण ही इसका नाम 'घनाक्षरी' पड़ा हो । इस तथ्य की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित करने वाले श्रीसुमित्रानंदन पंत है :
"उसमें यति के नियमों के पालनपूर्वक चाहे आप इकत्तीस गुरु अक्षर रख दें चाहे लघु, एक ही बात है; छन्द की रचना में अन्तर नहीं आता । इसका कारण यह है कि कवित्त में प्रत्येक अक्षर को चाहे वह लघु हो या गुरु एक ही मात्राकाल मिलता है, जिससे छन्दबद्ध शब्द एक दूसरे को झकझोरते परस्पर टकराते हुए उच्चारित होते हैं, हिंदी का स्वाभाविक संगीत नष्ट हो जाता है। सारी शब्दावली जैसे मद्यपान कर लड़खड़ाती हुई, अड़ती खिंचती, एक उत्तेजित तथा विदेशी स्वरपात के साथ बोलती है।"
उच्चारणप्रणाली के इस निष्कर्ष से हम सहमत हैं, किंतु प्रश्न यह है कि घनाक्षरी का 'स्वरपात' हिंदी के लिये विदेशी है या नहीं ?
घनाक्षरी का वर्तमान रूप सर्वप्रथम हमें सोलहवीं सदी से मिलने लगता है। इसके पूर्व इसका प्रयोग नहीं मिलता। प्राकृतपैंगलम् और वाणीभूषण में घनाक्षरी छन्द नहीं मिलता और न पुरानी हिंदी के प्रामाणिक काव्य 'कीर्तिलता' में ही विद्यापति ने इसका प्रयोग किया है । इससे यह तो स्पष्ट है कि चौदहवीं सदी के अंत तक घनाक्षरी का वर्तमान रूप विकसित नहीं हुआ था और सोलहवीं सदी से इसका निरन्तर प्रयोग संकेत करता है कि इसका विकास पन्द्रहवीं सदी में हुआ है। घनाक्षरी छन्द ध्रुपद ताल पर मजे से गाया जाता रहा है। अतः हो सकता है, इसका विकास अपभ्रंश काल के किसी गेय तालच्छंद से हुआ हो और इसके वर्तमान रूप को देने में गोपालनायक, बैजूबावरा, तानसेन जैसे ध्रुपदियों का खास हाथ रहा हो । ध्रुपद शैली के आविष्कर्ता ग्वालियर के महाराजा मानसिंह तोमर माने जाते हैं, जिनका समय पन्द्रहवीं शती है। इनमें भी पहले मध्यदेश में हिंदी पद-साहित्य की रचना होने लगी थी और गोस्वामी विष्णुदास के पदों का पता चलता है। इसके बाद बैजू और बख्शू नामक दो संगीतज्ञों के अनेक ध्रुपद के पद मिलते हैं। ये दोनों मानसिंह के दरबार में थे । ध्रुपद की बंदिश में जो गेय छंद गाये जाते रहे होंगे, उन्हीं में से एक छंद मध्ययुगीन हिंदी कवियों के यहाँ आकर पाठ्य छंद के रूप में घनाक्षरी बन बैठा जान पड़ता है । घनाक्षरी का मूलाधार वस्तुतः मात्रिक तालच्छन्द ही है, इसका संकेत हम आगे करेंगे ।
मध्ययुगीन हिंदी काव्यपरम्परा में पहला घनाक्षरी सेन कवि का मिलता है, जिनका रचनाकाल १५६० वि० (ईसवी सोलहवीं शती पूर्वार्ध) माना जाता है। श्रीअनूपशर्मा की कल्पना है कि, “सेन कवि अवश्य कोई संगीतज्ञ अथवा मार्दगिक होंगे, क्योंकि घनाक्षरी छन्द ध्रुपद ताल पर बहुत अच्छा बैठता है ।"५ सूरदास के समय तक घनाक्षरी का प्रयोग मुक्तक पाठ्य छन्द तथा गेय पद दोनों रूप में मिलने लगता है। गंग, नरहरि, नरोत्तमदास, तुलसी आदि के बाद पाठ्यछंद के रूप में इसका प्रचुर प्रयोग होता रहा है। कबीर के पदों में तो हमें घनाक्षरी के अंतरे नहीं मिले, लेकिन सूर और तुलसी के पदों में घनाक्षरी का प्रयोग मिलता है। राग आसावरी में गाया जाने वाला चार चरणों का यह पद वस्तुतः एक पूरा घनाक्षरी ही है :
माई कृष्ण-नाम जब, तैं स्रवन सुन्यो है री, तब तैं भूली री मौन बावरी सी भई री । भरि भरि आवें नैन, चित न रहत चैन, बैन नहिं सूधौ दसा औरहिं द्वै गई री ॥ कौन माता, कौन पिता, कौन भैनी, कौन भ्राता, कौन ज्ञान, कौन ध्यान, मनमथ हुई री ॥
सूर स्याम जब तैं परे री मेरे डीठि बाम, काम, धाम, लोक-लाज कुल-कानि नई री ॥६ तुलसीदास की गीतावली और विनयपत्रिका में घनाक्षरी की मूलभित्ति पर बने पद हैं। गीतावली बालकांड के दसवें और ग्यारहवें पद जिन्हें राग केदारा में गाया जाता है, दो दो घनाक्षरियों से बने पद है। दसवें पद का आधा अंश पूरा एक घनाक्षरी है, जिसमें घनाक्षरी के पहले ही चरण को - सूर से उद्धृत पद की तरह ही - स्थायी मानकर गाया जाता है, शेष चरण अंतरे के रूप में गाये जाते हैं । सम्पूर्ण पद दो घनाक्षरियों से निर्मित है :१. पल्लव (प्रवेश)
२. हरिहरनिवास द्विवेदी : मध्यदेशीय भाषा पृ० ७७ ३. वही पृ० ७८-७९
४. आधुनिक हिंदी काव्य में छंदयोजना पृ० १६० ५. शर्वाणी (भूमिका) पृ० ३
६. सूरसागर (दशमस्कंध) पद सं० १८९६, पृ० ९०८
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org