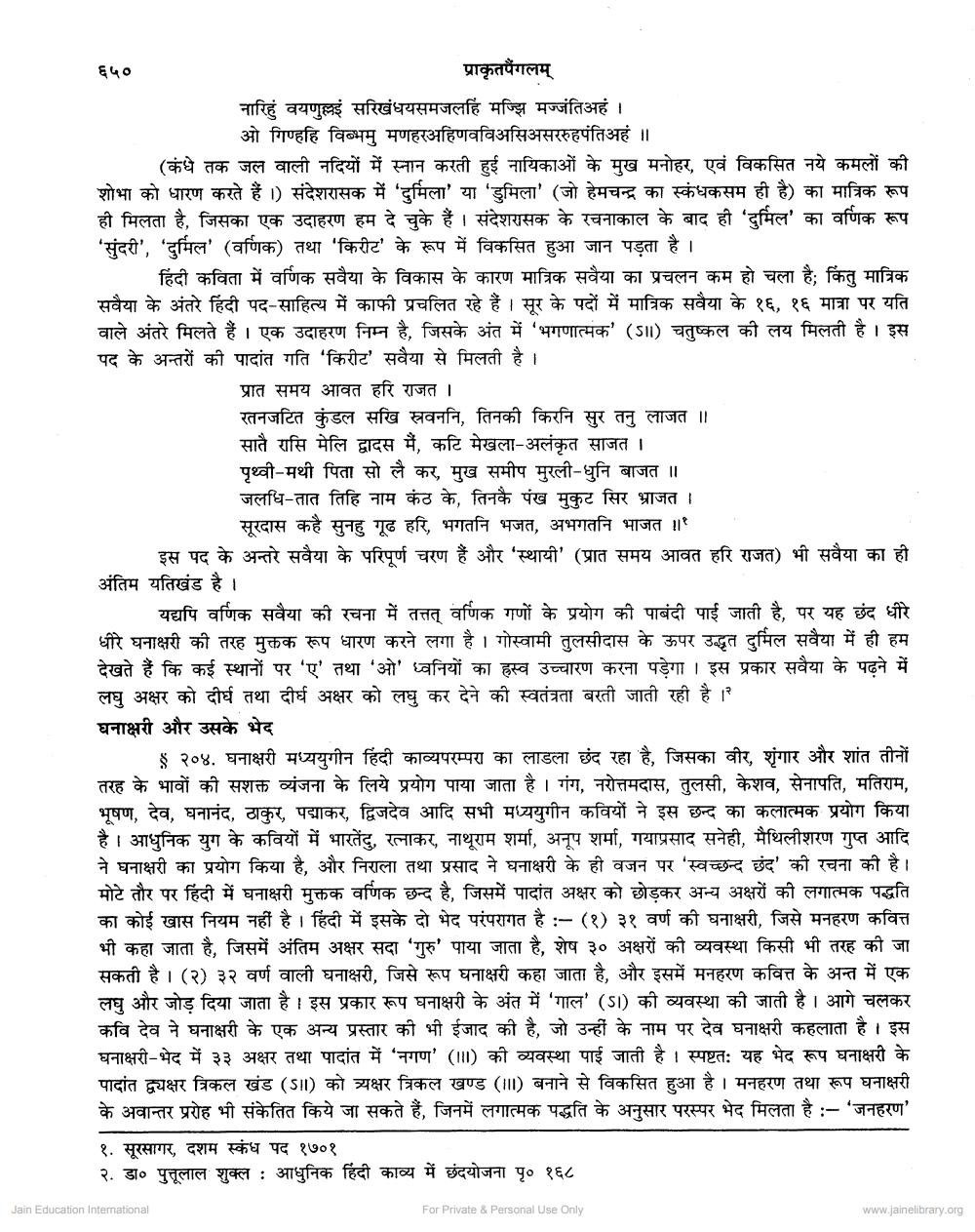________________
६५०
प्राकृतपैंगलम् नारिहं वयणुल्लई सरिखंधयसमजलहिं मज्झि मज्जंतिअहं ।
ओ गिण्हहि विब्भमु मणहरअहिणवविअसिअसररुहपंतिअहं ।। (कंधे तक जल वाली नदियों में स्नान करती हुई नायिकाओं के मुख मनोहर, एवं विकसित नये कमलों की शोभा को धारण करते हैं ।) संदेशरासक में 'दुर्मिला' या 'डुमिला' (जो हेमचन्द्र का स्कंधकसम ही है) का मात्रिक रूप ही मिलता है, जिसका एक उदाहरण हम दे चुके हैं। संदेशरासक के रचनाकाल के बाद ही 'दुर्मिल' का वर्णिक रूप 'सुंदरी', 'दुर्मिल' (वणिक) तथा 'किरीट' के रूप में विकसित हुआ जान पड़ता है।
हिंदी कविता में वर्णिक सवैया के विकास के कारण मात्रिक सवैया का प्रचलन कम हो चला है; किंतु मात्रिक सवैया के अंतरे हिंदी पद-साहित्य में काफी प्रचलित रहे हैं। सूर के पदों में मात्रिक सवैया के १६, १६ मात्रा पर यति वाले अंतरे मिलते हैं । एक उदाहरण निम्न है, जिसके अंत में 'भगणात्मक' (1) चतुष्कल की लय मिलती है। इस पद के अन्तरों की पादांत गति 'किरीट' सवैया से मिलती है ।
प्रात समय आवत हरि राजत । रतनजटित कुंडल सखि स्रवननि, तिनकी किरनि सुर तनु लाजत ।। सातै रासि मेलि द्वादस मैं, कटि मेखला-अलंकृत साजत । पृथ्वी-मथी पिता सो लै कर, मुख समीप मुरली-धुनि बाजत ।। जलधि-तात तिहि नाम कंठ के, तिनकै पंख मुकुट सिर भ्राजत ।
सूरदास कहै सुनहु गूढ हरि, भगतनि भजत, अभगतनि भाजत ॥ इस पद के अन्तरे सवैया के परिपूर्ण चरण हैं और 'स्थायी' (प्रात समय आवत हरि राजत) भी सवैया का ही अंतिम यतिखंड है।
यद्यपि वर्णिक सवैया की रचना में तत्तत् वर्णिक गणों के प्रयोग की पाबंदी पाई जाती है, पर यह छंद धीरे धीरे घनाक्षरी की तरह मुक्तक रूप धारण करने लगा है । गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर उद्धृत दुर्मिल सवैया में ही हम देखते हैं कि कई स्थानों पर 'ए' तथा 'ओ' ध्वनियों का ह्रस्व उच्चारण करना पड़ेगा । इस प्रकार सवैया के पढ़ने में लघु अक्षर को दीर्घ तथा दीर्घ अक्षर को लघु कर देने की स्वतंत्रता बरती जाती रही है । घनाक्षरी और उसके भेद
२०४. घनाक्षरी मध्ययुगीन हिंदी काव्यपरम्परा का लाडला छंद रहा है, जिसका वीर, शृंगार और शांत तीनों तरह के भावों की सशक्त व्यंजना के लिये प्रयोग पाया जाता है। गंग, नरोत्तमदास, तुलसी, केशव, सेनापति, मतिराम, भूषण, देव, घनानंद, ठाकुर, पद्माकर, द्विजदेव आदि सभी मध्ययुगीन कवियों ने इस छन्द का कलात्मक प्रयोग किया है। आधुनिक युग के कवियों में भारतेंदु, रत्नाकर, नाथूराम शर्मा, अनूप शर्मा, गयाप्रसाद सनेही, मैथिलीशरण गुप्त आदि ने घनाक्षरी का प्रयोग किया है, और निराला तथा प्रसाद ने घनाक्षरी के ही वजन पर 'स्वच्छन्द छंद' की रचना की है। मोटे तौर पर हिंदी में घनाक्षरी मुक्तक वर्णिक छन्द है, जिसमें पादांत अक्षर को छोड़कर अन्य अक्षरों की लगात्मक पद्धति का कोई खास नियम नहीं है। हिंदी में इसके दो भेद परंपरागत है :- (१) ३१ वर्ण की घनाक्षरी, जिसे मनहरण कवित्त भी कहा जाता है, जिसमें अंतिम अक्षर सदा 'गुरु' पाया जाता है, शेष ३० अक्षरों की व्यवस्था किसी भी तरह की जा सकती है। (२) ३२ वर्ण वाली घनाक्षरी, जिसे रूप घनाक्षरी कहा जाता है, और इसमें मनहरण कवित्त के अन्त में एक लघु और जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार रूप घनाक्षरी के अंत में 'गाल' (51) की व्यवस्था की जाती है। आगे चलकर कवि देव ने घनाक्षरी के एक अन्य प्रस्तार की भी ईजाद की है, जो उन्हीं के नाम पर देव घनाक्षरी कहलाता है। इस घनाक्षरी-भेद में ३३ अक्षर तथा पादांत में 'नगण' (III) की व्यवस्था पाई जाती है। स्पष्टतः यह भेद रूप घनाक्षरी के पादांत व्यक्षर त्रिकल खंड (51) को त्र्यक्षर त्रिकल खण्ड (III) बनाने से विकसित हुआ है। मनहरण तथा रूप घनाक्षरी के अवान्तर प्ररोह भी संकेतित किये जा सकते हैं, जिनमें लगात्मक पद्धति के अनुसार परस्पर भेद मिलता है :- 'जनहरण'
१. सूरसागर, दशम स्कंध पद १७०१ २. डा० पुत्तूलाल शुक्ल : आधुनिक हिंदी काव्य में छंदयोजना पृ० १६८
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org