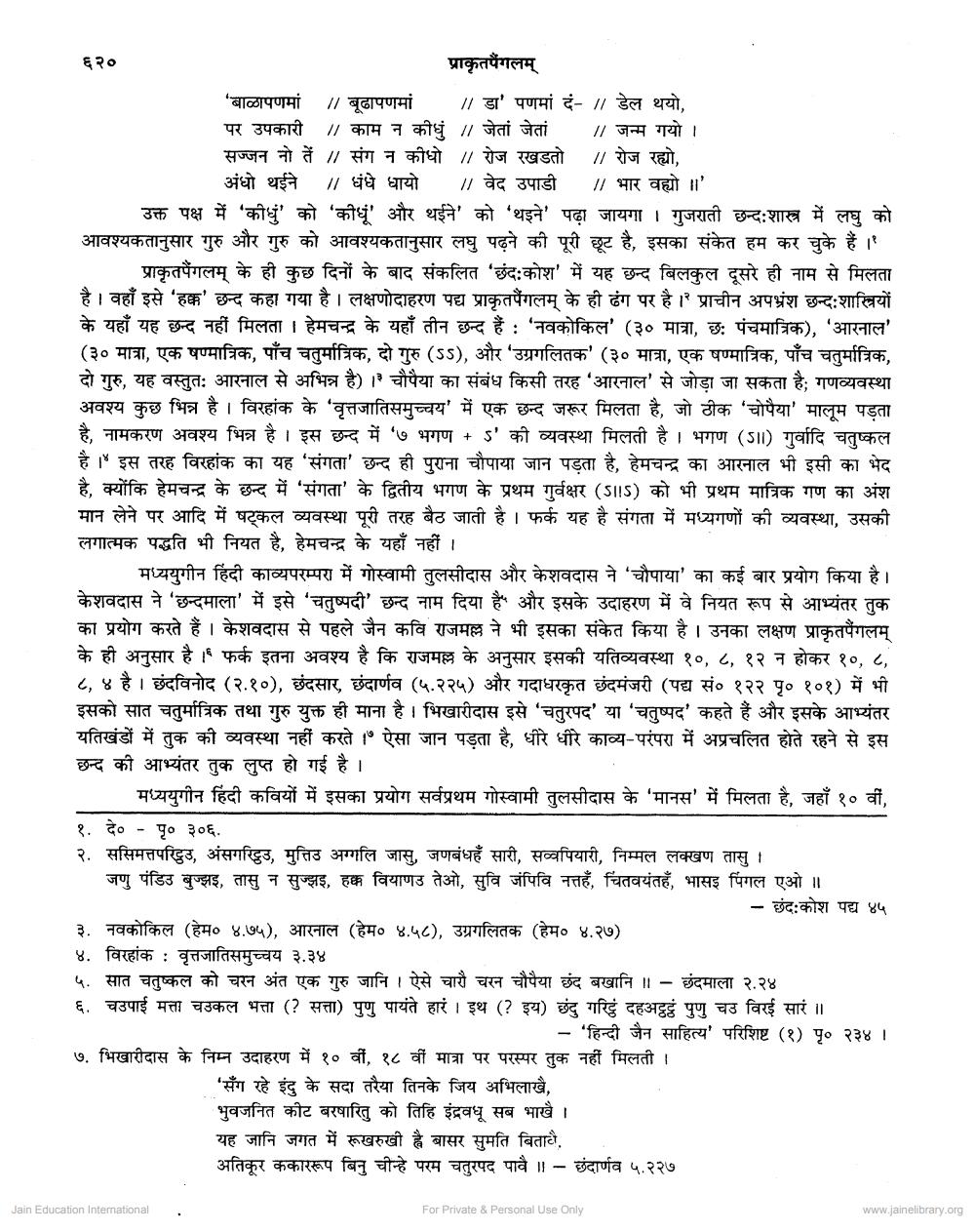________________
प्राकृतपैंगलम्
'बाळापणमां ॥ बूढापणमां ॥डा' पणमां दं- || डेल थयो, पर उपकारी ॥ काम न कीg // जेतां जेतां ॥ जन्म गयो । सज्जन नो तें ॥ संग न कीधो ॥ रोज रखडतो ॥ रोज रह्यो,
अंधो थईने ॥ धंधे धायो ॥ वेद उपाडी ॥ भार वह्यो ।' उक्त पक्ष में 'कीधु' को 'कीबूं' और थईने' को 'थइने' पढ़ा जायगा । गुजराती छन्दःशास्त्र में लघु को आवश्यकतानुसार गुरु और गुरु को आवश्यकतानुसार लघु पढ़ने की पूरी छूट है, इसका संकेत हम कर चुके हैं ।
प्राकृतपैंगलम् के ही कुछ दिनों के बाद संकलित 'छंदःकोश' में यह छन्द बिलकुल दूसरे ही नाम से मिलता है। वहाँ इसे 'हक्क' छन्द कहा गया है । लक्षणोदाहरण पद्य प्राकृतपैंगलम् के ही ढंग पर है। प्राचीन अपभ्रंश छन्दःशास्त्रियों के यहाँ यह छन्द नहीं मिलता । हेमचन्द्र के यहाँ तीन छन्द हैं : 'नवकोकिल' (३० मात्रा, छ: पंचमात्रिक), 'आरनाल' (३० मात्रा, एक षण्मात्रिक, पाँच चतुर्मात्रिक, दो गुरु (55), और 'उग्रगलितक' (३० मात्रा, एक षण्मात्रिक, पाँच चतुर्मात्रिक, दो गुरु, यह वस्तुत: आरनाल से अभिन्न है)। चौपैया का संबंध किसी तरह 'आरनाल' से जोड़ा जा सकता है; गणव्यवस्था अवश्य कुछ भिन्न है। विरहांक के 'वृत्तजातिसमुच्चय' में एक छन्द जरूर मिलता है, जो ठीक 'चोपैया' मालूम पड़ता है, नामकरण अवश्य भिन्न है। इस छन्द में '७ भगण + ऽ' की व्यवस्था मिलती है । भगण (50) गुर्वादि चतुष्कल है। इस तरह विरहांक का यह 'संगता' छन्द ही पुराना चौपाया जान पड़ता है, हेमचन्द्र का आरनाल भी इसी का भेद है, क्योंकि हेमचन्द्र के छन्द में 'संगता' के द्वितीय भगण के प्रथम गुर्वक्षर (SIS) को भी प्रथम मात्रिक गण का अंश मान लेने पर आदि में षट्कल व्यवस्था पूरी तरह बैठ जाती है । फर्क यह है संगता में मध्यगणों की व्यवस्था, उसकी लगात्मक पद्धति भी नियत है, हेमचन्द्र के यहाँ नहीं ।
मध्ययुगीन हिंदी काव्यपरम्परा में गोस्वामी तुलसीदास और केशवदास ने 'चौपाया' का कई बार प्रयोग किया है। केशवदास ने 'छन्दमाला' में इसे 'चतुष्पदी' छन्द नाम दिया है और इसके उदाहरण में वे नियत रूप से आभ्यंतर तुक का प्रयोग करते हैं । केशवदास से पहले जैन कवि राजमल्ल ने भी इसका संकेत किया है । उनका लक्षण प्राकृतपैंगलम् के ही अनुसार है। फर्क इतना अवश्य है कि राजमल्ल के अनुसार इसकी यतिव्यवस्था १०, ८, १२ न होकर १०, ८, ८, ४ है । छंदविनोद (२.१०), छंदसार, छंदार्णव (५.२२५) और गदाधरकृत छंदमंजरी (पद्य सं० १२२ पृ० १०१) में भी इसको सात चतुर्मात्रिक तथा गुरु युक्त ही माना है। भिखारीदास इसे 'चतुरपद' या 'चतुष्पद' कहते हैं और इसके आभ्यंतर यतिखंडों में तुक की व्यवस्था नहीं करते। ऐसा जान पड़ता है, धीरे धीरे काव्य-परंपरा में अप्रचलित होते रहने से इस छन्द की आभ्यंतर तुक लुप्त हो गई है।
मध्ययुगीन हिंदी कवियों में इसका प्रयोग सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास के 'मानस' में मिलता है, जहाँ १० वीं, १. दे० - पृ० ३०६. २. ससिमत्तपरिटुउ, अंसगरिटुउ, मुत्तिउ अग्गलि जासु, जणबंधहँ सारी, सव्वपियारी, निम्मल लक्खण तासु । जणु पंडिउ बुज्झइ, तासु न सुज्झइ, हक्क वियाणउ तेओ, सुवि जंपिवि नत्तहँ, चिंतवयंतहँ, भासइ पिंगल एओ ॥
- छंद:कोश पद्य ४५ ३. नवकोकिल (हेम० ४.७५), आरनाल (हेम० ४.५८), उग्रगलितक (हेम० ४.२७) ४. विरहांक : वृत्तजातिसमुच्चय ३.३४ ५. सात चतुष्कल को चरन अंत एक गुरु जानि । ऐसे चारौ चरन चौपैया छंद बखानि ॥ - छंदमाला २.२४ ६. चउपाई मत्ता चउकल भत्ता (? सत्ता) पुणु पायंते हारं । इथ (? इय) छंदु गरिटुं दहअट्ठट्ठ पुणु चउ विरई सारं ।।
- "हिन्दी जैन साहित्य' परिशिष्ट (१) पृ० २३४ । ७. भिखारीदास के निम्न उदाहरण में १० वी, १८ वी मात्रा पर परस्पर तुक नहीं मिलती ।
"सँग रहे इंदु के सदा तरैया तिनके जिय अभिलाखै, भुवजनित कीट बरषारितु को तिहि इंद्रवधू सब भाखै । यह जानि जगत में रूखरुखी है बासर सुमति बिताटी. अतिकूर ककाररूप बिनु चीन्हे परम चतुरपद पावै ॥ - छंदार्णव ५.२२७
Jain Education International
.
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org