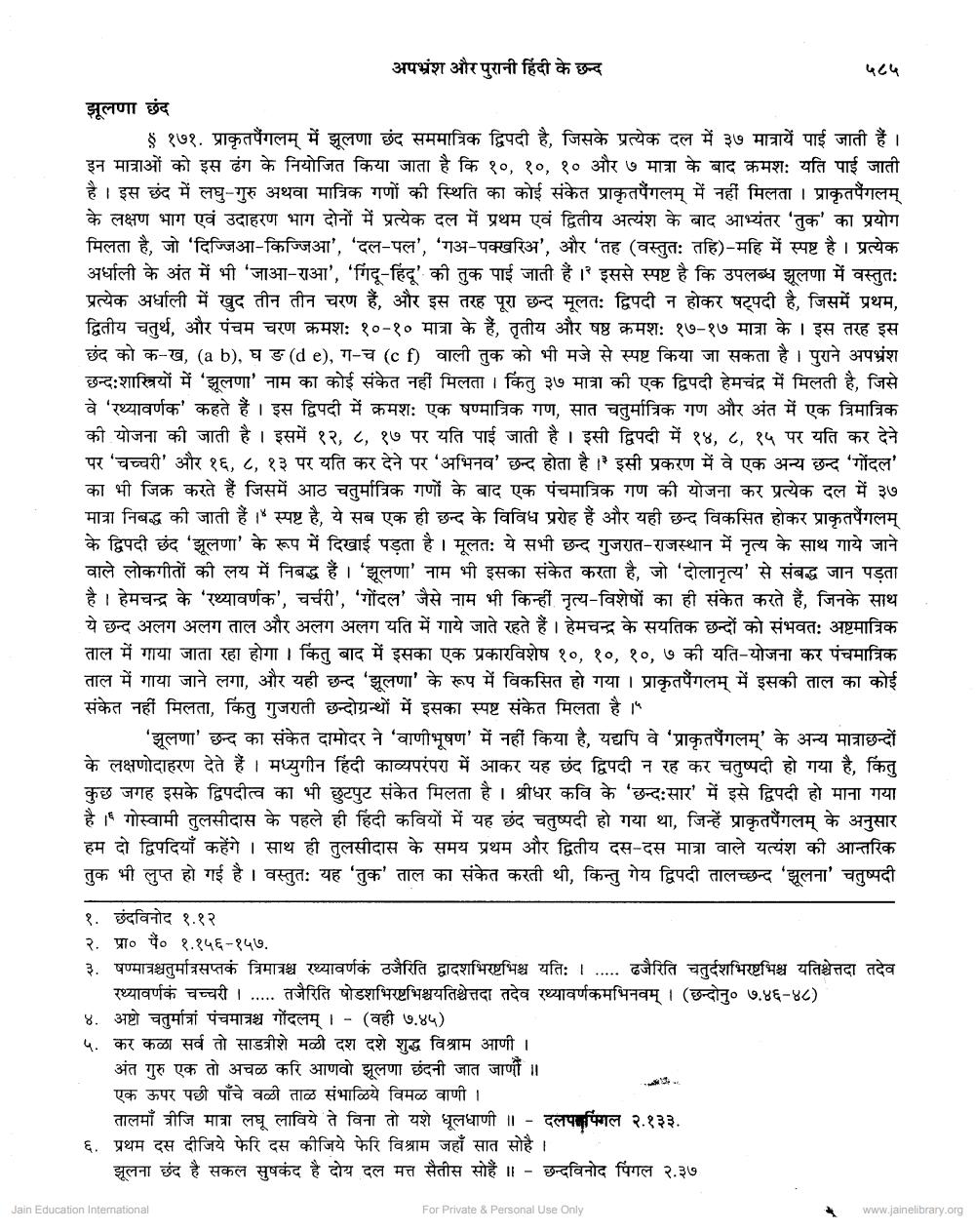________________
अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के छन्द
५८५
झूलणा छंद
६ १७१. प्राकृतपैंगलम् में झूलणा छंद सममात्रिक द्विपदी है, जिसके प्रत्येक दल में ३७ मात्रायें पाई जाती हैं। इन मात्राओं को इस ढंग के नियोजित किया जाता है कि १०, १०, १० और ७ मात्रा के बाद क्रमशः यति पाई जाती है। इस छंद में लघु-गुरु अथवा मात्रिक गणों की स्थिति का कोई संकेत प्राकृतपैंगलम् में नहीं मिलता । प्राकृतपैंगलम् के लक्षण भाग एवं उदाहरण भाग दोनों में प्रत्येक दल में प्रथम एवं द्वितीय अत्यंश के बाद आभ्यंतर 'तुक' का प्रयोग मिलता है, जो 'दिज्जिआ-किज्जिआ', 'दल-पल', 'गअ-पक्खरिअ', और 'तह (वस्तुत: तहि)-महि में स्पष्ट है । प्रत्येक अर्धाली के अंत में भी 'जाआ-राआ', 'गिंदू-हिंदू' की तुक पाई जाती हैं। इससे स्पष्ट है कि उपलब्ध झूलणा में वस्तुतः प्रत्येक अर्धाली में खुद तीन तीन चरण हैं, और इस तरह पूरा छन्द मूलतः द्विपदी न होकर षट्पदी है, जिसमें प्रथम, द्वितीय चतुर्थ, और पंचम चरण क्रमशः १०-१० मात्रा के हैं, तृतीय और षष्ठ क्रमश: १७-१७ मात्रा के । इस तरह इस छंद को क-ख, (a b), घ ङ (de), ग-च (cf) वाली तुक को भी मजे से स्पष्ट किया जा सकता है। पुराने अपभ्रंश छन्दःशास्त्रियों में 'झूलणा' नाम का कोई संकेत नहीं मिलता । किंतु ३७ मात्रा की एक द्विपदी हेमचंद्र में मिलती है, जिसे वे 'रथ्यावर्णक' कहते हैं । इस द्विपदी में क्रमशः एक षण्मात्रिक गण, सात चतुर्मात्रिक गण और अंत में एक त्रिमात्रिक की योजना की जाती है । इसमें १२, ८, १७ पर यति पाई जाती है। इसी द्विपदी में १४, ८, १५ पर यति कर देने पर 'चच्चरी' और १६, ८, १३ पर यति कर देने पर 'अभिनव' छन्द होता है। इसी प्रकरण में वे एक अन्य छन्द 'गोंदल' का भी जिक्र करते हैं जिसमें आठ चतुर्मात्रिक गणों के बाद एक पंचमात्रिक गण की योजना कर प्रत्येक दल में ३७ मात्रा निबद्ध की जाती हैं । स्पष्ट है, ये सब एक ही छन्द के विविध प्ररोह हैं और यही छन्द विकसित होकर प्राकृतपैंगलम् के द्विपदी छंद 'झूलणा' के रूप में दिखाई पड़ता है । मूलतः ये सभी छन्द गुजरात-राजस्थान में नृत्य के साथ गाये जाने वाले लोकगीतों की लय में निबद्ध हैं । 'झूलणा' नाम भी इसका संकेत करता है, जो 'दोलानृत्य' से संबद्ध जान पड़ता है । हेमचन्द्र के 'रथ्यावर्णक', चर्चरी', 'गोंदल' जैसे नाम भी किन्हीं नृत्य-विशेषों का ही संकेत करते हैं, जिनके साथ ये छन्द अलग अलग ताल और अलग अलग यति में गाये जाते रहते हैं। हेमचन्द्र के सयतिक छन्दों को संभवत: अष्टमात्रिक ताल में गाया जाता रहा होगा। किंतु बाद में इसका एक प्रकारविशेष १०, १०, १०, ७ की यति-योजना कर पंचमात्रिक ताल में गाया जाने लगा, और यही छन्द 'झूलणा' के रूप में विकसित हो गया । प्राकृतपैंगलम् में इसकी ताल का कोई संकेत नहीं मिलता, किंतु गुजराती छन्दोग्रन्थों में इसका स्पष्ट संकेत मिलता है ।५।।
'झुलणा' छन्द का संकेत दामोदर ने 'वाणीभूषण' में नहीं किया है, यद्यपि वे 'प्राकृतपैंगलम्' के अन्य मात्राछन्दों के लक्षणोदाहरण देते हैं । मध्युगीन हिंदी काव्यपरंपरा में आकर यह छंद द्विपदी न रह कर चतुष्पदी हो गया है, किंतु कुछ जगह इसके द्विपदीत्व का भी छुटपुट संकेत मिलता है । श्रीधर कवि के 'छन्दःसार' में इसे द्विपदी हो माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास के पहले ही हिंदी कवियों में यह छंद चतुष्पदी हो गया था, जिन्हें प्राकृतपैंगलम् के अनुसार हम दो द्विपदियाँ कहेंगे । साथ ही तुलसीदास के समय प्रथम और द्वितीय दस-दस मात्रा वाले यत्यंश की आन्तरिक तुक भी लुप्त हो गई है। वस्तुतः यह 'तुक' ताल का संकेत करती थी, किन्तु गेय द्विपदी तालच्छन्द 'झूलना' चतुष्पदी
१. छंदविनोद १.१२ २. प्रा० पैं० १.१५६-१५७. ३. षण्मात्रश्चतुर्मात्रसप्तकं त्रिमात्रश्च रथ्यावर्णकं ठजैरिति द्वादशभिरष्टभिश्च यतिः । ..... ढजैरिति चतुर्दशभिरष्टभिश्च यतिश्चेत्तदा तदेव
रथ्यावर्णकं चच्चरी । ..... तजैरिति षोडशभिरष्टभिश्चयतिश्चेत्तदा तदेव रथ्यावर्णकमभिनवम् । (छन्दोनु० ७.४६-४८) ४. अष्टो चतुर्मात्रां पंचमात्रश्च गोंदलम् । - (वही ७.४५)
कर कळा सर्व तो साडीशे मळी दश दशे शुद्ध विश्राम आणी । अंत गुरु एक तो अचळ करि आणवो झूलणा छंदनी जात जाणौँ । एक ऊपर पछी पाँचे वळी ताळ संभाळिये विमळ वाणी ।।
तालमाँ त्रीजि मात्रा लघू लाविये ते विना तो यशे धूलधाणी ॥ - दलपलपिंगल २.१३३. ६. प्रथम दस दीजिये फेरि दस कीजिये फेरि विश्राम जहाँ सात सोहै ।
झूलना छंद है सकल सुषकंद है दोय दल मत्त सैतीस सोहैं ।। - छन्दविनोद पिंगल २.३७
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org