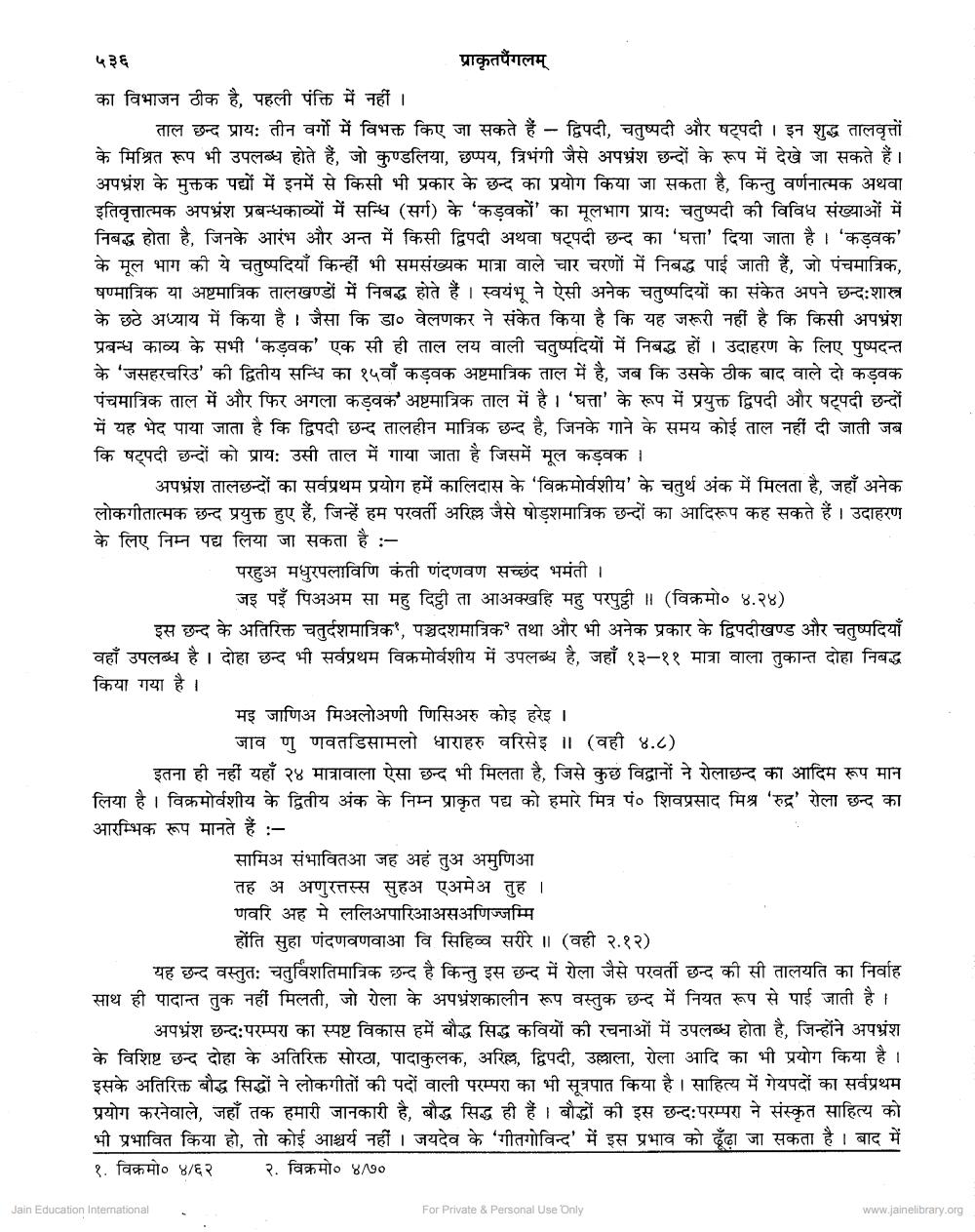________________
५३६
का विभाजन ठीक है, पहली पंक्ति में नहीं ।
ताल छन्द प्रायः तीन वर्गों में विभक्त किए जा सकते हैं - द्विपदी, चतुष्पदी और षट्पदी । इन शुद्ध तालवृत्तों के मिश्रित रूप भी उपलब्ध होते हैं, जो कुण्डलिया, छप्पय, त्रिभंगी जैसे अपभ्रंश छन्दों के रूप में देखे जा सकते हैं। अपभ्रंश के मुक्तक पद्मों में इनमें से किसी भी प्रकार के छन्द का प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु वर्णनात्मक अथवा इतिवृत्तात्मक अपभ्रंश प्रबन्धकाव्यों में सन्धि (सर्ग) के 'कड़वकों' का मूलभाग प्रायः चतुष्पदी की विविध संख्याओं में निबद्ध होता है, जिनके आरंभ और अन्त में किसी द्विपदी अथवा षट्पदी छन्द का 'घत्ता' दिया जाता है। 'कड़वक' के मूल भाग की ये चतुष्पदियाँ किन्हीं भी समसंख्यक मात्रा वाले चार चरणों में निबद्ध पाई जाती हैं, जो पंचमात्रिक, षण्मात्रिक या अष्टमात्रिक तालखण्डों में निबद्ध होते हैं। स्वयंभू ने ऐसी अनेक चतुष्पदियों का संकेत अपने छन्दः शास्त्र के छठे अध्याय में किया है। जैसा कि डा० वेलणकर ने संकेत किया है कि यह जरूरी नहीं है कि किसी अपभ्रंश प्रबन्ध काव्य के सभी 'कड़वक' एक सी ही ताल लय वाली चतुष्यदियों में निबद्ध हों। उदाहरण के लिए पुष्पदन्त के 'जसहरचरिउ' की द्वितीय सन्धि का १५वाँ कड़वक अष्टमात्रिक ताल में है, जब कि उसके ठीक बाद वाले दो कड़वक पंचमात्रिक ताल में और फिर अगला कड़वक' अष्टमात्रिक ताल में है । 'घत्ता' के रूप में प्रयुक्त द्विपदी और षट्पदी छन्दों में यह भेद पाया जाता है कि द्विपदी छन्द सालहीन मात्रिक छन्द है, जिनके गाने के समय कोई ताल नहीं दी जाती जब कि षट्पदी छन्दों को प्रायः उसी ताल में गाया जाता है जिसमें मूल कड़वक ।
प्राकृतपैंगलम्
अपभ्रंश तालछन्दों का सर्वप्रथम प्रयोग हमें कालिदास के 'विक्रमोर्वशीय' के चतुर्थ अंक में मिलता है, जहाँ अनेक लोकगीतात्मक छन्द प्रयुक्त हुए हैं, जिन्हें हम परवर्ती अलि जैसे षोड्शमात्रिक छन्दों का आदिरूप कह सकते हैं। उदाहरण के लिए निम्न पद्य लिया जा सकता है :
परहुअ मधुरपलाविणि कंती गंदणवण सच्छंद भमंती ।
जड़ पड़ें पिअअम सा महु दिट्ठी ता आअक्खहि महु परपुट्टी | (विक्रमो० ४.२४)
इस छन्द के अतिरिक्त चतुर्दशमात्रिक' पञ्चदशमात्रिक तथा और भी अनेक प्रकार के द्विपदीखण्ड और चतुष्पदियाँ वहाँ उपलब्ध है। दोहा छन्द भी सर्वप्रथम विक्रमोर्वशीय में उपलब्ध है, जहाँ १३ ११ मात्रा वाला तुकान्त दोहा निबद्ध किया गया है ।
Jain Education International
मह जाणिअ मिअलोअणी णिसिअरु कोइ हरेइ ।
जाव णु णवतडिसामली धाराहरु वरिसेइ ॥ ( वही ४.८ )
इतना ही नहीं यहाँ २४ मात्रावाला ऐसा छन्द भी मिलता है, जिसे कुछ विद्वानों ने रोलाछन्द का आदिम रूप मान लिया है। विक्रमोर्वशीय के द्वितीय अंक के निम्न प्राकृत पद्य को हमारे मित्र पं० शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्र' रोला छन्द का आरम्भिक रूप मानते हैं :
सामिअ संभावितआ जह अहं तु अमुणिआ
तह अ अणुरतस्स सुहअ एअमेअ तुह ।
णवरि अह मे ललिअपारिआ असअणिज्जम्मि
होंति सुहा णंदणवणवाआ वि सिहिव्व सरीरे ॥ ( वही २.१२)
यह छन्द वस्तुतः चतुर्विंशतिमात्रिक छन्द है किन्तु इस छन्द में रोला जैसे परवर्ती छन्द की सी तालयति का निर्वाह साथ ही पादान्त तुक नहीं मिलती, जो रोला के अपभ्रंशकालीन रूप वस्तुक छन्द में नियत रूप से पाई जाती है। अपभ्रंश छन्दः परम्परा का स्पष्ट विकास हमें बौद्ध सिद्ध कवियों की रचनाओं में उपलब्ध होता है, जिन्होंने अपभ्रंश के विशिष्ट छन्द दोहा के अतिरिक्त सोरठा, पादाकुलक, अरिल्ल, द्विपदी, उल्लाला, रोला आदि का भी प्रयोग किया है । इसके अतिरिक्त बौद्ध सिद्धों ने लोकगीतों की पदों वाली परम्परा का भी सूत्रपात किया है । साहित्य में गेयपदों का सर्वप्रथम प्रयोग करनेवाले, जहाँ तक हमारी जानकारी है, बौद्ध सिद्ध ही हैं। बौद्धों की इस छन्दः परम्परा ने संस्कृत साहित्य को भी प्रभावित किया हो, तो कोई आश्चर्य नहीं । जयदेव के 'गीतगोविन्द' में इस प्रभाव को ढूँढ़ा जा सकता है । बाद में १. विक्रमो० ४ / ६२
२. विक्रमो० ४/७०
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org