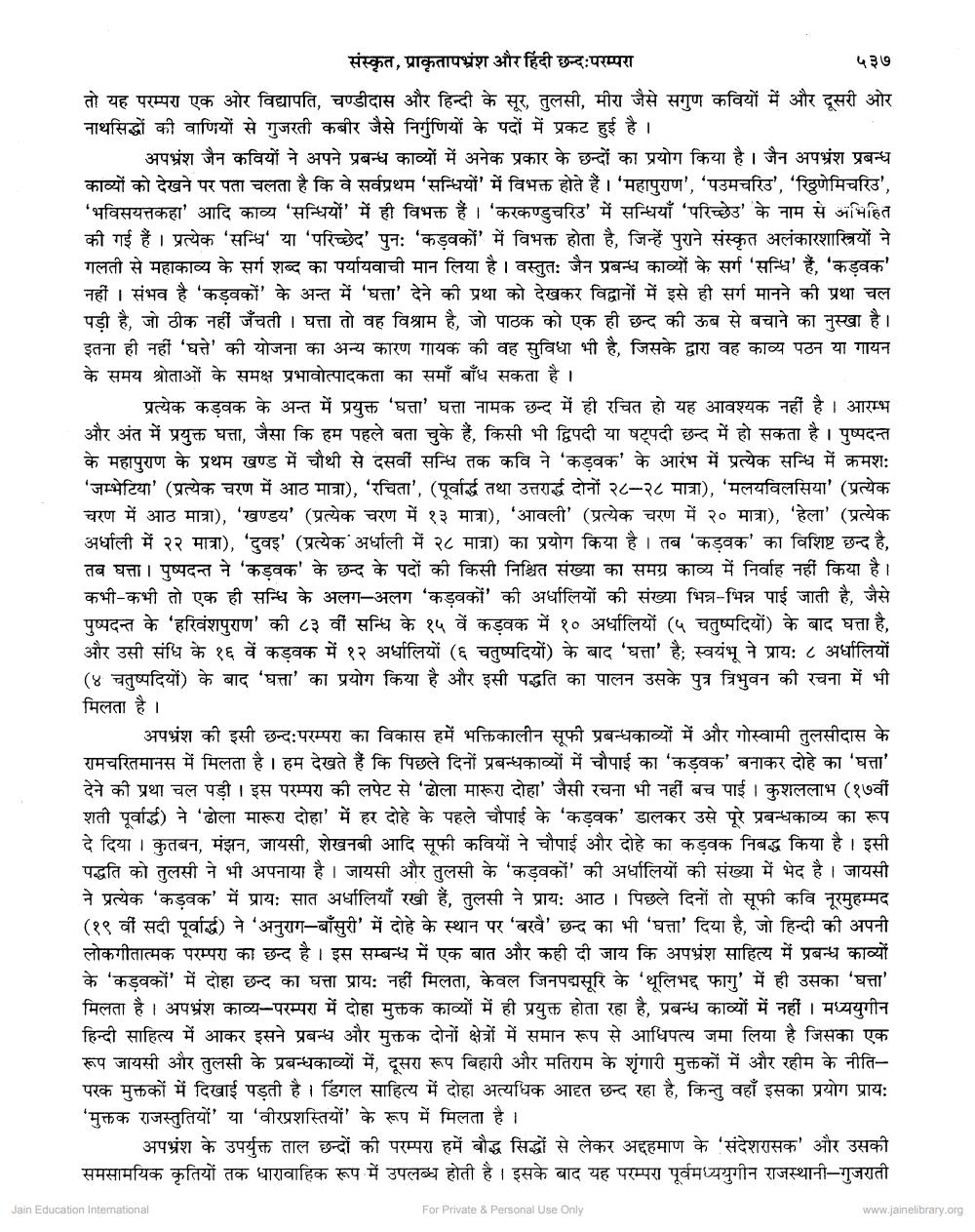________________
संस्कृत, प्राकृतापभ्रंश और हिंदी छन्दःपरम्परा
५३७ तो यह परम्परा एक ओर विद्यापति, चण्डीदास और हिन्दी के सूर, तुलसी, मीरा जैसे सगुण कवियों में और दूसरी ओर नाथसिद्धों की वाणियों से गुजरती कबीर जैसे निर्गुणियों के पदों में प्रकट हुई है।
___अपभ्रंश जैन कवियों ने अपने प्रबन्ध काव्यों में अनेक प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया है। जैन अपभ्रंश प्रबन्ध काव्यों को देखने पर पता चलता है कि वे सर्वप्रथम 'सन्धियों' में विभक्त होते हैं। 'महापुराण', 'पउमचरिउ', 'खिणेमिचरिउ', 'भविसयत्तकहा' आदि काव्य 'सन्धियों' में ही विभक्त हैं । 'करकण्डुचरिउ' में सन्धियाँ 'परिच्छेउ' के नाम से अभिहित की गई हैं। प्रत्येक 'सन्धि' या 'परिच्छेद' पुनः 'कड़वकों' में विभक्त होता है, जिन्हें पुराने संस्कृत अलंकारशास्त्रियों ने गलती से महाकाव्य के सर्ग शब्द का पर्यायवाची मान लिया है। वस्तुत: जैन प्रबन्ध काव्यों के सर्ग 'सन्धि' हैं, 'कड़वक' नहीं । संभव है 'कड़वकों' के अन्त में 'घत्ता' देने की प्रथा को देखकर विद्वानों में इसे ही सर्ग मानने की प्रथा चल पड़ी है, जो ठीक नहीं ऊँचती । घत्ता तो वह विश्राम है, जो पाठक को एक ही छन्द की ऊब से बचाने का नुस्खा है। इतना ही नहीं 'घत्ते' की योजना का अन्य कारण गायक की वह सुविधा भी है, जिसके द्वारा वह काव्य पठन या गायन के समय श्रोताओं के समक्ष प्रभावोत्पादकता का समाँ बाँध सकता है।
प्रत्येक कड़वक के अन्त में प्रयुक्त 'घत्ता' घत्ता नामक छन्द में ही रचित हो यह आवश्यक नहीं है। आरम्भ और अंत में प्रयुक्त घत्ता, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, किसी भी द्विपदी या षट्पदी छन्द में हो सकता है । पुष्पदन्त के महापुराण के प्रथम खण्ड में चौथी से दसवीं सन्धि तक कवि ने 'कड़वक' के आरंभ में प्रत्येक सन्धि में क्रमश: 'जम्भेटिया' (प्रत्येक चरण में आठ मात्रा), 'रचिता', (पूर्वार्द्ध तथा उत्तरार्द्ध दोनों २८-२८ मात्रा), 'मलयविलसिया' (प्रत्येक चरण में आठ मात्रा), 'खण्डय' (प्रत्येक चरण में १३ मात्रा), 'आवली' (प्रत्येक चरण में २० मात्रा), 'हेला' (प्रत्येक अर्धाली में २२ मात्रा), 'दुवइ' (प्रत्येक अर्धाली में २८ मात्रा) का प्रयोग किया है। तब 'कड़वक' का विशिष्ट छन्द है, तब घत्ता। पुष्पदन्त ने 'कड़वक' के छन्द के पदों की किसी निश्चित संख्या का समग्र काव्य में निर्वाह नहीं किया है। कभी-कभी तो एक ही सन्धि के अलग-अलग 'कड़वकों' की अर्धालियों की संख्या भिन्न-भिन्न पाई जाती है, जैसे पुष्पदन्त के 'हरिवंशपुराण' की ८३ वी सन्धि के १५ वें कड़वक में १० अर्धालियों (५ चतुष्पदियों) के बाद घत्ता है,
और उसी संधि के १६ वें कड़वक में १२ अर्धालियों (६ चतुष्पदियों) के बाद 'घत्ता' है; स्वयंभू ने प्रायः ८ अर्धालियों (४ चतुष्पदियों) के बाद 'घत्ता' का प्रयोग किया है और इसी पद्धति का पालन उसके पुत्र त्रिभुवन की रचना में भी मिलता है।
अपभ्रंश की इसी छन्दःपरम्परा का विकास हमें भक्तिकालीन सूफी प्रबन्धकाव्यों में और गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में मिलता है। हम देखते हैं कि पिछले दिनों प्रबन्धकाव्यों में चौपाई का 'कड़वक' बनाकर दोहे का 'घत्ता' देने की प्रथा चल पड़ी। इस परम्परा की लपेट से 'ढोला मारूरा दोहा' जैसी रचना भी नहीं बच पाई। कुशललाभ (१७वीं शती पूर्वाद्ध) ने 'ढोला मारूरा दोहा' में हर दोहे के पहले चौपाई के 'कड़वक' डालकर उसे पूरे प्रबन्धकाव्य का रूप दे दिया । कुतबन, मंझन, जायसी, शेखनबी आदि सूफी कवियों ने चौपाई और दोहे का कड़वक निबद्ध किया है। इसी पद्धति को तुलसी ने भी अपनाया है । जायसी और तुलसी के 'कड़वकों' की अर्धालियों की संख्या में भेद है। जायसी ने प्रत्येक 'कड़वक' में प्रायः सात अर्धालियाँ रखी हैं, तुलसी ने प्रायः आठ । पिछले दिनों तो सूफी कवि नूरमुहम्मद (१९ वीं सदी पूर्वार्द्ध) ने 'अनुराग-बाँसुरी' में दोहे के स्थान पर 'बरवै' छन्द का भी 'घत्ता' दिया है, जो हिन्दी की अपनी लोकगीतात्मक परम्परा का छन्द है। इस सम्बन्ध में एक बात और कही दी जाय कि अपभ्रंश साहित्य में प्रबन्ध काव्यों के 'कड़वकों' में दोहा छन्द का घत्ता प्रायः नहीं मिलता, केवल जिनपद्मसूरि के 'थूलिभद्द फागु' में ही उसका 'घत्ता' मिलता है। अपभ्रंश काव्य-परम्परा में दोहा मुक्तक काव्यों में ही प्रयुक्त होता रहा है, प्रबन्ध काव्यों में नहीं । मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में आकर इसने प्रबन्ध और मुक्तक दोनों क्षेत्रों में समान रूप से आधिपत्य जमा लिया है जिसका एक रूप जायसी और तुलसी के प्रबन्धकाव्यों में, दूसरा रूप बिहारी और मतिराम के शृंगारी मुक्तकों में और रहीम के नीतिपरक मुक्तकों में दिखाई पड़ती है। डिंगल साहित्य में दोहा अत्यधिक आदृत छन्द रहा है, किन्तु वहाँ इसका प्रयोग प्रायः 'मुक्तक राजस्तुतियों' या 'वीरप्रशस्तियों' के रूप में मिलता है।
अपभ्रंश के उपर्युक्त ताल छन्दों की परम्परा हमें बौद्ध सिद्धों से लेकर अद्दहमाण के 'संदेशरासक' और उसकी समसामयिक कृतियों तक धारावाहिक रूप में उपलब्ध होती है । इसके बाद यह परम्परा पूर्वमध्ययुगीन राजस्थानी-गुजराती
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org