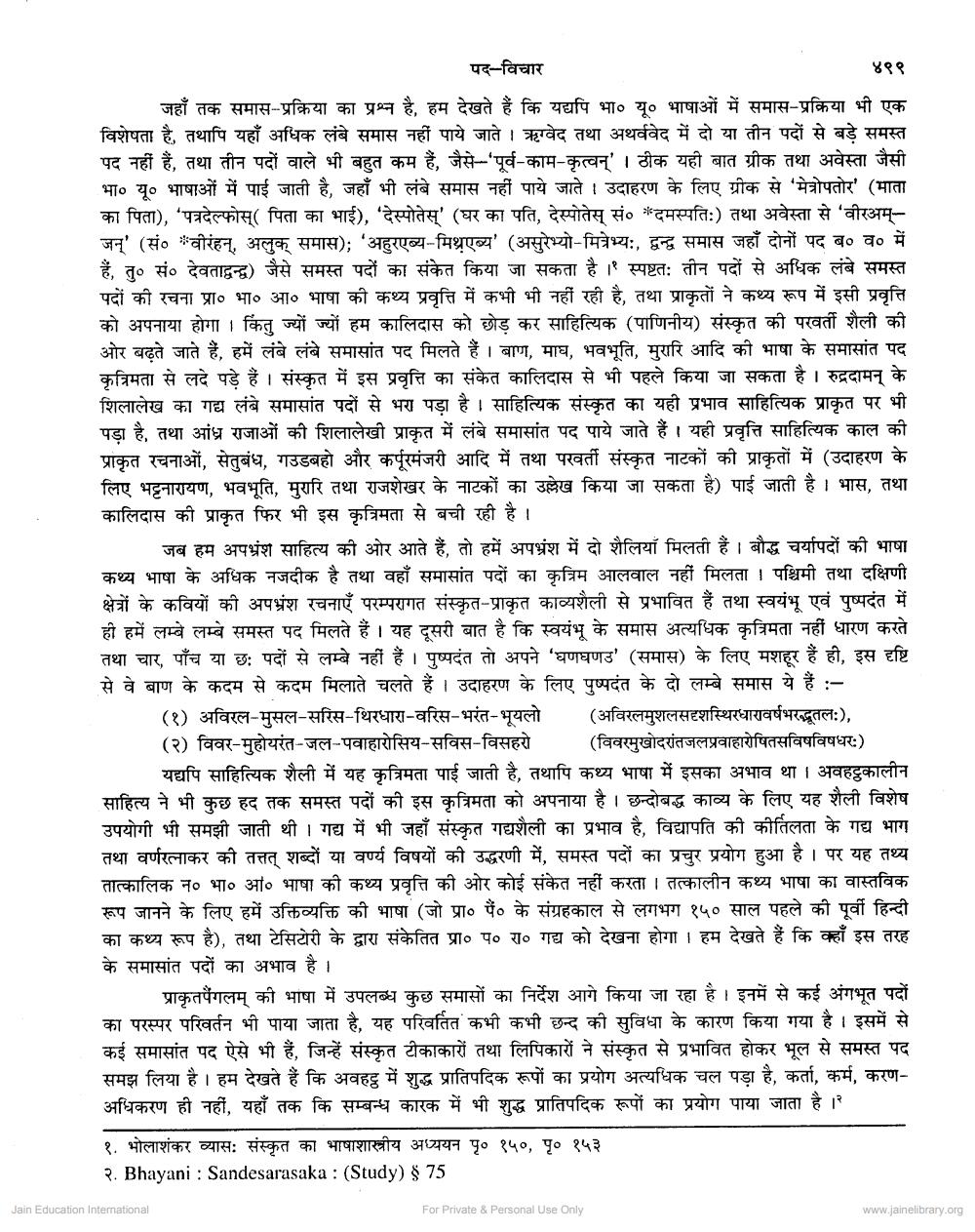________________
४९९
पद-विचार जहाँ तक समास-प्रक्रिया का प्रश्न है, हम देखते हैं कि यद्यपि भा० यू० भाषाओं में समास-प्रक्रिया भी एक विशेषता है, तथापि यहाँ अधिक लंबे समास नहीं पाये जाते । ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में दो या तीन पदों से बड़े समस्त पद नहीं हैं, तथा तीन पदों वाले भी बहुत कम हैं, जैसे-'पूर्व-काम-कृत्वन्' । ठीक यही बात ग्रीक तथा अवेस्ता जैसी भा० यू० भाषाओं में पाई जाती है, जहाँ भी लंबे समास नहीं पाये जाते । उदाहरण के लिए ग्रीक से 'मेत्रोपतोर' (माता का पिता), 'पत्रदेल्फोस्( पिता का भाई), 'देस्पोतेस्' (घर का पति, देस्पोतेस् सं० *दमस्पतिः) तथा अवेस्ता से 'वीरअम्जन्' (सं० *वीरंहन्, अलुक् समास); 'अहुरएब्य-मिथ्रएब्य' (असुरेभ्यो-मित्रेभ्यः, द्वन्द्व समास जहाँ दोनों पद ब० व० में हैं, तु० सं० देवताद्वन्द्व) जैसे समस्त पदों का संकेत किया जा सकता है। स्पष्टतः तीन पदों से अधिक लंबे समस्त पदों की रचना प्रा० भा० आ० भाषा की कथ्य प्रवृत्ति में कभी भी नहीं रही है, तथा प्राकृतों ने कथ्य रूप में इसी प्रवृत्ति को अपनाया होगा । किंतु ज्यों ज्यों हम कालिदास को छोड़ कर साहित्यिक (पाणिनीय) संस्कृत की परवर्ती शैली की ओर बढ़ते जाते हैं, हमें लंबे लंबे समासांत पद मिलते हैं । बाण, माघ, भवभूति, मुरारि आदि की भाषा के समासांत पद कृत्रिमता से लदे पड़े हैं । संस्कृत में इस प्रवृत्ति का संकेत कालिदास से भी पहले किया जा सकता है । रुद्रदामन् के शिलालेख का गद्य लंबे समासांत पदों से भरा पड़ा है। साहित्यिक संस्कृत का यही प्रभाव साहित्यिक प्राकृत पर भी पड़ा है, तथा आंध्र राजाओं की शिलालेखी प्राकृत में लंबे समासांत पद पाये जाते हैं। यही प्रवृत्ति साहित्यिक काल की प्राकृत रचनाओं, सेतुबंध, गउडबहो और कर्पूरमंजरी आदि में तथा परवर्ती संस्कृत नाटकों की प्राकृतों में (उदाहरण के लिए भट्टनारायण, भवभूति, मुरारि तथा राजशेखर के नाटकों का उल्लेख किया जा सकता है) पाई जाती है। भास, तथा कालिदास की प्राकृत फिर भी इस कृत्रिमता से बची रही है।
जब हम अपभ्रंश साहित्य की ओर आते हैं, तो हमें अपभ्रंश में दो शैलियाँ मिलती हैं । बौद्ध चर्यापदों की भाषा कथ्य भाषा के अधिक नजदीक है तथा वहाँ समासांत पदों का कृत्रिम आलवाल नहीं मिलता | पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों के कवियों की अपभ्रंश रचनाएँ परम्परागत संस्कृत-प्राकृत काव्यशैली से प्रभावित हैं तथा स्वयंभू एवं पुष्पदंत में ही हमें लम्बे लम्बे समस्त पद मिलते हैं । यह दूसरी बात है कि स्वयंभू के समास अत्यधिक कृत्रिमता नहीं धारण करते तथा चार, पाँच या छ: पदों से लम्बे नहीं हैं। पुष्पदंत तो अपने 'घणघणउ' (समास) के लिए मशहूर हैं ही, इस दृष्टि से वे बाण के कदम से कदम मिलाते चलते हैं । उदाहरण के लिए पुष्पदंत के दो लम्बे समास ये हैं :
(१) अविरल-मुसल-सरिस-थिरधारा-वरिस-भरंत-भूयलो (अविरलमुशलसदृशस्थिरधारावर्षभरद्भूतलः), (२) विवर-मुहोयरंत-जल-पवाहारोसिय-सविस-विसहरो (विवरमुखोदरांतजलप्रवाहारोषितसविषविषधरः)
यद्यपि साहित्यिक शैली में यह कृत्रिमता पाई जाती है, तथापि कथ्य भाषा में इसका अभाव था । अवहट्ठकालीन साहित्य ने भी कुछ हद तक समस्त पदों की इस कृत्रिमता को अपनाया है। छन्दोबद्ध काव्य के लिए यह शैली विशेष उपयोगी भी समझी जाती थी। गद्य में भी जहाँ संस्कृत गद्यशैली का प्रभाव है, विद्यापति की कीर्तिलता के गद्य भाग तथा वर्णरत्नाकर की तत्तत् शब्दों या वर्ण्य विषयों की उद्धरणी में, समस्त पदों का प्रचुर प्रयोग हुआ है। पर यह तथ्य तात्कालिक न० भा० आं० भाषा की कथ्य प्रवृत्ति की ओर कोई संकेत नहीं करता । तत्कालीन कथ्य भाषा का वास्तविक रूप जानने के लिए हमें उक्तिव्यक्ति की भाषा (जो प्रा० पैं. के संग्रहकाल से लगभग १५० साल पहले की पूर्वी हिन्दी का कथ्य रूप है), तथा टेसिटोरी के द्वारा संकेतित प्रा०प० रा० गद्य को देखना होगा । हम देखते हैं कि वहाँ इस तरह के समासांत पदों का अभाव है।
प्राकृतपैंगलम् की भाषा में उपलब्ध कुछ समासों का निर्देश आगे किया जा रहा है। इनमें से कई अंगभूत पदों का परस्पर परिवर्तन भी पाया जाता है, यह परिवर्तित कभी कभी छन्द की सुविधा के कारण किया गया है। इसमें से कई समासांत पद ऐसे भी हैं, जिन्हें संस्कृत टीकाकारों तथा लिपिकारों ने संस्कृत से प्रभावित होकर भूल से समस्त पद समझ लिया है। हम देखते हैं कि अवहट्ठ में शुद्ध प्रातिपदिक रूपों का प्रयोग अत्यधिक चल पड़ा है, कर्ता, कर्म, करणअधिकरण ही नहीं, यहाँ तक कि सम्बन्ध कारक में भी शुद्ध प्रातिपदिक रूपों का प्रयोग पाया जाता है ।२
१. भोलाशंकर व्यासः संस्कृत का भाषाशास्त्रीय अध्ययन पृ० १५०, पृ० १५३ २. Bhayani : Sandesarasaka : (Study) 875
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org