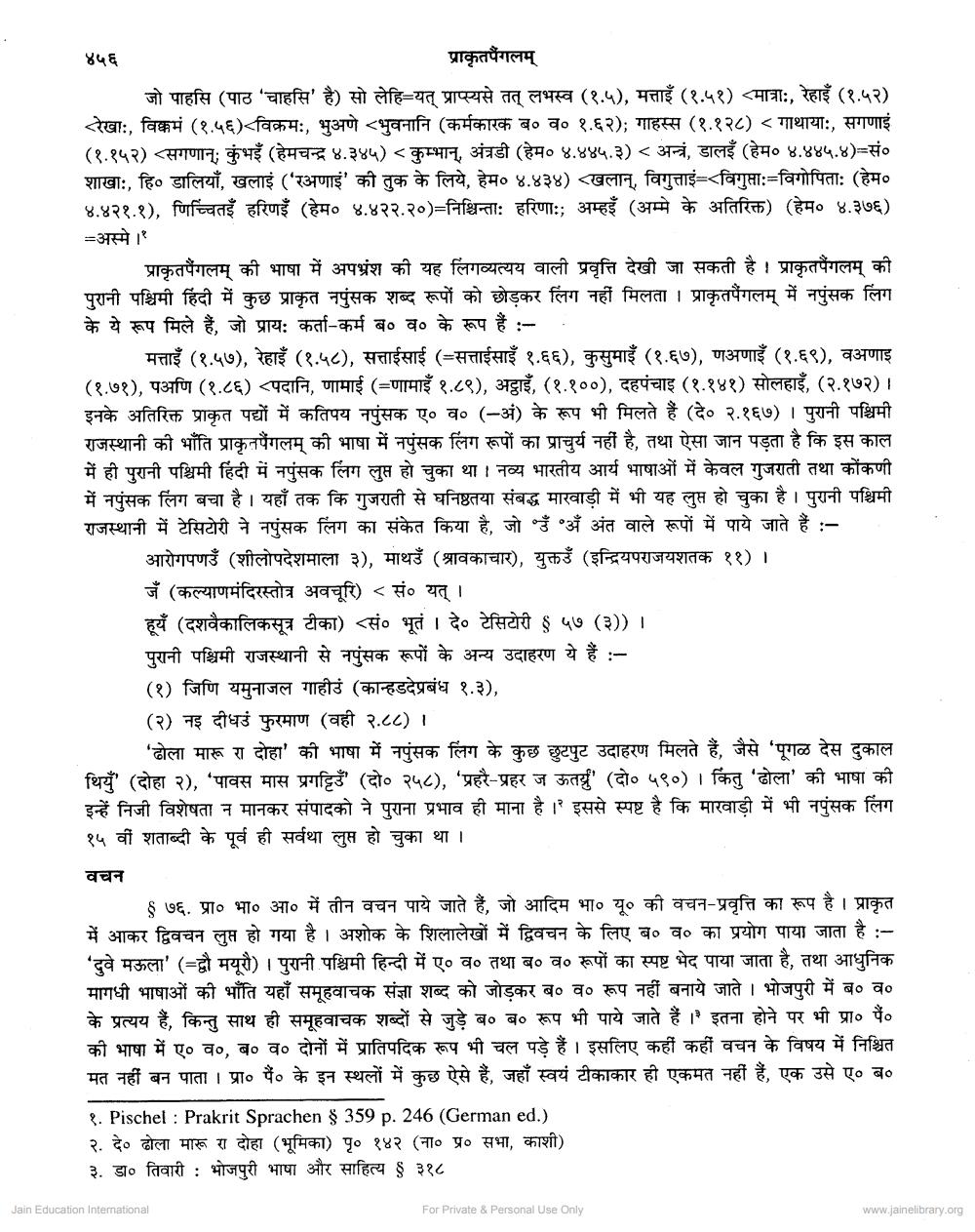________________
४५६
प्राकृतपैंगलम् जो पाहसि (पाठ 'चाहसि' है) सो लेहि यत् प्राप्स्यसे तत् लभस्व (१.५), मत्ता' (१.५१) <मात्राः, रेहाइँ (१.५२) रेखाः, विक्कम (१.५६)< विक्रमः, भुअणे <भुवनानि (कर्मकारक ब० व० १.६२); गाहस्स (१.१२८) < गाथायाः, सगणाई (१.१५२) <सगणान्; कुंभइँ (हेमचन्द्र ४.३४५) < कुम्भान्, अंबडी (हेम० ४.४४५.३) < अन्त्रं, डालइँ (हेम० ४.४४५.४)=सं० शाखाः, हि० डालियाँ, खलाई ('रअणाई' की तुक के लिये, हेम० ४.४३४) <खलान्, विगुत्ताई=<विगुप्ता: विगोपिताः (हेम० ४.४२१.१), णिच्चितइँ हरिणइँ (हेम० ४.४२२.२०) निश्चिन्ताः हरिणाः; अम्हइँ (अम्मे के अतिरिक्त) (हेम० ४.३७६) =अस्मे ।।
प्राकृतपैंगलम् की भाषा में अपभ्रंश की यह लिंगव्यत्यय वाली प्रवृत्ति देखी जा सकती है। प्राकृतपैंगलम् की
पश्चिमी हिंदी में कछ प्राकत नपंसक शब्द रूपों को छोडकर लिंग नहीं मिलता । प्राकृतपैंगलम् में नपुंसक लिंग के ये रूप मिले हैं, जो प्रायः कर्ता-कर्म ब० व० के रूप हैं :
___ मत्ताइँ (१.५७), रेहाइँ (१.५८), सत्ताईसाई (=सत्ताईसाइँ १.६६), कुसुमाइँ (१.६७), णअणाइँ (१.६९), वअणाइ (१.७१), पअणि (१.८६) <पदानि, णामाई (=णामाइँ १.८९), अट्ठाइँ, (१.१००), दहपंचाइ (१.१४१) सोलहाइँ, (२.१७२) । इनके अतिरिक्त प्राकृत पद्यों में कतिपय नपुंसक ए० व० (-अं) के रूप भी मिलते हैं (दे० २.१६७) । पुरानी पश्चिमी राजस्थानी की भाँति प्राकृतपैंगलम् की भाषा में नपुंसक लिंग रूपों का प्राचुर्य नहीं है, तथा ऐसा जान पड़ता है कि इस काल में ही पुरानी पश्चिमी हिंदी में नपुंसक लिंग लुप्त हो चुका था। नव्य भारतीय आर्य भाषाओं में केवल गुजराती तथा कोंकणी में नपुंसक लिंग बचा है। यहाँ तक कि गुजराती से घनिष्ठतया संबद्ध मारवाड़ी में भी यह लुप्त हो चुका है। पुरानी पश्चिमी राजस्थानी में टेसिटोरी ने नपुंसक लिंग का संकेत किया है, जो उँ अँ अंत वाले रूपों में पाये जाते हैं :
आरोगपणउँ (शीलोपदेशमाला ३), माथउँ (श्रावकाचार), युक्तउँ (इन्द्रियपराजयशतक ११)। ज (कल्याणमंदिरस्तोत्र अवचूरि) < सं० यत् । हूय (दशवैकालिकसूत्र टीका) <सं० भूतं । दे० टेसिटोरी $ ५७ (३)) । पुरानी पश्चिमी राजस्थानी से नपुंसक रूपों के अन्य उदाहरण ये हैं :(१) जिणि यमुनाजल गाहीउं (कान्हडदेप्रबंध १.३), (२) नइ दीधउं फुरमाण (वही २.८८) ।
'ढोला मारू रा दोहा' की भाषा में नपुंसक लिंग के कुछ छुटपुट उदाहरण मिलते हैं, जैसे 'पूगळ देस दुकाल थियँ' (दोहा २), 'पावस मास प्रगट्टिउँ' (दो० २५८), 'प्रहरै-प्रहर ज ऊतयु' (दो० ५९०) । किंतु 'ढोला' की भाषा की इन्हें निजी विशेषता न मानकर संपादको ने पुराना प्रभाव ही माना है। इससे स्पष्ट है कि मारवाड़ी में भी नपुंसक लिंग १५ वीं शताब्दी के पूर्व ही सर्वथा लुप्त हो चुका था ।
वचन
७६. प्रा० भा० आ० में तीन वचन पाये जाते हैं, जो आदिम भा० यू० की वचन-प्रवृत्ति का रूप है । प्राकृत में आकर द्विवचन लुप्त हो गया है। अशोक के शिलालेखों में द्विवचन के लिए ब० व० का प्रयोग पाया जाता है :'दुवे मऊला' (=द्वौ मयूरो)। पुरानी पश्चिमी हिन्दी में ए० व० तथा ब० व० रूपों का स्पष्ट भेद पाया जाता है, तथा आधुनिक मागधी भाषाओं की भाँति यहाँ समूहवाचक संज्ञा शब्द को जोड़कर ब० व० रूप नहीं बनाये जाते । भोजपुरी में ब० व० के प्रत्यय हैं, किन्तु साथ ही समूहवाचक शब्दों से जुड़े ब० ब० रूप भी पाये जाते हैं। इतना होने पर भी प्रा० पैं० की भाषा में ए० व०, ब० व० दोनों में प्रातिपदिक रूप भी चल पड़े हैं। इसलिए कहीं कहीं वचन के विषय में निश्चित मत नहीं बन पाता । प्रा० पैं० के इन स्थलों में कुछ ऐसे हैं, जहाँ स्वयं टीकाकार ही एकमत नहीं हैं, एक उसे ए० ब०
१. Pischel : Prakrit Sprachen 8359 p. 246 (German ed.) २. दे० ढोला मारू रा दोहा (भूमिका) पृ० १४२ (ना० प्र० सभा, काशी) ३. डा० तिवारी : भोजपुरी भाषा और साहित्य $ ३१८
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org