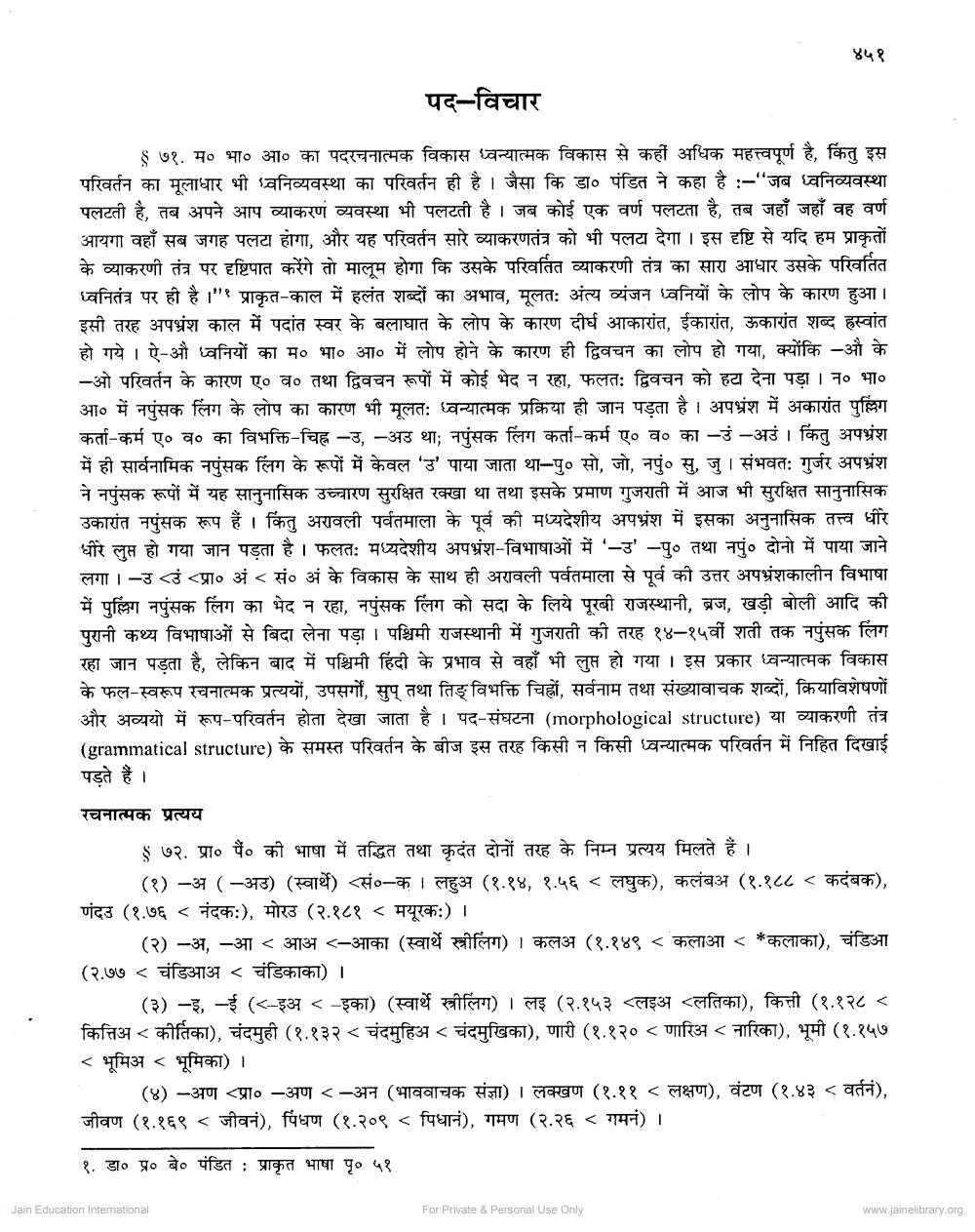________________
४५१
४५१
पद-विचार
६७१. म० भा० आ० का पदरचनात्मक विकास ध्वन्यात्मक विकास से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है, किंतु इस परिवर्तन का मूलाधार भी ध्वनिव्यवस्था का परिवर्तन ही है । जैसा कि डा० पंडित ने कहा है :-"जब ध्वनिव्यवस्था पलटती है, तब अपने आप व्याकरण व्यवस्था भी पलटती है। जब कोई एक वर्ण पलटता है, तब जहाँ जहाँ वह वर्ण आयगा वहाँ सब जगह पलटा होगा, और यह परिवर्तन सारे व्याकरणतंत्र को भी पलटा देगा । इस दृष्टि से यदि हम प्राकृतों के व्याकरणी तंत्र पर दृष्टिपात करेंगे तो मालूम होगा कि उसके परिवर्तित व्याकरणी तंत्र का सारा आधार उसके परिवर्तित ध्वनितंत्र पर ही है।"१ प्राकृत-काल में हलंत शब्दों का अभाव, मूलतः अंत्य व्यंजन ध्वनियों के लोप के कारण हुआ। इसी तरह अपभ्रंश काल में पदांत स्वर के बलाघात के लोप के कारण दीर्घ आकारांत, ईकारांत, ऊकारांत शब्द ह्रस्वांत हो गये । ऐ-औ ध्वनियों का म० भा० आ० में लोप होने के कारण ही द्विवचन का लोप हो गया, क्योंकि -औ के -ओ परिवर्तन के कारण ए० व० तथा द्विवचन रूपों में कोई भेद न रहा, फलतः द्विवचन को हटा देना पड़ा । न० भा० आ० में नपुंसक लिंग के लोप का कारण भी मूलतः ध्वन्यात्मक प्रक्रिया ही जान पड़ता है। अपभ्रंश में अकारांत पुल्लिंग कर्ता-कर्म ए० व० का विभक्ति-चिह्न -उ, -अउ था; नपुंसक लिंग कर्ता-कर्म ए० व० का -उं-अउं । किंतु अपभ्रंश में ही सार्वनामिक नपुंसक लिंग के रूपों में केवल 'उ' पाया जाता था-पु० सो, जो, नपुं० सु, जु । संभवत: गुर्जर अपभ्रंश ने नपुंसक रूपों में यह सानुनासिक उच्चारण सुरक्षित रक्खा था तथा इसके प्रमाण गुजराती में आज भी सुरक्षित सानुनासिक उकारांत नपुंसक रूप हैं। किंतु अरावली पर्वतमाला के पूर्व की मध्यदेशीय अपभ्रंश में इसका अनुनासिक तत्त्व धीरे धीरे लुप्त हो गया जान पड़ता है। फलतः मध्यदेशीय अपभ्रंश-विभाषाओं में '-उ' -पु० तथा नपुं० दोनो में पाया जाने लगा। -उ <उं <प्रा० अं< सं० अं के विकास के साथ ही अरावली पर्वतमाला से पूर्व की उत्तर अपभ्रंशकालीन विभाषा में पुल्लिंग नपुंसक लिंग का भेद न रहा, नपुंसक लिंग को सदा के लिये पूरबी राजस्थानी, ब्रज, खड़ी बोली आदि की पुरानी कथ्य विभाषाओं से बिदा लेना पड़ा । पश्चिमी राजस्थानी में गुजराती की तरह १४-१५वीं शती तक नपुंसक लिंग रहा जान पड़ता है, लेकिन बाद में पश्चिमी हिंदी के प्रभाव से वहाँ भी लुप्त हो गया । इस प्रकार ध्वन्यात्मक विकास के फल-स्वरूप रचनात्मक प्रत्ययों, उपसर्गों, सुप् तथा ति विभक्ति चिह्नों, सर्वनाम तथा संख्यावाचक शब्दों, क्रियाविशेषणों
और अव्ययो में रूप-परिवर्तन होता देखा जाता है । पद-संघटना (morphological structure) या व्याकरणी तंत्र (grammatical structure) के समस्त परिवर्तन के बीज इस तरह किसी न किसी ध्वन्यात्मक परिवर्तन में निहित दिखाई पड़ते हैं। रचनात्मक प्रत्यय
६ ७२. प्रा० ० की भाषा में तद्धित तथा कृदंत दोनों तरह के निम्न प्रत्यय मिलते हैं ।
(१) -अ (-अउ) (स्वार्थे) <सं०-क । लहुअ (१.१४, १.५६ < लघुक), कलंबअ (१.१८८ < कदंबक), णंदउ (१.७६ < नंदकः), मोरउ (२.१८१ < मयूरकः) ।
(२) -अ, -आ < आअ <-आका (स्वार्थे स्त्रीलिंग) । कलअ (१.१४९ < कलाआ < *कलाका), चंडिआ (२.७७ < चंडिआअ < चंडिकाका) ।
(३) -इ, -ई (<-इअ < -इका) (स्वार्थे स्त्रीलिंग) । लइ (२.१५३ <लइअ <लतिका), कित्ती (१.१२८ < कित्तिअ< कीर्तिका), चंदमुही (१.१३२ < चंदमुहिअ < चंदमुखिका), णारी (१.१२० <णारिअ< नारिका), भूमी (१.१५७ < भूमिअ < भूमिका)।
(४)-अण <प्रा० -अण <-अन (भाववाचक संज्ञा) । लक्खण (१.११ < लक्षण), वंटण (१.४३ ८ वर्तन), जीवण (१.१६९ < जीवन), पिंधण (१.२०९ < पिधान), गमण (२.२६ < गमनं) ।
१. डा० प्र० बे० पंडित : प्राकृत भाषा पृ० ५१
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org