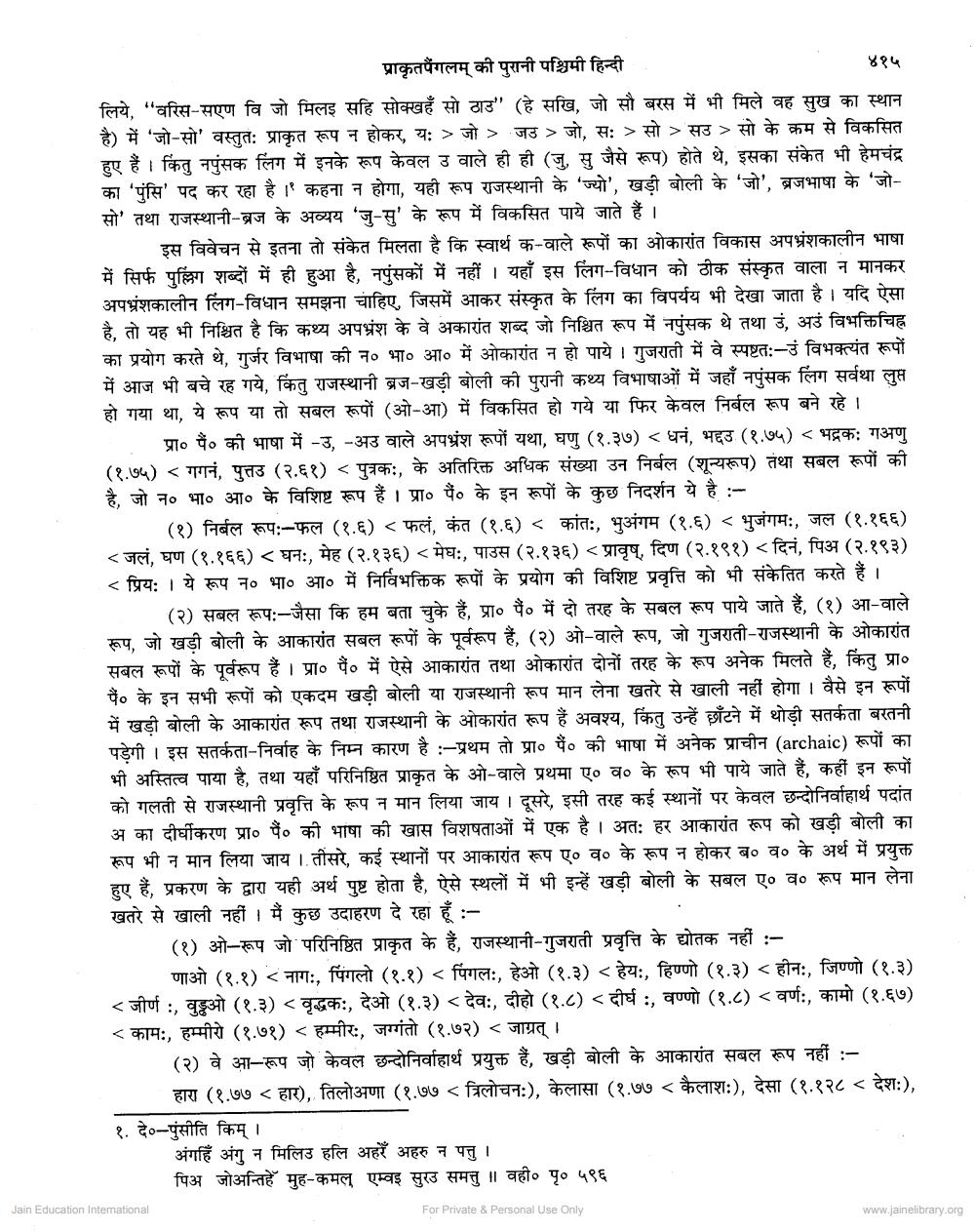________________
४१५
प्राकृतपैंगलम् की पुरानी पश्चिमी हिन्दी । लिये, "वरिस-सएण वि जो मिलइ सहि सोक्खहँ सो ठाउ" (हे सखि, जो सौ बरस में भी मिले वह सुख का स्थान है) में 'जो-सो' वस्तुतः प्राकृत रूप न होकर, यः > जो > जउ > जो, सः > सो > सउ > सो के क्रम से विकसित हुए हैं। किंतु नपुंसक लिंग में इनके रूप केवल उ वाले ही ही (जु, सु जैसे रूप) होते थे, इसका संकेत भी हेमचंद्र का 'पुंसि' पद कर रहा है। कहना न होगा, यही रूप राजस्थानी के 'ज्यो', खड़ी बोली के 'जो', ब्रजभाषा के 'जोसो' तथा राजस्थानी-ब्रज के अव्यय 'जु-सु' के रूप में विकसित पाये जाते हैं ।
इस विवेचन से इतना तो संकेत मिलता है कि स्वार्थ क-वाले रूपों का ओकारांत विकास अपभ्रंशकालीन भाषा में सिर्फ पुल्लिंग शब्दों में ही हुआ है, नपुंसकों में नहीं । यहाँ इस लिंग-विधान को ठीक संस्कृत वात अपभ्रंशकालीन लिंग-विधान समझना चाहिए, जिसमें आकर संस्कृत के लिंग का विपर्यय भी देखा जाता है। यदि ऐसा है, तो यह भी निश्चित है कि कथ्य अपभ्रंश के वे अकारांत शब्द जो निश्चित रूप में नपुंसक थे तथा उं, अउं विभक्तिचिह्न का प्रयोग करते थे, गुर्जर विभाषा की न० भा० आ० में ओकारांत न हो पाये । गुजराती में वे स्पष्टतः-उं विभक्त्यंत रूपों में आज भी बचे रह गये, किंतु राजस्थानी ब्रज-खड़ी बोली की पुरानी कथ्य विभाषाओं में जहाँ नपुंसक लिंग सर्वथा लुप्त हो गया था, ये रूप या तो सबल रूपों (ओ-आ) में विकसित हो गये या फिर केवल निर्बल रूप बने रहे ।
. प्रा० ० की भाषा में -उ, -अउ वाले अपभ्रंश रूपों यथा, घणु (१.३७) < धनं, भद्दउ (१.७५) < भद्रक: गअणु (१.७५) < गगनं, पुत्तउ (२.६१) < पुत्रकः, के अतिरिक्त अधिक संख्या उन निर्बल (शून्यरूप) तथा सबल रूपों की है, जो न० भा० आ० के विशिष्ट रूप हैं । प्रा० पैं० के इन रूपों के कुछ निदर्शन ये है :
(१) निर्बल रूपः-फल (१.६) < फलं, कंत (१.६) < कांतः, भुअंगम (१.६) < भुजंगमः, जल (१.१६६) < जलं, घण (१.१६६) < घनः, मेह (२.१३६) < मेघः, पाउस (२.१३६) < प्रावृष, दिण (२.१९१) < दिनं, पिअ (२.१९३) < प्रियः । ये रूप न० भा० आ० में निर्विभक्तिक रूपों के प्रयोग की विशिष्ट प्रवृत्ति को भी संकेतित करते हैं ।
(२) सबल रूपः-जैसा कि हम बता चुके हैं, प्रा० पै० में दो तरह के सबल रूप पाये जाते हैं, (१) आ-वाले रूप, जो खड़ी बोली के आकारांत सबल रूपों के पूर्वरूप हैं, (२) ओ-वाले रूप, जो गुजराती-राजस्थानी के ओकारांत सबल रूपों के पूर्वरूप हैं । प्रा० पैं० में ऐसे आकारांत तथा ओकारांत दोनों तरह के रूप अनेक मिलते हैं, किंतु प्रा० पैं० के इन सभी रूपों को एकदम खड़ी बोली या राजस्थानी रूप मान लेना खतरे से खाली नहीं होगा। वैसे इन रूपों में खड़ी बोली के आकारांत रूप तथा राजस्थानी के ओकारांत रूप हैं अवश्य, किंतु उन्हें छाँटने में थोड़ी सतर्कता बरतनी पड़ेगी । इस सतर्कता-निर्वाह के निम्न कारण है :-प्रथम तो प्रा० पैं० की भाषा में अनेक प्राचीन (archaic) रूपों का भी अस्तित्व पाया है, तथा यहाँ परिनिष्ठित प्राकृत के ओ-वाले प्रथमा ए० व० के रूप भी पाये जाते हैं, कहीं इन रूपों को गलती से राजस्थानी प्रवृत्ति के रूप न मान लिया जाय । दूसरे, इसी तरह कई स्थानों पर केवल छन्दोनिर्वाहार्थ पदांत अ का दीर्धीकरण प्रा० पैं. की भाषा की खास विशषताओं में एक है । अतः हर आकारांत रूप को खड़ी बोली का रूप भी न मान लिया जाय । तीसरे, कई स्थानों पर आकारांत रूप ए० व० के रूप न होकर ब० व० के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं, प्रकरण के द्वारा यही अर्थ पुष्ट होता है, ऐसे स्थलों में भी इन्हें खड़ी बोली के सबल ए० व० रूप मान लेना खतरे से खाली नहीं । मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ :
(१) ओ-रूप जो परिनिष्ठित प्राकृत के हैं, राजस्थानी-गुजराती प्रवृत्ति के द्योतक नहीं :
णाओ (१.१) < नागः, पिंगलो (१.१) < पिंगलः, हेओ (१.३) < हेयः, हिण्णो (१.३) < हीनः, जिण्णो (१.३) < जीर्ण :, वुड्डओ (१.३) < वृद्धकः, देओ (१.३) < देवः, दीहो (१.८) < दीर्घ :, वण्णो (१.८) < वर्णः, कामो (१.६७) < कामः, हम्मीरो (१.७१) < हम्मीरः, जग्गंतो (१.७२) < जाग्रत् ।
(२) वे आ-रूप जो केवल छन्दोनिर्वाहार्थ प्रयुक्त हैं, खड़ी बोली के आकारांत सबल रूप नहीं :
हारा (१.७७ < हार), तिलोअणा (१.७७ < त्रिलोचनः), केलासा (१.७७ < कैलाशः), देसा (१.१२८ < देश:), १. दे०-पुंसीति किम् ।
अंगहिँ अंगु न मिलिउ हलि अह अहरु न पत्तु ।
पिअ जोअन्तिहें मुह-कमल एम्वइ सुरउ समत्तु ॥ वही० पृ० ५९६ Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org