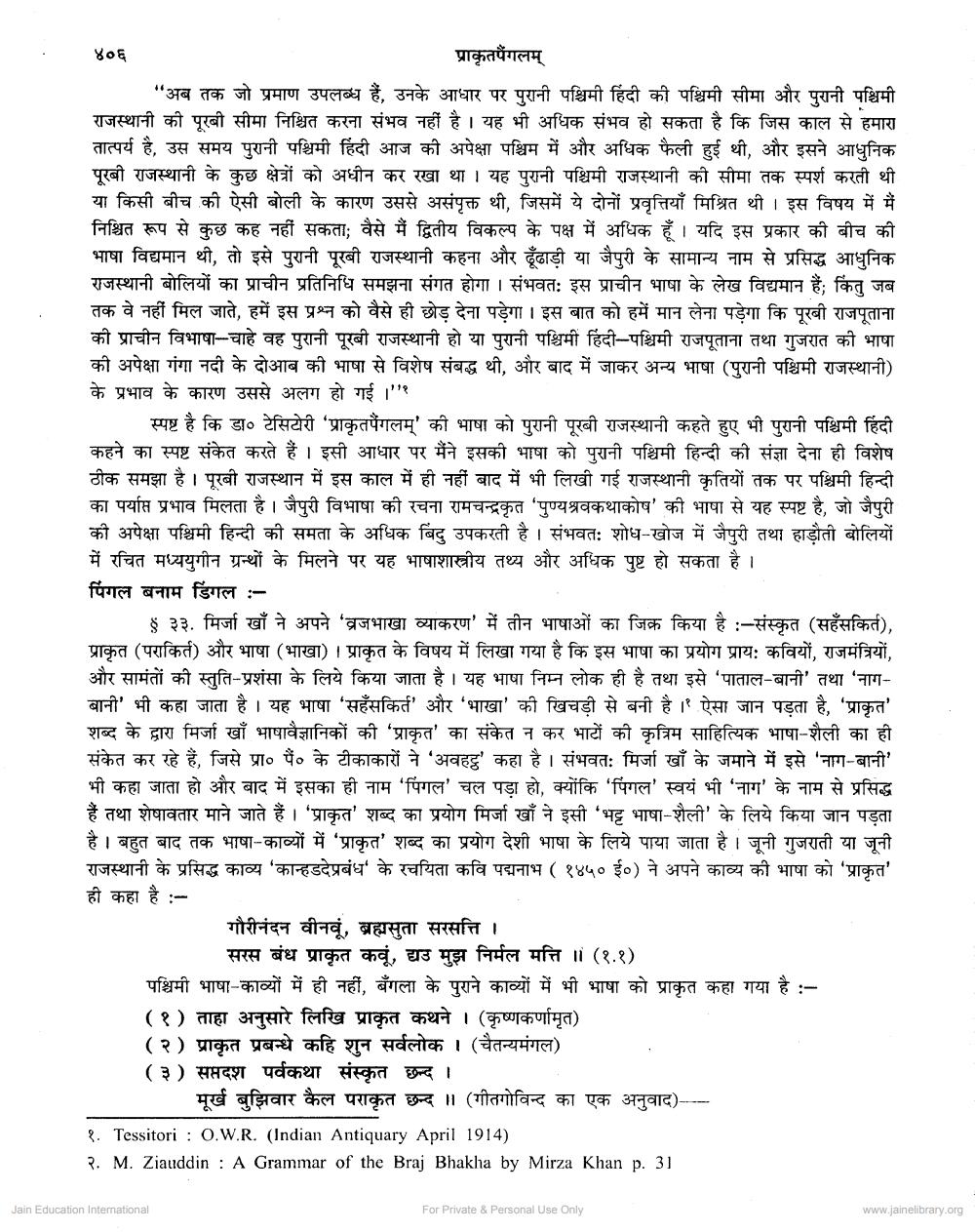________________
४०६
प्राकृतपैंगलम् "अब तक जो प्रमाण उपलब्ध हैं, उनके आधार पर पुरानी पश्चिमी हिंदी की पश्चिमी सीमा और पुरानी पश्चिमी राजस्थानी की पूरबी सीमा निश्चित करना संभव नहीं है । यह भी अधिक संभव हो सकता है कि जिस काल से हमारा तात्पर्य है, उस समय पुरानी पश्चिमी हिंदी आज की अपेक्षा पश्चिम में और अधिक फैली हुई थी, और इसने आधुनिक पूरबी राजस्थानी के कुछ क्षेत्रों को अधीन कर रखा था । यह पुरानी पश्चिमी राजस्थानी की सीमा तक स्पर्श करती थी या किसी बीच की ऐसी बोली के कारण उससे असंपृक्त थी, जिसमें ये दोनों प्रवृत्तियाँ मिश्रित थी। इस विषय में मैं निश्चित रूप से कुछ कह नहीं सकता; वैसे मैं द्वितीय विकल्प के पक्ष में अधिक हूँ। यदि इस प्रकार की बीच की भाषा विद्यमान थी, तो इसे पुरानी पूरबी राजस्थानी कहना और ढूंढाड़ी या जैपुरी के सामान्य नाम से प्रसिद्ध आधुनिक राजस्थानी बोलियों का प्राचीन प्रतिनिधि समझना संगत होगा । संभवत: इस प्राचीन भाषा के लेख विद्यमान हैं; किंतु जब तक वे नहीं मिल जाते, हमें इस प्रश्न को वैसे ही छोड़ देना पड़ेगा। इस बात को हमें मान लेना पड़ेगा कि पूरबी राजपूताना की प्राचीन विभाषा-चाहे वह पुरानी पूरबी राजस्थानी हो या पुरानी पश्चिमी हिंदी-पश्चिमी राजपूताना तथा गुजरात की भाषा की अपेक्षा गंगा नदी के दोआब की भाषा से विशेष संबद्ध थी, और बाद में जाकर अन्य भाषा (पुरानी पश्चिमी राजस्थानी) के प्रभाव के कारण उससे अलग हो गई ।'१
स्पष्ट है कि डा० टेसिटोरी 'प्राकृतपैंगलम्' की भाषा को पुरानी पूरबी राजस्थानी कहते हुए भी पुरानी पश्चिमी हिंदी कहने का स्पष्ट संकेत करते हैं । इसी आधार पर मैंने इसकी भाषा को परानी पश्चिमी हिन्दी की संज्ञा देना ही विशेष ठीक समझा है। पूरबी राजस्थान में इस काल में ही नहीं बाद में भी लिखी गई राजस्थानी कृतियों तक पर पश्चिमी हिन्दी का पर्याप्त प्रभाव मिलता है । जैपुरी विभाषा की रचना रामचन्द्रकृत 'पुण्यश्रवकथाकोष' की भाषा से यह स्पष्ट है, जो जैपुरी की अपेक्षा पश्चिमी हिन्दी की समता के अधिक बिंदु उपकरती है । संभवतः शोध-खोज में जैपुरी तथा हाड़ौती बोलियों में रचित मध्ययुगीन ग्रन्थों के मिलने पर यह भाषाशास्त्रीय तथ्य और अधिक पुष्ट हो सकता है। पिंगल बनाम डिंगल :
३३. मिर्जा खाँ ने अपने 'व्रजभाखा व्याकरण' में तीन भाषाओं का जिक्र किया है :-संस्कृत (सहँसकिर्त) प्राकृत (पराकिर्त) और भाषा (भाखा) । प्राकृत के विषय में लिखा गया है कि इस भाषा का प्रयोग प्रायः कवियों, राजमंत्रियों,
और सामंतों की स्तुति-प्रशंसा के लिये किया जाता है। यह भाषा निम्न लोक ही है तथा इसे 'पाताल-बानी' तथा 'नागबानी' भी कहा जाता है। यह भाषा 'सहँसकिर्त' और 'भाखा' की खिचड़ी से बनी है । ऐसा जान पड़ता है, 'प्राकृत' शब्द के द्वारा मिर्जा खाँ भाषावैज्ञानिकों की 'प्राकृत' का संकेत न कर भाटों की कृत्रिम साहित्यिक भाषा-शैली का ही संकेत कर रहे हैं, जिसे प्रा० पैं० के टीकाकारों ने 'अवहट्ठ' कहा है। संभवतः मिर्जा खाँ के जमाने में इसे 'नाग-बानी' भी कहा जाता हो और बाद में इसका ही नाम 'पिंगल' चल पड़ा हो, क्योंकि 'पिंगल' स्वयं भी 'नाग' के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा शेषावतार माने जाते हैं । 'प्राकृत' शब्द का प्रयोग मिर्जा खाँ ने इसी 'भट्ट भाषा-शैली' के लिये किया जान पड़ता है। बहुत बाद तक भाषा-काव्यों में 'प्राकृत' शब्द का प्रयोग देशी भाषा के लिये पाया जाता है । जूनी गुजराती या जूनी राजस्थानी के प्रसिद्ध काव्य ‘कान्हडदेप्रबंध' के रचयिता कवि पद्मनाभ ( १४५० ई०) ने अपने काव्य की भाषा को 'प्राकृत' ही कहा है :
गौरीनंदन वीनवू, ब्रह्मसुता सरसत्ति ।
सरस बंध प्राकृत कवू, द्यउ मुझ निर्मल मत्ति ॥ (१.१) । पश्चिमी भाषा-काव्यों में ही नहीं, बँगला के पुराने काव्यों में भी भाषा को प्राकृत कहा गया है :(१) ताहा अनुसारे लिखि प्राकृत कथने । (कृष्णकर्णामृत) (२) प्राकृत प्रबन्धे कहि शुन सर्वलोक । (चैतन्यमंगल) (३) सप्तदश पर्वकथा संस्कृत छन्द ।
मूर्ख बुझिवार कैल पराकृत छन्द ।। (गीतगोविन्द का एक अनुवाद)---- १. Tessitori : O.W.R. (Indian Antiquary April 1914) २. M. Ziauddin : A Grammar of the Braj Bhakha by Mirza Khan p. 31
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org