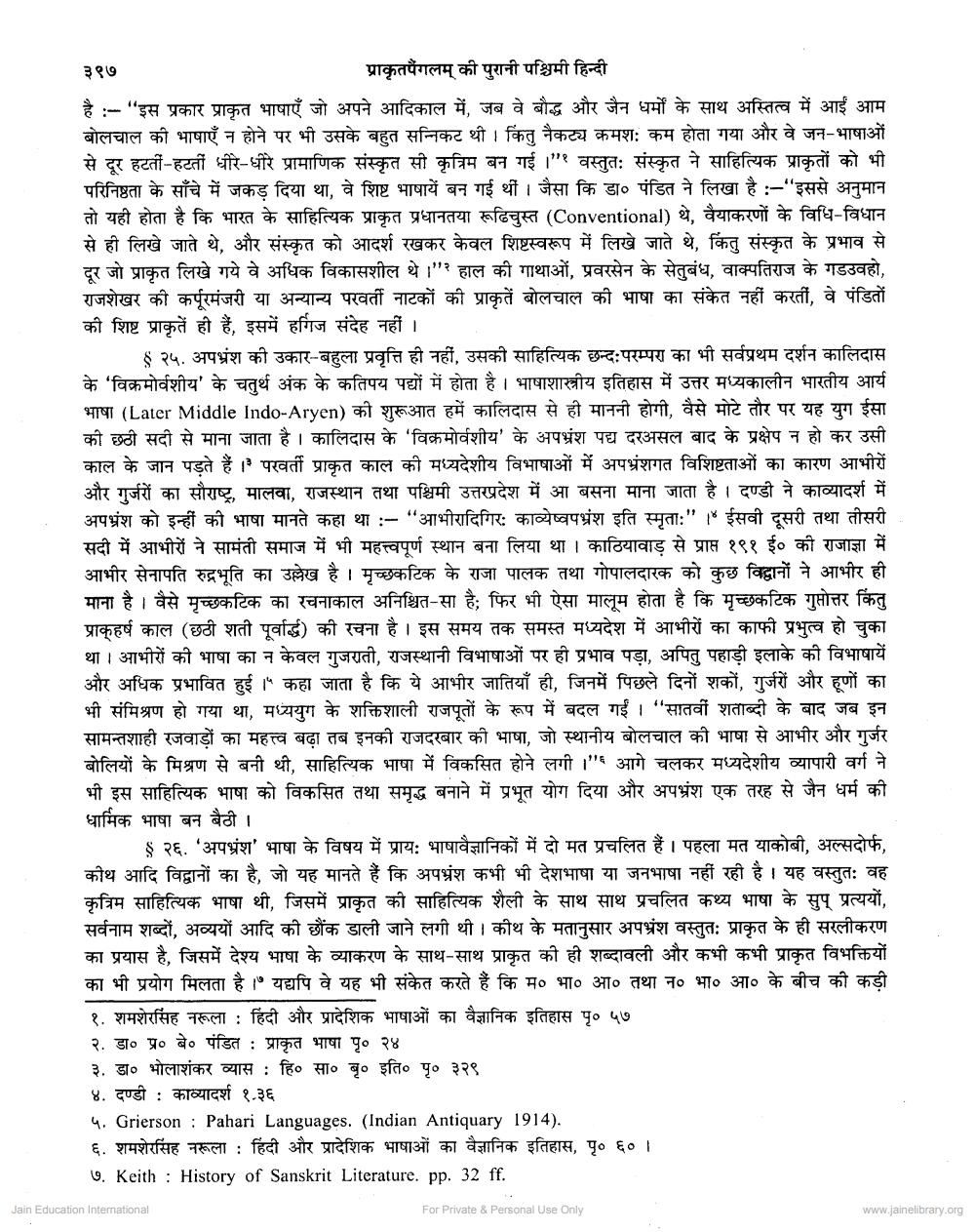________________
३९७
प्राकृतपैंगलम् की पुरानी पश्चिमी हिन्दी है :- "इस प्रकार प्राकृत भाषाएँ जो अपने आदिकाल में, जब वे बौद्ध और जैन धर्मों के साथ अस्तित्व में आईं आम बोलचाल की भाषाएँ न होने पर भी उसके बहुत सन्निकट थी। किंतु नैकट्य क्रमशः कम होता गया और वे जन-भाषाओं से दूर हटती-हटतीं धीरे-धीरे प्रामाणिक संस्कृत सी कृत्रिम बन गई ।"१ वस्तुतः संस्कृत ने साहित्यिक प्राकृतों को भी परिनिष्ठता के साँचे में जकड़ दिया था, वे शिष्ट भाषायें बन गई थीं। जैसा कि डा० पंडित ने लिखा है :-"इससे अनुमान तो यही होता है कि भारत के साहित्यिक प्राकृत प्रधानतया रूढिचुस्त (Conventional) थे, वैयाकरणों के विधि-विधान से ही लिखे जाते थे, और संस्कृत को आदर्श रखकर केवल शिष्टस्वरूप में लिखे जाते थे, किंतु संस्कृत के प्रभाव से दूर जो प्राकृत लिखे गये वे अधिक विकासशील थे।"२ हाल की गाथाओं, प्रवरसेन के सेतुबंध, वाक्पतिराज के गडउवहो, राजशेखर की कर्पूरमंजरी या अन्यान्य परवर्ती नाटकों की प्राकृतें बोलचाल की भाषा का संकेत नहीं करतीं, वे पंडितों की शिष्ट प्राकृतें ही हैं, इसमें हगिज संदेह नहीं ।
२५. अपभ्रंश की उकार-बहुला प्रवृत्ति ही नहीं, उसकी साहित्यिक छन्दःपरम्परा का भी सर्वप्रथम दर्शन कालिदास के 'विक्रमोर्वशीय' के चतुर्थ अंक के कतिपय पद्यों में होता है। भाषाशास्त्रीय इतिहास में उत्तर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा (Later Middle Indo-Aryen) की शुरूआत हमें कालिदास से ही माननी होगी, वैसे मोटे तौर पर यह युग ईसा की छठी सदी से माना जाता है। कालिदास के 'विक्रमोर्वशीय' के अपभ्रंश पद्य दरअसल बाद के प्रक्षेप न हो कर उसी काल के जान पड़ते हैं। परवर्ती प्राकृत काल की मध्यदेशीय विभाषाओं में अपभ्रंशगत विशिष्टताओं का कारण आभीरों और गुर्जरों का सौराष्ट्र, मालवा, राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तरप्रदेश में आ बसना माना जाता है । दण्डी ने काव्यादर्श में अपभ्रंश को इन्हीं की भाषा मानते कहा था :- "आभीरादिगिरः काव्येष्वपभ्रंश इति स्मृताः" । ईसवी दूसरी तथा तीसरी सदी में आभीरों ने सामंती समाज में भी महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया था। काठियावाड़ से प्राप्त १९१ ई० की राजाज्ञा में आभीर सेनापति रुद्रभूति का उल्लेख है। मृच्छकटिक के राजा पालक तथा गोपालदारक को कुछ विद्वानों ने आभीर ही माना है। वैसे मृच्छकटिक का रचनाकाल अनिश्चित-सा है; फिर भी ऐसा मालूम होता है कि मृच्छकटिक गुप्तोत्तर किंतु प्राक्हर्ष काल (छठी शती पूर्वार्द्ध) की रचना है। इस समय तक समस्त मध्यदेश में आभीरों का काफी प्रभुत्व हो चुका था। आभीरों की भाषा का न केवल गुजराती, राजस्थानी विभाषाओं पर ही प्रभाव पड़ा, अपितु पहाड़ी इलाके की विभाषायें और अधिक प्रभावित हुई। कहा जाता है कि ये आभीर जातियाँ ही, जिनमें पिछले दिनों शकों, गुर्जरों और हूणों का भी संमिश्रण हो गया था, मध्ययुग के शक्तिशाली राजपूतों के रूप में बदल गईं। "सातवीं शताब्दी के बाद जब इन सामन्तशाही रजवाड़ों का महत्त्व बढ़ा तब इनकी राजदरबार की भाषा, जो स्थानीय बोलचाल की भाषा से आभीर और गुर्जर बोलियों के मिश्रण से बनी थी, साहित्यिक भाषा में विकसित होने लगी ।" आगे चलकर मध्यदेशीय व्यापारी वर्ग ने भी इस साहित्यिक भाषा को विकसित तथा समृद्ध बनाने में प्रभूत योग दिया और अपभ्रंश एक तरह से जैन धर्म की धार्मिक भाषा बन बैठी ।
२६. 'अपभ्रंश' भाषा के विषय में प्रायः भाषावैज्ञानिकों में दो मत प्रचलित हैं। पहला मत याकोबी, अल्सदोर्फ, कीथ आदि विद्वानों का है, जो यह मानते हैं कि अपभ्रंश कभी भी देशभाषा या जनभाषा नहीं रही है। यह वस्तुतः वह कृत्रिम साहित्यिक भाषा थी, जिसमें प्राकृत की साहित्यिक शैली के साथ साथ प्रचलित कथ्य भाषा के सुप् प्रत्ययों, सर्वनाम शब्दों, अव्ययों आदि की छौंक डाली जाने लगी थी। कीथ के मतानुसार अपभ्रंश वस्तुतः प्राकृत के ही सरलीकरण का प्रयास है, जिसमें देश्य भाषा के व्याकरण के साथ-साथ प्राकृत की ही शब्दावली और कभी कभी प्राकृत विभक्तियों का भी प्रयोग मिलता है। यद्यपि वे यह भी संकेत करते हैं कि म० भा० आ० तथा न० भा० आ० के बीच की कड़ी १. शमशेरसिंह नरूला : हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं का वैज्ञानिक इतिहास पृ० ५७ २. डा० प्र० बे० पंडित : प्राकृत भाषा पृ० २४ ३. डा० भोलाशंकर व्यास : हि० सा० बृ. इति० पृ० ३२९ ४. दण्डी : काव्यादर्श १.३६ ५. Grierson : Pahari Languages. (Indian Antiquary 1914). ६. शमशेरसिंह नरूला : हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं का वैज्ञानिक इतिहास, पृ० ६० । ७. Keith : History of Sanskrit Literature. pp. 32 ff.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org