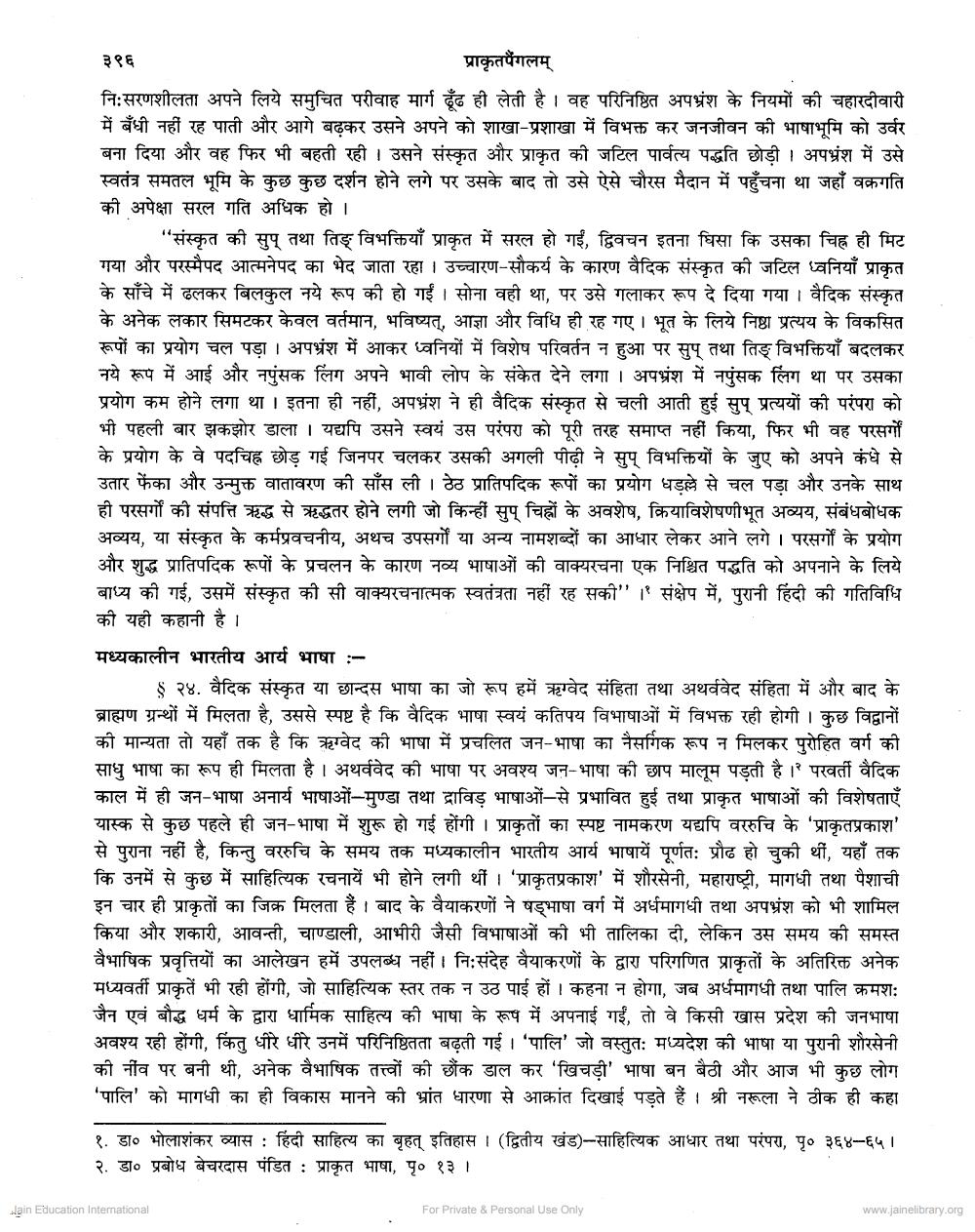________________
प्राकृतपैंगलम्
निःसरणशीलता अपने लिये समुचित परीवाह मार्ग ढूँढ ही लेती है । वह परिनिष्ठित अपभ्रंश के नियमों की चहारदीवारी में बँधी नहीं रह पाती और आगे बढ़कर उसने अपने को शाखा प्रशाखा में विभक्त कर जनजीवन की भाषाभूमि को उर्वर बना दिया और वह फिर भी बहती रही । उसने संस्कृत और प्राकृत की जटिल पार्वत्य पद्धति छोड़ी । अपभ्रंश में उसे स्वतंत्र समतल भूमि के कुछ कुछ दर्शन होने लगे पर उसके बाद तो उसे ऐसे चौरस मैदान में पहुँचना था जहाँ वक्रगति की अपेक्षा सरल गति अधिक हो ।
३९६
"संस्कृत की सुप् तथा तिङ् विभक्तियाँ प्राकृत में सरल हो गईं, द्विवचन इतना घिसा कि उसका चिह्न ही मिट गया और परस्मैपद आत्मनेपद का भेद जाता रहा । उच्चारण- सौकर्य के कारण वैदिक संस्कृत की जटिल ध्वनियाँ प्राकृत के साँचे में ढलकर बिलकुल नये रूप की हो गईं। सोना वही था, पर उसे गलाकर रूप दे दिया गया । वैदिक संस्कृत के अनेक लकार सिमटकर केवल वर्तमान, भविष्यत्, आज्ञा और विधि ही रह गए। भूत के लिये निष्ठा प्रत्यय के विकसित रूपों का प्रयोग चल पड़ा। अपभ्रंश में आकर ध्वनियों में विशेष परिवर्तन न हुआ पर सुप् तथा तिङ् विभक्तियाँ बदलकर नये रूप में आई और नपुंसक लिंग अपने भावी लोप के संकेत देने लगा । अपभ्रंश में नपुंसक लिंग था पर उसका प्रयोग कम होने लगा था। इतना ही नहीं, अपभ्रंश ने ही वैदिक संस्कृत से चली आती हुई सुप् प्रत्ययों की परंपरा को भी पहली बार झकझोर डाला । यद्यपि उसने स्वयं उस परंपरा को पूरी तरह समाप्त नहीं किया, फिर भी वह परसर्गों के प्रयोग के वे पदचिह्न छोड़ गई जिनपर चलकर उसकी अगली पीढ़ी ने सुप् विभक्तियों के जुए को अपने कंधे से उतार फेंका और उन्मुक्त वातावरण की साँस ली । ठेठ प्रातिपदिक रूपों का प्रयोग धड़ल्ले से चल पड़ा और उनके साथ ही परसर्गों की संपत्ति ऋद्ध से ऋद्धतर होने लगी जो किन्हीं सुप् चिह्नों के अवशेष, क्रियाविशेषणीभूत अव्यय, संबंधबोधक अव्यय, या संस्कृत के कर्मप्रवचनीय, अथच उपसर्गों या अन्य नामशब्दों का आधार लेकर आने लगे। परसर्गों के प्रयोग और शुद्ध प्रातिपदिक रूपों के प्रचलन के कारण नव्य भाषाओं की वाक्यरचना एक निश्चित पद्धति को अपनाने के लिये बाध्य की गई, उसमें संस्कृत की सी वाक्यरचनात्मक स्वतंत्रता नहीं रह सकी" ।" संक्षेप में, पुरानी हिंदी की गतिविधि की यही कहानी है ।
मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा :
२४. वैदिक संस्कृत या छान्दस भाषा का जो रूप हमें ऋग्वेद संहिता तथा अथर्ववेद संहिता में और बाद के ब्राह्मण ग्रन्थों में मिलता है, उससे स्पष्ट है कि वैदिक भाषा स्वयं कतिपय विभाषाओं में विभक्त रही होगी । कुछ विद्वानों की मान्यता तो यहाँ तक है कि ऋग्वेद की भाषा में प्रचलित जन- भाषा का नैसर्गिक रूप न मिलकर पुरोहित वर्ग की साधु भाषा का रूप ही मिलता है । अथर्ववेद की भाषा पर अवश्य जन - भाषा की छाप मालूम पड़ती है। परवर्ती वैदिक काल में ही जन-भाषा अनार्य भाषाओं- मुण्डा तथा द्राविड़ भाषाओं से प्रभावित हुई तथा प्राकृत भाषाओं की विशेषताएँ यास्क से कुछ पहले ही जन- भाषा में शुरू हो गई होंगी । प्राकृतों का स्पष्ट नामकरण यद्यपि वररुचि के 'प्राकृतप्रकाश' से पुराना नहीं है, किन्तु वररुचि के समय तक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषायें पूर्णतः प्रौढ हो चुकी थीं, यहाँ तक कि उनमें से कुछ में साहित्यिक रचनायें भी होने लगी थीं । 'प्राकृतप्रकाश' में शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी तथा पैशाची इन चार ही प्राकृतों का जिक्र मिलता हैं। बाद के वैयाकरणों ने षड्भाषा वर्ग में अर्धमागधी तथा अपभ्रंश को भी शामिल किया और शकारी, आवन्ती, चाण्डाली, आभीरी जैसी विभाषाओं की भी तालिका दी, लेकिन उस समय की समस्त वैभाषिक प्रवृत्तियों का आलेखन हमें उपलब्ध नहीं । निःसंदेह वैयाकरणों के द्वारा परिगणित प्राकृतों के अतिरिक्त अनेक मध्यवर्ती प्राकृतें भी रही होंगी, जो साहित्यिक स्तर तक न उठ पाई हों । कहना न होगा, जब अर्धमागधी तथा पालि क्रमशः जैन एवं बौद्ध धर्म के द्वारा धार्मिक साहित्य की भाषा के रूप में अपनाई गईं, तो वे किसी खास प्रदेश की जनभाषा अवश्य रही होंगी, किंतु धीरे धीरे उनमें परिनिष्ठितता बढ़ती गई। 'पालि' जो वस्तुतः मध्यदेश की भाषा या पुरानी शौरसेनी की नींव पर बनी थी, अनेक वैभाषिक तत्त्वों की छौंक डाल कर 'खिचड़ी' भाषा बन बैठी और आज भी कुछ लोग 'पालि' को मागधी का ही विकास मानने की भ्रांत धारणा से आक्रांत दिखाई पड़ते हैं। श्री नरूला ने ठीक ही कहा
१. डा० भोलाशंकर व्यास : हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास । (द्वितीय खंड ) - साहित्यिक आधार तथा परंपरा, पृ० ३६४-६५ । २. डा० प्रबोध बेचरदास पंडित: प्राकृत भाषा, पृ० १३ ।
Jain Education International
For Private Personal Use Only
www.jainelibrary.org