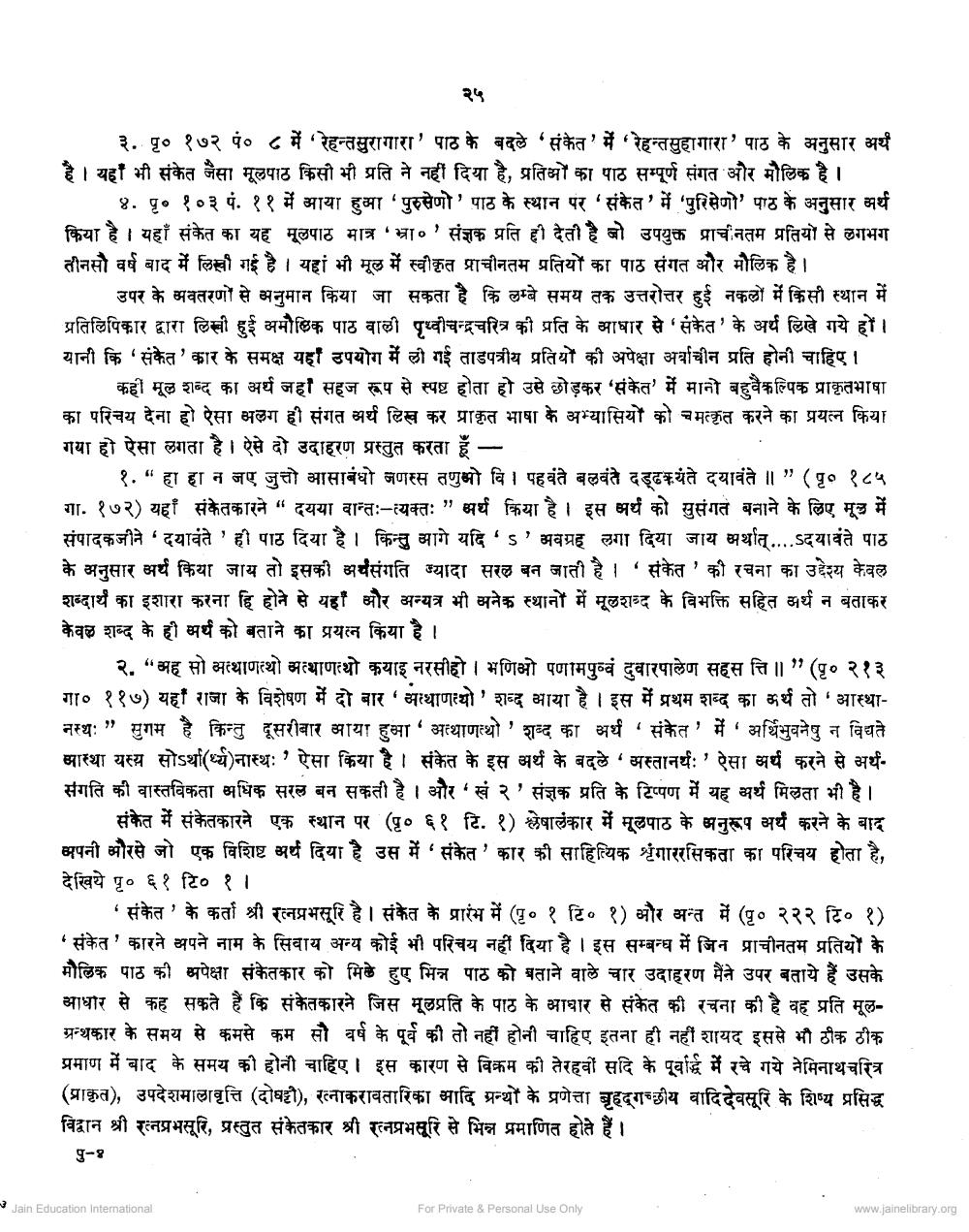________________
३. पृ० १७२ पं० ८ में 'रेहन्तसुरागारा' पाठ के बदले 'संकेत' में ' रेहन्तसुहागारा' पाठ के अनुसार अर्थ है । यहाँ भी संकेत जैसा मूलपाठ किसी भी प्रति ने नहीं दिया है, प्रतिओं का पाठ सम्पूर्ण संगत और मौलिक है ।
२५
४. पृ० १०३ पं. ११ में आया हुमा 'पुरुसेणो' पाठ के स्थान पर 'संकेत' में 'पुरिसेणो' पाठ के अनुसार अर्थ किया है । यहाँ संकेत का यह मूलपाठ मात्र 'भ्रा० ' संज्ञक प्रति ही देती है जो उपयुक्त प्राचीनतम प्रतियों से लगभग
वर्ष बाद में लिखी गई है। यहां भी मूल में स्वीकृत प्राचीनतम प्रतियों का पाठ संगत और मौलिक है ।
उपर के अवतरणों से अनुमान किया जा सकता है कि लम्बे समय तक उत्तरोत्तर हुई नकलों में किसी स्थान में प्रतिलिपिकार द्वारा लिखी हुई अमौलिक पाठ वाली पृथ्वीचन्द्रचरित्र की प्रति के आधार से 'संकेत' के अर्थ लिखे गये हों । यानी कि 'संकेत ' कार के समक्ष यहाँ उपयोग में ली गई ताडपत्रीय प्रतियों की अपेक्षा अर्वाचीन प्रति होनी चाहिए |
कहीं मूल शब्द का अर्थ जहाँ सहज रूप से स्पष्ट होता हो उसे छोड़कर 'संकेत' में मानो बहुवैकल्पिक प्राकृतभाषा का परिचय देना हो ऐसा अलग ही संगत अर्थ लिख कर प्राकृत भाषा के अभ्यासियों को चमत्कृत करने का प्रयत्न किया गया हो ऐसा लगता है। ऐसे दो उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ -
-
१. " हा हा न नए जुत्तो आसाबंधो जणस्स तणुओ वि । पहवंते बलवंते दड्ढकयंते दयावंते ॥ " ( पृ० १८५ गा. १७२) यहाँ संकेतकारने " दयया वान्तः - व्यक्तः " अर्थ किया है । इस अर्थ को सुसंगत बनाने के लिए मूल में संपादकजीने 'दयावंते ' ही पाठ दिया है। किन्तु आगे यदि ' ' अवग्रह लगा दिया जाय अर्थात् .... दयावंते पाठ के अनुसार अर्थ किया जाय तो इसकी अर्थसंगति ज्यादा सरल बन जाती है । ' संकेत ' की रचना का उद्देश्य केवल शब्दार्थं का इशारा करना हि होने से यहाँ और अन्यत्र भी अनेक स्थानों में मूलशब्द के विभक्ति सहित अर्थ न बताकर केवल शब्द के ही अर्थ को बताने का प्रयत्न किया है ।
२. " अह सो अस्थाणत्थो अत्थाणत्थो कयाइ नरसीहो । भणिओ पणामपुव्वं दुवारपालेण सहस त्ति ॥ " ( पृ० २१३ गा० ११७) यहाँ राजा के विशेषण में दो बार 'अस्थाणत्थो' शब्द आया है । इस में प्रथम शब्द का अर्थ तो ' आस्थानस्थ: सुगम है किन्तु दूसरी बार आया हुआ ' अत्थाणत्थो' शब्द का अर्थ ' संकेत' में ' अर्थिभुवनेषु न विद्यते यस्य सोऽर्था (र्ध्य) नास्थः ' ऐसा किया है । संकेत के इस अर्थ के बदले ' अस्तानर्थः ' ऐसा अर्थ करने से अर्थसंगति की वास्तविकता अधिक सरल बन सकती है । और ' खं २' संज्ञक प्रति के टिप्पण में यह अर्थ मिलता भी है। संकेत में संकेतकारने एक स्थान पर ( पृ० ६१ टि. १) श्लेषालंकार में मूलपाठ के अनुरूप अर्थ करने के बाद अपनी और से जो एक विशिष्ट अर्थ दिया है उस में ' संकेत ' कार की साहित्यिक शृंगाररसिकता का परिचय होता है, देखिये पृ० ६१ टि० १ ।
' संकेत ' के कर्ता श्री रत्नप्रभसूरि है। संकेत के प्रारंभ में ( पृ० १ टि० १) और अन्त में ( पृ० २२२ दि० १) ' संकेत ' कारने अपने नाम के सिवाय अन्य कोई भी परिचय नहीं दिया है। इस सम्बन्ध में जिन प्राचीनतम प्रतियों के मौलिक पाठ की अपेक्षा संकेतकार को मिले हुए भिन्न पाठ को बताने वाले चार उदाहरण मैंने उपर बताये हैं उसके आधार से कह सकते हैं कि संकेतकारने जिस मूलप्रति के पाठ के आधार से संकेत की रचना की है वह प्रति मूलग्रन्थकार के समय से कमसे कम सौ वर्ष के पूर्व की तो नहीं होनी चाहिए इतना ही नहीं शायद इससे भी ठीक ठीक प्रमाण में बाद के समय की होनी चाहिए। इस कारण से विक्रम की तेरहवीं सदि के पूर्वार्द्ध में रचे गये नेमिनाथचरित्र ( प्राकृत), उपदेशमालावृत्ति (दोषट्टी), रत्नाकरावतारिका आदि ग्रन्थों के प्रणेत्ता बृहद्गच्छीय वादिदेवसूरि के शिष्य प्रसिद्ध विद्वान श्री रत्नप्रभसूरि, प्रस्तुत संकेतकार श्री रत्नप्रभसूरि से भिन्न प्रमाणित होते हैं ।
g-8
"
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org