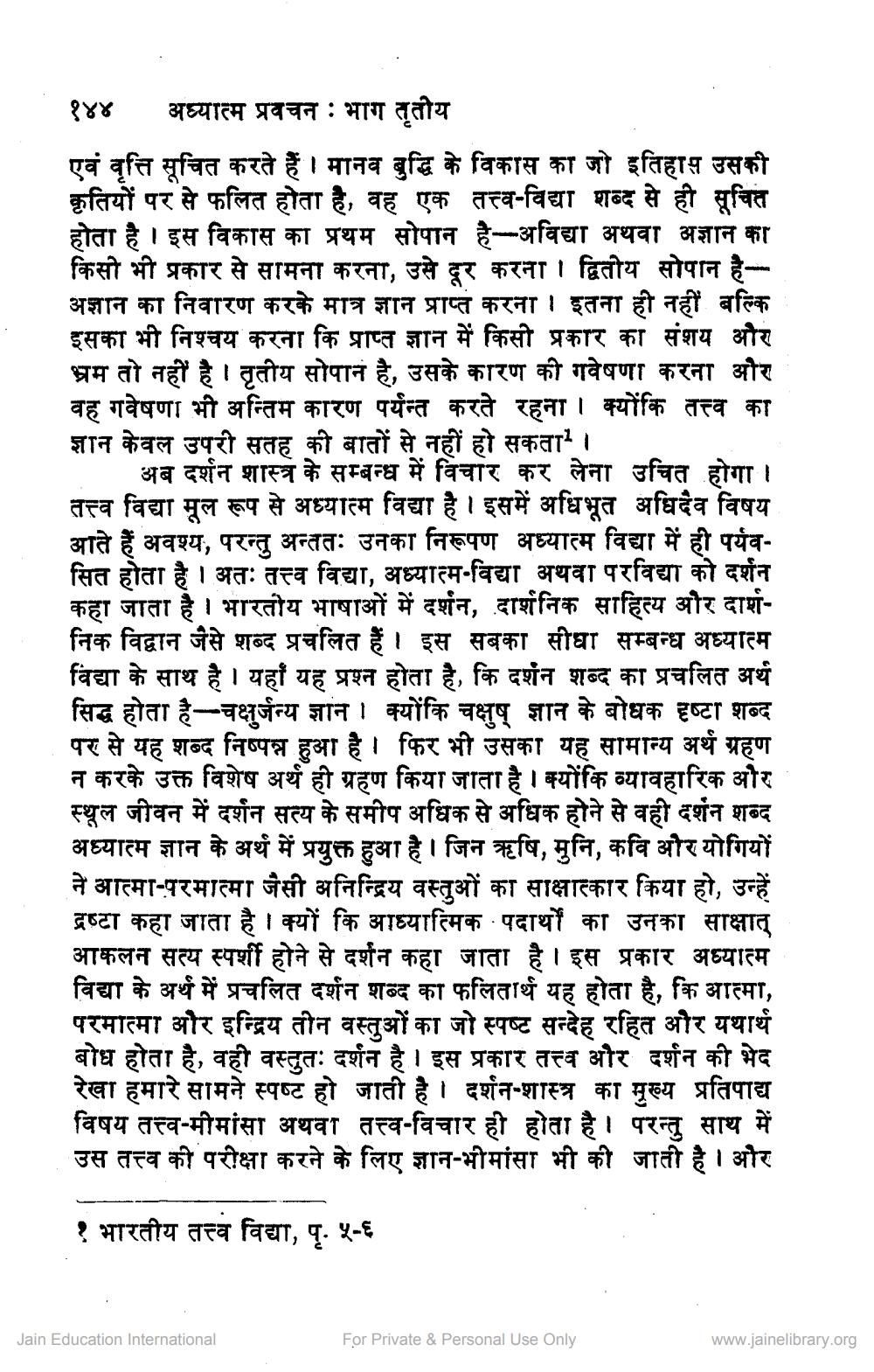________________
१४४ अध्यात्म प्रवचन : भाग तृतीय एवं वत्ति सूचित करते हैं। मानव बुद्धि के विकास का जो इतिहास उसकी कृतियों पर से फलित होता है, वह एक तत्त्व-विद्या शब्द से ही सूचित होता है । इस विकास का प्रथम सोपान है-अविद्या अथवा अज्ञान का किसी भी प्रकार से सामना करना, उसे दूर करना । द्वितीय सोपान हैअज्ञान का निवारण करके मात्र ज्ञान प्राप्त करना । इतना ही नहीं बल्कि इसका भी निश्चय करना कि प्राप्त ज्ञान में किसी प्रकार का संशय और भ्रम तो नहीं है । तृतीय सोपान है, उसके कारण की गवेषणा करना और वह गवेषणा भी अन्तिम कारण पर्यन्त करते रहना । क्योंकि तत्त्व का ज्ञान केवल उपरी सतह की बातों से नहीं हो सकता।
अब दर्शन शास्त्र के सम्बन्ध में विचार कर लेना उचित होगा। तत्त्व विद्या मूल रूप से अध्यात्म विद्या है । इसमें अधिभूत अधिदैव विषय आते हैं अवश्य, परन्तु अन्ततः उनका निरूपण अध्यात्म विद्या में ही पर्यवसित होता है । अतः तत्त्व विद्या, अध्यात्म-विद्या अथवा परविद्या को दर्शन कहा जाता है। भारतीय भाषाओं में दर्शन, दार्शनिक साहित्य और दार्शनिक विद्वान जैसे शब्द प्रचलित हैं। इस सबका सीधा सम्बन्ध अध्यात्म विद्या के साथ है। यहाँ यह प्रश्न होता है, कि दर्शन शब्द का प्रचलित अर्थ सिद्ध होता है-चक्षुर्जन्य ज्ञान । क्योंकि चक्षुष् ज्ञान के बोधक दृष्टा शब्द पर से यह शब्द निष्पन्न हुआ है। फिर भी उसका यह सामान्य अर्थ ग्रहण न करके उक्त विशेष अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। क्योंकि व्यावहारिक और स्थूल जीवन में दर्शन सत्य के समीप अधिक से अधिक होने से वही दर्शन शब्द अध्यात्म ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जिन ऋषि, मुनि, कवि और योगियों ने आत्मा-परमात्मा जैसी अनिन्द्रिय वस्तुओं का साक्षात्कार किया हो, उन्हें द्रष्टा कहा जाता है । क्यों कि आध्यात्मिक पदार्थों का उनका साक्षात् आकलन सत्य स्पर्शी होने से दर्शन कहा जाता है। इस प्रकार अध्यात्म विद्या के अर्थ में प्रचलित दर्शन शब्द का फलितार्थ यह होता है, कि आत्मा, परमात्मा और इन्द्रिय तीन वस्तुओं का जो स्पष्ट सन्देह रहित और यथार्थ बोध होता है, वही वस्तुतः दर्शन है। इस प्रकार तत्त्व और दर्शन की भेद रेखा हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है। दर्शन-शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय तत्त्व-मीमांसा अथवा तत्त्व-विचार ही होता है। परन्तु साथ में उस तत्त्व की परीक्षा करने के लिए ज्ञान-भीमांसा भी की जाती है । और
१ भारतीय तत्त्व विद्या, पृ. ५-६
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org