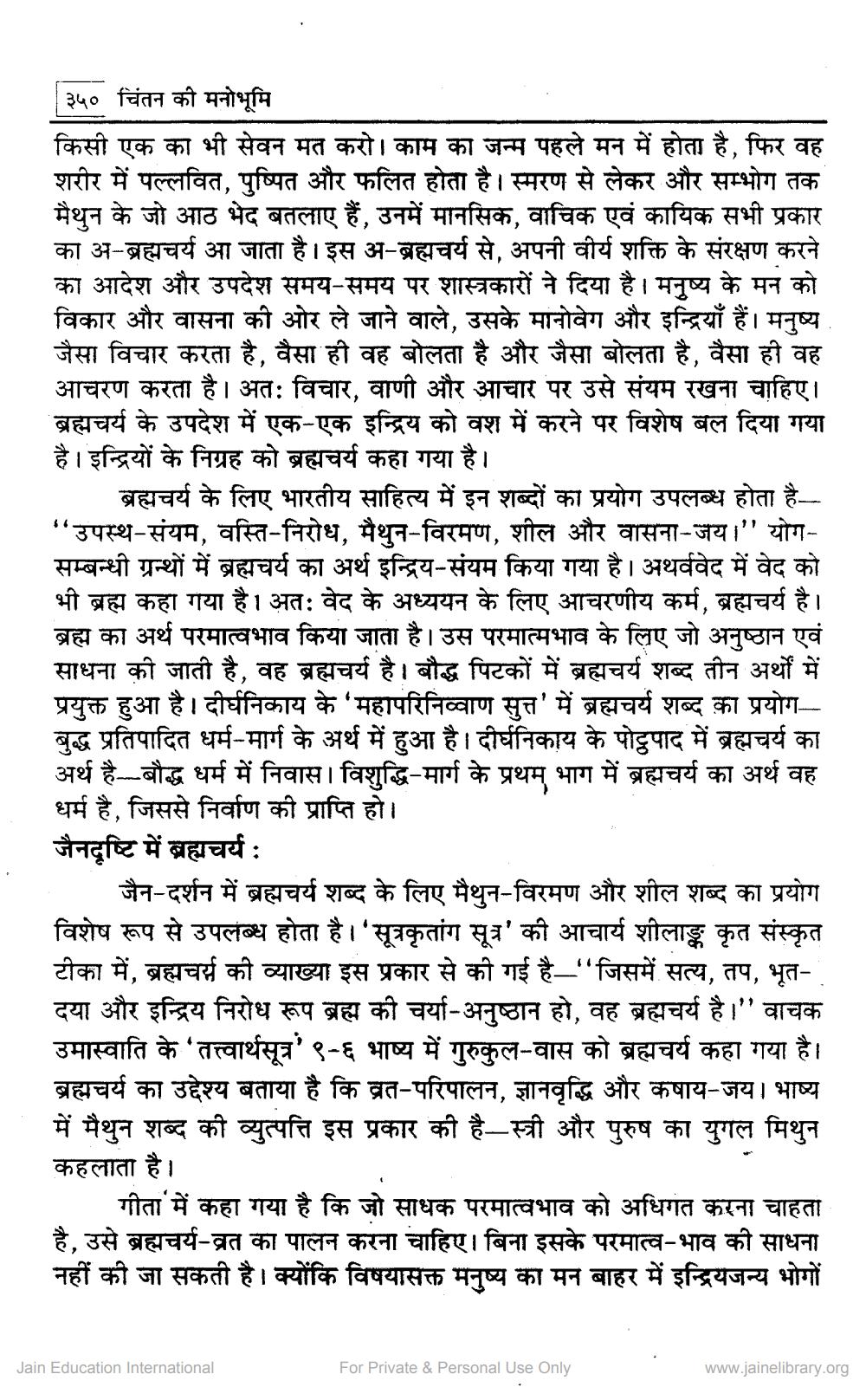________________
३५० चिंतन की मनोभूमि किसी एक का भी सेवन मत करो। काम का जन्म पहले मन में होता है, फिर वह शरीर में पल्लवित, पुष्पित और फलित होता है। स्मरण से लेकर और सम्भोग तक मैथन के जो आठ भेद बतलाए हैं, उनमें मानसिक, वाचिक एवं कायिक सभी प्रकार का अ-ब्रह्मचर्य आ जाता है। इस अ-ब्रह्मचर्य से, अपनी वीर्य शक्ति के संरक्षण करने का आदेश और उपदेश समय-समय पर शास्त्रकारों ने दिया है। मनुष्य के मन को विकार और वासना की ओर ले जाने वाले, उसके मानोवेग और इन्द्रियाँ हैं। मनुष्य जैसा विचार करता है, वैसा ही वह बोलता है और जैसा बोलता है, वैसा ही वह आचरण करता है। अत: विचार, वाणी और आचार पर उसे संयम रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य के उपदेश में एक-एक इन्द्रिय को वश में करने पर विशेष बल दिया गया है। इन्द्रियों के निग्रह को ब्रह्मचर्य कहा गया है।
ब्रह्मचर्य के लिए भारतीय साहित्य में इन शब्दों का प्रयोग उपलब्ध होता है"उपस्थ-संयम, वस्ति-निरोध, मैथुन-विरमण, शील और वासना-जय।" योगसम्बन्धी ग्रन्थों में ब्रह्मचर्य का अर्थ इन्द्रिय-संयम किया गया है। अथर्ववेद में वेद को भी ब्रह्म कहा गया है। अतः वेद के अध्ययन के लिए आचरणीय कर्म, ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म का अर्थ परमात्वभाव किया जाता है। उस परमात्मभाव के लिए जो अनुष्ठान एवं साधना की जाती है, वह ब्रह्मचर्य है। बौद्ध पिटकों में ब्रह्मचर्य शब्द तीन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। दीर्घनिकाय के 'महापरिनिव्वाण सुत्त' में ब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोगबुद्ध प्रतिपादित धर्म-मार्ग के अर्थ में हुआ है। दीर्घनिकाय के पोट्टपाद में ब्रह्मचर्य का अर्थ है-बौद्ध धर्म में निवास। विशुद्धि-मार्ग के प्रथम भाग में ब्रह्मचर्य का अर्थ वह धर्म है, जिससे निर्वाण की प्राप्ति हो।
जैनदृष्टि में ब्रह्मचर्य : - जैन-दर्शन में ब्रह्मचर्य शब्द के लिए मैथुन-विरमण और शील शब्द का प्रयोग विशेष रूप से उपलब्ध होता है। सूत्रकृतांग सूत्र' की आचार्य शीलाङ्क कृत संस्कृत टीका में, ब्रह्मचर्य की व्याख्या इस प्रकार से की गई है—“जिसमें सत्य, तप, भूतदया और इन्द्रिय निरोध रूप ब्रह्म की चर्या-अनुष्ठान हो, वह ब्रह्मचर्य है।" वाचक उमास्वाति के 'तत्त्वार्थसूत्र' ९-६ भाष्य में गुरुकुल-वास को ब्रह्मचर्य कहा गया है। ब्रह्मचर्य का उद्देश्य बताया है कि व्रत-परिपालन, ज्ञानवृद्धि और कषाय-जय। भाष्य में मैथुन शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है-स्त्री और पुरुष का युगल मिथुन कहलाता है।
गीता में कहा गया है कि जो साधक परमात्वभाव को अधिगत करना चाहता है, उसे ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन करना चाहिए। बिना इसके परमात्व-भाव की साधना नहीं की जा सकती है। क्योंकि विषयासक्त मनुष्य का मन बाहर में इन्द्रियजन्य भोगों
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org