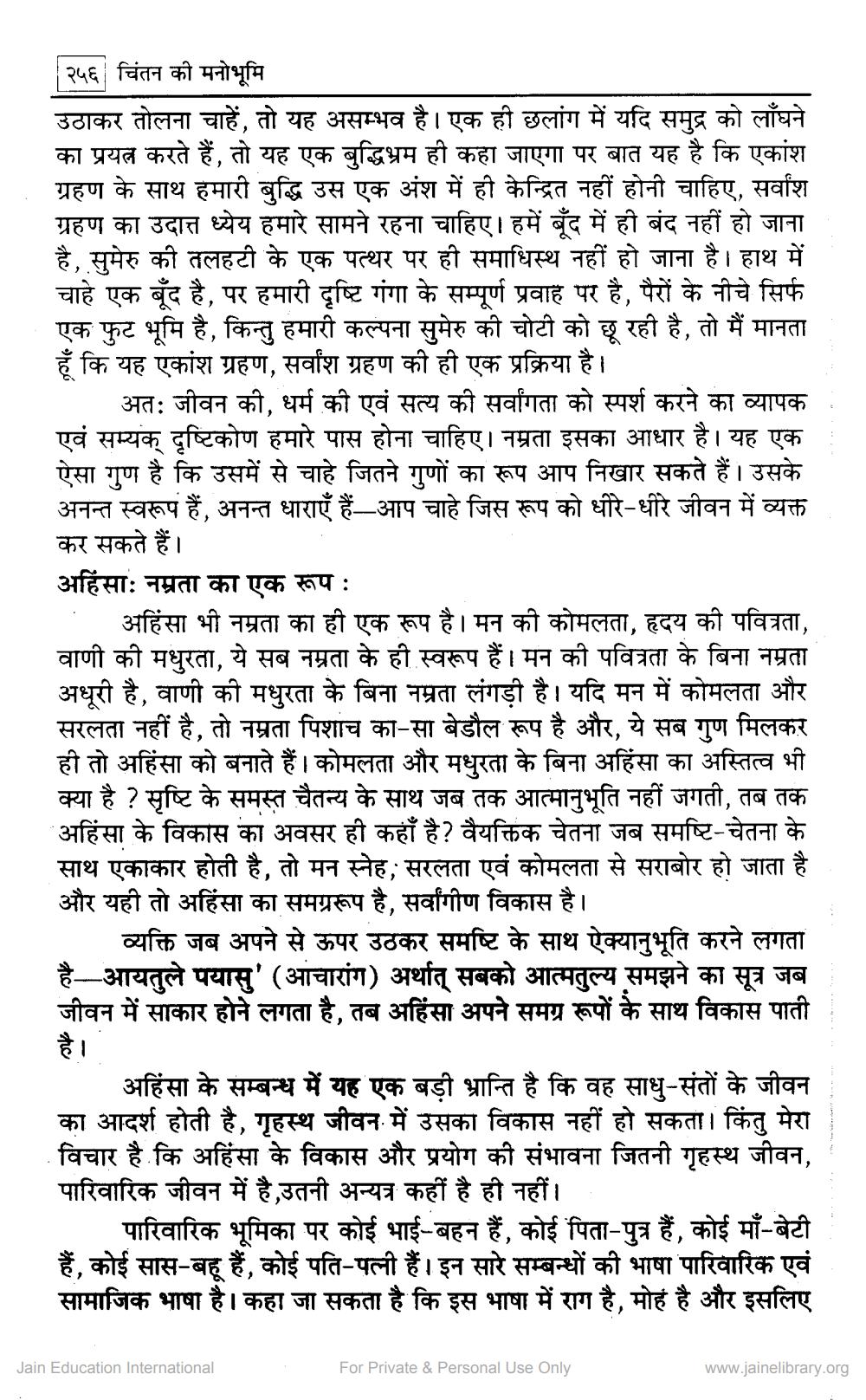________________
२५६ | चिंतन की मनोभूमि
उठाकर तोलना चाहें, तो यह असम्भव है। एक ही छलांग में यदि समुद्र को लाँघने का प्रयत्न करते हैं, तो यह एक बुद्धिभ्रम ही कहा जाएगा पर बात यह है कि एकांश ग्रहण के साथ हमारी बुद्धि उस एक अंश में ही केन्द्रित नहीं होनी चाहिए, सर्वांश ग्रहण का उदात्त ध्येय हमारे सामने रहना चाहिए। हमें बूँद में ही बंद नहीं हो जाना है, सुमेरु की तलहटी के एक पत्थर पर ही समाधिस्थ नहीं हो जाना है। हाथ में चाहे एक बूँद है, पर हमारी दृष्टि गंगा के सम्पूर्ण प्रवाह पर है, पैरों के नीचे सिर्फ एक फुट भूमि है, किन्तु हमारी कल्पना सुमेरु की चोटी को छू रही है, तो मैं मानता हूँ कि यह एकांश ग्रहण, सर्वांश ग्रहण की ही एक प्रक्रिया है ।
अतः जीवन की, धर्म की एवं सत्य की सर्वांगता को स्पर्श करने का व्यापक एवं सम्यक् दृष्टिकोण हमारे पास होना चाहिए। नम्रता इसका आधार है । यह एक ऐसा गुण है कि उसमें से चाहे जितने गुणों का रूप आप निखार सकते हैं। उसके अनन्त स्वरूप हैं, अनन्त धाराएँ हैं—आप चाहे जिस रूप को धीरे-धीरे जीवन में व्यक्त कर सकते हैं।
अहिंसाः नम्रता का एक रूप :
अहिंसा भी नम्रता का ही एक रूप है। मन की कोमलता, हृदय की पवित्रता, वाणी की मधुरता, ये सब नम्रता के ही स्वरूप हैं। मन की पवित्रता के बिना नम्रता अधूरी है, वाणी की मधुरता के बिना नम्रता लंगड़ी है। यदि मन में कोमलता और सरलता नहीं है, तो नम्रता पिशाच का - सा बेडौल रूप है और ये सब गुण मिलकर ही तो अहिंसा को बनाते हैं। कोमलता और मधुरता के बिना अहिंसा का अस्तित्व भी क्या है ? सृष्टि के समस्त चैतन्य के साथ जब तक आत्मानुभूति नहीं जगती, तब तक अहिंसा के विकास का अवसर ही कहाँ है? वैयक्तिक चेतना जब समष्टि-चेतना के साथ एकाकार होती है, तो मन स्नेह, सरलता एवं कोमलता से सराबोर हो जाता है और यही तो अहिंसा का समग्ररूप है, सर्वांगीण विकास है ।
व्यक्ति जब अपने से ऊपर उठकर समष्टि के साथ ऐक्यानुभूति करने लगता है – आयतुले पयासु' (आचारांग ) अर्थात् सबको आत्मतुल्य समझने का सूत्र जब जीवन में साकार होने लगता है, तब अहिंसा अपने समग्र रूपों के साथ विकास पाती
है ।
अहिंसा के सम्बन्ध में यह एक बड़ी भ्रान्ति है कि वह साधु-संतों के जीवन का आदर्श होती है, गृहस्थ जीवन में उसका विकास नहीं हो सकता। किंतु मेरा विचार है कि अहिंसा के विकास और प्रयोग की संभावना जितनी गृहस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन में है, उतनी अन्यत्र कहीं है ही नहीं ।
पारिवारिक भूमिका पर कोई भाई-बहन हैं, कोई पिता-पुत्र हैं, कोई माँ-बेटी हैं, कोई सास-बहू हैं, कोई पति-पत्नी हैं। इन सारे सम्बन्धों की भाषा पारिवारिक एवं सामाजिक भाषा है। कहा जा सकता है कि इस भाषा में राग है, मोहं है और इसलिए
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org