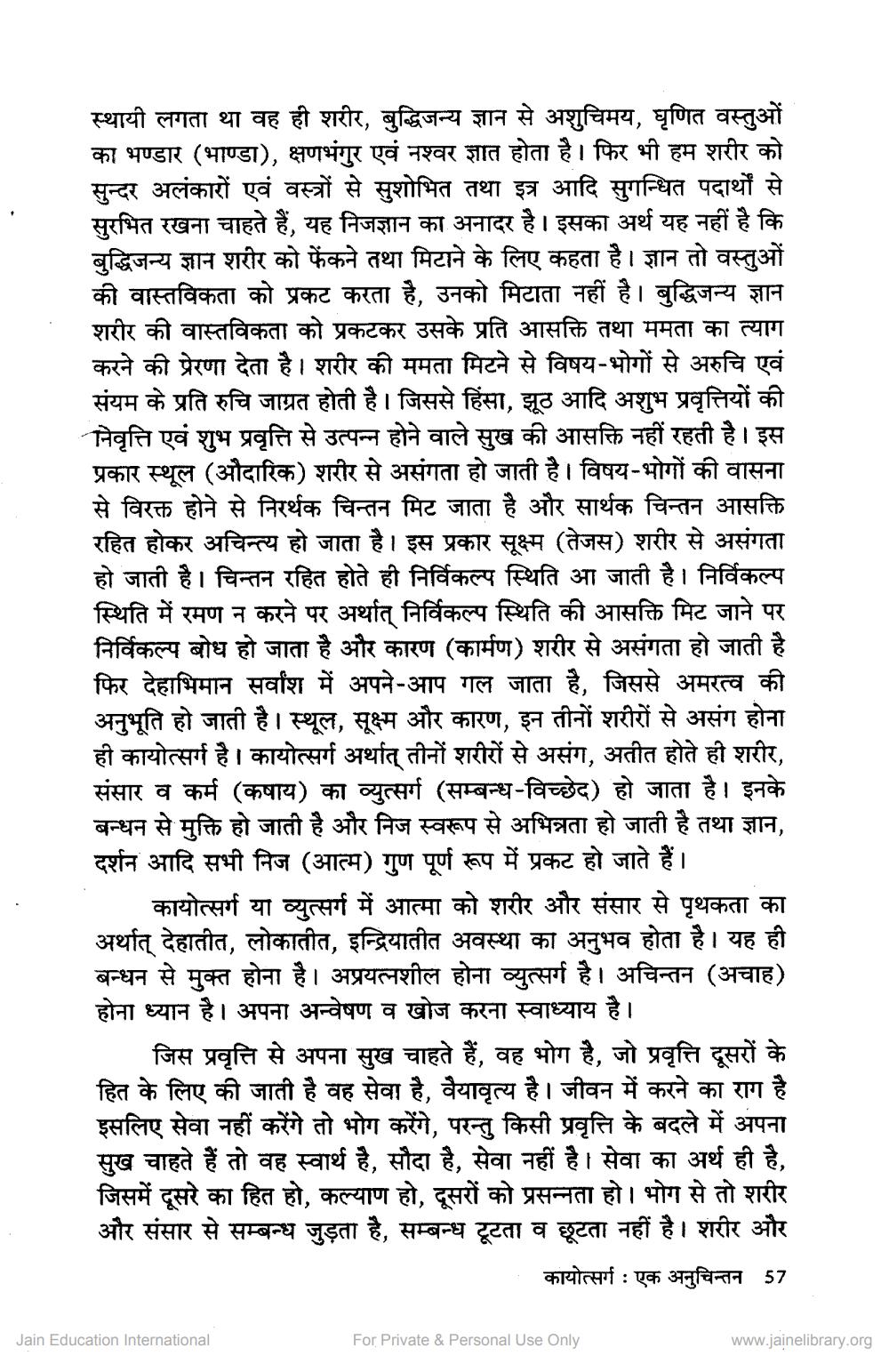________________
स्थायी लगता था वह ही शरीर, बुद्धिजन्य ज्ञान से अशुचिमय, घृणित वस्तुओं का भण्डार (भाण्डा), क्षणभंगुर एवं नश्वर ज्ञात होता है। फिर भी हम शरीर को सुन्दर अलंकारों एवं वस्त्रों से सुशोभित तथा इत्र आदि सुगन्धित पदार्थों से सुरभित रखना चाहते हैं, यह निजज्ञान का अनादर है। इसका अर्थ यह नहीं है कि बुद्धिजन्य ज्ञान शरीर को फेंकने तथा मिटाने के लिए कहता है। ज्ञान तो वस्तुओं की वास्तविकता को प्रकट करता है, उनको मिटाता नहीं है। बुद्धिजन्य ज्ञान शरीर की वास्तविकता को प्रकटकर उसके प्रति आसक्ति तथा ममता का त्याग करने की प्रेरणा देता है। शरीर की ममता मिटने से विषय-भोगों से अरुचि एवं संयम के प्रति रुचि जाग्रत होती है। जिससे हिंसा, झूठ आदि अशुभ प्रवृत्तियों की निवृत्ति एवं शुभ प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाले सुख की आसक्ति नहीं रहती है। इस प्रकार स्थूल (औदारिक) शरीर से असंगता हो जाती है। विषय-भोगों की वासना से विरक्त होने से निरर्थक चिन्तन मिट जाता है और सार्थक चिन्तन आसक्ति रहित होकर अचिन्त्य हो जाता है। इस प्रकार सूक्ष्म (तेजस) शरीर से असंगता हो जाती है। चिन्तन रहित होते ही निर्विकल्प स्थिति आ जाती है। निर्विकल्प स्थिति में रमण न करने पर अर्थात् निर्विकल्प स्थिति की आसक्ति मिट जाने पर निर्विकल्प बोध हो जाता है और कारण (कार्मण) शरीर से असंगता हो जाती है फिर देहाभिमान सर्वांश में अपने-आप गल जाता है, जिससे अमरत्व की अनुभूति हो जाती है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों से असंग होना ही कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग अर्थात् तीनों शरीरों से असंग, अतीत होते ही शरीर, संसार व कर्म (कषाय) का व्युत्सर्ग (सम्बन्ध-विच्छेद) हो जाता है। इनके बन्धन से मुक्ति हो जाती है और निज स्वरूप से अभिन्नता हो जाती है तथा ज्ञान, दर्शन आदि सभी निज (आत्म) गुण पूर्ण रूप में प्रकट हो जाते हैं।
कायोत्सर्ग या व्युत्सर्ग में आत्मा को शरीर और संसार से पृथकता का अर्थात् देहातीत, लोकातीत, इन्द्रियातीत अवस्था का अनुभव होता है। यह ही बन्धन से मुक्त होना है। अप्रयत्नशील होना व्युत्सर्ग है। अचिन्तन (अचाह) होना ध्यान है। अपना अन्वेषण व खोज करना स्वाध्याय है।
जिस प्रवृत्ति से अपना सुख चाहते हैं, वह भोग है, जो प्रवृत्ति दूसरों के हित के लिए की जाती है वह सेवा है, वैयावृत्य है। जीवन में करने का राग है इसलिए सेवा नहीं करेंगे तो भोग करेंगे, परन्तु किसी प्रवृत्ति के बदले में अपना सुख चाहते हैं तो वह स्वार्थ है, सौदा है, सेवा नहीं है। सेवा का अर्थ ही है, जिसमें दूसरे का हित हो, कल्याण हो, दूसरों को प्रसन्नता हो। भोग से तो शरीर और संसार से सम्बन्ध जुड़ता है, सम्बन्ध टूटता व छूटता नहीं है। शरीर और
कायोत्सर्ग : एक अनुचिन्तन 57
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org