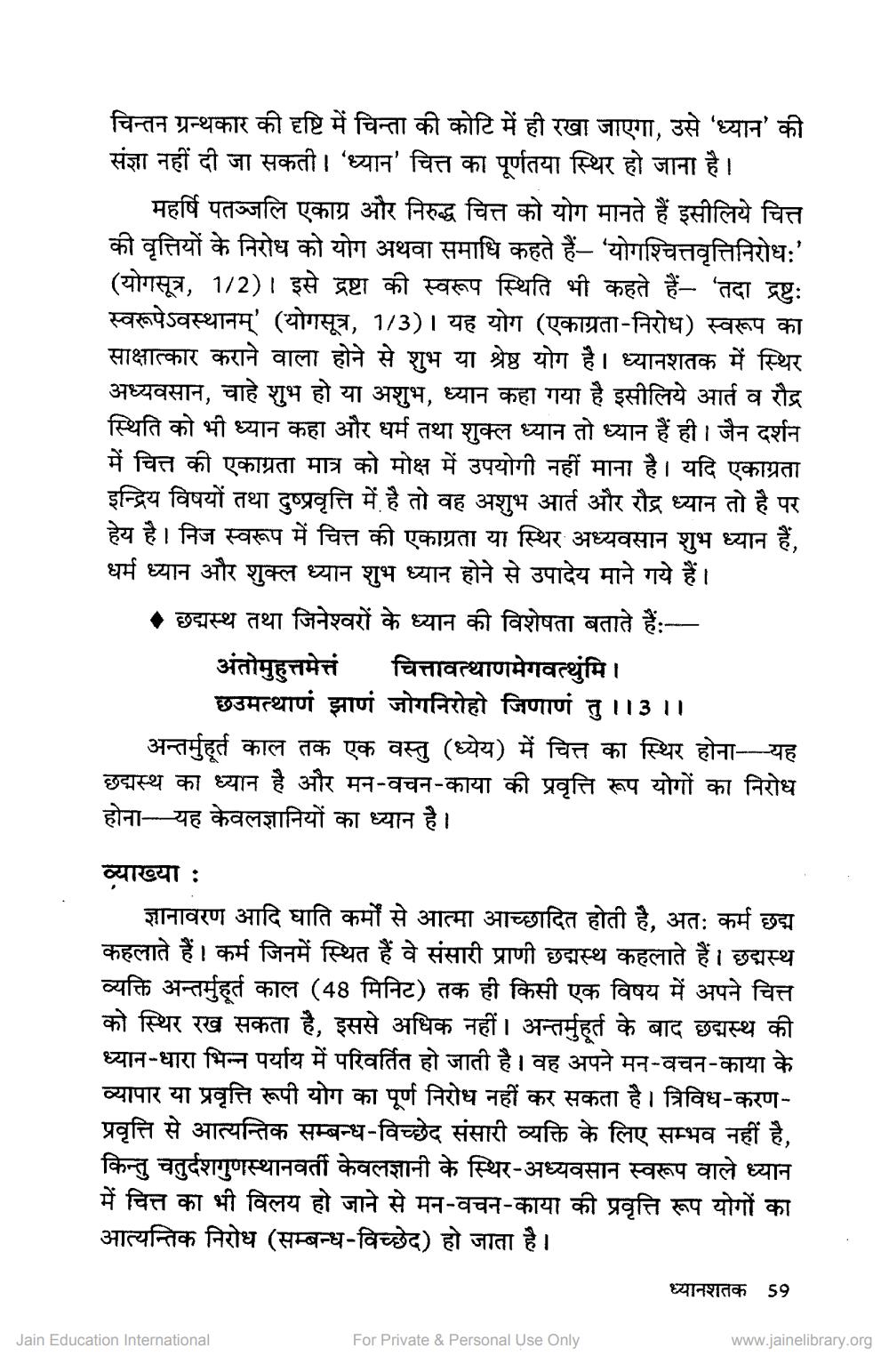________________
चिन्तन ग्रन्थकार की दृष्टि में चिन्ता की कोटि में ही रखा जाएगा, उसे 'ध्यान' की संज्ञा नहीं दी जा सकती। 'ध्यान' चित्त का पूर्णतया स्थिर हो जाना है। __ महर्षि पतञ्जलि एकाग्र और निरुद्ध चित्त को योग मानते हैं इसीलिये चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग अथवा समाधि कहते हैं- 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' (योगसूत्र, 1/2)। इसे द्रष्टा की स्वरूप स्थिति भी कहते हैं- 'तदा द्रष्टः स्वरूपेऽवस्थानम्' (योगसूत्र, 1/3)। यह योग (एकाग्रता-निरोध) स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाला होने से शुभ या श्रेष्ठ योग है। ध्यानशतक में स्थिर अध्यवसान, चाहे शुभ हो या अशुभ, ध्यान कहा गया है इसीलिये आर्त व रौद्र स्थिति को भी ध्यान कहा और धर्म तथा शुक्ल ध्यान तो ध्यान हैं ही। जैन दर्शन में चित्त की एकाग्रता मात्र को मोक्ष में उपयोगी नहीं माना है। यदि एकाग्रता इन्द्रिय विषयों तथा दुष्प्रवृत्ति में है तो वह अशुभ आर्त और रौद्र ध्यान तो है पर हेय है। निज स्वरूप में चित्त की एकाग्रता या स्थिर अध्यवसान शुभ ध्यान हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान शुभ ध्यान होने से उपादेय माने गये हैं। • छद्मस्थ तथा जिनेश्वरों के ध्यान की विशेषता बताते हैं:
अंतोमुहुत्तमेत्तं चित्तावत्थाणमेगवत्थुमि।
छउमत्थाणं झाणं जोगनिरोहो जिणाणं तु ।। 3 ।। अन्तर्मुहूर्त काल तक एक वस्तु (ध्येय) में चित्त का स्थिर होना-यह छद्मस्थ का ध्यान है और मन-वचन-काया की प्रवृत्ति रूप योगों का निरोध होना—यह केवलज्ञानियों का ध्यान है।
व्याख्या :
ज्ञानावरण आदि घाति कर्मों से आत्मा आच्छादित होती है, अतः कर्म छद्म कहलाते हैं। कर्म जिनमें स्थित हैं वे संसारी प्राणी छद्मस्थ कहलाते हैं। छद्मस्थ व्यक्ति अन्तर्मुहुर्त काल (48 मिनिट) तक ही किसी एक विषय में अपने चित्त को स्थिर रख सकता है, इससे अधिक नहीं। अन्तर्मुहूर्त के बाद छद्मस्थ की ध्यान-धारा भिन्न पर्याय में परिवर्तित हो जाती है। वह अपने मन-वचन-काया के व्यापार या प्रवृत्ति रूपी योग का पूर्ण निरोध नहीं कर सकता है। त्रिविध-करणप्रवृत्ति से आत्यन्तिक सम्बन्ध-विच्छेद संसारी व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं है, किन्तु चतुर्दशगुणस्थानवर्ती केवलज्ञानी के स्थिर-अध्यवसान स्वरूप वाले ध्यान में चित्त का भी विलय हो जाने से मन-वचन-काया की प्रवृत्ति रूप योगों का आत्यन्तिक निरोध (सम्बन्ध-विच्छेद) हो जाता है।
ध्यानशतक 59
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org