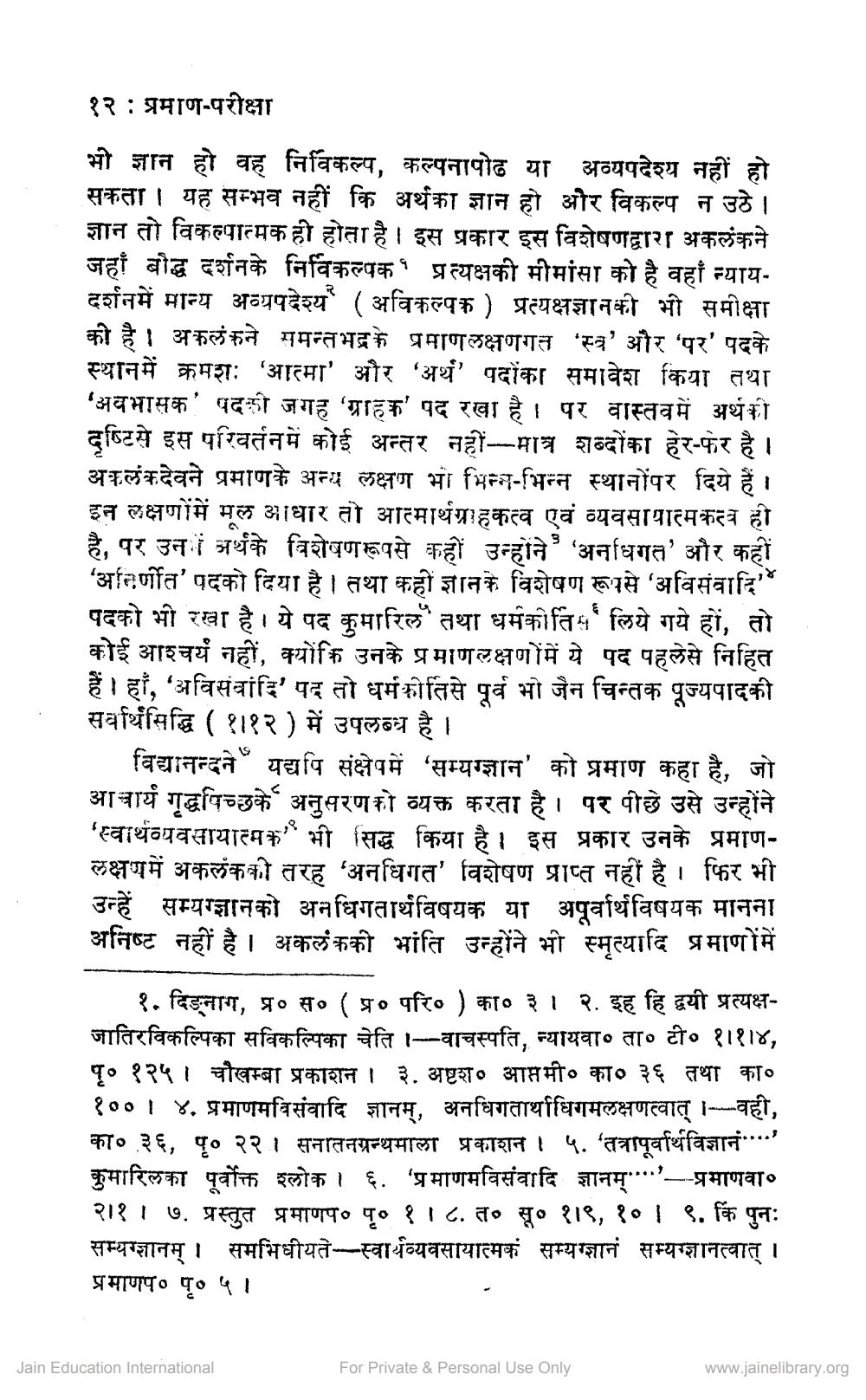________________
१२ : प्रमाण-परीक्षा भी ज्ञान हो वह निर्विकल्प, कल्पनापोढ या अव्यपदेश्य नहीं हो सकता। यह सम्भव नहीं कि अर्थका ज्ञान हो और विकल्प न उठे। ज्ञान तो विकल्पात्मक ही होता है। इस प्रकार इस विशेषणद्वारा अकलंकने जहाँ बौद्ध दर्शनके निर्विकल्पक' प्रत्यक्षकी मीमांसा को है वहाँ न्यायदर्शनमें मान्य अव्यपदेश्य' ( अविकल्पक ) प्रत्यक्षज्ञानकी भी समीक्षा की है। अकलंकने समन्तभद्र के प्रमाणलक्षणगत 'स्व' और 'पर' पदके स्थान में क्रमशः 'आत्मा' और 'अर्थ' पदोंका समावेश किया तथा 'अवभासक' पदकी जगह 'ग्राहक' पद रखा है। पर वास्तव में अर्थकी दृष्टिसे इस परिवर्तनमें कोई अन्तर नहीं-मात्र शब्दोंका हेर-फेर है । अकलंकदेवने प्रमाणके अन्य लक्षण भो भिन्न-भिन्न स्थानोंपर दिये हैं। इन लक्षणों में मल आधार तो आत्मार्थग्राहकत्व एवं व्यवसायात्मकत्व ही है, पर उन । अर्थके विशेषणरूपसे कहीं उन्होंने 'अनधिगत' और कहीं 'अनिर्णीत' पदको दिया है । तथा कहीं ज्ञान के विशेषण रूपसे 'अविसंवादि पदको भी रखा है। ये पद कुमारिल तथा धर्मकीति लिये गये हों, तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि उनके प्रमाणलक्षणोंमें ये पद पहलेसे निहित हैं। हाँ, 'अविसंवांदि' पद तो धर्मकोतिसे पूर्व भी जैन चिन्तक पूज्यपादकी सर्वार्थसिद्धि ( १११२ ) में उपलब्ध है।
विद्यानन्दने यद्यपि संक्षेप में 'सम्यग्ज्ञान' को प्रमाण कहा है, जो आचार्य गृद्धपिच्छके अनुसरणको व्यक्त करता है। पर पीछे उसे उन्होंने 'स्वार्थव्यवसायात्मक भी सिद्ध किया है। इस प्रकार उनके प्रमाणलक्षणमें अकलंककी तरह 'अनधिगत' विशेषण प्राप्त नहीं है। फिर भी उन्हें सम्यग्ज्ञानको अनधिगतार्थविषयक या अपूर्वार्थविषयक मानना अनिष्ट नहीं है। अकलंककी भांति उन्होंने भी स्मृत्यादि प्रमाणोंमें
१. दिङ्नाग, प्र० स० ( प्र० परि० ) का० ३ । २. इह हि द्वयी प्रत्यक्षजातिरविकल्पिका सविकल्पिका चेति ।-वाचस्पति, न्यायवा० ता० टी० १।१।४, पृ० १२५ । चौखम्बा प्रकाशन । ३. अष्टश० आप्तमी० का० ३६ तथा का० १०० । ४. प्रमाणमविसंवादि ज्ञानम्, अनधिगतार्थाधिगमलक्षणत्वात् ।वही, का० ३६, पृ० २२ । सनातनग्रन्थमाला प्रकाशन । ५. 'तत्रापूर्वार्थविज्ञानं....' कुमारिलका पूर्वोक्त श्लोक। ६. 'प्रमाणमविसंवादि ज्ञानम्...'.---प्रमाणवा० २।१ । ७. प्रस्तुत प्रमाणप० पृ० १ । ८. त० सू० ११९, १०। ९. किं पुनः सम्यग्ज्ञानम् । समभिधीयते-स्वार्थव्यवसायात्मकं सम्यग्ज्ञानं सम्यग्ज्ञानत्वात् । प्रमाणप० पृ० ५।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org