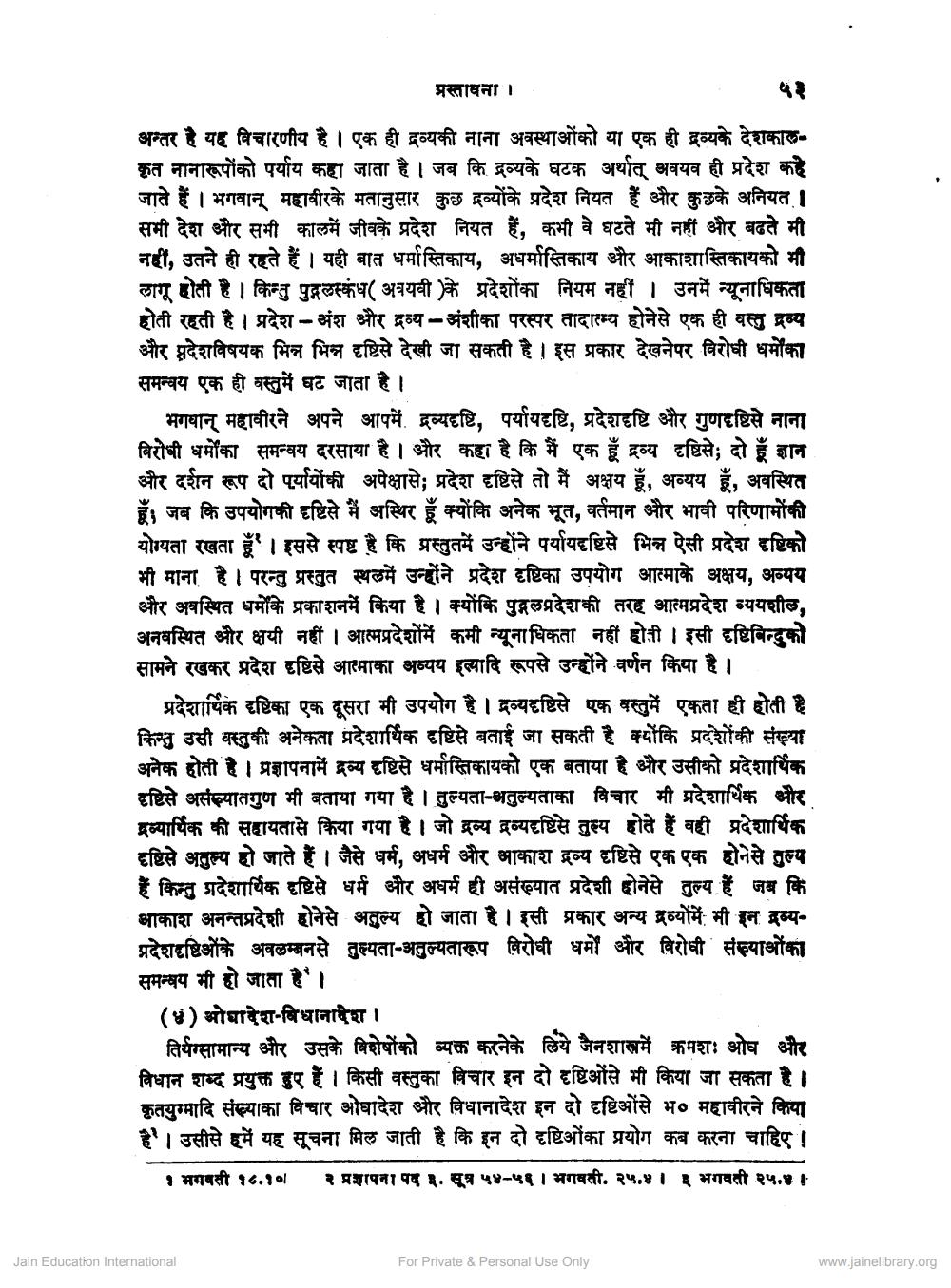________________
प्रस्तावना ।
५३
अन्तर है यह विचारणीय है । एक ही द्रव्यकी नाना अवस्थाओंको या एक ही द्रव्यके देशकाल - कृत नानारूपोंको पर्याय कहा जाता है। जब कि द्रव्यके घटक अर्थात् अवयव ही प्रदेश कहे जाते हैं । भगवान् महावीरके मतानुसार कुछ द्रव्योंके प्रदेश नियत हैं और कुछके अनियत । सभी देश और सभी कालमें जीवके प्रदेश नियत हैं, कभी घटते मी नहीं और बढते भी नहीं, उतने ही रहते हैं । यही बात धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकायको भी लागू होती है । किन्तु पुद्गलस्कंध ( अवयवी ) के प्रदेशोंका नियम नहीं । उनमें न्यूनाधिकता होती रहती है। प्रदेश - अंश और द्रव्य - अंशीका परस्पर तादात्म्य होनेसे एक ही वस्तु द्रव्य और प्रदेशविषयक भिन्न भिन्न दृष्टिसे देखी जा सकती है। इस प्रकार देखनेपर विरोधी धर्मोका समन्वय एक ही वस्तुमें घट जाता है।
भगवान् महावीर ने अपने आपमें द्रव्यदृष्टि, पर्यायदृष्टि, प्रदेशदृष्टि और गुणदृष्टिसे नाना विरोधी धर्मोका समन्वय दरसाया है । और कहा है कि मैं एक हूँ द्रव्य दृष्टिसे; दो हूँ ज्ञान और दर्शन रूप दो पर्यायोंकी अपेक्षासे; प्रदेश दृष्टिसे तो मैं अक्षय हूँ, अव्यय हूँ, अवस्थित हूँ, जब कि उपयोगकी दृष्टिसे मैं अस्थिर हूँ क्योंकि अनेक भूत, वर्तमान और भावी परिणामों की योग्यता रखता हूँ । इससे स्पष्ट है कि प्रस्तुतमें उन्होंने पर्यायदृष्टिसे भिन्न ऐसी प्रदेश दृष्टिको भी माना है। परन्तु प्रस्तुत स्थलमें उन्होंने प्रदेश दृष्टिका उपयोग आत्माके अक्षय, अव्यय और अवस्थित धर्मोप्रकाशनमें किया है। क्योंकि पुद्गलप्रदेशकी तरह आत्मप्रदेश व्ययशील, अनवस्थित और क्षयी नहीं । आत्मप्रदेशोंमें कमी न्यूनाधिकता नहीं होती । इसी दृष्टिबिन्दुको सामने रखकर प्रदेश दृष्टिसे आत्माका अव्यय इत्यादि रूपसे उन्होंने वर्णन किया है।
प्रदेशार्थिक दृष्टिका एक दूसरा भी उपयोग है । द्रव्यदृष्टिसे एक वस्तुमें एकता ही होती है। किन्तु उसी वस्तुकी अनेकता प्रदेशार्थिक दृष्टिसे बताई जा सकती है क्योंकि प्रदेशोंकी संख्या अनेक होती है । प्रज्ञापनामें द्रव्य दृष्टिसे धर्मास्तिकायको एक बताया है और उसीको प्रदेशार्षिक दृष्टिसे असंख्यातगुण भी बताया गया है । तुल्यता- अतुल्यताका विचार मी प्रदेशार्थिक और द्रव्यार्थिक की सहायता से किया गया है। जो द्रव्य द्रव्यदृष्टिसे तुल्य होते हैं वही प्रदेशार्थिक दृष्टिसे अतुल्य हो जाते हैं। जैसे धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य दृष्टिसे एक एक होने से तुल्य हैं किन्तु प्रदेशार्थिक दृष्टिसे धर्म और अधर्म ही असंख्यात प्रदेशी होनेसे तुल्य हैं जब कि आकाश अनन्तप्रदेशी होनेसे अतुल्य हो जाता है। इसी प्रकार अन्य द्रव्योंमें भी इन द्रव्यप्रदेशदृष्टिओंके अवलम्बन से तुल्यता- अतुल्यतारूप विरोधी धर्मों और विरोधी संख्याओंका समन्वय भी हो जाता है।
(४) ओघादेश - विधानादेश ।
तिर्यग्सामान्य और उसके विशेषोंको व्यक्त करनेके लिये जैनशास्त्रमें क्रमशः ओघ और विधान शब्द प्रयुक्त हुए हैं। किसी वस्तुका विचार इन दो दृष्टिओंसे भी किया जा सकता है। कृतयुग्मादि संख्याका विचार ओघादेश और विधानादेश इन दो दृष्टिओंसे भ० महावीरने किया है'। उसीसे हमें यह सूचना मिल जाती है कि इन दो दृष्टिओं का प्रयोग कब करना चाहिए ।
१ भगवती १८.१० / २ प्रज्ञापना पद ६. सूत्र ५४-५६ । भगवती. २५.४ । ६ भगवती २५.४ ॥
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org