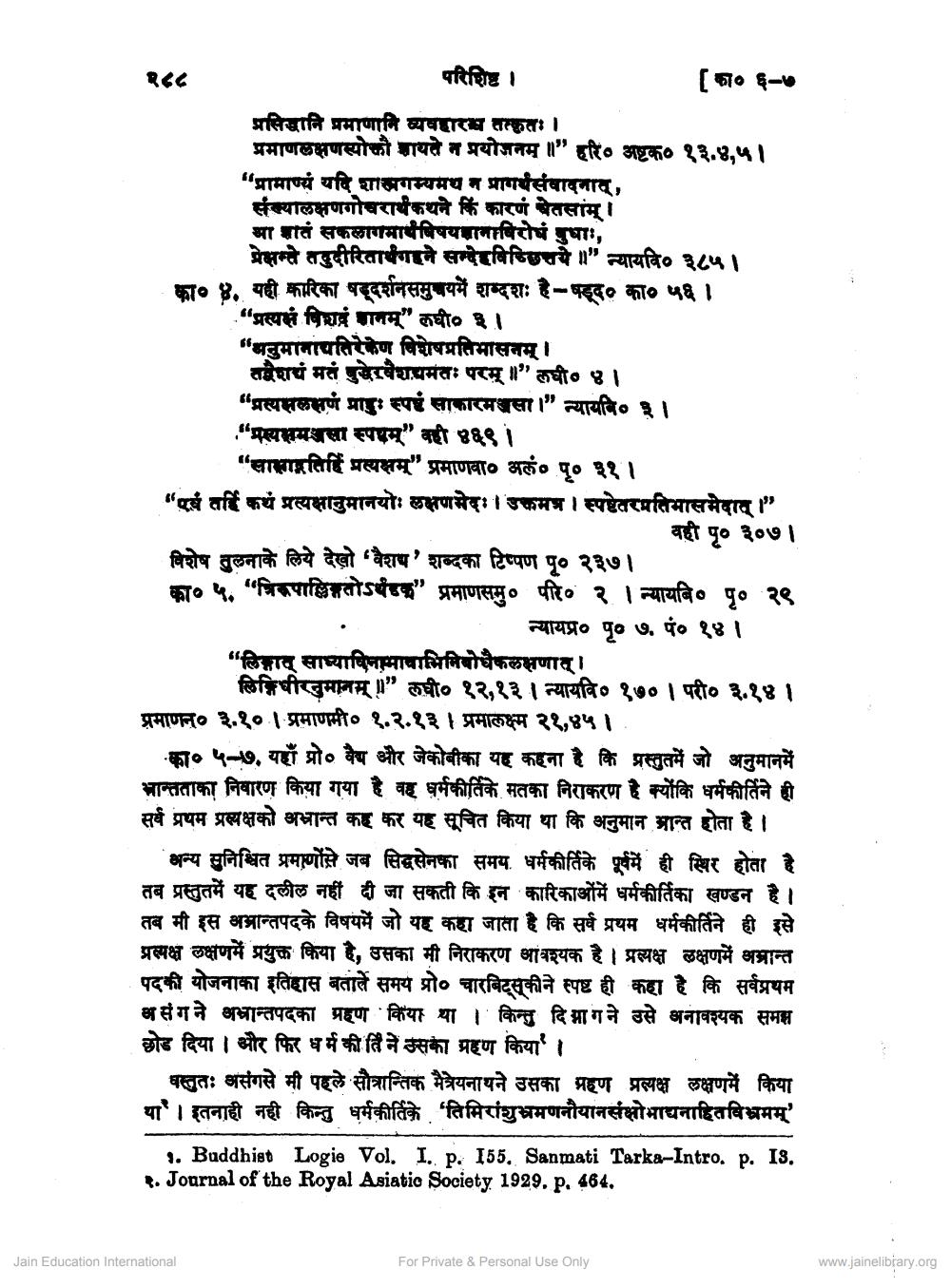________________
२८८
परिशिष्ट ।
[का०६-. प्रसिद्धानि प्रमाणानि व्यवहारब तत्कृतः। प्रमाणलक्षणस्योको ज्ञायते न प्रयोजनम ॥" हरि० अष्टक० १३.४,५। "प्रामाण्यं यदि शासगम्यमयन प्रागर्थसंवादनात्, संख्यालक्षणगोचराकथने किं कारणं घेतसाम् । आशातं सकलागमाविषयज्ञानाविरोधं दुधार,
प्रेक्षन्ते तदुदीरितायंगहने सन्देहविच्छित्तये ॥" न्यायवि० ३८५। का०४. यही क्रारिका षड्दर्शनसमुचयमें शम्दशः है-षड्द० का० ५६ ।
"प्रत्यक्ष विशवं शानम्" लघी० ३।। "अनुमानायतिरेकेण विशेषप्रतिमासनम् । तबेशचं मतं बुद्धेरवैशयमतः परम् ॥" लघी०४। "प्रत्यमलमणं प्राहु रूप साकारमजसा।" न्यायवि०३। "प्रत्यक्षमाला पपम्" वही १६९ |
"सामाइतिर्हि प्रत्यक्षम्" प्रमाणवा० अलं० पृ० ३१ । "एवं तर्हि कथं प्रत्यक्षानुमानयोः लक्षणमेदः । उकमत्र । स्पष्टेतरतिमासमेदात् ।"
वही पृ० ३०७।
विशेष तुलनाके लिये देखो 'वैशष' शब्दका टिप्पण पृ० २३७।। का० ५. "त्रिकपालिङ्गतोऽयंरक" प्रमाणसमु० परि० २ । न्यायबि० पृ० २९
__न्यायप्र० पृ० ७. पं० १४ । "लिसात् साध्याविनामावामिमिवोधैकलक्षणात्।
लिङ्गिधीरनुमानम् ॥" लघी० १२,१३ । न्यायवि० १७० । परी० ३.१४ । प्रमाणन० ३.१० । प्रमाणमी० १.२.१३ । प्रमालक्ष्म २१,४५। .
का०५-७. यहाँ प्रो० वैध और जेकोबीका यह कहना है कि प्रस्तुतमें जो अनुमानमें भान्तताका निवारण किया गया है वह धर्मकीर्तिक मतका निराकरण है क्योंकि धर्मकीर्तिने ही सर्व प्रथम प्रत्यक्षको अभ्रान्त कह कर यह सूचित किया था कि अनुमान प्रान्त होता है।
अन्य सुनिश्चित प्रमाणोंसे जब सिद्धसेनका समय. धर्मकीर्तिके पूर्वमें ही स्थिर होता है तब प्रस्तुतमें यह दलील नहीं दी जा सकती कि इन कारिकाओंमें धर्मकीर्तिका खण्डन है। तब मी इस अमान्तपदके विषयमें जो यह कहा जाता है कि सर्व प्रथम धर्मकीर्तिने ही इसे प्रत्यक्ष लक्षणमें प्रयुक्त किया है, उसका मी निराकरण आवश्यक है। प्रत्यक्ष लक्षणमें अप्रान्त पदकी योजनाका इतिहास बताते समय प्रो० चारबिट्स्कीने स्पष्ट ही कहा है कि सर्वप्रथम असं गने अभ्रान्तपदका ग्रहण किया था । किन्तु दिमाग ने उसे अनावश्यक समझ छोड दिया । और फिर धर्म की ति ने उसका ग्रहण किया।
वस्तुतः असंगसे मी पहले सौत्रान्तिक मैत्रेयनायने उसका ग्रहण प्रत्यक्ष लक्षणमें किया या। इतनाही नही किन्तु धर्मकीर्तिके 'तिमिरांशुभ्रमणनीयानसंक्षोभाधनाहितविभ्रमम्'
1. Buddhist Logie Vol. I. p. 155. Sanmati Tarka-Intro. p. IS. १. Journal of the Royal Asiatic Society 1929. p.464.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org