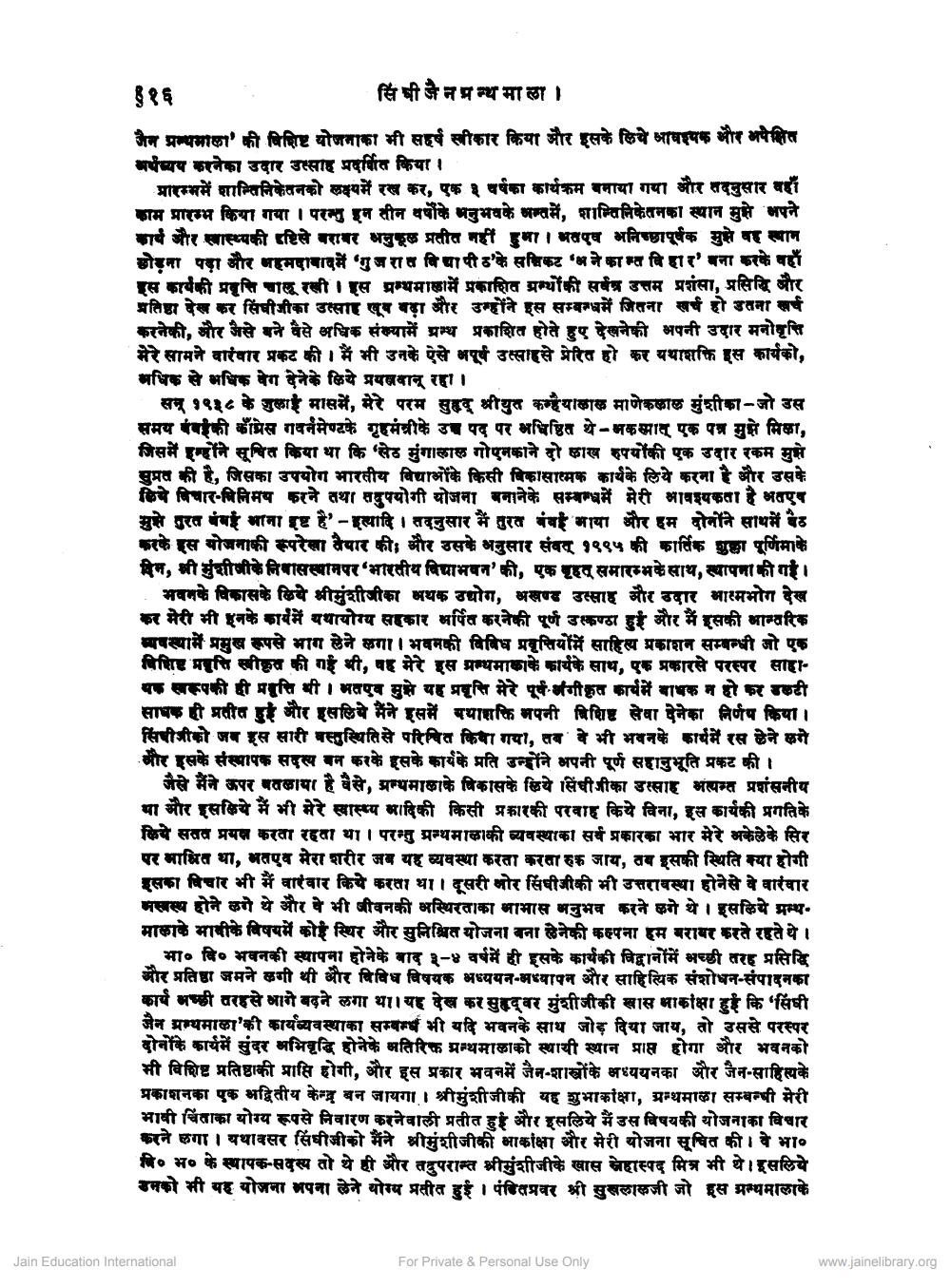________________
सिंघी जैन प्रन्थमाला।
जैन प्रन्यमाला' की विशिष्ट योजनाका भी सहर्ष स्वीकार किया और इसके लिये आवश्यक और अपेक्षित अर्थव्यय करनेका उदार उत्साह प्रदर्शित किया।
प्रारम्भमें शान्तिनिकेतनको लक्ष्य में रख कर, एक वर्षका कार्यक्रम बनाया गया और तदनुसार वहाँ काम प्रारम्भ किया गया । परन्तु इन तीन वर्षोंके अनुभवके अन्त में, शान्तिनिकेतनका स्थान मुझे अपने कार्य और स्वास्थ्यकी दृष्टिसे बराबर अनुकूल प्रतीत नहीं हुमा । अतएव अनिच्छापूर्वक मुझे वह स्थान छोड़ना पड़ा और अहमदाबादमें गुजरात विद्यापीठ'के ससिकट बने कान्त विहार' बना करके वहाँ इस कार्यकी प्रवृत्ति चालू रखी। इस प्रथमालामें प्रकाशित अन्योंकी सर्वत्र उत्तम प्रशंसा, प्रसिदि और प्रतिष्ठा देखकर सिंधीजीका उत्साह खूब बढ़ा और उन्होंने इस सम्बन्ध में जितना खर्च हो उतना खर्च करनेकी, और जैसे बने वैसे अधिक संख्यामें प्रन्थ प्रकाशित होते हुए देखनेकी अपनी उदार मनोवृत्ति मेरे सामने वारंवार प्रकट की। मैं भी उनके ऐसे अपूर्व उत्साहसे प्रेरित हो कर यथाशक्ति इस कार्यको, अधिक से अधिक वेग देनेके लिये प्रयतवान् रहा। .
सन् १९५० के जुलाई मासमें, मेरे परम सुहृद् श्रीयुत कन्हैयालाल माणेकलाल मुंशीका-जो उस समयबईकी काँग्रेस गवर्नमेण्टके गृहमंत्रीके उस पद पर अधिष्ठित थे-अकस्मात् एक पत्र मुझे मिका, जिसमें इन्होंने सूचित किया था कि 'सेठ मुंगालाल गोएनकाने दो लाख रुपयोंकी एक उदार रकम मुझे सुप्रवकी है, जिसका उपयोग भारतीय विद्याओंके किसी विकासात्मक कार्यके लिये करना है और उसके लिये विचार-विनिमय करने तथा सदुपयोगी योजना बनानेके सम्बन्धमें मेरी आवश्यकता है अतएष मुझे तुरत बंबई मामा इष्ट है' - इत्यादि । तदनुसार मैं तुरत बंबई माया और हम दोनोंने साथमें बैठ करके इस योजनाकी रूपरेखा तैयार की और उसके अनुसार संवत् १९९५ की कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाके दिन, श्री मुंशीजीके निवासस्वामपर भारतीय विद्याभवन' की, एक वृहत् समारम्भके साथ, स्थापना की गई। । भवनके विकासके लिये श्रीमुंशीजीका अथक उद्योग, अखण्ड उत्साह और उदार भास्मभोग देख कर मेरी भी इनके कार्यमें यथायोग्य सहकार अर्पित करनेकी पूर्ण उत्कण्ठा हुई और मैं इसकी आन्तरिक व्यवस्थामें प्रमुख रूपसे भाग लेने लगा। भवनकी विविध प्रवृत्तियों में साहित्य प्रकाशन सम्बन्धी जो एक विशिष्मति स्वीकृत की गई थी, वह मेरे इस अन्धमाकाके कार्यके साथ, एक प्रकारसे परस्पर साहापाखरूपकी ही प्रवृत्ति थी। भतएव मुझे यह प्रवृत्ति मेरे पूर्व अंगीकृत कार्य में बाधक न होकर उलटी साधक ही प्रतीताई और इसलिये मैंने इसमें यथाशक्किमपनी विशिष्ट सेवा देनेका निर्णय किया। सिंधीजीको जब इस सारी वस्तुस्थिति से परिचित किया गया, तब वे भी भवनके कार्य में रस लेने लगे और इसके संस्थापक सदस्य बन करके इसके कार्यके प्रति उन्होंने अपनी पूर्ण सहानुभूति प्रकट की।
जैसे मैंने ऊपर बतलाया है वैसे, अन्धमाकाके विकासके लिये सिंधीजीका उत्साह अत्यन्त प्रशंसनीय था और इसलिये मैं भी मेरे स्वास्थ्य मादिकी किसी प्रकारकी परवाह किये विना, इस कार्यकी प्रगतिके किये सतत प्रयत करता रहता था । परन्तु ग्रन्थमालाकी व्यवस्थाका सर्व प्रकारका भार मेरे अकेलेके सिर परमाधित था, भतएव मेरा शरीर जब यह व्यवस्था करता करता रुक जाय, तब इसकी स्थिति क्या होगी इसका विचार भी मैं वारंवार किये करता था। दूसरी ओर सिंधीजीकी भी उत्सरावस्था होनेसे वे वारंवार मस्वस्थ होने लगे थे और वे भी जीवनकी अस्थिरताका माभास अनुभव करने लगे थे। इसलिये मन्थ. मालाके मावीके विषयमें कोई स्थिर और सुनिश्चित योजना बना लेनेकी कल्पना हम बराबर करते रहते थे।
भा०वि० भवनकी स्थापना होनेके बाद ३-४ वर्षमें ही इसके कार्यकी विद्वानों में अच्छी तरह प्रसिदि और प्रतिष्ठा जमने लगी थी और विविध विषयक अध्ययन-अध्यापन और साहित्यिक संशोधन-संपादनका कार्य अच्छी तरहसे आगे बढ़ने लगा था। यह देख कर सुहद्वर मुंशीजीकी खास भाकांक्षा हुई कि 'सिंघी जैन अन्यमाला की कार्यव्यवस्थाका सम्बन्ध भी यदि भवनके साथ जोड़ दिया जाय, तो उससे परस्पर दोनोंके कार्यमें सुंदर अभिवृद्धि होनेके अतिरिक्त ग्रन्थमालाको स्थायी स्थान प्राप्त होगा और भवनको भी विशिष्ट प्रतिष्ठाकी प्राप्ति होगी, और इस प्रकार भवनमें जैन-शास्त्रोंके अध्ययनका और जैन-साहित्यके प्रकाशनका एक अद्वितीय केन्द्र बन जायगा । श्रीमुंशीजीकी यह शुभाकांक्षा, ग्रन्थमाला सम्बन्धी मेरी भावी चिंताका योग्य रूपसे निवारण करनेवाली प्रतीत हो और इसलिये मैं उस विषयकी योजनाका विचार करने लगा। यथावसर सिंघीजीको मैंने श्रीमुंशीजीकी भाकांक्षा और मेरी योजना सूचित की। वे भा० वि० भ० के स्थापक-सदस्य तो थे ही और तदुपरान्त श्रीमुंशीजीके खास बेहास्पद मित्र भी थे। इसलिये उनको भी यह योजना अपना लेने योग्य प्रतीत हुई। पंडितप्रवर श्री सुखलालजी जो इस ग्रन्थमालाके
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org