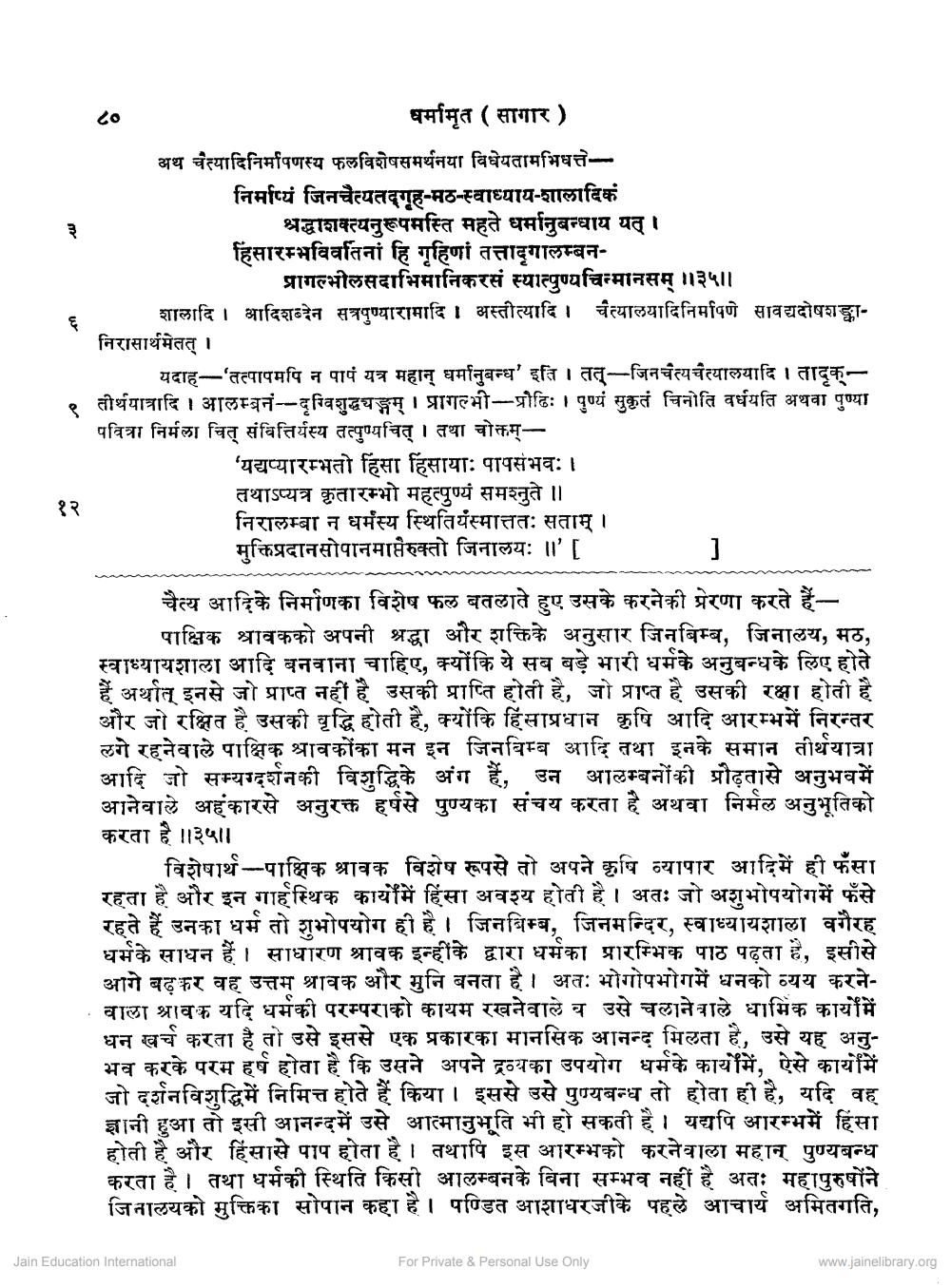________________
धर्मामृत ( सागार) अथ चैत्यादिनिर्मापणस्य फलविशेषसमर्थनया विधेयतामभिधत्ते
निर्माप्यं जिनचैत्यतद्गृह-मठ-स्वाध्याय-शालादिकं
___ श्रद्धाशक्त्यनुरूपमस्ति महते धर्मानुबन्धाय यत् । हिंसारम्भविवर्तिनां हि गृहिणां तत्तादृगालम्बन
प्रागल्भीलसदाभिमानिकरसं स्यात्पुण्यचिन्मानसम् ॥३५।। शालादि । आदिशब्देन सत्रपुण्यारामादि । अस्तीत्यादि । चैत्यालयादिनिर्मापणे सावद्यदोषशङ्कानिरासार्थमेतत् ।
यदाह-'तत्पापमपि न पापं यत्र महान् धर्मानुबन्ध' इति । तत्-जिनचैत्यचैत्यालयादि । तादकतीर्थयात्रादि । आलम्बनं-दग्विशुद्धघङ्गम् । प्रागल्भी-प्रौढिः । पुण्यं सुकृतं चिनोति वर्धयति अथवा पुण्या पवित्रा निर्मला चित् संवित्तिर्यस्य तत्पुण्यचित् । तथा चोक्तम्
'यद्यप्यारम्भतो हिंसा हिंसायाः पापसंभवः । तथाऽप्यत्र कृतारम्भो महत्पुण्यं समश्नुते ॥ निरालम्बा न धर्मस्य स्थितियस्मात्ततः सताम् । मुक्तिप्रदानसोपानमाप्तैरुक्तो जिनालयः ॥' [
चैत्य आदिके निर्माणका विशेष फल बतलाते हुए उसके करनेकी प्रेरणा करते हैं
पाक्षिक श्रावकको अपनी श्रद्धा और शक्तिके अनुसार जिनबिम्ब, जिनालय, मठ, स्वाध्यायशाला आदि बनवाना चाहिए, क्योंकि ये सब बड़े भारी धर्मके अनुबन्धके लिए होते हैं अर्थात इनसे जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति होती है, जो प्राप्त है उसकी रक्षा होती है और जो रक्षित है उसकी वृद्धि होती है, क्योंकि हिंसाप्रधान कृषि आदि आरम्भमें निरन्तर लगे रहनेवाले पाक्षिक श्रावकोंका मन इन जिनबिम्ब आदि तथा इनके समान तीर्थयात्रा आदि जो सम्यग्दर्शनकी विशुद्धिके अंग हैं, उन आलम्बनोंकी प्रौढ़तासे अनुभवमें आनेवाले अहंकारसे अनुरक्त हर्षसे पुण्यका संचय करता है अथवा निर्मल अनुभूतिको करता है ।।३५।।
विशेषार्थ-पाक्षिक श्रावक विशेष रूपसे तो अपने कृषि व्यापार आदिमें ही फंसा रहता है और इन गार्ह स्थिक कार्यों में हिंसा अवश्य होती है । अतः जो अशुभोपयोगमें फंसे रहते हैं उनका धर्म तो शुभोपयोग ही है। जिनबिम्ब, जिनमन्दिर, स्वाध्यायशाला वगैरह धर्म के साधन हैं। साधारण श्रावक इन्हींके द्वारा धर्मका प्रारम्भिक पाठ पढ़ता है, इसीसे आगे बढ़कर वह उत्तम श्रावक और मुनि बनता है। अतः भोगोपभोगमें धनको व्यय करनेवाला श्रावक यदि धर्मकी परम्पराको कायम रखनेवाले व उसे चलाने वाले धार्मिक कार्यों में धन खर्च करता है तो उसे इससे एक प्रकारका मानसिक आनन्द मिलता है, उसे यह अनुभव करके परम हर्ष होता है कि उसने अपने द्रव्यका उपयोग धर्मके कार्यों में, ऐसे कार्यों में जो दर्शनविशुद्धिमें निमित्त होते हैं किया। इससे उसे पुण्यबन्ध तो होता ही है, यदि वह ज्ञानी हुआ तो इसी आनन्दमें उसे आत्मानुभूति भी हो सकती है। यद्यपि आरम्भमें हिंसा होती है और हिंसासे पाप होता है । तथापि इस आरम्भको करनेवाला महान् पुण्यबन्ध करता है। तथा धर्मकी स्थिति किसी आलम्बनके बिना सम्भव नहीं है अतः महापुरुषोंने जिनालयको मुक्तिका सोपान कहा है। पण्डित आशाधरजीके पहले आचार्य अमितगति,
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org