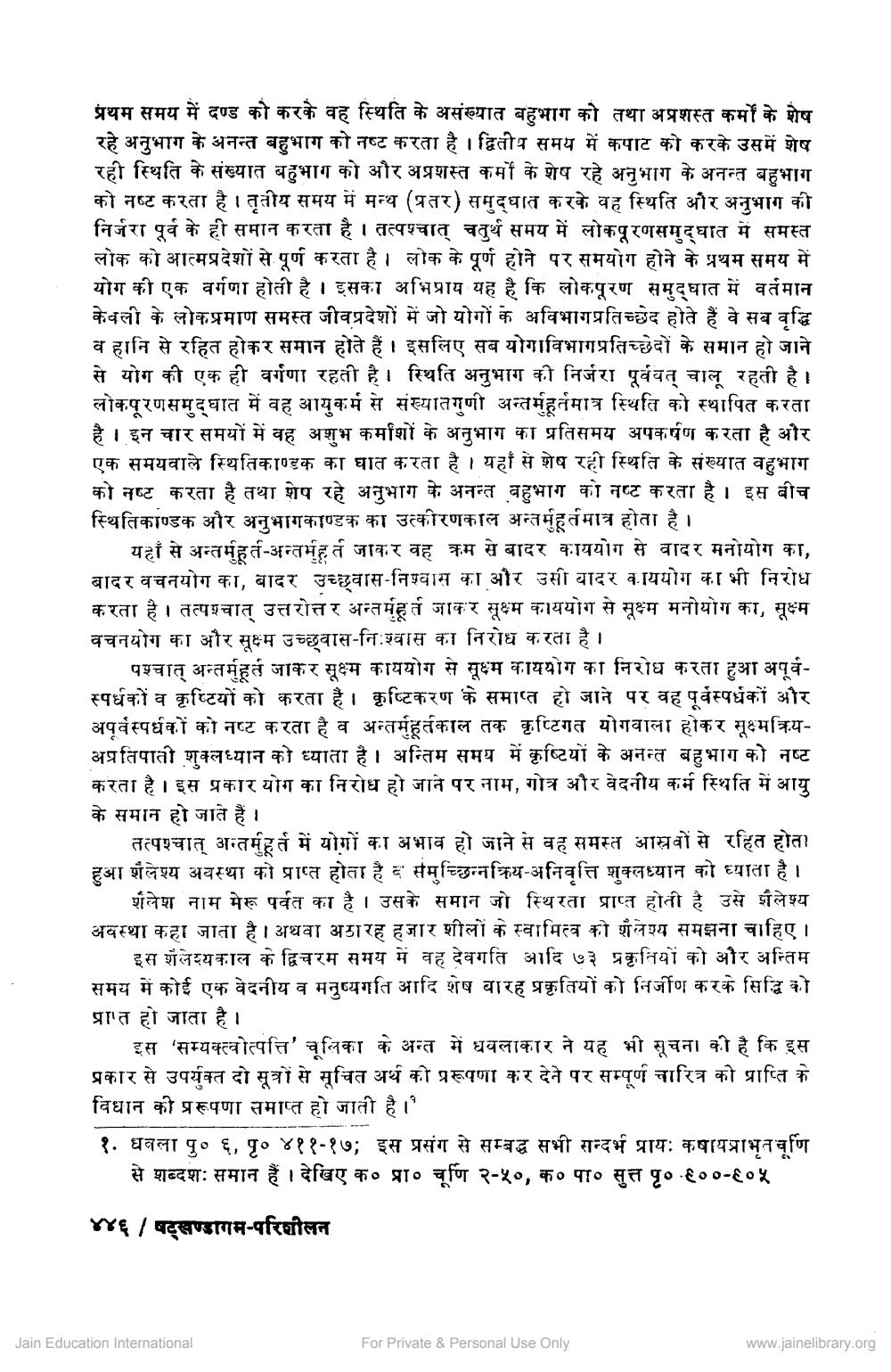________________
प्रथम समय में दण्ड को करके वह स्थिति के असंख्यात बहुभाग को तथा अप्रशस्त कर्मों के शेष रहे अनुभाग के अनन्त बहुभाग को नष्ट करता है । द्वितीय समय में कपाट को करके उसमें शेष रही स्थिति के संख्यात बहुभाग को और अप्रशस्त कर्मो के शेष रहे अनुभाग के अनन्त बहुभाग को नष्ट करता है । तृतीय समय में मन्थ (प्रतर) समुद्घात करके वह स्थिति और अनुभाग की निर्जरा पूर्व के ही समान करता है । तत्पश्चात् चतुर्थ समय में लोकपूरणसमुद्घात में समस्त लोक को आत्मप्रदेशों से पूर्ण करता है। लोक के पूर्ण होने पर समयोग होने के प्रथम समय में योग की एक वर्गणा होती है । इसका अभिप्राय यह है कि लोकपूरण समुद्घात में वर्तमान केवली के लोकप्रमाण समस्त जीवप्रदेशों में जो योगों के अविभागप्रतिच्छेद होते हैं वे सब वृद्धि व हानि से रहित होकर समान होते हैं । इसलिए सब योगाविभागप्रतिच्छेदों के समान हो जाने से योग की एक ही वर्गणा रहती है। स्थिति अनुभाग की निर्जरा पूर्ववत् चालू रहती है। लोकपूरणसमुद्घात में वह आयुकर्म से संख्यातगुणी अन्तर्मुहूर्तमात्र स्थिति को स्थापित करता है । इन चार समयों में वह अशुभ कर्माशों के अनुभाग का प्रतिसमय अपकर्षण करता है और एक समयवाले स्थितिकाण्डक का घात करता है । यहाँ से शेष रही स्थिति के संख्यात वहुभाग को नष्ट करता है तथा शेष रहे अनुभाग के अनन्त बहभाग को नष्ट करता है। इस बीच स्थितिकाण्डक और अनभागकाण्डक का उत्कीरणकाल अन्तर्महर्तमात्र होता है। ___ यहाँ से अन्तर्मुहूर्त-अन्तर्मुहुर्त जाकर वह क्रम से बादर काययोग से वादर मनोयोग का, बादर वचनयोग का, बादर उच्छ्वास-निश्वास का और उसी बादर काययोग का भी निरोध करता है। तत्पश्चात् उत्तरोत्तर अन्तर्मुहूर्त जाकर सूक्ष्म काययोग से सूक्ष्म मनोयोग का, सूक्ष्म वचनयोग का और सूक्ष्म उच्छ्वास-निःश्वास का निरोध करता है।
पश्चात् अन्तर्मुहूर्त जाकर सूक्ष्म काययोग से सूक्ष्म काययोग का निरोध करता हुआ अपूर्वस्पर्धकों व कृष्टियों को करता है। कृष्टिकरण के समाप्त हो जाने पर वह पूर्वस्पर्धकों और अपूर्वस्पर्धकों को नष्ट करता है व अन्तर्मुहूर्तकाल तक कृप्टिगत योगवाला होकर सूक्ष्मत्रियअप्रतिपाती शुक्लध्यान को ध्याता है। अन्तिम समय में कृष्टियों के अनन्त बहुभाग को नष्ट करता है । इस प्रकार योग का निरोध हो जाने पर नाम, गोत्र और वेदनीय कर्म स्थिति में आयु के समान हो जाते हैं।
तत्पश्चात् अन्तर्मुहूर्त में योगों का अभाव हो जाने से वह समस्त आस्रवों से रहित होता हुआ शैलेश्य अवस्था को प्राप्त होता है व समुच्छिन्नक्रिय-अनिवृत्ति शुक्लध्यान को ध्याता है ।
शैलेश नाम मेरू पर्वत का है । उसके समान जो स्थिरता प्राप्त होती है उसे शैलेश्य अवस्था कहा जाता है । अथवा अठारह हजार शीलों के स्वामित्व को शैलेश्य समझना चाहिए।
इस शैलेश्यकाल के द्विचरम समय में वह देवगति आदि ७३ प्रकृतियों को और अन्तिम समय में कोई एक वेदनीय व मनुष्यगति आदि शेष बारह प्रकृतियों को निर्जीण करके सिद्धि को प्राप्त हो जाता है।
इस 'सम्यक्त्वोत्पत्ति' चूलिका के अन्त में धवलाकार ने यह भी सूचना की है कि इस प्रकार से उपर्युक्त दो सूत्रों से सूचित अर्थ को प्ररूपणा कर देने पर सम्पूर्ण चारित्र को प्राप्ति के विधान की प्ररूपणा समाप्त हो जाती है।' १. धवला पु० ६, पृ० ४११-१७; इस प्रसंग से सम्बद्ध सभी सन्दर्भ प्रायः कषायप्राभूत चूर्णि
से शब्दशः समान हैं । देखिए क० प्रा० चूणि २-५०, क० पा० सुत्त पृ०.६००-६०५ ४६ / षट्खण्डागम-परिशीलन
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org