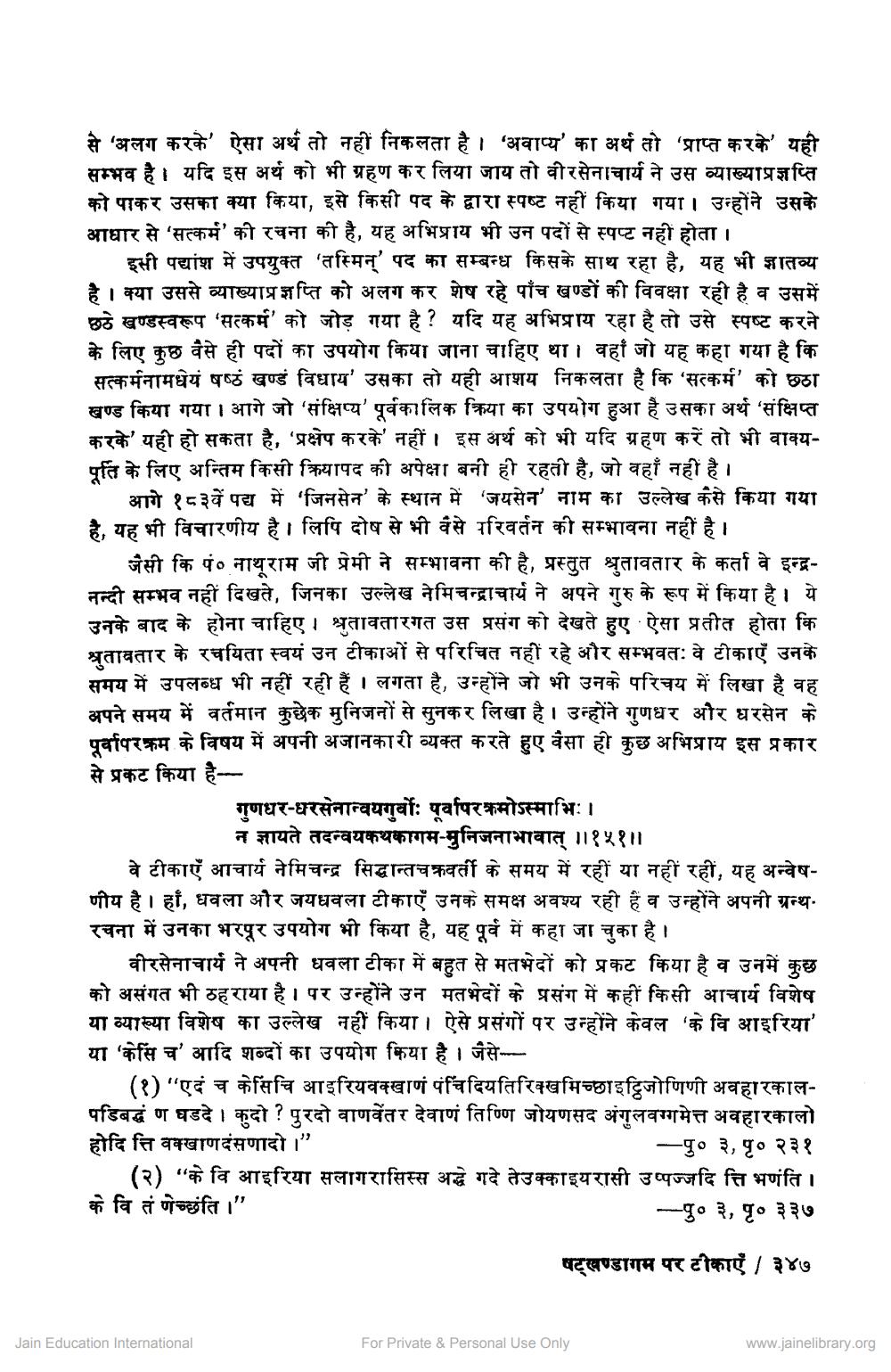________________
से 'अलग करके' ऐसा अर्थ तो नहीं निकलता है। 'अवाप्य' का अर्थ तो 'प्राप्त करके' यही सम्भव है। यदि इस अर्थ को भी ग्रहण कर लिया जाय तो वीरसेनाचार्य ने उस व्याख्याप्रज्ञप्ति को पाकर उसका क्या किया, इसे किसी पद के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया। उन्होंने उसके आधार से 'सत्कर्म' की रचना की है, यह अभिप्राय भी उन पदों से स्पष्ट नहीं होता। ___इसी पद्यांश में उपयुक्त 'तस्मिन्' पद का सम्बन्ध किसके साथ रहा है, यह भी ज्ञातव्य है। क्या उससे व्याख्याप्रज्ञप्ति को अलग कर शेष रहे पाँच खण्डों की विवक्षा रही है व उसमें छठे खण्डस्वरूप 'सत्कर्म' को जोड़ गया है ? यदि यह अभिप्राय रहा है तो उसे स्पष्ट करने के लिए कुछ वैसे ही पदों का उपयोग किया जाना चाहिए था। वहाँ जो यह कहा गया है कि सत्कर्मनामधेयं षष्ठं खण्ड विधाय' उसका तो यही आशय निकलता है कि 'सत्कर्म' को छठा खण्ड किया गया। आगे जो 'संक्षिप्य' पूर्वकालिक क्रिया का उपयोग हुआ है उसका अर्थ 'संक्षिप्त करके' यही हो सकता है, 'प्रक्षेप करके' नहीं। इस अर्थ को भी यदि ग्रहण करें तो भी वाक्यपूर्ति के लिए अन्तिम किसी क्रियापद की अपेक्षा बनी ही रहती है, जो वहाँ नहीं है।
आगे १८३वें पद्य में 'जिनसेन' के स्थान में 'जयसेन' नाम का उल्लेख कैसे किया गया है, यह भी विचारणीय है। लिपि दोष से भी वैसे परिवर्तन की सम्भावना नहीं है।
जैसी कि पं० नाथूराम जी प्रेमी ने सम्भावना की है, प्रस्तुत श्रुतावतार के कर्ता वे इन्द्रनन्दी सम्भव नहीं दिखते, जिनका उल्लेख नेमिचन्द्राचार्य ने अपने गुरु के रूप में किया है। ये उनके बाद के होना चाहिए। श्रुतावतारगत उस प्रसंग को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता कि श्रतावतार के रचयिता स्वयं उन टीकाओं से परिचित नहीं रहे और सम्भवतः वे टीकाएँ उनके समय में उपलब्ध भी नहीं रही हैं । लगता है, उन्होंने जो भी उनके परिचय में लिखा है वह अपने समय में वर्तमान कुछेक मुनिजनों से सुनकर लिखा है। उन्होंने गुणधर और धरसेन के पूर्वापरक्रम के विषय में अपनी अजानकारी व्यक्त करते हुए वैसा ही कुछ अभिप्राय इस प्रकार से प्रकट किया है
गुणधर-धरसेनान्वयगुर्वोः पूर्वापरक्रमोऽस्माभिः ।
न ज्ञायते तदन्वयकथकागम-मुनिजनाभावात् ॥१५१॥ वे टीकाएँ आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती के समय में रहीं या नहीं रहीं, यह अन्वेषणीय है। हाँ, धवला और जयधवला टीकाएँ उनके समक्ष अवश्य रही हैं व उन्होंने अपनी ग्रन्थरचना में उनका भरपूर उपयोग भी किया है, यह पूर्व में कहा जा चुका है।
वीरसेनाचार्य ने अपनी धवला टीका में बहुत से मतभेदों को प्रकट किया है व उनमें कुछ को असंगत भी ठहराया है। पर उन्होंने उन मतभेदों के प्रसंग में कहीं किसी आचार्य विशेष या व्याख्या विशेष का उल्लेख नहीं किया। ऐसे प्रसंगों पर उन्होंने केवल 'के वि आइरिया' या 'केसि च' आदि शब्दों का उपयोग किया है । जैसे-~
(१) "एदं च केसिंचि आइरियवक्खाणं पंचिंदियतिरिक्खमिच्छाइटिजोणिणी अवहारकालपडिबद्धं ण घडदे। कुदो ? पुरदो वाणवेतर देवाणं तिण्णि जोयणसद अंगुलवग्गमेत्त अवहारकालो होदि त्ति वक्खाणदंसणादो।"
-पु० ३, पृ० २३१ (२) “के वि आइरिया सलागरासिस्स अद्धे गदे तेउक्काइयरासी उप्पज्जदि त्ति भणंति । के वि तं णेच्छति ।"
पु० ३, पृ० ३३७
षट्खण्डागम पर टीकाएँ | ३४७
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org