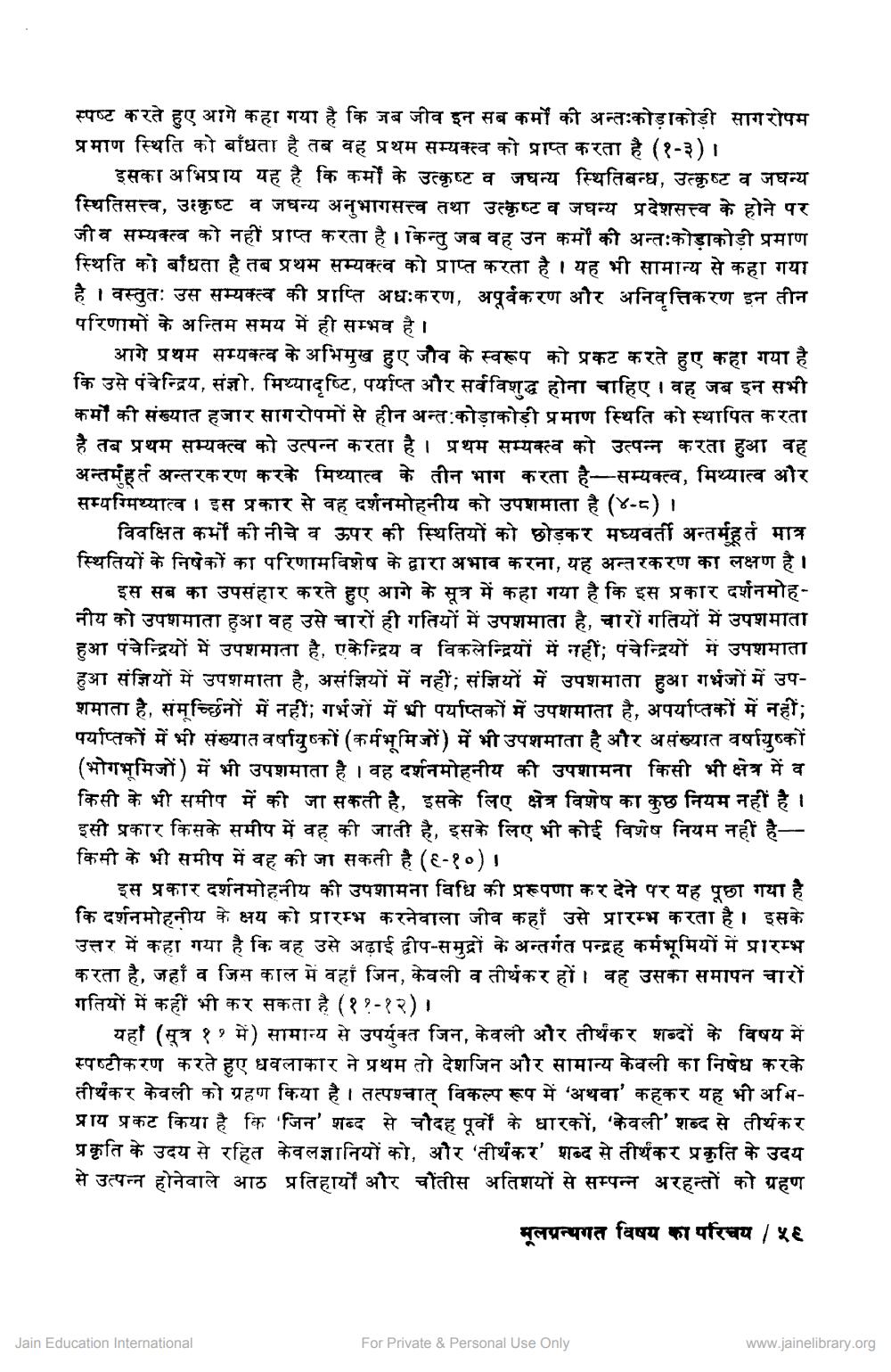________________
स्पष्ट करते हुए आगे कहा गया है कि जब जीव इन सब कर्मों की अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण स्थिति को बाँधता है तब वह प्रथम सम्यक्त्व को प्राप्त करता है (१-३) ।
इसका अभिप्राय यह है कि कर्मों के उत्कृष्ट व जघन्य स्थितिबन्ध, उत्कृष्ट व जघन्य स्थितिसत्त्व, उत्कृष्ट व जघन्य अनुभागसत्त्व तथा उत्कृष्ट व जघन्य प्रदेशसत्त्व के होने पर जीव सम्यक्त्व को नहीं प्राप्त करता है । किन्तु जब वह उन कर्मों की अन्तःकोड़ाकोड़ी प्रमाण स्थिति को बाँधता है तब प्रथम सम्यक्त्व को प्राप्त करता है । यह भी सामान्य से कहा गया है । वस्तुतः उस सम्यक्त्व की प्राप्ति अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण इन तीन परिणामों के अन्तिम समय में ही सम्भव है ।
आगे प्रथम सम्यक्त्व के अभिमुख हुए जौव के स्वरूप को प्रकट करते हुए कहा गया है कि उसे पंचेन्द्रिय, संज्ञो मिथ्यादृष्टि, पर्याप्त और सर्वविशुद्ध होना चाहिए। वह जब इन सभी कर्मों की संख्यात हजार सागरोपमों से हीन अन्तः कोड़ाकोड़ी प्रमाण स्थिति को स्थापित करता है तब प्रथम सम्यक्त्व को उत्पन्न करता है । प्रथम सम्यक्त्व को उत्पन्न करता हुआ वह अन्तर्मुहूर्त अन्तरकरण करके मिथ्यात्व के तीन भाग करता है— सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व | इस प्रकार से वह दर्शनमोहनीय को उपशमाता है (४-८ ) ।
विवक्षित कर्मों की नीचे व ऊपर की स्थितियों को छोड़कर मध्यवर्ती अन्तर्मुहूर्त मात्र स्थितियों के निषेकों का परिणामविशेष के द्वारा अभाव करना, यह अन्तरकरण का लक्षण है ।
इस सब का उपसंहार करते हुए आगे के सूत्र में कहा गया है कि इस प्रकार दर्शनमोहनी को उपशमाता हुआ वह उसे चारों ही गतियों में उपशमाता है, चारों गतियों में उपशमाता हुआ पंचेन्द्रियों में उपशमाता है, एकेन्द्रिय व विकलेन्द्रियों में नहीं; पंचेन्द्रियों में उपशमाता हुआ संज्ञियों में उपशमाता है, असंज्ञियों में नहीं; संज्ञियों में उपशमाता हुआ गर्भजों में उपशमाता है, संमूर्च्छिनों में नहीं; गर्भजों में भी पर्याप्तकों में उपशमाता है, अपर्याप्तकों में नहीं; पर्याप्तकों में भी संख्यात वर्षायुष्कों (कर्मभूमिजों) में भी उपशमाता है और असंख्यात वर्षायुष्कों (भोगभूमिजों) में भी उपशमाता है । वह दर्शनमोहनीय की उपशामना किसी भी क्षेत्र में व किसी के भी समीप में की जा सकती है, इसके लिए क्षेत्र विशेष का कुछ नियम नहीं है । इसी प्रकार किसके समीप में वह की जाती है, इसके लिए भी कोई विशेष नियम नहीं हैकिसी के भी समीप में वह की जा सकती है ( ६-१० ) ।
इस प्रकार दर्शनमोहनीय की उपशामना विधि की प्ररूपणा कर देने पर यह पूछा गया है कि दर्शनमोहनीय के क्षय को प्रारम्भ करनेवाला जीव कहाँ उसे प्रारम्भ करता है । इसके उत्तर में कहा गया है कि वह उसे अढ़ाई द्वीप - समुद्रों के अन्तर्गत पन्द्रह कर्मभूमियों में प्रारम्भ करता है, जहाँ व जिस काल में वहाँ जिन, केवली व तीर्थकर हों। वह उसका समापन चारों गतियों में कहीं भी कर सकता है (११-१२) ।
यहाँ ( सुत्र ११ में) सामान्य से उपर्युक्त जिन, केवली और तीर्थंकर शब्दों के विषय में स्पष्टीकरण करते हुए धवलाकार ने प्रथम तो देशजिन और सामान्य केवली का निषेध करके तीर्थंकर केवली को ग्रहण किया है । तत्पश्चात् विकल्प रूप में ' अथवा ' कहकर यह भी अभिप्राय प्रकट किया है कि 'जिन' शब्द से चौदह पूर्वी के धारकों, 'केवली' शब्द से तीर्थकर प्रकृति के उदय से रहित केवलज्ञानियों को, और 'तीर्थंकर' शब्द से तीर्थंकर प्रकृति के उदय से उत्पन्न होनेवाले आठ प्रतिहार्यो और चौंतीस अतिशयों से सम्पन्न अरहन्तों को ग्रहण
मूलग्रन्थगत विषय का परिचय / ५६
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org