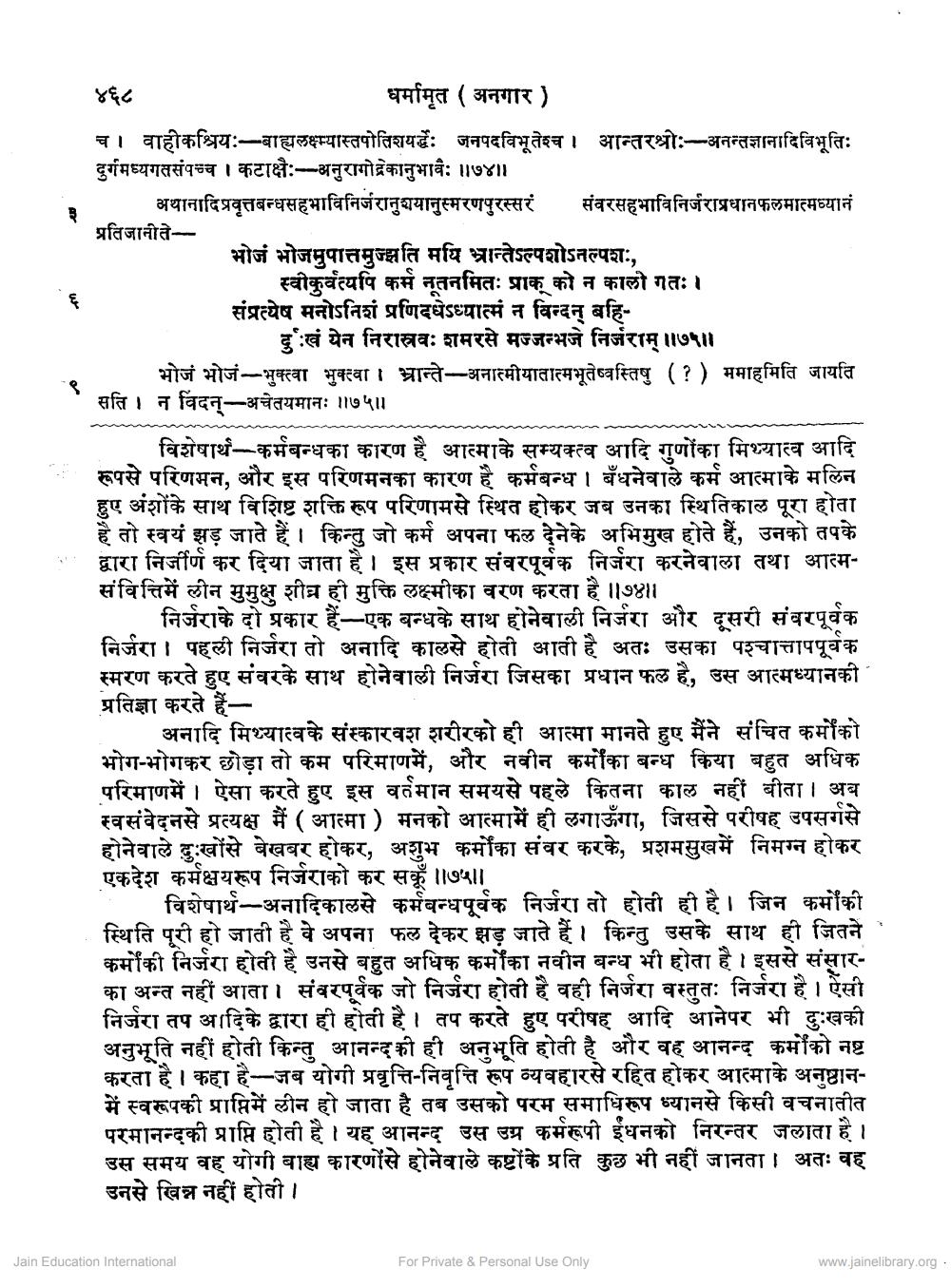________________
४६८
धर्मामृत ( अनगार ) च। वाहीकश्रियः-बाह्यलक्ष्म्यास्तपोतिशयद्धैः जनपदविभूतेश्च । आन्तरश्री:-अनन्तज्ञानादिविभूतिः दुर्गमध्यगतसंपच्च । कटाक्षः-अनुरागोद्रेकानुभावैः ।।७४॥ ___अथानादिप्रवृत्तबन्धसहभाविनिर्जरानुशयानुस्मरणपुरस्सरं संवरसहभाविनिर्जराप्रधानफलमात्मध्यानं प्रतिजानीते
भोज भोजमुपात्तमुज्झति मयि भ्रान्तेऽल्पशोऽनल्पशः,
स्वीकुर्वत्यपि कर्म नतनमितः प्राक् को न काली गतः। संप्रत्येष मनोऽनिशं प्रणिदधेऽध्यात्मं न विन्दन् बहि
दु:खं येन निरास्रवः शमरसे मज्जन्भजे निर्जराम् ॥७॥ __ भोज भोज-भुक्त्वा भुक्त्वा । भ्रान्ते-अनात्मीयातात्मभूतेष्वस्तिषु (?) ममाहमिति जायति ' सति । न विदन्-अचेतयमानः ॥७५॥
विशेषार्थ-कर्मबन्धका कारण है आत्माके सम्यक्त्व आदि गुणोंका मिथ्यात्व आदि रूपसे परिणमन, और इस परिणमनका कारण है कर्मबन्ध । बँधनेवाले कर्म आत्माके मलिन हुए अंशोंके साथ विशिष्ट शक्ति रूप परिणामसे स्थित होकर जब उनका स्थितिकाल पूरा होता है तो स्वयं झड़ जाते हैं। किन्तु जो कर्म अपना फल देनेके अभिमुख होते हैं, उनको तपके द्वारा निर्जीर्ण कर दिया जाता है। इस प्रकार संवरपूर्वक निर्जरा करनेवाला तथा आत्मसंवित्तिमें लीन मुमुक्षु शीघ्र ही मुक्ति लक्ष्मीका वरण करता है ।।७४॥
निर्जराके दो प्रकार हैं-एक बन्धके साथ होनेवाली निर्जरा और दूसरी संवरपूर्वक निर्जरा। पहली निर्जरा तो अनादि कालसे होती आती है अतः उसका पश्चात्तापपूर्वक स्मरण करते हुए संवरके साथ होनेवाली निजरा जिसका प्रधान
र आत्मध्यानकी प्रतिज्ञा करते हैं
_अनादि मिथ्यात्वके संस्कारवश शरीरको ही आत्मा मानते हुए मैंने संचित कर्मोंको भोग-भोगकर छोड़ा तो कम परिमाणमें, और नवीन कर्मोंका बन्ध किया बहुत अधिक परिमाणमें । ऐसा करते हुए इस वर्तमान समयसे पहले कितना काल नहीं बीता। अब स्वसंवेदनसे प्रत्यक्ष मैं (आत्मा) मनको आत्मामें ही लगाऊँगा, जिससे परीषह उपसर्गसे होनेवाले दुःखोंसे बेखबर होकर, अशुभ कर्मोका संवर करके, प्रशमसुखमें निमग्न होकर एकदेश कर्मक्षयरूप निर्जराको कर सकूँ ॥७॥
विशेषार्थ-अनादिकालसे कर्मवन्धपूर्वक निर्जरा तो होती ही है। जिन कर्मोंकी स्थिति पूरी हो जाती है वे अपना फल देकर झड़ जाते हैं। किन्तु उसके साथ ही जितने कर्मोंकी निर्जरा होती है उनसे बहुत अधिक कर्मोंका नवीन बन्ध भी होता है। इससे संसारका अन्त नहीं आता। संवरपूर्वक जो निर्जरा होती है वही निर्जरा वस्तुतः निर्जरा है । ऐसी निर्जरा तप आदिके द्वारा ही होती है। तप करते हुए परीषह आदि आनेपर भी दुःखकी अनुभूति नहीं होती किन्तु आनन्द की ही अनुभूति होती है और वह आनन्द कर्मोको नष्ट करता है। कहा है-जब योगी प्रवृत्ति-निवृत्ति रूप व्यवहारसे रहित होकर आत्माके अनुष्ठानमें स्वरूपकी प्राप्तिमें लीन हो जाता है तब उसको परम समाधिरूप ध्यानसे किसी वचनातीत परमानन्दकी प्राप्ति होती है । यह आनन्द उस उग्र कर्मरूपी ईंधनको निरन्तर जलाता है । उस समय वह योगी बाह्य कारणोंसे होनेवाले कष्टोंके प्रति कुछ भी नहीं जानता। अतः वह उनसे खिन्न नहीं होती।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org ..