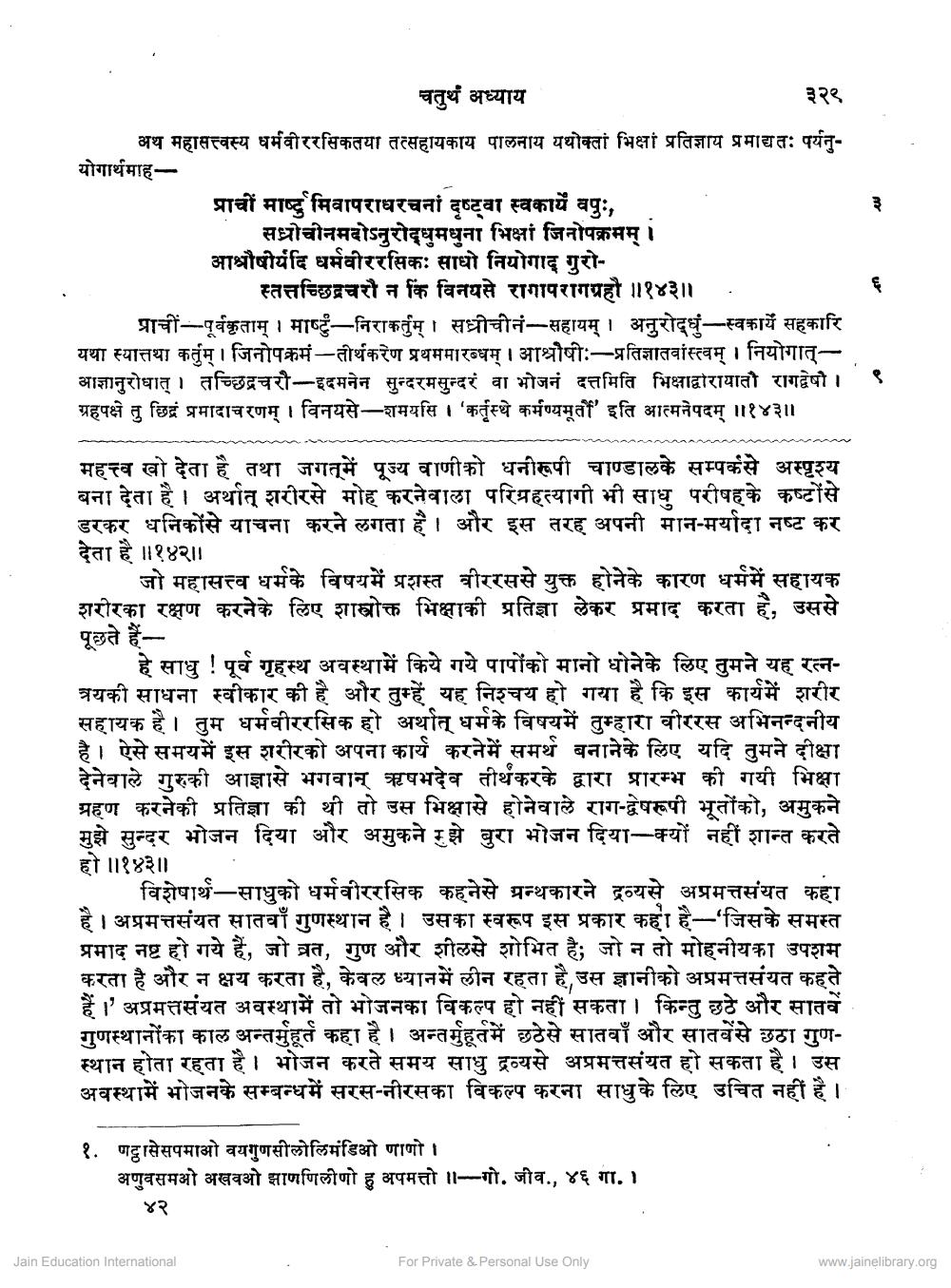________________
चतुर्थ अध्याय
३२९ अथ महासत्त्वस्य धर्मवीररसिकतया तत्सहायकाय पालनाय यथोक्तां भिक्षां प्रतिज्ञाय प्रमाद्यतः पर्यनुयोगार्थमाह
प्राची माष्टुमिवापराधरचनां दृष्ट्वा स्वकायें वपुः,
सध्रोचीनमदोऽनुरोधमधुना भिक्षां जिनोपक्रमम् । आश्रौषोयदि धर्मवीररसिकः साधो नियोगाद् गुरो
स्तत्तच्छिद्रचरौ न कि विनयसे रागापरागग्रहौ ॥१४३॥ . प्राची-पूर्वकृताम् । माष्टुं–निराकर्तुम् । सध्रीचीनं-सहायम् । अनुरोर्बु-स्वकार्ये सहकारि यथा स्यात्तथा कर्तुम् । जिनोपक्रम-तीर्थकरेण प्रथममारब्धम् । आश्रौषीः-प्रतिज्ञातवांस्त्वम् । नियोगात्आज्ञानुरोधात् । तच्छिद्रचरौ-इदमनेन सुन्दरमसुन्दरं वा भोजनं दत्तमिति भिक्षाद्वोरायातौ रागद्वेषौ। ९ ग्रहपक्षे तु छिद्रं प्रमादाचरणम् । विनयसे-शमयसि । 'कर्तृस्थे कर्मण्यमूर्ती' इति आत्मनेपदम् ॥१४३॥
महत्त्व खो देता है तथा जगत्में पूज्य वाणीको धनीरूपी चाण्डालके सम्पर्कसे अस्पृश्य बना देता है। अर्थात् शरीरसे मोह करनेवाला परिग्रहत्यागी भी साधु परीषहके कष्टोंसे डरकर धनिकोंसे याचना करने लगता है। और इस तरह अपनी मान-मयोंदा नष्ट कर देता है ।।१४२।।
जो महासत्त्व धर्मके विषयमें प्रशस्त वीररससे युक्त होनेके कारण धर्ममें सहायक शरीरका रक्षण करनेके लिए शास्त्रोक्त भिक्षाकी प्रतिज्ञा लेकर प्रमाद करता है, उससे
पूछते हैं
हे साधु ! पूर्व गृहस्थ अवस्थामें किये गये पापोंको मानो धोनेके लिए तुमने यह रत्नत्रयकी साधना स्वीकार की है और तुम्हें यह निश्चय हो गया है कि इस कार्य में शरीर सहायक है। तुम धर्मवीररसिक हो अर्थात् धर्म के विषयमें तुम्हारा वीररस अभिनन्दनीय है। ऐसे समयमें इस शरीरको अपना कार्य करने में समर्थ बनानेके लिए यदि तुमने दीक्षा देनेवाले गुरुकी आज्ञासे भगवान् ऋषभदेव तीर्थकरके द्वारा प्रारम्भ की गयी भिक्षा ग्रहण करनेकी प्रतिज्ञा की थी तो उस भिक्षासे होनेवाले राग-द्वेषरूपी भूतोंको, अमुकने मुझे सुन्दर भोजन दिया और अमुकने मुझे बुरा भोजन दिया-क्यों नहीं शान्त करते हो ॥१४३॥
विशेषार्थ–साधुको धर्मवीररसिक कहनेसे ग्रन्थकारने द्रव्यसे अप्रमत्तसंयत कहा है। अप्रमत्तसंयत सातवाँ गुणस्थान है। उसका स्वरूप इस प्रकार कहा हैप्रमाद नष्ट हो गये हैं, जो व्रत, गुण और शीलसे शोभित है; जो न तो मोहनीयका उपशम करता है और न क्षय करता है, केवल ध्यान में लीन रहता है, उस ज्ञानीको अप्रमत्तसंयत कहते हैं।' अप्रमत्तसंयत अवस्थामें तो भोजनका विकल्प हो नहीं सकता। किन्तु छठे और सातवें गुणस्थानोंका काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । अन्तर्मुहूर्तमें छठेसे सातवाँ और सातवेंसे छठा गुणस्थान होता रहता है। भोजन करते समय साधु द्रव्यसे अप्रमत्तसंयत हो सकता है। उस अवस्थामें भोजनके सम्बन्धमें सरस-नीरसका विकल्प करना साधु के लिए उचित नहीं है ।
१. णदासेसपमाओ वयगुणसीलोलिमंडिओ णाणो ।
अणुवसमओ अखवओ झाणणिलीणो ह अपमत्तो ॥-गो. जीव., ४६ गा.।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org