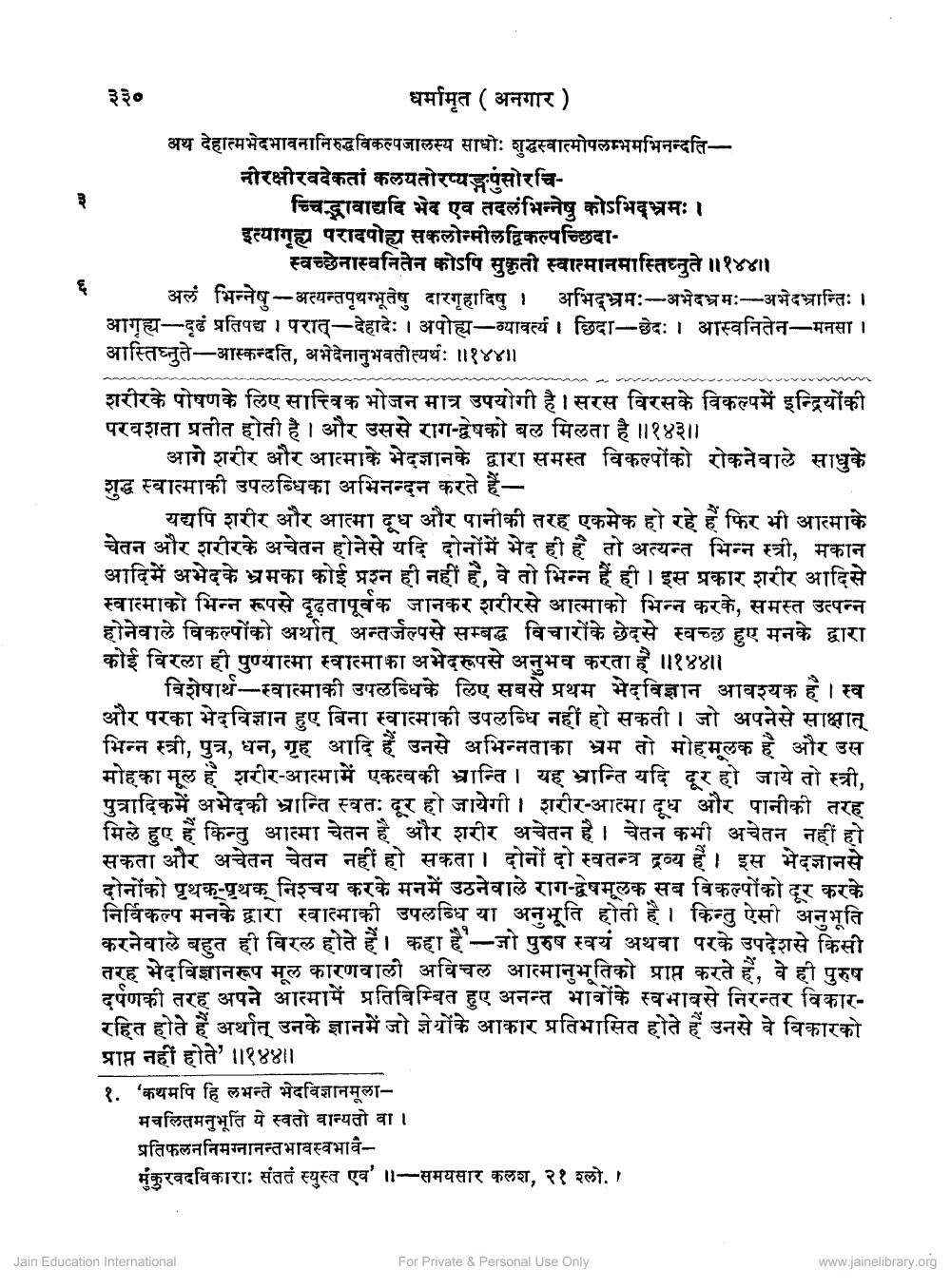________________
६
३३०
धर्मामृत (अनगार)
अथ देहात्मभेदभावनानिरुद्धविकल्पजालस्य साधोः शुद्धस्वात्मोपलम्भमभिनन्दति - नीरक्षीरवदेकतां कलयतोरप्यङ्गपुंसोरचि
च्चिद्भावाद्यदि भेद एव तदलंभिन्नेषु कोऽभिदुद्भ्रमः । इत्यगृह्य परादपोह्य सकलोन्मीलद्विकल्पच्छिदा
स्वच्छेनास्वनितेन कोऽपि सुकृती स्वात्मानमास्तिनुते ॥ १४४॥
अलं भिन्नेषु - अत्यन्तपृथग्भूतेषु दारगृहादिषु अभिद्भ्रमः - अभेदभ्रमः - अभेदभ्रान्तिः । आगृह्य - दृढं प्रतिपद्य । परात् - देहादेः । अपोह्य - व्यावर्त्य । छिदा - छेदः । आस्वनितेन मनसा । आस्तिघ्नुते - आस्कन्दति, अभेदेनानुभवतीत्यर्थः ॥ १४४ ॥
शरीर के पोषण के लिए सात्त्विक भोजन मात्र उपयोगी है। सरस विरसके विकल्पमें इन्द्रियोंकी परवशता प्रतीत होती है। और उससे राग-द्वेषको बल मिलता है ॥ १४३॥
आगे शरीर और आत्माके भेदज्ञानके द्वारा समस्त विकल्पोंको रोकनेवाले साधुके शुद्ध स्वात्माकी उपलब्धिका अभिनन्दन करते हैं
यद्यपि शरीर और आत्मा दूध और पानीकी तरह एकमेक हो रहे हैं फिर भी आत्मा के चेतन और शरीर के अचेतन होनेसे यदि दोनोंमें भेद ही है तो अत्यन्त भिन्न स्त्री, मकान आदि में अभेदके भ्रमका कोई प्रश्न ही नहीं है, वे तो भिन्न हैं ही। इस प्रकार शरीर आदि से स्वात्माको भिन्न रूपसे दृढ़तापूर्वक जानकर शरीर से आत्माको भिन्न करके, समस्त उत्पन्न होनेवाले विकल्पोंको अर्थात् अन्तर्जल्पसे सम्बद्ध विचारोंके छेद से स्वच्छ हुए मनके द्वारा कोई विरला ही पुण्यात्मा स्वात्मा का अभेदरूपसे अनुभव करता है ॥१४४॥
विशेषार्थ-स्वात्माकी उपलब्धिके लिए सबसे प्रथम भेदविज्ञान आवश्यक है । स्व और परका भेदविज्ञान हुए बिना स्वात्माकी उपलब्धि नहीं हो सकती । जो अपनेसे साक्षात् भिन्न स्त्री, पुत्र, धन, गृह आदि हैं उनसे अभिन्नताका भ्रम तो मोहमूलक है और उस मोहका मूल है शरीर आत्मा में एकत्वकी भ्रान्ति । यह भ्रान्ति यदि दूर हो जाये तो स्त्री, पुत्रादिकमें अभेदकी भ्रान्ति स्वतः दूर हो जायेगी । शरीर- आत्मा दूध और पानीकी तरह मिले हुए हैं किन्तु आत्मा चेतन है और शरीर अचेतन है | चेतन कभी अचेतन नहीं हो सकता और अचेतन चेतन नहीं हो सकता । दोनों दो स्वतन्त्र द्रव्य हैं । इस भेदज्ञानसे दोनोंको पृथक-पृथक निश्चय करके मनमें उठनेवाले राग-द्वेषमूलक सब विकल्पों को दूर करके निर्विकल्प मनके द्वारा स्वात्माकी उपलब्धि या अनुभूति होती है । किन्तु ऐसी अनुभूति करनेवाले बहुत ही विरल होते हैं। कहा है- जो पुरुष स्वयं अथवा परके उपदेश से किसी तरह भेदविज्ञानरूप मूल कारणवालो अविचल आत्मानुभूतिको प्राप्त करते हैं, वे ही पुरुष दर्पणकी तरह अपने आत्मामें प्रतिबिम्बित हुए अनन्त भावोंके स्वभावसे निरन्तर विकाररहित होते हैं अर्थात् उनके ज्ञानमें जो ज्ञेयोंके आकार प्रतिभासित होते हैं उनसे वे विकारको प्राप्त नहीं होते ' ॥ १४४ ॥
१. 'कथमपि हि लभन्ते भेदविज्ञानमूला
मचलितमनुभूति ये स्वतो वान्यतो वा ।
प्रतिफलन निमग्नानन्तभावस्वभाव
मुंकुरवदविकाराः संततं स्युस्त एव ॥ - समयसार कलश, २१ श्लो. ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org