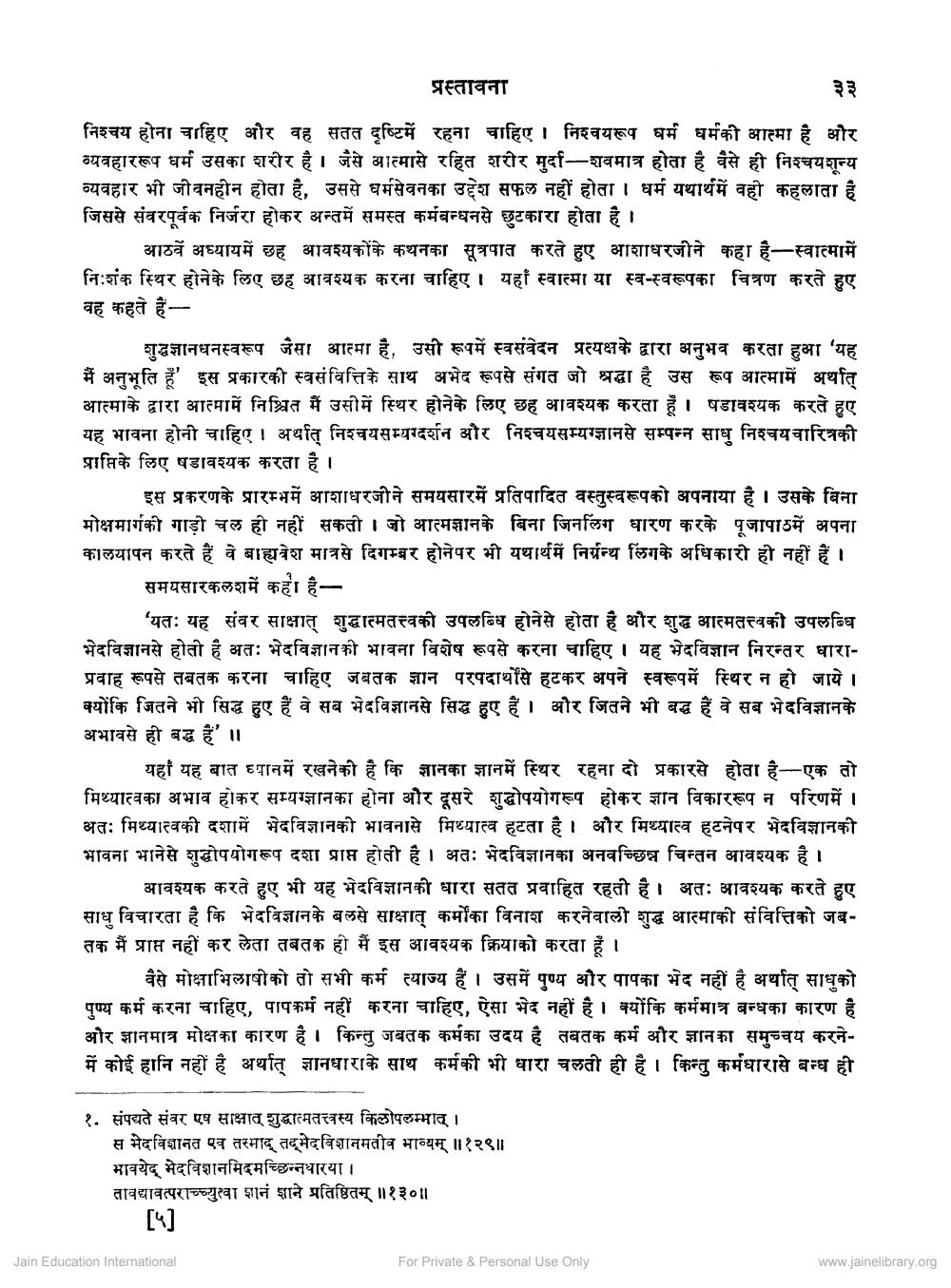________________
प्रस्तावना
निश्चय होना चाहिए और वह सतत दृष्टिमें रहना चाहिए। निश्चयरूप धर्म धर्मकी आत्मा है और व्यवहाररूप धर्म उसका शरीर है । जैसे आत्मासे रहित शरीर मुर्दा-शवमात्र होता है वैसे ही निश्चयशन्य व्यवहार भी जीवनहीन होता है, उससे धर्मसेवनका उद्देश सफल नहीं होता। धर्म यथार्थमें वही कहलाता है जिससे संवरपूर्वक निर्जरा होकर अन्तमें समस्त कर्मबन्धनसे छुटकारा होता है।
आठवें अध्यायमें छह आवश्यकोंके कथनका सूत्रपात करते हुए आशाधरजीने कहा है-स्वात्मामें निःशंक स्थिर होनेके लिए छह आवश्यक करना चाहिए । यहाँ स्वात्मा या स्व-स्वरूपका चित्रण करते हुए वह कहते हैं
शुद्धज्ञानधनस्वरूप जैसा आत्मा है, उसी रूपमें स्वसंवेदन प्रत्यक्षके द्वारा अनुभव करता हआ 'यह मैं अनुभूति हूँ' इस प्रकारको स्वसंवित्तिके साथ अभेद रूपसे संगत जो श्रद्धा है उस रूप आत्मामें अर्थात आत्माके द्वारा आत्मामें निश्चित मैं उसी में स्थिर होनेके लिए छह आवश्यक करता हूँ। षडावश्यक करते हुए यह भावना होनी चाहिए । अर्थात् निश्चयसम्यग्दर्शन और निश्चयसम्यग्ज्ञानसे सम्पन्न साधु निश्चयचारित्रकी प्राप्तिके लिए षडावश्यक करता है ।
इस प्रकरणके प्रारम्भमें आशाधरजीने समयसारमें प्रतिपादित वस्तुस्वरूपको अपनाया है । उसके बिना मोक्षमार्गको गाडी चल ही नहीं सकती। जो आत्मज्ञानके बिना जिनलिंग धारण करके पजापाठमें अपना कालयापन करते हैं वे बाह्यवेश मात्रसे दिगम्बर होनेपर भी यथार्थमें निर्ग्रन्थ लिंगके अधिकारी ही नहीं हैं।
समयसारकलशमें कहा है
'यतः यह संवर साक्षात् शुद्धात्मतत्त्वकी उपलब्धि होनेसे होता है और शुद्ध आत्मतत्त्वकी उपलब्धि भेदविज्ञानसे होती है अतः भेदविज्ञानको भावना विशेष रूपसे करना चाहिए । यह भेदविज्ञान निरन्तर धाराप्रवाह रूपसे तबतक करना चाहिए जबतक ज्ञान परपदार्थोसे हटकर अपने स्वरूप में स्थिर न हो जाये । क्योंकि जितने भी सिद्ध हुए हैं वे सब भेदविज्ञानसे सिद्ध हुए हैं। और जितने भी बद्ध हैं वे सब भेदविज्ञानके अभावसे ही बद्ध हैं।
यहाँ यह बात ध्यानमें रखने की है कि ज्ञानका ज्ञानमें स्थिर रहना दो प्रकारसे होता है-एक तो मिथ्यात्वका अभाव होकर सम्यग्ज्ञानका होना और दूसरे शुद्धोपयोगरूप होकर ज्ञान विकाररूप न परिणमें । अतः मिथ्यात्वकी दशामें भेदविज्ञानको भावनासे मिथ्यात्व हटता है। और मिथ्यात्व हटनेपर भेदविज्ञानकी भावना भानेसे शुद्धोपयोगरूप दशा प्राप्त होती है। अतः भेदविज्ञानका अनवच्छिन्न चिन्तन आवश्यक है।
आवश्यक करते हुए भी यह भेदविज्ञानको धारा सतत प्रवाहित रहती है। अतः आवश्यक करते हुए साध विचारता है कि भेदविज्ञानके बलसे साक्षात् कर्मोंका विनाश करनेवाली शुद्ध आत्माको संवित्तिको जबतक मैं प्राप्त नहीं कर लेता तबतक ही मैं इस आवश्यक क्रियाको करता हूँ।
वैसे मोक्षाभिलाषीको तो सभी कर्म त्याज्य हैं। उसमें पुण्य और पापका भेद नहीं है अर्थात् साधुको पुण्य कर्म करना चाहिए, पापकर्म नहीं करना चाहिए, ऐसा भेद नहीं है। क्योंकि कर्ममात्र बन्धका कारण है और ज्ञानमात्र मोक्षका कारण है। किन्तु जबतक कर्मका उदय है तबतक कर्म और ज्ञानका समुच्चय करनेमें कोई हानि नहीं है अर्थात ज्ञानधाराके साथ कर्मकी भी धारा चलती ही है। किन्तु कर्मधारासे बन्ध ही
१. संपद्यते संवर एष साक्षात् शुद्धात्मतत्वस्य किलोपलम्भात् ।
स भेद विज्ञानत एव तस्माद् तभेदविज्ञानमतीव भाव्यम् ॥१२९॥ भावयेद् भेद विज्ञानमिदमच्छिन्नधारया । तावद्यावत्पराच्छ्युत्वा शानं शाने प्रतिष्ठितम् ॥१३०॥
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org