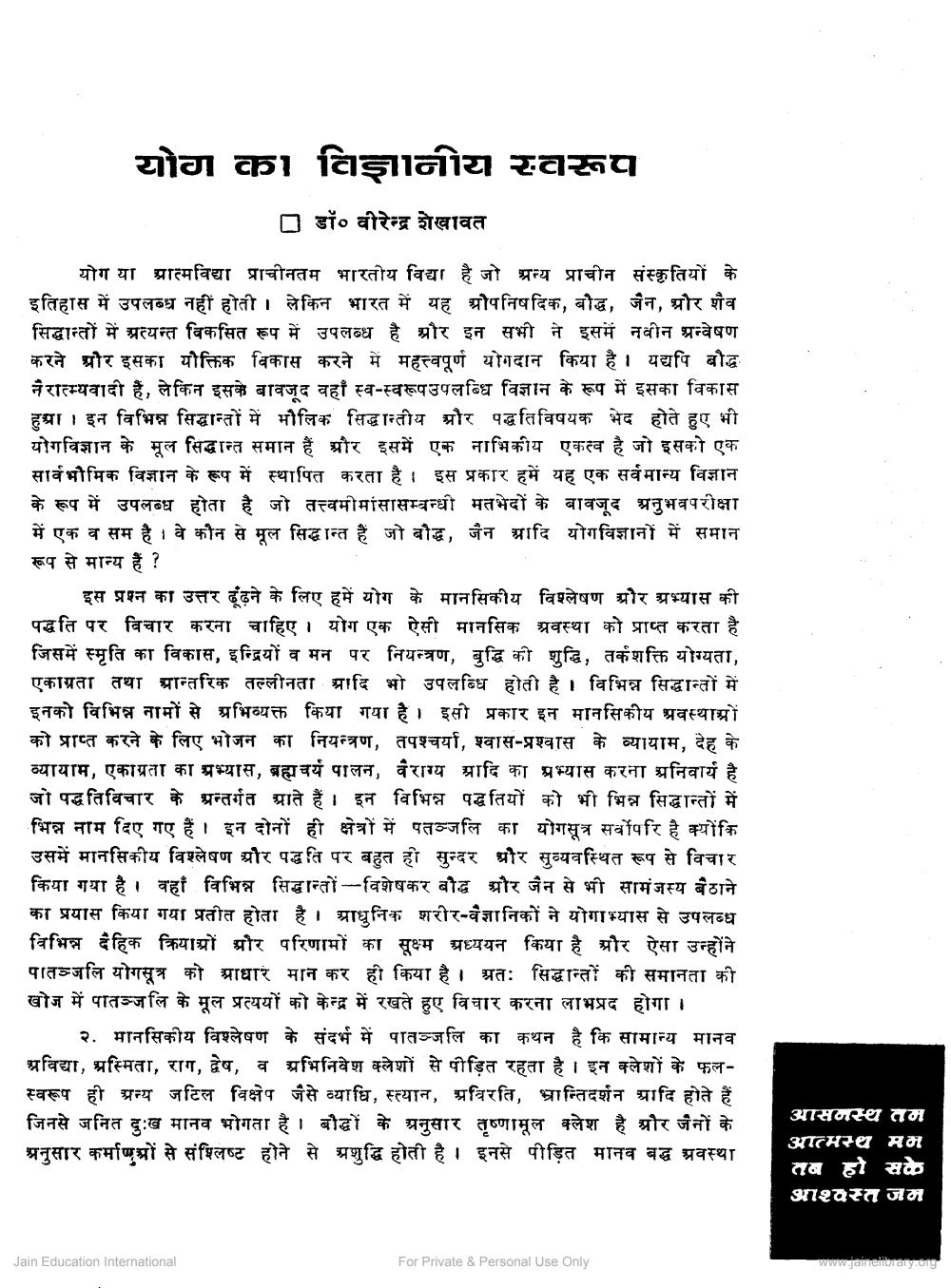Book Title: Yoga ka Vigyaniya Swarup Author(s): Virendra Shekhawat Publisher: Z_Umravkunvarji_Diksha_Swarna_Jayanti_Smruti_Granth_012035.pdf View full book textPage 1
________________ योग का विज्ञानीय स्वरूप ० डॉ० वीरेन्द्र शेखावत योग या प्रात्मविद्या प्राचीनतम भारतीय विद्या है जो अन्य प्राचीन संस्कृतियों के इतिहास में उपलब्ध नहीं होती। लेकिन भारत में यह प्रोपनिषदिक, बौद्ध, जैन, और शैव सिद्धान्तों में अत्यन्त विकसित रूप में उपलब्ध है और इन सभी ने इसमें नवीन अन्वेषण करने और इसका यौक्तिक विकास करने में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। यद्यपि बौद्ध नैरात्म्यवादी हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ स्व-स्वरूप उपलब्धि विज्ञान के रूप में इसका विकास हुअा । इन विभिन्न सिद्धान्तों में मौलिक सिद्धान्तीय और पद्धतिविषयक भेद होते हुए भी योगविज्ञान के मूल सिद्धान्त समान हैं और इसमें एक नाभिकीय एकत्व है जो इसको एक सार्वभौमिक विज्ञान के रूप में स्थापित करता है। इस प्रकार हमें यह एक सर्वमान्य विज्ञान के रूप में उपलब्ध होता है जो तत्त्वमीमांसासम्बन्धी मतभेदों के बावजूद अनुभवपरीक्षा में एक व सम है। वे कौन से मूल सिद्धान्त हैं जो बौद्ध, जैन आदि योगविज्ञानों में समान रूप से मान्य हैं ? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ़ने के लिए हमें योग के मानसिकीय विश्लेषण और अभ्यास की पद्धति पर विचार करना चाहिए। योग एक ऐसी मानसिक अवस्था को प्राप्त करता है जिसमें स्मृति का विकास, इन्द्रियों व मन पर नियन्त्रण, बुद्धि की शूद्धि, तर्कशक्ति योग्यता, एकाग्रता तथा प्रान्तरिक तल्लीनता आदि भो उपलब्धि होती है। विभिन्न सिद्धान्तों में इनको विभिन्न नामों से अभिव्यक्त किया गया है। इसी प्रकार इन मानसिकीय अवस्थानों को प्राप्त करने के लिए भोजन का नियन्त्रण, तपश्चर्या, श्वास-प्रश्वास के व्यायाम, देह के व्यायाम, एकाग्रता का अभ्यास, ब्रह्मचर्य पालन, वैराग्य प्रादि का अभ्यास करना अनिवार्य है जो पद्धतिविचार के अन्तर्गत पाते हैं। इन विभिन्न पद्धतियों को भी भिन्न सिद्धान्तों में भिन्न नाम दिए गए हैं। इन दोनों ही क्षेत्रों में पतञ्जलि का योगसत्र सर्वोपरि है क्योंकि उसमें मानसिकीय विश्लेषण और पद्धति पर बहुत ही सुन्दर और सुव्यवस्थित रूप से विचार किया गया है। वहाँ विभिन्न सिद्धान्तों-विशेषकर बौद्ध और जैन से भी सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया गया प्रतीत होता है। आधुनिक शरीर-वैज्ञानिकों ने योगाभ्यास से उपलब्ध विभिन्न दैहिक क्रियाओं और परिणामों का सूक्ष्म अध्ययन किया है और ऐसा उन्होंने पातञ्जलि योगसूत्र को आधार मान कर ही किया है। अतः सिद्धान्तों की समानता की खोज में पातञ्जलि के मूल प्रत्ययों को केन्द्र में रखते हुए विचार करना लाभप्रद होगा। २. मानसिकीय विश्लेषण के संदर्भ में पातञ्जलि का कथन है कि सामान्य मानव अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, व अभिनिवेश क्लेशों से पीड़ित रहता है। इन क्लेशों के फलस्वरूप ही अन्य जटिल विक्षेप जैसे व्याधि, स्त्यान, अविरति, भ्रान्तिदर्शन प्रादि होते हैं जिनसे जनित दु:ख मानव भोगता है। बौद्धों के अनुसार तृष्णामूल क्लेश है और जनों के अनुसार कर्माणों से संश्लिष्ट होने से अशुद्धि होती है । इनसे पीड़ित मानव बद्ध अवस्था आसनस्थ तम आत्मस्थ मम तब हो सके आश्वस्त जम Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jamembrary.orgPage Navigation
1 2 3