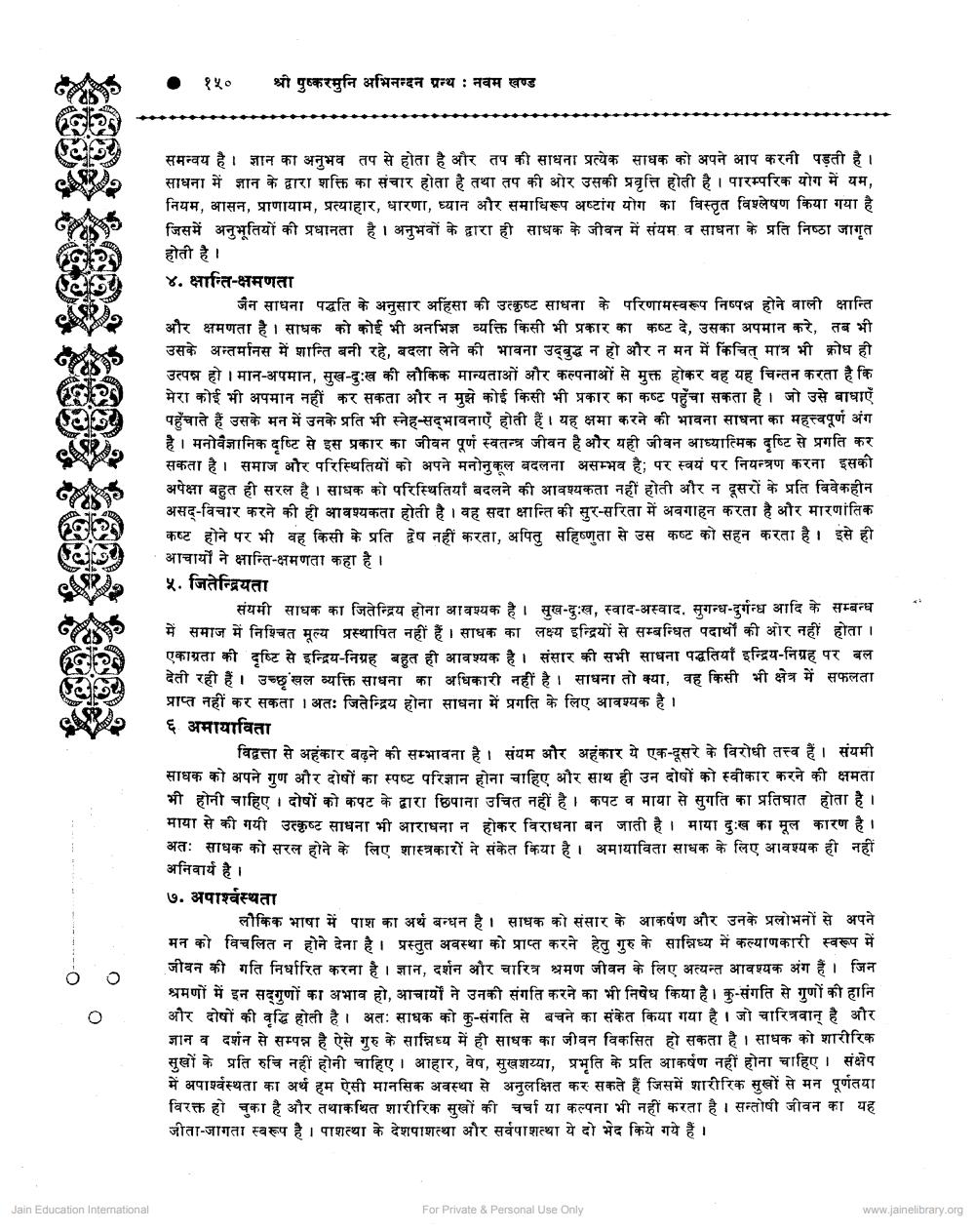Book Title: Yoga Sadhna Ek Paryavekshan Author(s): Fulchandra Jain Shatri Publisher: Z_Pushkarmuni_Abhinandan_Granth_012012.pdf View full book textPage 3
________________ १५० श्री पुष्करमुनि अभिनन्दन प्रन्थ : नवम खण्ड CE समन्वय है। ज्ञान का अनुभव तप से होता है और तप की साधना प्रत्येक साधक को अपने आप करनी पड़ती है। साधना में ज्ञान के द्वारा शक्ति का संचार होता है तथा तप की ओर उसकी प्रवृत्ति होती है । पारम्परिक योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधिरूप अष्टांग योग का विस्तृत विश्लेषण किया गया है जिसमें अनुभूतियों की प्रधानता है । अनुभवों के द्वारा ही साधक के जीवन में संयम व साधना के प्रति निष्ठा जागृत होती है। ४. क्षान्ति-क्षमणता जैन साधना पद्धति के अनुसार अहिंसा की उत्कृष्ट साधना के परिणामस्वरूप निष्पन्न होने वाली क्षान्ति और क्षमणता है। साधक को कोई भी अनभिज्ञ व्यक्ति किसी भी प्रकार का कष्ट दे, उसका अपमान करे, तब भी उसके अन्तर्मानस में शान्ति बनी रहे, बदला लेने की भावना उद्बुद्ध न हो और न मन में किंचित् मात्र भी क्रोध ही उत्पन्न हो । मान-अपमान, सुख-दुःख की लौकिक मान्यताओं और कल्पनाओं से मुक्त होकर वह यह चिन्तन करता है कि मेरा कोई भी अपमान नहीं कर सकता और न मुझे कोई किसी भी प्रकार का कष्ट पहुँचा सकता है। जो उसे बाधाएँ पहुँचाते हैं उसके मन में उनके प्रति भी स्नेह-सद्भावनाएं होती हैं। यह क्षमा करने की भावना साधना का महत्त्वपूर्ण अंग है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इस प्रकार का जीवन पूर्ण स्वतन्त्र जीवन है और यही जीवन आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगति कर सकता है। समाज और परिस्थितियों को अपने मनोनुकूल बदलना असम्भव है; पर स्वयं पर नियन्त्रण करना इसकी अपेक्षा बहुत ही सरल है। साधक को परिस्थितियाँ बदलने की आवश्यकता नहीं होती और न दूसरों के प्रति विवेकहीन असद्-विचार करने की ही आवश्यकता होती है। वह सदा क्षान्ति की सुर-सरिता में अवगाहन करता है और मारणांतिक कष्ट होने पर भी वह किसी के प्रति द्वेष नहीं करता, अपितु सहिष्णुता से उस कष्ट को सहन करता है। इसे ही आचार्यों ने क्षान्ति-क्षमणता कहा है। ५. जितेन्द्रियता संयमी साधक का जितेन्द्रिय होना आवश्यक है। सुख-दुःख, स्वाद-अस्वाद. सुगन्ध-दुर्गन्ध आदि के सम्बन्ध में समाज में निश्चित मूल्य प्रस्थापित नहीं हैं। साधक का लक्ष्य इन्द्रियों से सम्बन्धित पदार्थों की ओर नहीं होता। एकाग्रता की दृष्टि से इन्द्रिय-निग्रह बहुत ही आवश्यक है। संसार की सभी साधना पद्धतियाँ इन्द्रिय-निग्रह पर बल देती रही हैं। उच्छृखल व्यक्ति साधना का अधिकारी नहीं है। साधना तो क्या, वह किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता । अतः जितेन्द्रिय होना साधना में प्रगति के लिए आवश्यक है। ६ अमायाविता विद्वत्ता से अहंकार बढ़ने की सम्भावना है। संयम और अहंकार ये एक-दूसरे के विरोधी तत्त्व हैं। संयमी साधक को अपने गुण और दोषों का स्पष्ट परिज्ञान होना चाहिए और साथ ही उन दोषों को स्वीकार करने की क्षमता भी होनी चाहिए। दोषों को कपट के द्वारा छिपाना उचित नहीं है। कपट व माया से सुगति का प्रतिघात होता है। माया से की गयी उत्कृष्ट साधना भी आराधना न होकर विराधना बन जाती है। माया दुःख का मूल कारण है। अतः साधक को सरल होने के लिए शास्त्रकारों ने संकेत किया है। अमायाविता साधक के लिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। ७. अपार्श्वस्थता लौकिक भाषा में पाश का अर्थ बन्धन है। साधक को संसार के आकर्षण और उनके प्रलोभनों से अपने मन को विचलित न होने देना है। प्रस्तुत अवस्था को प्राप्त करने हेतु गुरु के सान्निध्य में कल्याणकारी स्वरूप में जीवन की गति निर्धारित करना है । ज्ञान, दर्शन और चारित्र श्रमण जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक अंग हैं। जिन श्रमणों में इन सद्गुणों का अभाव हो, आचार्यों ने उनकी संगति करने का भी निषेध किया है। कु-संगति से गुणों की हानि और दोषों की वृद्धि होती है। अतः साधक को कु-संगति से बचने का संकेत किया गया है । जो चारित्रवान् है और ज्ञान व दर्शन से सम्पन्न है ऐसे गुरु के सान्निध्य में ही साधक का जीवन विकसित हो सकता है। साधक को शारीरिक सुखों के प्रति रुचि नहीं होनी चाहिए। आहार, वेष, सुखशय्या, प्रभृति के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। संक्षेप में अपार्श्वस्थता का अर्थ हम ऐसी मानसिक अवस्था से अनुलक्षित कर सकते हैं जिसमें शारीरिक सुखों से मन पूर्णतया विरक्त हो चुका है और तथाकथित शारीरिक सुखों की चर्चा या कल्पना भी नहीं करता है । सन्तोषी जीवन का यह जीता-जागता स्वरूप है । पाशत्था के देशपाशत्था और सर्वपाशत्था ये दो भेद किये गये हैं। ०० Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4