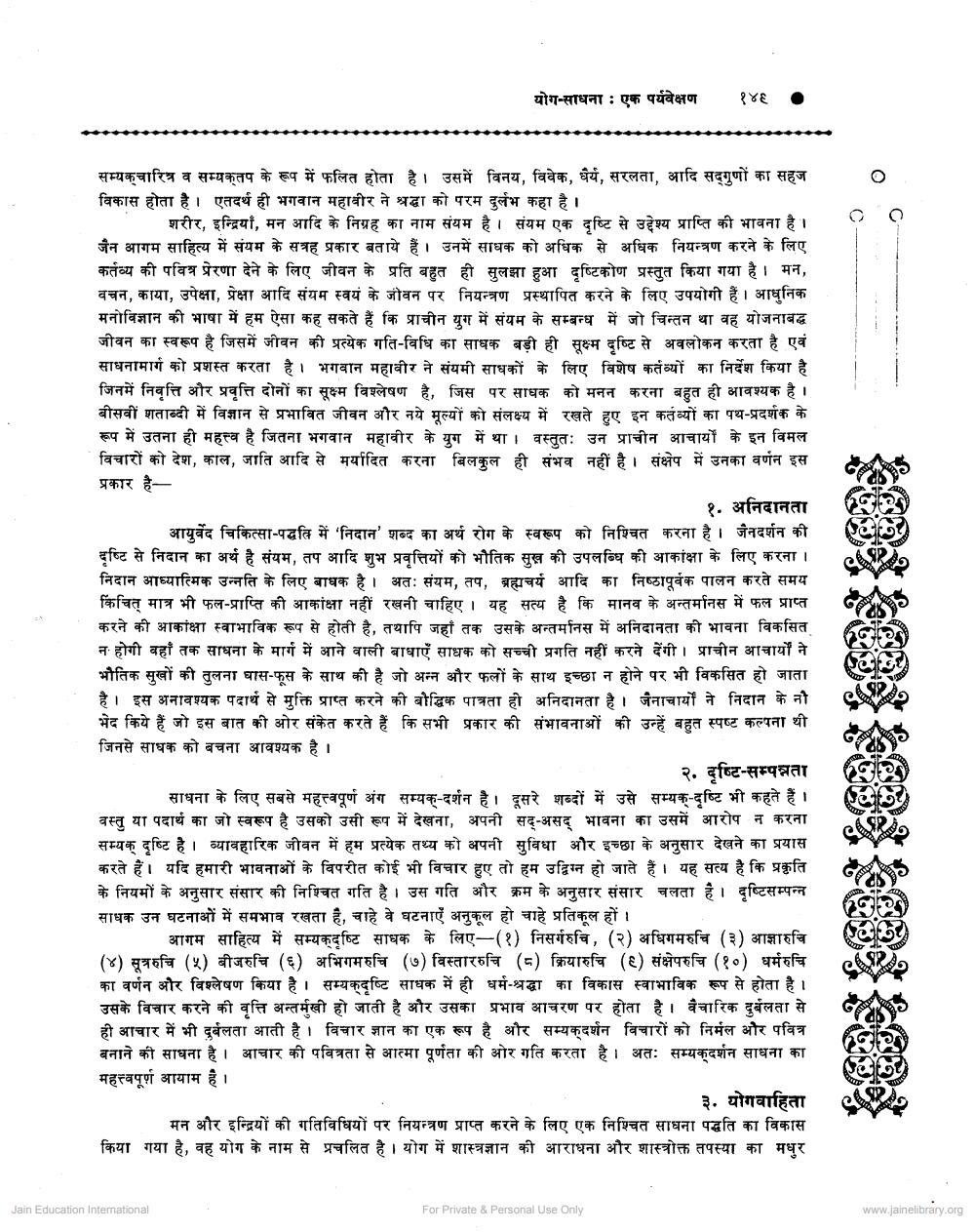Book Title: Yoga Sadhna Ek Paryavekshan Author(s): Fulchandra Jain Shatri Publisher: Z_Pushkarmuni_Abhinandan_Granth_012012.pdf View full book textPage 2
________________ योग-साधना : एक पर्यवेक्षण सम्यक्चारित्र व सम्यकृतप के रूप में फलित होता है। उसमें विनय, विवेक, धैर्य, सरलता, आदि सद्गुणों का सहज विकास होता है । एतदर्थ ही भगवान महावीर ने श्रद्धा को परम दुर्लभ कहा है । शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदि के निग्रह का नाम संयम है। संयम एक दृष्टि से उद्देश्य प्राप्ति की भावना है। जैन आगम साहित्य में संयम के सत्रह प्रकार बताये हैं । उनमें साधक को अधिक से अधिक नियन्त्रण करने के लिए कर्तव्य की पवित्र प्रेरणा देने के लिए जीवन के प्रति बहुत ही सुलझा हुआ दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। मन, वचन, काया, उपेक्षा, प्रेक्षा आदि संयम स्वयं के जीवन पर नियन्त्रण प्रस्थापित करने के लिए उपयोगी हैं। आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में हम ऐसा कह सकते हैं कि प्राचीन युग में संयम के सम्बन्ध में जो चिन्तन था वह योजनाबद्ध जीवन का स्वरूप है जिसमें जीवन की प्रत्येक गतिविधि का साधक बड़ी ही सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करता है एवं साधनामार्ग को प्रशस्त करता है। भगवान महावीर ने संयमी साधकों के लिए विशेष कर्तव्यों का निर्देश किया है जिनमें निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों का सूक्ष्म विश्लेषण है, जिस पर साधक को मनन करना बहुत ही आवश्यक है । बीसवीं शताब्दी में विज्ञान से प्रभावित जीवन और नये मूल्यों को संलक्ष्य में रखते हुए इन कर्तव्यों का पथ-प्रदर्शक के रूप में उतना ही महत्त्व है जितना भगवान महावीर के युग में था । वस्तुतः उन प्राचीन आचार्यों के इन विमल विचारों को देश, काल, जाति आदि से मर्यादित करना बिलकुल ही संभव नहीं है । संक्षेप में उनका वर्णन इस प्रकार है १४६ १. अनिदानता आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में 'निदान' शब्द का अर्थ रोग के स्वरूप को निश्चित करना है। जैनदर्शन की दृष्टि से निदान का अर्थ है संयम, तप आदि शुभ प्रवृत्तियों को भौतिक सुख की उपलब्धि की आकांक्षा के लिए करना । निदान आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाधक है। अतः संयम, तप, ब्रह्मचर्य आदि का निष्ठापूर्वक पालन करते समय किंचित् मात्र भी फल प्राप्ति की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। यह सत्य है कि मानव के अन्तर्मानस में फल प्राप्त करने की आकांक्षा स्वाभाविक रूप से होती है, तथापि जहाँ तक उसके अन्तर्मानस में अनिदानता की भावना विकसित न होगी वहाँ तक साधना के मार्ग में आने वाली बाधाएँ साधक को सच्ची प्रगति नहीं करने देंगी। प्राचीन आचार्यों ने भौतिक सुखों की तुलना घास-फूस के साथ की है जो अन्न और फलों के साथ इच्छा न होने पर भी विकसित हो जाता अनिदानता है। जैनाचार्यों ने निदान के नौ संभावनाओं की उन्हें बहुत स्पष्ट कल्पना थी है । इस अनावश्यक पदार्थ से मुक्ति प्राप्त करने की बौद्धिक पात्रता हो भेद किये हैं जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि सभी प्रकार की जिनसे साधक को बचना आवश्यक है । २. दृष्टि सम्पन्नता साधना के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण अंग सम्यक दर्शन है। दूसरे शब्दों में उसे सम्यक दृष्टि भी कहते हैं। वस्तु या पदार्थ का जो स्वरूप है उसको उसी रूप में देखना, अपनी सद्-असद् भावना का उसमें आरोप न करना सम्यक् दृष्टि है । व्यावहारिक जीवन में हम प्रत्येक तथ्य को अपनी सुविधा और इच्छा के अनुसार देखने का प्रयास करते हैं । यदि हमारी भावनाओं के विपरीत कोई भी विचार हुए तो हम उद्विग्न हो जाते हैं । यह सत्य है कि प्रकृति के नियमों के अनुसार संसार की निश्चित गति है । उस गति और क्रम के अनुसार संसार चलता है । दृष्टिसम्पन्न साधक उन घटनाओं में समभाव रखता है, चाहे वे घटनाएँ अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हों । आगम साहित्य में सम्यष्टि सामक के लिए (१) निसर्गरुचि, (२) अधिगमरुचि (३) आशारचि (४) सूत्ररुचि ( ५ ) बीजरुचि ( ६ ) अभिगमरुचि ( ७ ) विस्तार रुचि (८) क्रियारुचि ( ६ ) संक्षेपरुचि (१०) धर्मरुचि का वर्णन और विश्लेषण किया है । सम्यक्दृष्टि साधक में ही धर्म श्रद्धा का विकास स्वाभाविक रूप से होता है । उसके विचार करने की वृत्ति अन्तर्मुखी हो जाती है और उसका प्रभाव आचरण पर होता है। वैचारिक दुर्बलता से ही आचार में भी दुर्बलता आती है। विचार ज्ञान का एक रूप है और सम्यक्दर्शन विचारों को निर्मल और पवित्र बनाने की साधना है । आचार की पवित्रता से आत्मा पूर्णता की ओर गति करता है। अतः सम्यक्दर्शन साधना का महत्त्वपूर्ण आयाम है | Jain Education International ३. योगवाहिता मन और इन्द्रियों की गतिविधियों पर नियन्त्रण प्राप्त करने के लिए एक निश्चित साधना पद्धति का विकास किया गया है, वह योग के नाम से प्रचलित है। योग में शास्त्रज्ञान की आराधना और शास्त्रोक्त तपस्या का मधुर For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4