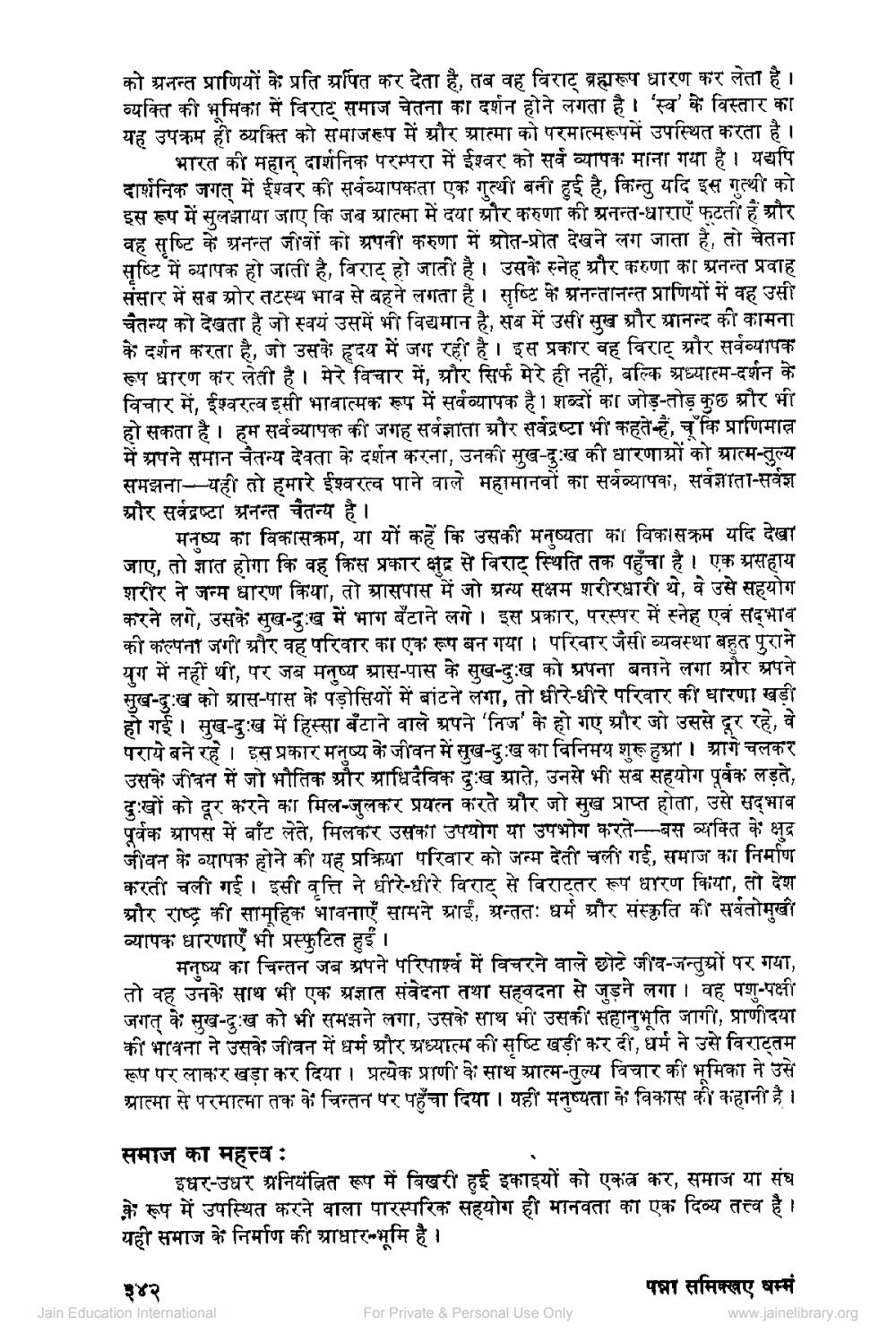Book Title: Vyakti Aur Samaj Author(s): Amarmuni Publisher: Z_Panna_Sammikkhaye_Dhammam_Part_01_003408_HR.pdf View full book textPage 2
________________ अनन्त प्राणियों के प्रति अर्पित कर देता है, तब वह विराट् ब्रह्मरूप धारण कर लेता है। व्यक्ति की भूमिका में विराट् समाज चेतना का दर्शन होने लगता है । 'स्व' के विस्तार का यह उपक्रम ही व्यक्ति को समाजरूप में और आत्मा को परमात्मरूपमें उपस्थित करता है । भारत की महान् दार्शनिक परम्परा में ईश्वर को सर्व व्यापक माना गया है । यद्यपि दार्शनिक जगत में ईश्वर की सर्वव्यापकता एक गुत्थी बनी हुई है, किन्तु यदि इस गुत्थी को इस रूप में सुलझाया जाए कि जब आत्मा में दया और करुणा की अनन्त धाराएँ फटती हैं और वह सृष्टि के अनन्त जीवों को अपनी करुणा में प्रोत-प्रोत देखने लग जाता है, तो चेतना सृष्टि में व्यापक हो जाती है, विराट् हो जाती है। उसके स्नेह और करुणा का अनन्त प्रवाह संसार में सब ओर तटस्थ भाव से बहने लगता है । सृष्टि के अनन्तानन्त प्राणियों में वह उसी चैतन्य को देखता है जो स्वयं उसमें भी विद्यमान है, सब में उसी सुख और आनन्द की कामना के दर्शन करता है, जो उसके हृदय में जग रही है। इस प्रकार वह विराट् और सर्वव्यापक रूप धारण कर लेती है। मेरे विचार में, और सिर्फ मेरे ही नहीं, बल्कि अध्यात्म-दर्शन के विचार में, ईश्वरत्व इसी भावात्मक रूप में सर्वव्यापक है । शब्दों का जोड़-तोड़ कुछ और भी हो सकता है । हम सर्वव्यापक की जगह सर्वज्ञाता और सर्वद्रष्टा भी कहते हैं, चूँ कि प्राणिमात्र समान चैतन्य देवता के दर्शन करना, उनकी सुख-दुःख की धारणाओं को प्रात्म-तुल्य समझना - यही तो हमारे ईश्वरत्व पाने वाले महामानवों का सर्वव्यापक, सर्वज्ञाता - सर्वश और सर्वद्रष्टा अनन्त चैतन्य है । मनुष्य का विकासक्रम, या यों कहें कि उसकी मनुष्यता का विकासक्रम यदि देखा जाए, तो ज्ञात होगा कि वह किस प्रकार क्षुद्र से विराट् स्थिति तक पहुँचा है । एक असहाय शरीर ने जन्म धारण किया, तो आसपास में जो अन्य सक्षम शरीरधारी थे, वे उसे सहयोग करने लगे, उसके सुख-दुःख में भाग बँटाने लगे। इस प्रकार, परस्पर में स्नेह एवं सद्भाव कल्पना जगी और वह परिवार का एक रूप बन गया। परिवार जैसी व्यवस्था बहुत पुराने युग में नहीं थी, पर जब मनुष्य प्रास-पास के सुख-दुःख को अपना बनाने लगा और अपने सुख-दुःख को आस-पास के पड़ोसियों में बांटने लगा, तो धीरे-धीरे परिवार की धारणा खड़ी हो गई। सुख-दुःख में हिस्सा बँटाने वाले अपने 'निज' के हो गए और जो उससे दूर रहे, वे परा बने रहे। इस प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख-दुःख का विनिमय शुरू हुआ। आगे चलकर उसके जीवन में जो भौतिक और आधिदैविक दुःख आते, उनसे भी सब सहयोग पूर्वक लड़ते, दुःखों को दूर करने का मिल-जुलकर प्रयत्न करते और जो सुख प्राप्त होता, उसे सद्भाव पूर्वक आपस में बाँट लेते, मिलकर उसका उपयोग या उपभोग करते - बस व्यक्ति के क्षुद्र जीवन के व्यापक होने की यह प्रक्रिया परिवार को जन्म देती चली गई, समाज का निर्माण करती चली गई । इसी वृत्ति ने धीरे-धीरे विराट् से विराट्तर रूप धारण किया, तो देश और राष्ट्र की सामूहिक भावनाएँ सामने आईं, अन्तत: धर्म और संस्कृति की सर्वतोमुखी व्यापक धारणाएँ भी प्रस्फुटित हुईं। मनुष्य का चिन्तन जब अपने परिपार्श्व में विचरने वाले छोटे जीव-जन्तुनों पर गया, तो वह उनके साथ भी एक अज्ञात संवेदना तथा सहवदना से जुड़ने लगा । वह पशु-पक्षी जगत् के सुख-दुःख को भी समझने लगा, उसके साथ भी उसकी सहानुभूति जागी, प्राणीदया की भावना ने उसके जीवन में धर्म और अध्यात्म की सृष्टि खड़ी कर दी, धर्म ने उसे विराट्तम रूप पर लाकर खड़ा कर दिया। प्रत्येक प्राणी के साथ आत्म-तुल्य विचार की भूमिका ने उसे श्रात्मा से परमात्मा तक के चिन्तन पर पहुँचा दिया। यही मनुष्यता के विकास की कहानी है । समाज का महत्त्व : इधर-उधर नियंत्रित रूप में बिखरी हुई इकाइयों को एकत्र कर, समाज या संघ के रूप 'उपस्थित करने वाला पारस्परिक सहयोग ही मानवता का एक दिव्य तत्त्व है । यही समाज के निर्माण की आधार भूमि है । ३४२ Jain Education International For Private & Personal Use Only पन्ना समिक्ख धम्मं www.jainelibrary.org.Page Navigation
1 2 3 4 5 6 7