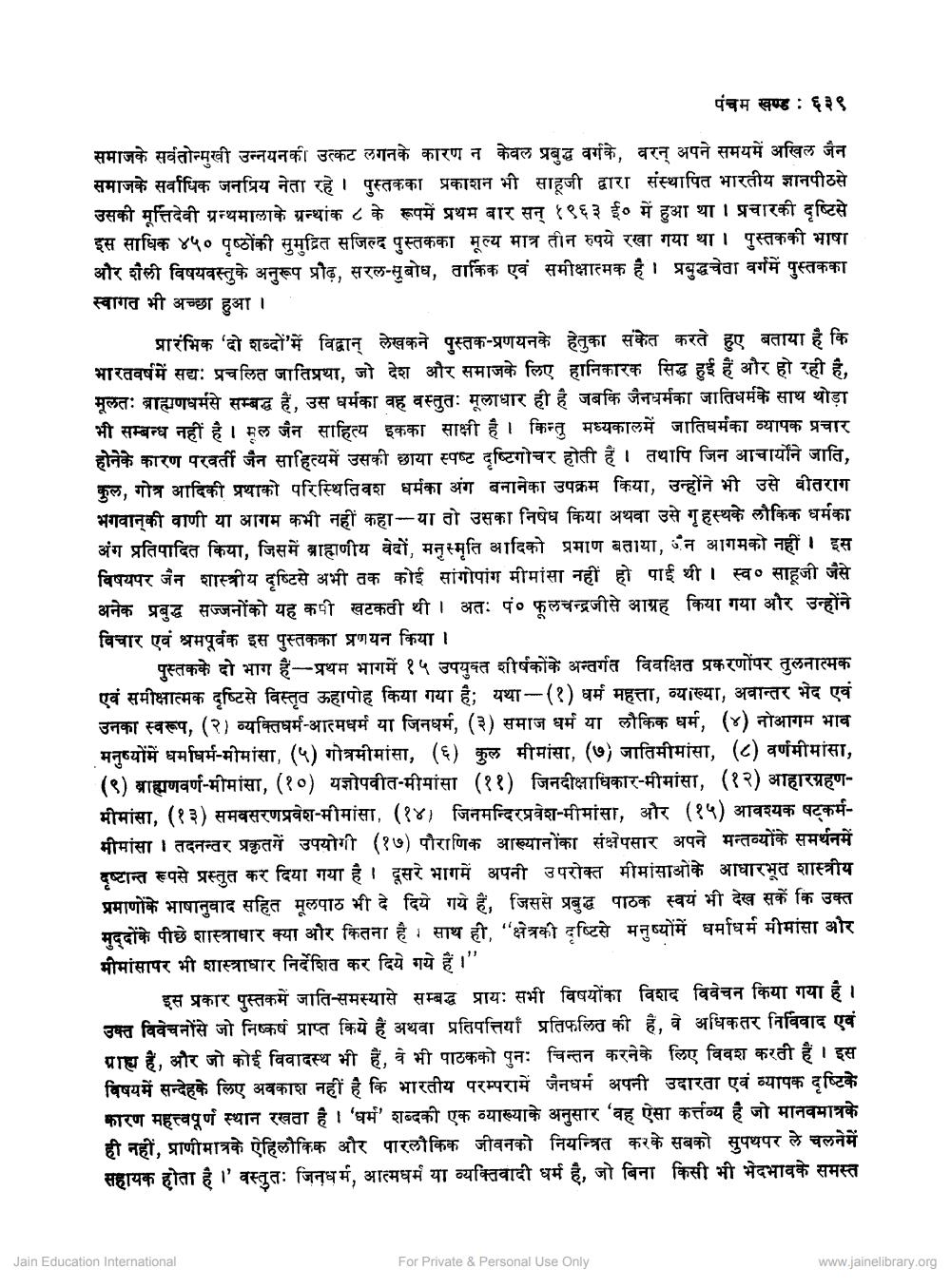Book Title: Varna Jati aur Dharm ek Chintan Author(s): Jyoti Prasad Jain Publisher: Z_Fulchandra_Shastri_Abhinandan_Granth_012004.pdf View full book textPage 2
________________ पंचम खण्ड: ६३९ समाजके सर्वतोन्मुखी उन्नयनकी उत्कट लगनके कारण न केवल प्रबुद्ध वर्गके, वरन् अपने समयमें अखिल जैन समाजके सर्वाधिक जनप्रिय नेता रहे। पुस्तकका प्रकाशन भी साहजी द्वारा संस्थापित भारतीय ज्ञानपीठसे उसकी मूत्तिदेवी ग्रन्थमालाके ग्रन्थांक ८ के रूपमें प्रथम बार सन् १९६३ ई० में हुआ था । प्रचारकी दृष्टिसे इस साधिक ४५० पृष्ठोंकी सुमुद्रित सजिल्द पुस्तकका मूल्य मात्र तीन रुपये रखा गया था। पुस्तककी भाषा और शैली विषयवस्तु के अनुरूप प्रौढ़, सरल-सुबोध, तार्किक एवं समीक्षात्मक है। प्रबुद्धचेता वर्ग में पुस्तकका स्वागत भी अच्छा हुआ। प्रारंभिक 'दो शब्दों में विद्वान लेखकने पुस्तक-प्रणयनके हेतुका संकेत करते हए बताया है कि भारतवर्ष में सद्यः प्रचलित जातिप्रथा, जो देश और समाजके लिए हानिकारक सिद्ध हुई हैं और हो रही है, मूलतः ब्राह्मणधर्मसे सम्बद्ध हैं, उस धर्मका वह वस्तुतः मूलाधार ही है जबकि जैनधर्मका जातिधर्मके साथ थोड़ा भी सम्बन्ध नहीं है । मल जैन साहित्य इकका साक्षी है। किन्तु मध्यकालमें जातिधर्मका व्यापक प्रचार होनेके कारण परवर्ती जैन साहित्यमें उसकी छाया स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं । तथापि जिन आचार्योंने जाति, कुल, गोत्र आदिकी प्रथाको परिस्थितिवश धर्मका अंग बनानेका उपक्रम किया, उन्होंने भी उसे वीतराग भगवान्की वाणी या आगम कभी नहीं कहा-या तो उसका निषेध किया अथवा उसे गृहस्थके लौकिक धर्मका अंग प्रतिपादित किया, जिसमें ब्राहाणीय वेदों, मनुस्मति आदिको प्रमाण बताया, न आगमको नहीं। इस विषयपर जैन शास्त्रीय दृष्टिसे अभी तक कोई सांगोपांग मीमांसा नहीं हो पाई थी। स्व० साहजी जैसे क प्रबुद्ध सज्जनोंको यह कपी खटकती थी। अतः ५० फूलचन्द्रजीसे आग्रह किया गया और उन्होंने विचार एवं श्रमपूर्वक इस पुस्तकका प्रणयन किया । पुस्तकके दो भाग है-प्रथम भागमें १५ उपयुक्त शीर्षकोंके अन्तर्गत विवक्षित प्रकरणोंपर तुलनात्मक एवं समीक्षात्मक दृष्टिसे विस्तृत ऊहापोह किया गया है; यथा-(१) धर्म महत्ता, व्याख्या, अवान्तर भेद एवं उनका स्वरूप, (२) व्यक्तिधर्म-आत्मधर्म या जिनधर्म, (३) समाज धर्म या लौकिक धर्म, (४) नोआगम भाव मनुष्योंमें धर्माधर्म-मीमांसा, (५) गोत्रमीमांसा, (६) कुल मीमांसा, (७) जातिमीमांसा, (८) वर्णमीमांसा, (९) ब्राह्मणवर्ण-मीमांसा, (१०) यज्ञोपवीत-मीमांसा (११) जिनदीक्षाधिकार-मीमांसा, (१२) आहारग्रहणमीमांसा, (१३) समवसरणप्रवेश-मीमांसा, (१४) जिनमन्दिरप्रवेश-मीमांसा, और (१५) आवश्यक षट्कर्ममीमांसा । तदनन्तर प्रकृतमें उपयोगी (१७) पौराणिक आख्यानोंका संक्षेपसार अपने मन्तव्योंके समर्थनमें दृष्टान्त रूपसे प्रस्तुत कर दिया गया है। दूसरे भागमें अपनी उपरोक्त मीमांसाओंके आधारभूत शास्त्रीय प्रमाणोंके भाषानुवाद सहित मूलपाठ भी दे दिये गये हैं, जिससे प्रबुद्ध पाठक स्वयं भी देख सकें कि उक्त मददोंके पीछे शास्त्राधार क्या और कितना है। साथ ही. "क्षेत्रकी दष्टिसे मनुष्योंमें धर्माधर्म मीमांसा और मीमांसापर भी शास्त्राधार निर्देशित कर दिये गये हैं।" इस प्रकार पुस्तकमें जाति-समस्यासे सम्बद्ध प्रायः सभी विषयोंका विशद विवेचन किया गया है। उक्त विवेचनोंसे जो निष्कर्ष प्राप्त किये हैं अथवा प्रतिपत्तियाँ प्रतिफलित की है, वे अधिकतर निर्विवाद एवं प्राह्य है, और जो कोई विवादस्थ भी है, वे भी पाठकको पुनः चिन्तन करनेके लिए विवश करती हैं । इस विषयमें सन्देहके लिए अवकाश नहीं है कि भारतीय परम्परामें जैनधर्म अपनी उदारता एवं व्यापक दृष्टिके कारण महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । 'धर्म' शब्दकी एक व्याख्याके अनुसार 'वह ऐसा कर्तव्य है जो मानवमात्रके ही नहीं, प्राणीमात्रके ऐहिलौकिक और पारलौकिक जीवनको नियन्त्रित करके सबको सुपथपर ले चलने में सहायक होता है । वस्तुतः जिनधर्म, आत्मधर्म या व्यक्तिवादी धर्म है, जो बिना किसी भी भेदभावके समस्त Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5