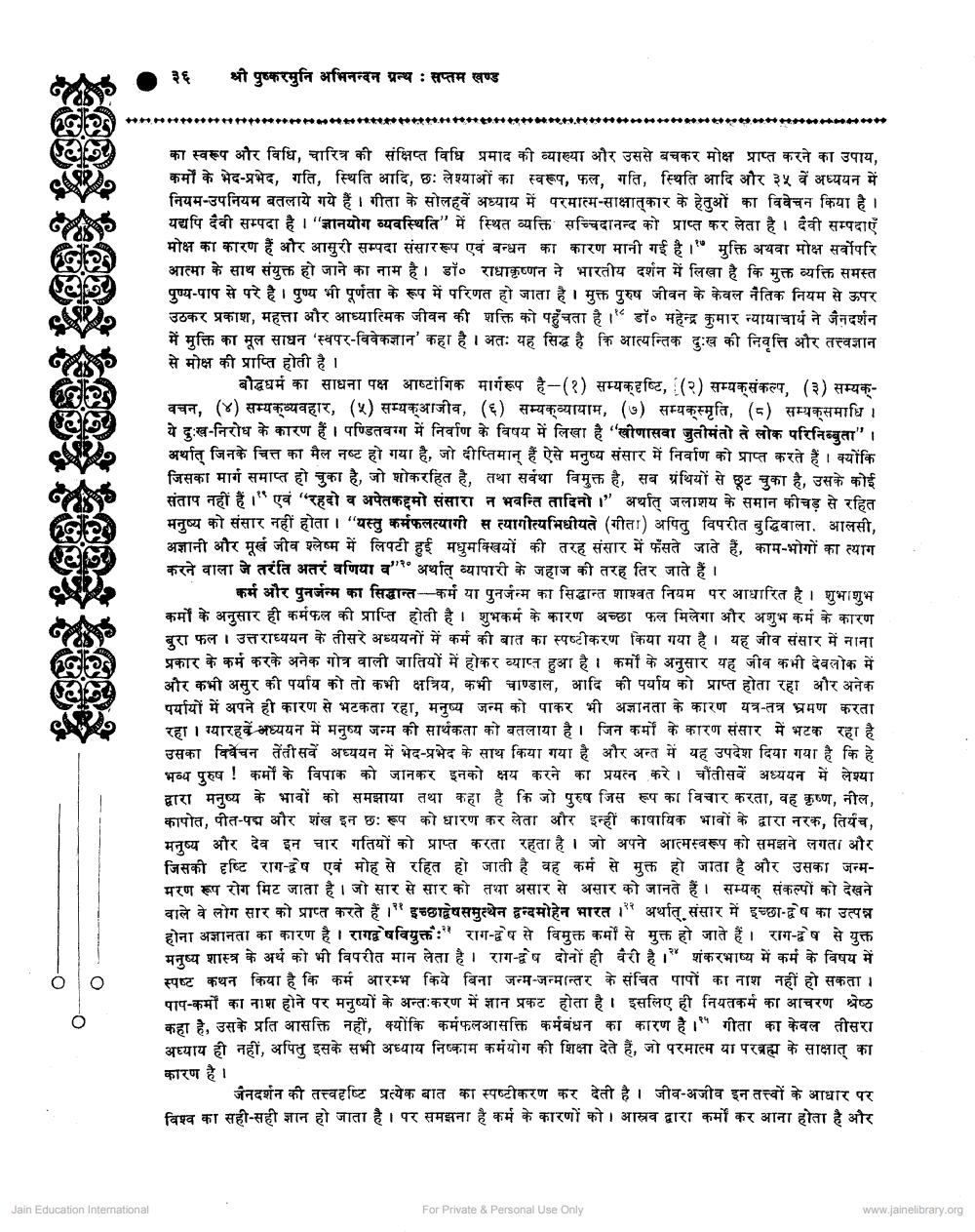Book Title: Uttaradhyayan Geeta aur Dhammapada Ek Tulna Author(s): Udaychandra Publisher: Z_Pushkarmuni_Abhinandan_Granth_012012.pdf View full book textPage 4
________________ .३६ श्री पुष्करमुनि अभिनन्दन ग्रन्थ : सप्तम खण्ड RA का स्वरूप और विधि, चारित्र की संक्षिप्त विधि प्रमाद की व्याख्या और उससे बचकर मोक्ष प्राप्त करने का उपाय, कर्मों के भेद-प्रभेद, गति, स्थिति आदि, छः लेश्याओं का स्वरूप, फल, गति, स्थिति आदि और ३५ वें अध्ययन में नियम-उपनियम बतलाये गये हैं। गीता के सोलहवें अध्याय में परमात्म-साक्षात्कार के हेतुओं का विवेचन किया है। यद्यपि दैवी सम्पदा है । "ज्ञानयोग व्यवस्थिति" में स्थित व्यक्ति सच्चिदानन्द को प्राप्त कर लेता है। देवी सम्पदाएँ मोक्ष का कारण हैं और आसुरी सम्पदा संसाररूप एवं बन्धन का कारण मानी गई है। मुक्ति अथवा मोक्ष सर्वोपरि आत्मा के साथ संयुक्त हो जाने का नाम है। डॉ० राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन में लिखा है कि मुक्त व्यक्ति समस्त पुण्य-पाप से परे है। पुण्य भी पूर्णता के रूप में परिणत हो जाता है। मुक्त पुरुष जीवन के केवल नैतिक नियम से ऊपर उठकर प्रकाश, महत्ता और आध्यात्मिक जीवन की शक्ति को पहुँचता है। डॉ० महेन्द्र कुमार न्यायाचार्य ने जनदर्शन में मुक्ति का मूल साधन 'स्वपर-विवेकज्ञान' कहा है । अतः यह सिद्ध है कि आत्यन्तिक दुःख की निवृत्ति और तत्त्वज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है । बौद्धधर्म का साधना पक्ष आष्टांगिक मार्गरूप है-(१) सम्यक्दृष्टि, (२) सम्यक्संकल्प, (३) सम्यक्वचन, (४) सम्यक्व्यवहार, (५) सम्यक्आजीव, (६) सम्यव्यायाम, (७) सम्यकस्मृति, (८) सम्यक्समाधि । ये दुःख-निरोध के कारण हैं । पण्डितवग्ग में निर्वाण के विषय में लिखा है "खीणासवा जुतीमंतो ते लोक परिनिब्बुता"। अर्थात् जिनके चित्त का मैल नष्ट हो गया है, जो दीप्तिमान् हैं ऐसे मनुष्य संसार में निर्वाण को प्राप्त करते हैं। क्योंकि जिसका मार्ग समाप्त हो चुका है, जो शोकरहित है, तथा सर्वथा विमुक्त है, सब ग्रंथियों से छूट चुका है, उसके कोई संताप नहीं हैं।" एवं "रहदो व अपेतकद्दमो संसारा न भवन्ति तादिनो।" अर्थात् जलाशय के समान कीचड़ से रहित मनुष्य को संसार नहीं होता। “यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागोत्यभिधीयते (गीता) अपितु विपरीत बुद्धिवाला. आलसी, अज्ञानी और मूर्ख जीव श्लेष्म में लिपटी हुई मधुमक्खियों की तरह संसार में फंसते जाते हैं, काम-भोगों का त्याग करने वाला जे तरंति अतरं वणिया व"२० अर्थात् व्यापारी के जहाज की तरह तिर जाते हैं। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धान्त-कर्म या पुनर्जन्म का सिद्धान्त शाश्वत नियम पर आधारित है। शुभाशुभ कर्मों के अनुसार ही कर्मफल की प्राप्ति होती है। शुभकर्म के कारण अच्छा फल मिलेगा और अशुभ कर्म के कारण बुरा फल । उत्तराध्ययन के तीसरे अध्ययनों में कर्म की बात का स्पष्टीकरण किया गया है। यह जीव संसार में नाना प्रकार के कर्म करके अनेक गोत्र वाली जातियों में होकर व्याप्त हुआ है। कर्मों के अनुसार यह जीव कभी देवलोक में और कभी असुर की पर्याय को तो कभी क्षत्रिय, कभी चाण्डाल, आदि की पर्याय को प्राप्त होता रहा और अनेक पर्यायों में अपने ही कारण से भटकता रहा, मनुष्य जन्म को पाकर भी अज्ञानता के कारण यत्र-तत्र भ्रमण करता रहा । ग्यारहवें अध्ययन में मनुष्य जन्म की सार्थकता को बतलाया है। जिन कर्मों के कारण संसार में भटक रहा है उसका विवेचन तेंतीसवें अध्ययन में भेद-प्रभेद के साथ किया गया है और अन्त में यह उपदेश दिया गया है कि हे भव्य पुरुष ! कर्मों के विपाक को जानकर इनको क्षय करने का प्रयत्न करे। चौंतीसवें अध्ययन में लेश्या द्वारा मनुष्य के भावों को समझाया तथा कहा है कि जो पुरुष जिस रूप का विचार करता, वह कृष्ण, नील, कापोत, पीत-पद्म और शंख इन छ: रूप को धारण कर लेता और इन्हीं काषायिक भावों के द्वारा नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव इन चार गतियों को प्राप्त करता रहता है । जो अपने आत्मस्वरूप को समझने लगता और जिसकी दृष्टि राग-द्वेष एवं मोह से रहित हो जाती है वह कर्म से मुक्त हो जाता है और उसका जन्ममरण रूप रोग मिट जाता है। जो सार से सार को तथा असार से असार को जानते हैं। सम्यक् संकल्पों को देखने वाले वे लोग सार को प्राप्त करते हैं । इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्दमोहेन भारत । अर्थात् संसार में इच्छा-द्वेष का उत्पन्न होना अज्ञानता का कारण है । रागद्वषवियुक्त:" राग-द्वेष से विमुक्त कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। राग-द्वेष से युक्त मनुष्य शास्त्र के अर्थ को भी विपरीत मान लेता है। राग-द्वेष दोनों ही वैरी है।" शंकरभाष्य में कर्म के विषय में स्पष्ट कथन किया है कि कर्म आरम्भ किये बिना जन्म-जन्मान्तर के संचित पापों का नाश नहीं हो सकता। पाप-कर्मों का नाश होने पर मनुष्यों के अन्तःकरण में ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए ही नियतकर्म का आचरण श्रेष्ठ कहा है, उसके प्रति आसक्ति नहीं, क्योंकि कर्मफलआसक्ति कर्मबंधन का कारण है। गीता का केवल तीसरा अध्याय ही नहीं, अपितु इसके सभी अध्याय निष्काम कर्मयोग की शिक्षा देते हैं, जो परमात्म या परब्रह्म के साक्षात् का कारण है। जैनदर्शन की तत्त्वदृष्टि प्रत्येक बात का स्पष्टीकरण कर देती है। जीव-अजीव इन तत्त्वों के आधार पर विश्व का सही-सही ज्ञान हो जाता है। पर समझना है कर्म के कारणों को। आस्रव द्वारा कर्मों कर आना होता है और ०० Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6