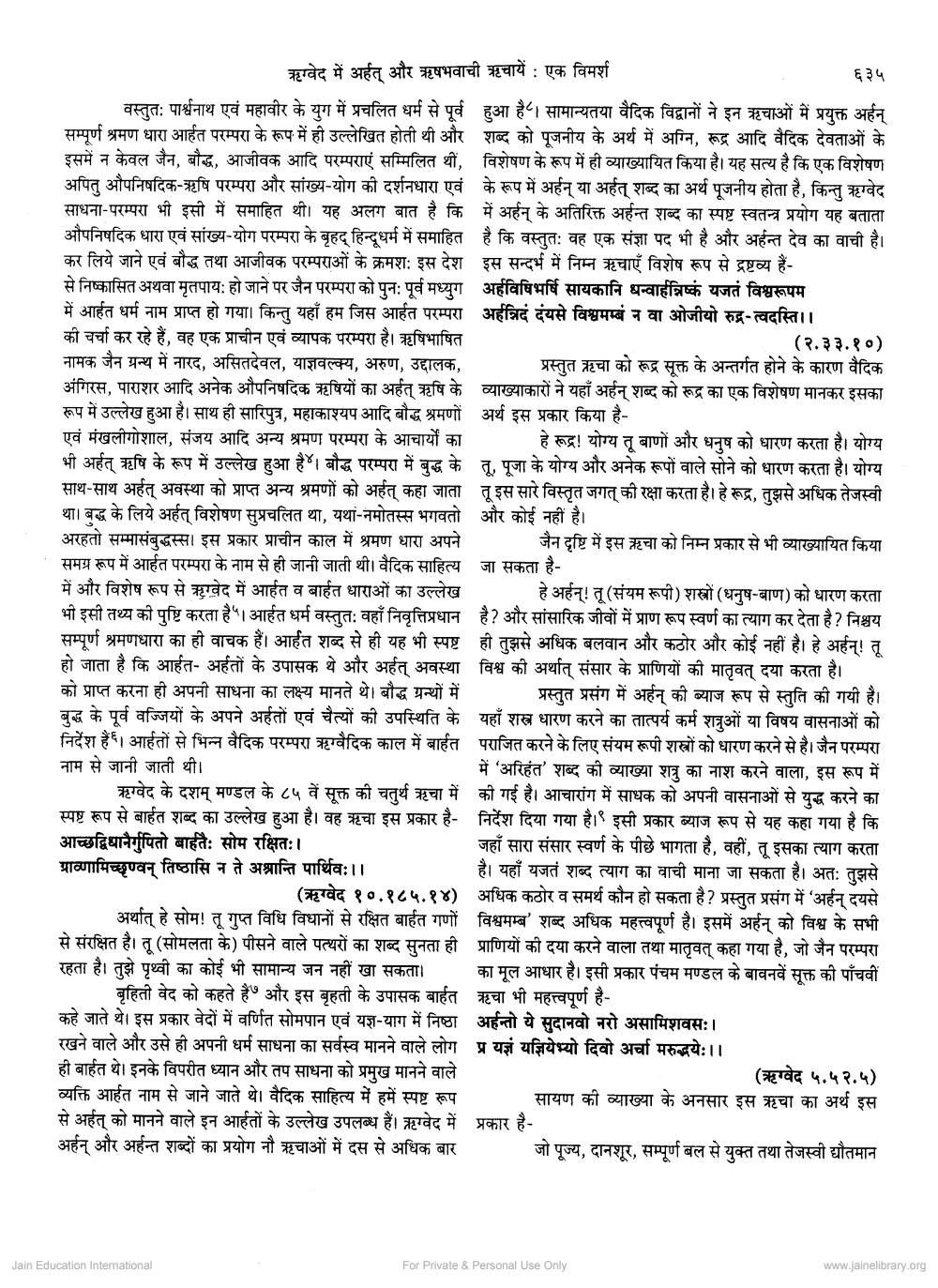Book Title: Swetambar Mulsangh evam Mathursangh ek Vimarsh Author(s): Sagarmal Jain Publisher: Z_Shwetambar_Sthanakvasi_Jain_Sabha_Hirak_Jayanti_Granth_012052.pdf View full book textPage 6
________________ ऋग्वेद में अर्हत् और ऋषभवाची ऋचायें : एक विमर्श ६३५ वस्तुतः पार्श्वनाथ एवं महावीर के युग में प्रचलित धर्म से पूर्व हुआ है। सामान्यतया वैदिक विद्वानों ने इन ऋचाओं में प्रयुक्त अर्हन् सम्पूर्ण श्रमण धारा आर्हत परम्परा के रूप में ही उल्लेखित होती थी और शब्द को पूजनीय के अर्थ में अग्नि, रूद्र आदि वैदिक देवताओं के इसमें न केवल जैन, बौद्ध, आजीवक आदि परम्पराएं सम्मिलित थीं, विशेषण के रूप में ही व्याख्यायित किया है। यह सत्य है कि एक विशेषण अपितु औपनिषदिक-ऋषि परम्परा और सांख्य-योग की दर्शनधारा एवं के रूप में अर्हन् या अर्हत् शब्द का अर्थ पूजनीय होता है, किन्तु ऋग्वेद साधना-परम्परा भी इसी में समाहित थी। यह अलग बात है कि में अर्हन् के अतिरिक्त अर्हन्त शब्द का स्पष्ट स्वतन्त्र प्रयोग यह बताता औपनिषदिक धारा एवं सांख्य-योग परम्परा के बृहद् हिन्दूधर्म में समाहित है कि वस्तुत: वह एक संज्ञा पद भी है और अर्हन्त देव का वाची है। कर लिये जाने एवं बौद्ध तथा आजीवक परम्पराओं के क्रमश: इस देश इस सन्दर्भ में निम्न ऋचाएँ विशेष रूप से द्रष्टव्य हैंसे निष्कासित अथवा मृतपाय: हो जाने पर जैन परम्परा को पुन: पूर्व मध्युग अर्हविषिभर्षि सायकानि धन्वाहन्निष्कं यजतं विश्वरूपम में आर्हत धर्म नाम प्राप्त हो गया। किन्तु यहाँ हम जिस आहेत परम्परा अर्हन्निदं दयसे विश्वमम्बं न वा ओजीयो रुद्र-त्वदस्ति।। की चर्चा कर रहे हैं, वह एक प्राचीन एवं व्यापक परम्परा है। ऋषिभाषित (२.३३.१०) नामक जैन ग्रन्थ में नारद, असितदेवल, याज्ञवल्क्य, अरुण, उद्दालक, प्रस्तुत ऋचा को रूद्र सूक्त के अन्तर्गत होने के कारण वैदिक अंगिरस, पाराशर आदि अनेक औपनिषदिक ऋषियों का अर्हत् ऋषि के व्याख्याकारों ने यहाँ अर्हन् शब्द को रूद्र का एक विशेषण मानकर इसका रूप में उल्लेख हुआ है। साथ ही सारिपुत्र, महाकाश्यप आदि बौद्ध श्रमणों अर्थ इस प्रकार किया हैएवं मंखलीगोशाल, संजय आदि अन्य श्रमण परम्परा के आचार्यों का हे रूद्र! योग्य तू बाणों और धनुष को धारण करता है। योग्य भी अर्हत् ऋषि के रूप में उल्लेख हुआ है। बौद्ध परम्परा में बुद्ध के तू, पूजा के योग्य और अनेक रूपों वाले सोने को धारण करता है। योग्य साथ-साथ अर्हत् अवस्था को प्राप्त अन्य श्रमणों को अर्हत् कहा जाता तू इस सारे विस्तृत जगत् की रक्षा करता है। हे रूद्र, तुझसे अधिक तेजस्वी था। बद्ध के लिये अर्हत् विशेषण सुप्रचलित था, यथा-नमोतस्स भगवतो और कोई नहीं है। अरहतो सम्मासंबुद्धस्स। इस प्रकार प्राचीन काल में श्रमण धारा अपने जैन दृष्टि में इस ऋचा को निम्न प्रकार से भी व्याख्यायित किया समग्र रूप में आर्हत परम्परा के नाम से ही जानी जाती थी। वैदिक साहित्य जा सकता हैमें और विशेष रूप से ऋग्वेद में आहत व बार्हत धाराओं का उल्लेख हे अर्हन्! तू (संयम रूपी) शस्त्रों (धनुष-बाण) को धारण करता भी इसी तथ्य की पुष्टि करता है। आर्हत धर्म वस्तुत: वहाँ निवृत्तिप्रधान है? और सांसारिक जीवों में प्राण रूप स्वर्ण का त्याग कर देता है? निश्चय सम्पूर्ण श्रमणधारा का ही वाचक हैं। आहत शब्द से ही यह भी स्पष्ट ही तुझसे अधिक बलवान और कठोर और कोई नहीं है। हे अर्हन्! तू हो जाता है कि आर्हत- अर्हतों के उपासक थे और अर्हत् अवस्था विश्व की अर्थात् संसार के प्राणियों की मातृवत् दया करता है। को प्राप्त करना ही अपनी साधना का लक्ष्य मानते थे। बौद्ध ग्रन्थों में प्रस्तुत प्रसंग में अर्हन् की ब्याज रूप से स्तुति की गयी है। बुद्ध के पूर्व वज्जियों के अपने अर्हतों एवं चैत्यों की उपस्थिति के यहाँ शस्त्र धारण करने का तात्पर्य कर्म शत्रुओं या विषय वासनाओं को निर्देश हैं। आर्हतों से भिन्न वैदिक परम्परा ऋग्वैदिक काल में बार्हत पराजित करने के लिए संयम रूपी शस्त्रों को धारण करने से है। जैन परम्परा नाम से जानी जाती थी। में 'अरिहंत' शब्द की व्याख्या शत्रु का नाश करने वाला, इस रूप में ऋग्वेद के दशम् मण्डल के ८५ वें सूक्त की चतुर्थ ऋचा में की गई है। आचारांग में साधक को अपनी वासनाओं से युद्ध करने का स्पष्ट रूप से बार्हत शब्द का उल्लेख हुआ है। वह ऋचा इस प्रकार है- निर्देश दिया गया है। इसी प्रकार ब्याज रूप से यह कहा गया है कि आच्छद्विधानैर्गुपितो बाहतैः सोम रक्षितः। जहाँ सारा संसार स्वर्ण के पीछे भागता है, वहीं, तू इसका त्याग करता प्राव्णामिच्छृण्वन् तिष्ठासि न ते अश्रान्ति पार्थिवः।। है। यहाँ यजतं शब्द त्याग का वाची माना जा सकता है। अत: तुझसे (ऋग्वेद १०.१८५.१४) अधिक कठोर व समर्थ कौन हो सकता है? प्रस्तुत प्रसंग में 'अर्हन् दयसे अर्थात् हे सोम! तू गुप्त विधि विधानों से रक्षित बार्हत गणों विश्वमम्ब' शब्द अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसमें अर्हन् को विश्व के सभी से संरक्षित है। तू (सोमलता के) पीसने वाले पत्थरों का शब्द सुनता ही प्राणियों की दया करने वाला तथा मातृवत् कहा गया है, जो जैन परम्परा रहता है। तुझे पृथ्वी का कोई भी सामान्य जन नहीं खा सकता। का मूल आधार है। इसी प्रकार पंचम मण्डल के बावनवें सूक्त की पाँचवीं बृहिती वेद को कहते हैं और इस बृहती के उपासक बार्हत ऋचा भी महत्त्वपूर्ण हैकहे जाते थे। इस प्रकार वेदों में वर्णित सोमपान एवं यज्ञ-याग में निष्ठा अर्हन्तो ये सुदानवो नरो असामिशवसः। रखने वाले और उसे ही अपनी धर्म साधना का सर्वस्व मानने वाले लोग प्र यज्ञं यज्ञियेभ्यो दिवो अर्चा मरुद्धयः।। ही बार्हत थे। इनके विपरीत ध्यान और तप साधना को प्रमुख मानने वाले (ऋग्वेद ५.५२.५) व्यक्ति आर्हत नाम से जाने जाते थे। वैदिक साहित्य में हमें स्पष्ट रूप सायण की व्याख्या के अनसार इस ऋचा का अर्थ इस से अर्हत् को मानने वाले इन आर्हतों के उल्लेख उपलब्ध हैं। ऋग्वेद में प्रकार हैअर्हन् और अर्हन्त शब्दों का प्रयोग नौ ऋचाओं में दस से अधिक बार जो पूज्य, दानशूर, सम्पूर्ण बल से युक्त तथा तेजस्वी द्यौतमान Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 4 5 6 7