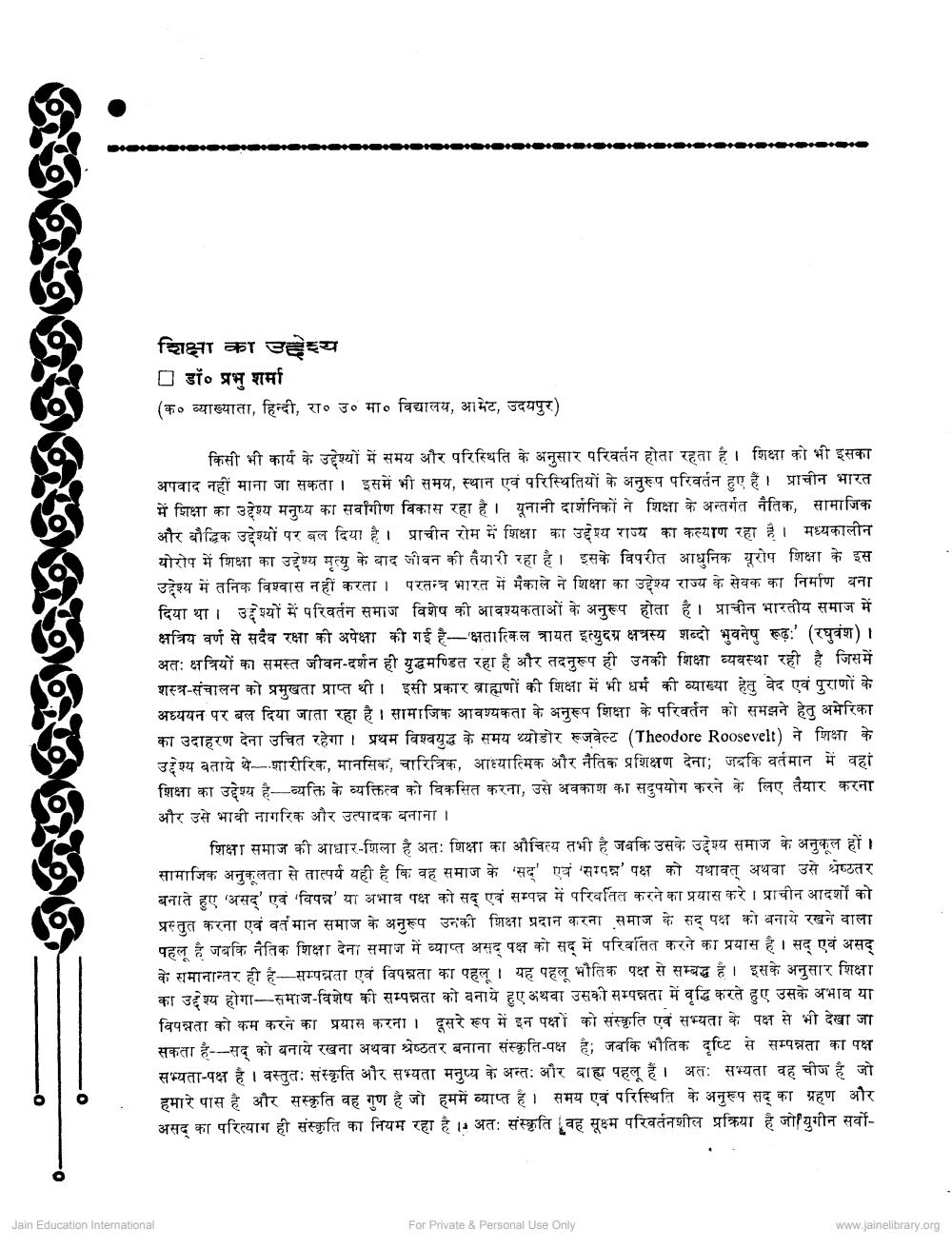Book Title: Shiksha ka Uddeshya Author(s): Prabhu Sharma Publisher: Z_Kesarimalji_Surana_Abhinandan_Granth_012044.pdf View full book textPage 1
________________ शिक्षा का उद्देश्य 0 डॉ० प्रभु शर्मा (क० व्याख्याता, हिन्दी, रा० उ० मा० विद्यालय, आमेट, उदयपुर) किसी भी कार्य के उद्देश्यों में समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। शिक्षा को भी इसका अपवाद नहीं माना जा सकता। इसमें भी समय, स्थान एवं परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन हुए हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास रहा है। यूनानी दार्शनिकों ने शिक्षा के अन्तर्गत नैतिक, सामाजिक और बौद्धिक उद्देश्यों पर बल दिया है। प्राचीन रोम में शिक्षा का उद्देश्य राज्य का कल्याण रहा है। मध्यकालीन योरोप में शिक्षा का उद्देश्य मृत्यु के बाद जीवन की तैयारी रहा है। इसके विपरीत आधुनिक यूरोप शिक्षा के इस उद्देश्य में तनिक विश्वास नहीं करता। परतन्त्र भारत में मैकाले ने शिक्षा का उद्देश्य राज्य के सेवक का निर्माण बना दिया था। उद्देश्यों में परिवर्तन समाज विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। प्राचीन भारतीय समाज में क्षत्रिय वर्ण से सदैव रक्षा की अपेक्षा की गई है-'क्षतात्किल त्रायत इत्युदन क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ़:' (रघुवंश)। अतः क्षत्रियों का समस्त जीवन-दर्शन ही युद्धमण्डित रहा है और तदनुरूप ही उनकी शिक्षा व्यवस्था रही है जिसमें शस्त्र-संचालन को प्रमुखता प्राप्त थी। इसी प्रकार ब्राह्मणों की शिक्षा में भी धर्म की व्याख्या हेतु वेद एवं पुराणों के अध्ययन पर बल दिया जाता रहा है। सामाजिक आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा के परिवर्तन को समझने हेतु अमेरिका का उदाहरण देना उचित रहेगा। प्रथम विश्वयुद्ध के समय थ्योडोर रूजवेल्ट (Theodore Roosevelt) ने शिक्षा के उद्देश्य बताये थे-शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक और नैतिक प्रशिक्षण देना; जबकि वर्तमान में वहां शिक्षा का उद्देश्य है—व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करना, उसे अवकाश का सदुपयोग करने के लिए तैयार करना और उसे भावी नागरिक और उत्पादक बनाना । शिक्षा समाज की आधारशिला है अतः शिक्षा का औचित्य तभी है जबकि उसके उद्देश्य समाज के अनुकूल हों। सामाजिक अनुकूलता से तात्पर्य यही है कि वह समाज के 'सद्' एवं 'सम्पन्न' पक्ष को यथावत् अथवा उसे श्रेष्ठतर बनाते हुए 'असद्' एवं 'विपन्न' या अभाव पक्ष को सद् एवं सम्पन्न में परिवर्तित करने का प्रयास करे । प्राचीन आदर्शों को प्रस्तुत करना एवं वर्तमान समाज के अनुरूप उनकी शिक्षा प्रदान करना समाज के सद् पक्ष को बनाये रखने वाला पहल है जबकि नैतिक शिक्षा देना समाज में व्याप्त असद् पक्ष को सद् में परिवर्तित करने का प्रयास है। सद् एवं असद् के समानान्तर ही है-सम्पन्नता एवं विपन्नता का पहलू । यह पहलू भौतिक पक्ष से सम्बद्ध है। इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होगा-समाज-विशेष की सम्पन्नता को बनाये हुए अथवा उसकी सम्पन्नता में वृद्धि करते हुए उसके अभाव या विपन्नता को कम करने का प्रयास करना। दूसरे रूप में इन पक्षों को संस्कृति एवं सभ्यता के पक्ष से भी देखा जा सकता है--सद् को बनाये रखना अथवा श्रेष्ठतर बनाना संस्कृति-पक्ष है; जबकि भौतिक दृष्टि से सम्पन्नता का पक्ष सभ्यता-पक्ष है । वस्तुतः संस्कृति और सभ्यता मनुष्य के अन्तः और बाह्य पहलू हैं। अत: सभ्यता वह चीज है जो हमारे पास है और संस्कृति वह गुण है जो हममें व्याप्त है। समय एवं परिस्थिति के अनुरूप सद् का ग्रहण और असद् का परित्याग ही संस्कृति का नियम रहा है । अत: संस्कृति वह सूक्ष्म परिवर्तनशील प्रक्रिया है जो युगीन सर्वो Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3