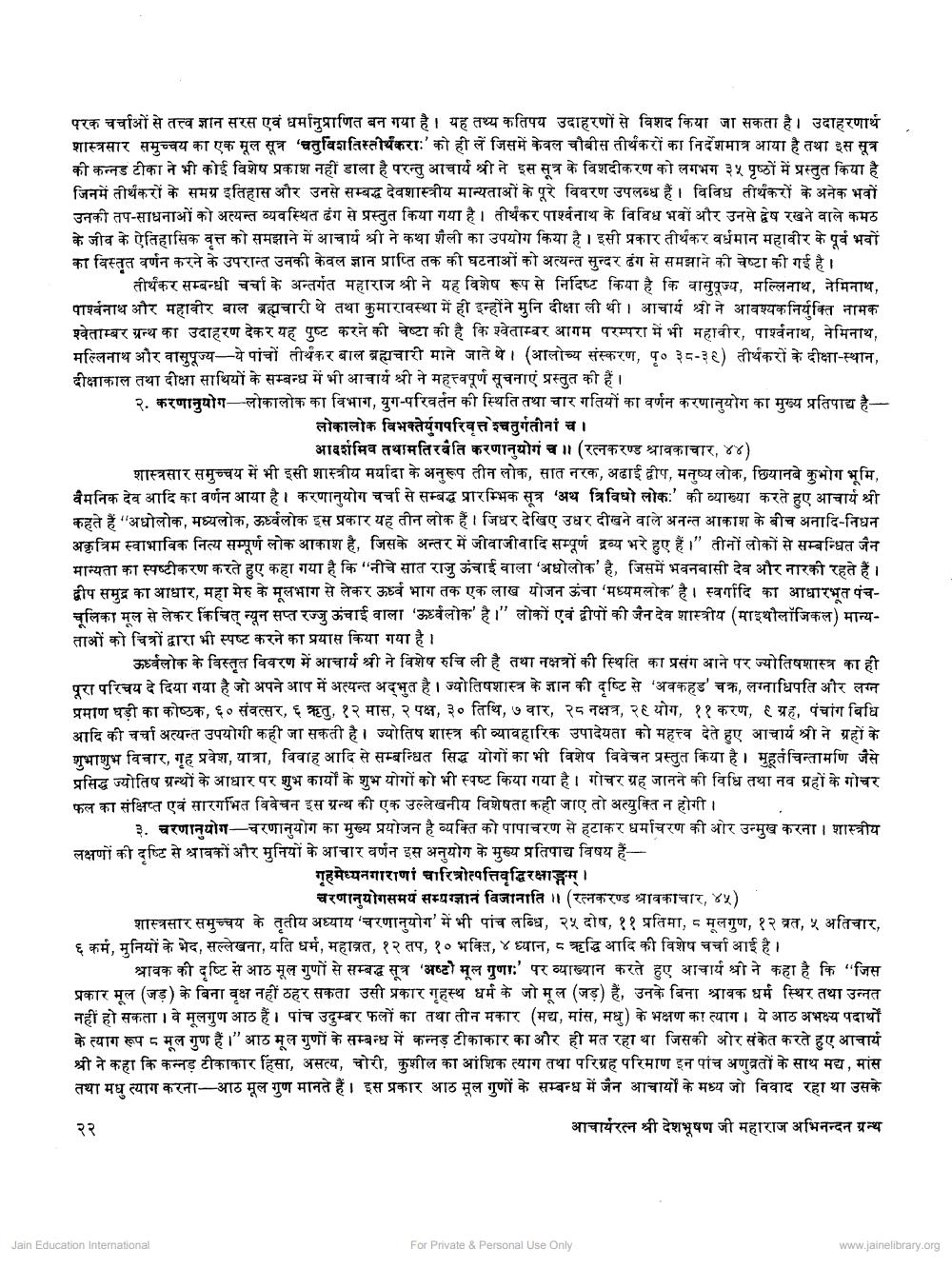Book Title: Shastrasar Samucchay Author(s): Mohanchand Publisher: Z_Deshbhushanji_Maharaj_Abhinandan_Granth_012045.pdf View full book textPage 2
________________ परक चर्चाओं से तत्त्व ज्ञान सरस एवं धर्मानुप्राणित बन गया है। यह तथ्य कतिपय उदाहरणों से विशद किया जा सकता है। उदाहरणार्थ शास्त्रसार समुच्चय का एक मूल सूत्र 'चतुविशतिस्तीर्थकराः' को ही लें जिसमें केवल चौबीस तीर्थंकरों का निर्देशमात्र आया है तथा इस सूत्र की कन्नड टीका ने भी कोई विशेष प्रकाश नहीं डाला है परन्तु आचार्य श्री ने इस सूत्र के विशदीकरण को लगभग ३५ पृष्ठों में प्रस्तुत किया है जिनमें तीर्थंकरों के समग्र इतिहास और उनसे सम्बद्ध देवशास्त्रीय मान्यताओं के पूरे विवरण उपलब्ध हैं। विविध तीर्थंकरों के अनेक भवों उनकी तप-साधनाओं को अत्यन्त व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तीर्थंकर पार्श्वनाथ के विविध भवों और उनसे द्वेष रखने वाले कमठ के जीव के ऐतिहासिक बत्त को समझाने में आचार्य श्री ने कथा शैली का उपयोग किया है। इसी प्रकार तीर्थंकर वर्धमान महावीर के पूर्व भवों का विस्तृत वर्णन करने के उपरान्त उनकी केवल ज्ञान प्राप्ति तक की घटनाओं को अत्यन्त सुन्दर ढंग से समझाने की चेष्टा की गई है। तीर्थंकर सम्बन्धी चर्चा के अन्तर्गत महाराज श्री ने यह विशेष रूप से निर्दिष्ट किया है कि वासुपूज्य, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर बाल ब्रह्मचारी थे तथा कुमारावस्था में ही इन्होंने मुनि दीक्षा ली थी। आचार्य श्री ने आवश्यक नियुक्ति नामक श्वेताम्बर ग्रन्थ का उदाहरण देकर यह पुष्ट करने की चेष्टा की है कि श्वेताम्बर आगम परम्परा में भी महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, मल्लिनाथ और वासुपूज्य-ये पांचों तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी माने जाते थे। (आलोच्य संस्करण, प०३८-३६) तीर्थंकरों के दीक्षा-स्थान, दीक्षाकाल तथा दीक्षा साथियों के सम्बन्ध में भी आचार्य श्री ने महत्त्वपूर्ण सूचनाएं प्रस्तुत की हैं। २. करणानुयोग-लोकालोक का विभाग, युग-परिवर्तन की स्थिति तथा चार गतियों का वर्णन करणानुयोग का मुख्य प्रतिपाद्य है लोकालोक विभक्तेर्युगपरिवृत्त श्चतुर्गतीनां च। आवर्शमिव तथामतिरवैति करणानुयोगं च ॥ (रत्नकरण्ड श्रावकाचार, ४४) शास्त्रसार समुच्चय में भी इसी शास्त्रीय मर्यादा के अनुरूप तीन लोक, सात नरक, अढाई द्वीप, मनुष्य लोक, छियानबे कुभोग भूमि, वैमनिक देव आदि का वर्णन आया है। करणानुयोग चर्चा से सम्बद्ध प्रारम्भिक सूत्र 'अथ त्रिविधो लोकः' की व्याख्या करते हुए आचार्य श्री कहते हैं 'अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक इस प्रकार यह तीन लोक हैं। जिधर देखिए उधर दीखने वाले अनन्त आकाश के बीच अनादि-निधन अकृत्रिम स्वाभाविक नित्य सम्पूर्ण लोक आकाश है, जिसके अन्तर में जीवाजीवादि सम्पूर्ण द्रव्य भरे हुए हैं।" तीनों लोकों से सम्बन्धित जैन मान्यता का स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया है कि "नीचे सात राजु ऊंचाई वाला 'अधोलोक' है, जिसमें भवनवासी देव और नारकी रहते हैं। द्वीप समुद्र का आधार, महा मेरु के मूलभाग से लेकर ऊर्ध्व भाग तक एक लाख योजन ऊंचा 'मध्यमलोक' है। स्वर्गादि का आधारभूत पंचचलिका मल से लेकर किंचित न्यून सप्त रज्जु ऊंचाई वाला 'ऊर्ध्वलोक' है।" लोकों एवं द्वीपों की जैन देव शास्त्रीय (माइथोलॉजिकल) मान्यताओं को चित्रों द्वारा भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। ऊर्ध्वलोक के विस्तृत विवरण में आचार्य श्री ने विशेष रुचि ली है तथा नक्षत्रों की स्थिति का प्रसंग आने पर ज्योतिषशास्त्र का ही पूरा परिचय दे दिया गया है जो अपने आप में अत्यन्त अद्भुत है। ज्योतिषशास्त्र के ज्ञान की दृष्टि से 'अवकहड' चक्र, लग्नाधिपति और लग्न प्रमाण घड़ी का कोष्ठक, ६० संवत्सर, ६ ऋतु, १२ मास, २ पक्ष, ३० तिथि, ७ वार, २८ नक्षत्र, २६ योग, ११ करण, ग्रह, पंचांग बिधि आदि की चर्चा अत्यन्त उपयोगी कही जा सकती है। ज्योतिष शास्त्र की व्यावहारिक उपादेयता को महत्त्व देते हुए आचार्य श्री ने ग्रहों के शुभाशुभ विचार, गृह प्रवेश, यात्रा, विवाह आदि से सम्बन्धित सिद्ध योगों का भी विशेष विवेचन प्रस्तुत किया है। मुहुर्त चिन्तामणि जैसे प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रन्थों के आधार पर शुभ कार्यों के शुभ योगों को भी स्पष्ट किया गया है। गोचर ग्रह जानने की विधि तथा नव ग्रहों के गोचर फल का संक्षिप्त एवं सारगर्भित विवेचन इस ग्रन्थ की एक उल्लेखनीय विशेषता कही जाए तो अत्युक्ति न होगी। ३. चरणानुयोग-चरणानुयोग का मुख्य प्रयोजन है व्यक्ति को पापाचरण से हटाकर धर्माचरण की ओर उन्मुख करना। शास्त्रीय लक्षणों की दष्टि से श्रावकों और मुनियों के आचार वर्णन इस अनुयोग के मुख्य प्रतिपाद्य विषय हैं गृहमेध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षाङ्गम् । चरणानुयोगसमयं सम्यग्ज्ञानं विजानाति ।। (रत्नकरण्ड श्रावकाचार, ४५) शास्त्रसार समुच्चय के तृतीय अध्याय 'चरणानुयोग' में भी पांच लब्धि, २५ दोष, ११ प्रतिमा, ८ मूलगुण, १२ व्रत, ५ अतिचार, ६ कर्म, मुनियों के भेद, सल्लेखना, यति धर्म, महाव्रत, १२ तप, १० भक्ति, ४ ध्यान, ८ ऋद्धि आदि की विशेष चर्चा आई है। ___ श्रावक की दृष्टि से आठ मूल गुणों से सम्बद्ध सूत्र 'अष्टो मूल गुणा:' पर व्याख्यान करते हुए आचार्य श्री ने कहा है कि "जिस प्रकार मूल (जड़) के बिना वृक्ष नहीं ठहर सकता उसी प्रकार गृहस्थ धर्म के जो मूल (जड़) हैं, उनके बिना श्रावक धर्म स्थिर तथा उन्नत नहीं हो सकता। वे मूलगुण आठ हैं। पांच उदुम्बर फलों का तथा तीन मकार (मद्य, मांस, मधु) के भक्षण का त्याग। ये आठ अभक्ष्य पदार्थों के त्याग रूप ८ मूल गुण हैं।" आठ मूल गुणों के सम्बन्ध में कन्नड़ टीकाकार का और ही मत रहा था जिसकी ओर संकेत करते हुए आचार्य श्री ने कहा कि कन्नड़ टीकाकार हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील का आंशिक त्याग तथा परिग्रह परिमाण इन पांच अणुव्रतों के साथ मद्य , मांस तथा मधु त्याग करना-आठ मूल गुण मानते हैं। इस प्रकार आठ मूल गुणों के सम्बन्ध में जैन आचार्यों के मध्य जो विवाद रहा था उसके २२ आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4