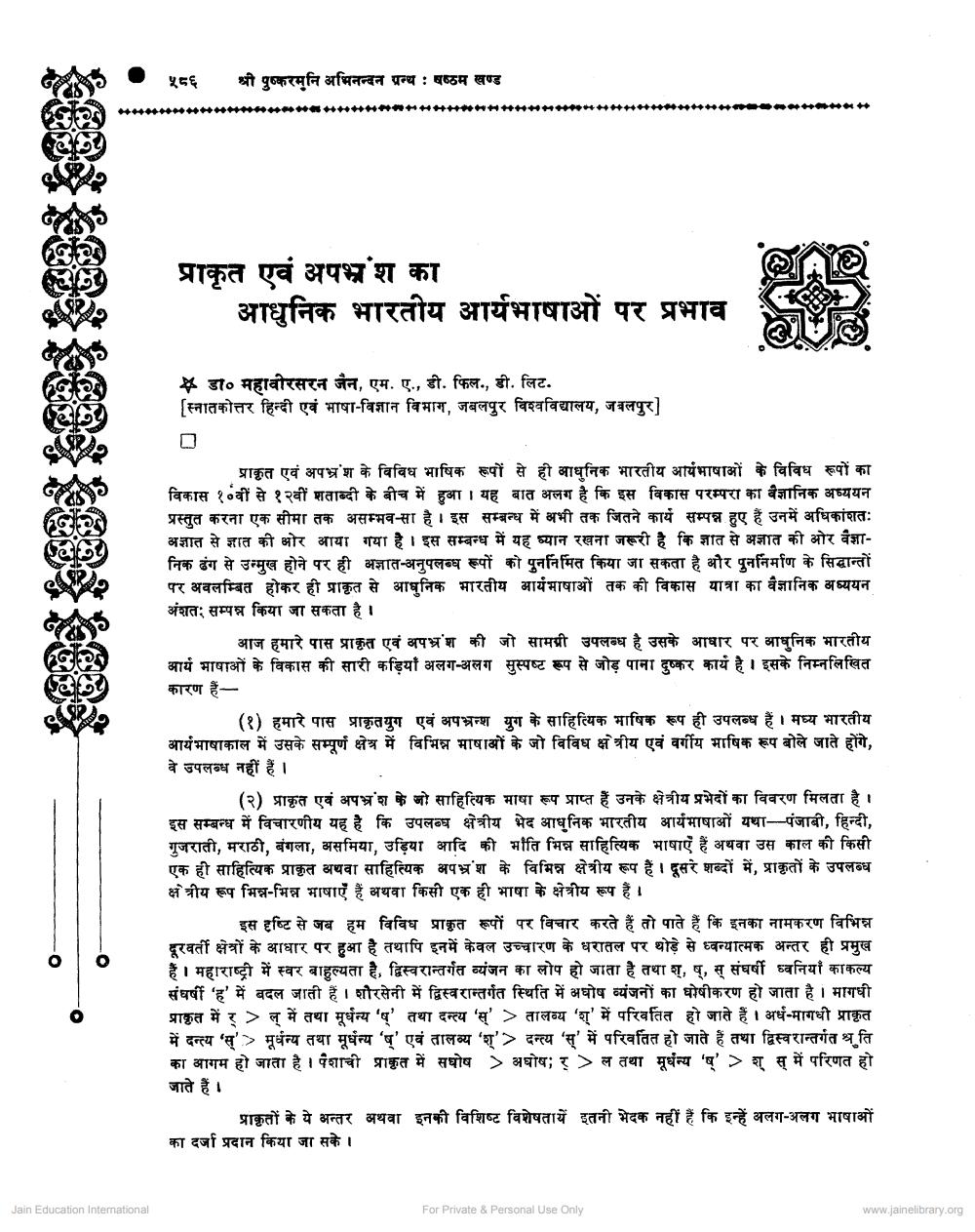Book Title: Prakrit evam Apbhramsa ka Adhunik Bharatiya Aryabhasha par Prabhav Author(s): Mahavirsaran Jain Publisher: Z_Pushkarmuni_Abhinandan_Granth_012012.pdf View full book textPage 1
________________ • ५८६ श्री पुष्करमुनि अभिनन्दन प्रन्थ : षष्ठम खण्ड प्राकृत एवं अपभ्रंश का आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं पर प्रभाव * डा० महावीरसरन जैन, एम. ए., डी. फिल., डी. लिट. [स्नातकोत्तर हिन्दी एवं भाषा-विज्ञान विभाग, जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर] प्राकृत एवं अपभ्रंश के विविध भाषिक रूपों से ही आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं के विविध रूपों का विकास १०वीं से १२वीं शताब्दी के बीच में हुआ। यह बात अलग है कि इस विकास परम्परा का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करना एक सीमा तक असम्भव-सा है। इस सम्बन्ध में अभी तक जितने कार्य सम्पन्न हुए हैं उनमें अधिकांशतः अज्ञात से ज्ञात की ओर आया गया है। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना जरूरी है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर वैज्ञानिक ढंग से उन्मुख होने पर ही अज्ञात-अनुपलब्ध रूपों को पुननिर्मित किया जा सकता है और पुनर्निर्माण के सिद्धान्तों पर अवलम्बित होकर ही प्राकृत से आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं तक की विकास यात्रा का वैज्ञानिक अध्ययन अंशतः सम्पन्न किया जा सकता है। आज हमारे पास प्राकृत एवं अपभ्रंश की जो सामग्री उपलब्ध है उसके आधार पर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विकास की सारी कड़ियाँ अलग-अलग सुस्पष्ट रूप से जोड़ पाना दुष्कर कार्य है । इसके निम्नलिखित कारण हैं (१) हमारे पास प्राकृतयुग एवं अपभ्रन्श युग के साहित्यिक भाषिक रूप ही उपलब्ध हैं । मध्य भारतीय आर्यभाषाकाल में उसके सम्पूर्ण क्षेत्र में विभिन्न भाषाओं के जो विविध क्षेत्रीय एवं वर्गीय भाषिक रूप बोले जाते होंगे, वे उपलब्ध नहीं हैं। (२) प्राकृत एवं अपभ्रंश के जो साहित्यिक भाषा रूप प्राप्त हैं उनके क्षेत्रीय प्रभेदों का विवरण मिलता है। इस सम्बन्ध में विचारणीय यह है कि उपलब्ध क्षेत्रीय भेद आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं यथा-पंजाबी, हिन्दी, गुजराती, मराठी, बंगला, असमिया, उड़िया आदि की भांति भिन्न साहित्यिक भाषाएँ हैं अथवा उस काल की किसी एक ही साहित्यिक प्राकृत अथवा साहित्यिक अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूप हैं। दूसरे शब्दों में, प्राकृतों के उपलब्ध क्षेत्रीय रूप भिन्न-भिन्न भाषाएँ हैं अथवा किसी एक ही भाषा के क्षेत्रीय रूप हैं। इस दृष्टि से जब हम विविध प्राकृत रूपों पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि इनका नामकरण विभिन्न दूरवर्ती क्षेत्रों के आधार पर हुआ है तथापि इनमें केवल उच्चारण के धरातल पर थोड़े से ध्वन्यात्मक अन्तर ही प्रमुख हैं । महाराष्ट्री में स्वर बाहुल्यता है, द्विस्वरान्तर्गत व्यंजन का लोप हो जाता है तथा श, ष, स् संघर्षी ध्वनियाँ काकल्य संघर्षी 'ह' में बदल जाती हैं । शौरसेनी में द्विस्वरान्तर्गत स्थिति में अघोष व्यंजनों का घोषीकरण हो जाता है । मागधी प्राकृत में र् > ल में तथा मूर्धन्य 'ए' तथा दन्त्य 'स्' > तालव्य 'श्' में परिवर्तित हो जाते हैं । अर्ध-मागधी प्राकृत में दन्त्य 'स्' > मूर्धन्य तथा मूर्धन्य '' एवं तालव्य 'श्'> दन्त्य 'स्' में परिवर्तित हो जाते हैं तथा द्विस्वरान्तर्गत श्रुति का आगम हो जाता है । पेशाची प्राकृत में सघोष > अघोष; र > ल तथा मूर्धन्य 'ष' > श् स् में परिणत हो जाते हैं। प्राकृतों के ये अन्तर अथवा इनकी विशिष्ट विशेषतायें इतनी भेदक नहीं हैं कि इन्हें अलग-अलग भाषाओं का दर्जा प्रदान किया जा सके। ०० Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10