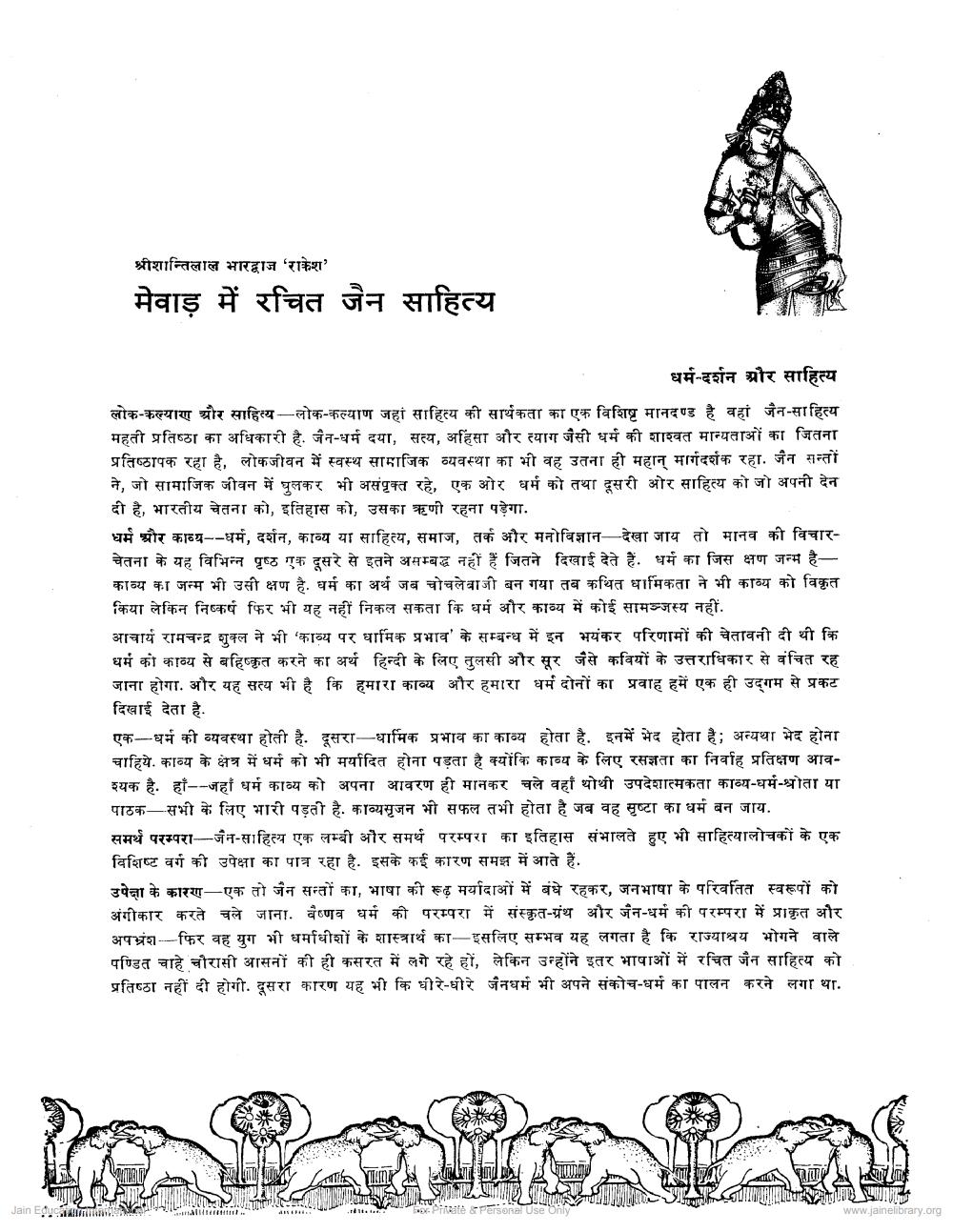Book Title: Mevad me Rachit Jain Sahitya Author(s): Shantilal Bharadwaj Publisher: Z_Hajarimalmuni_Smruti_Granth_012040.pdf View full book textPage 1
________________ श्रीशान्तिलाल भारद्वाज 'राकेश' मेवाड़ में रचित जैन साहित्य धर्म-दर्शन और साहित्य लोक-कल्याण और साहित्य-लोक-कल्याण जहां साहित्य की सार्थकता का एक विशिष्ट मानदण्ड है वहां जैन-साहित्य महती प्रतिष्ठा का अधिकारी है. जैन-धर्म दया, सत्य, अहिंसा और त्याग जैसी धर्म की शाश्वत मान्यताओं का जितना प्रतिष्ठापक रहा है, लोकजीवन में स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था का भी वह उतना ही महान् मार्गदर्शक रहा. जैन सन्तों ने, जो सामाजिक जीवन में घुलकर भी असंपृक्त रहे, एक ओर धर्म को तथा दूसरी ओर साहित्य को जो अपनी देन दी है, भारतीय चेतना को, इतिहास को, उसका ऋणी रहना पड़ेगा. धर्म और काव्य--धर्म, दर्शन, काव्य या साहित्य, समाज, तर्क और मनोविज्ञान–देखा जाय तो मानव की विचारचेतना के यह विभिन्न पृष्ठ एक दुसरे से इतने असम्बद्ध नहीं हैं जितने दिखाई देते हैं. धर्म का जिस क्षण जन्म हैकाव्य का जन्म भी उसी क्षण है. धर्म का अर्थ जब चोचलेबाजी बन गया तब कथित धार्मिकता ने भी काव्य को विकृत किया लेकिन निष्कर्ष फिर भी यह नहीं निकल सकता कि धर्म और काव्य में कोई सामञ्जस्य नहीं. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भी 'काव्य पर धार्मिक प्रभाव' के सम्बन्ध में इन भयंकर परिणामों की चेतावनी दी थी कि धर्म को काव्य से बहिष्कृत करने का अर्थ हिन्दी के लिए तुलसी और सूर जैसे कवियों के उत्तराधिकार से वंचित रह जाना होगा. और यह सत्य भी है कि हमारा काव्य और हमारा धर्म दोनों का प्रवाह हमें एक ही उद्गम से प्रकट दिखाई देता है. एक-धर्म की व्यवस्था होती है. दूसरा-धार्मिक प्रभाव का काव्य होता है. इनमें भेद होता है; अन्यथा भेद होना चाहिये. काव्य के क्षेत्र में धर्म को भी मर्यादित होना पड़ता है क्योंकि काव्य के लिए रसज्ञता का निर्वाह प्रतिक्षण आवश्यक है. हाँ--जहाँ धर्म काव्य को अपना आवरण ही मानकर चले वहाँ थोथी उपदेशात्मकता काव्य-धर्म-श्रोता या पाठक-सभी के लिए भारी पड़ती है. काव्यसृजन भी सफल तभी होता है जब वह सृष्टा का धर्म बन जाय. समर्थ परम्परा-जैन-साहित्य एक लम्बी और समर्थ परम्परा का इतिहास संभालते हुए भी साहित्यालोचकों के एक विशिष्ट वर्ग की उपेक्षा का पात्र रहा है. इसके कई कारण समझ में आते हैं. उपेक्षा के कारण एक तो जैन सन्तों का, भाषा की रूढ़ मर्यादाओं में बंधे रहकर, जनभाषा के परिवर्तित स्वरूपों को अंगीकार करते चले जाना. वैष्णव धर्म की परम्परा में संस्कृत-ग्रंथ और जैन-धर्म की परम्परा में प्राकृत और अपभ्रंश-फिर वह युग भी धर्माधीशों के शास्त्रार्थ का-इसलिए सम्भव यह लगता है कि राज्याश्रय भोगने वाले पण्डित चाहे चौरासी आसनों की ही कसरत में लगे रहे हों, लेकिन उन्होंने इतर भाषाओं में रचित जैन साहित्य को प्रतिष्ठा नहीं दी होगी. दूसरा कारण यह भी कि धीरे-धीरे जैनधर्म भी अपने संकोच-धर्म का पालन करने लगा था. KURIHIHAR MAHRAMA Jain EducTITA My LITERTAIMER PHATARNAKAMANASVEERIMILA FORPrivate spersonal use only DAam -n.tw www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11