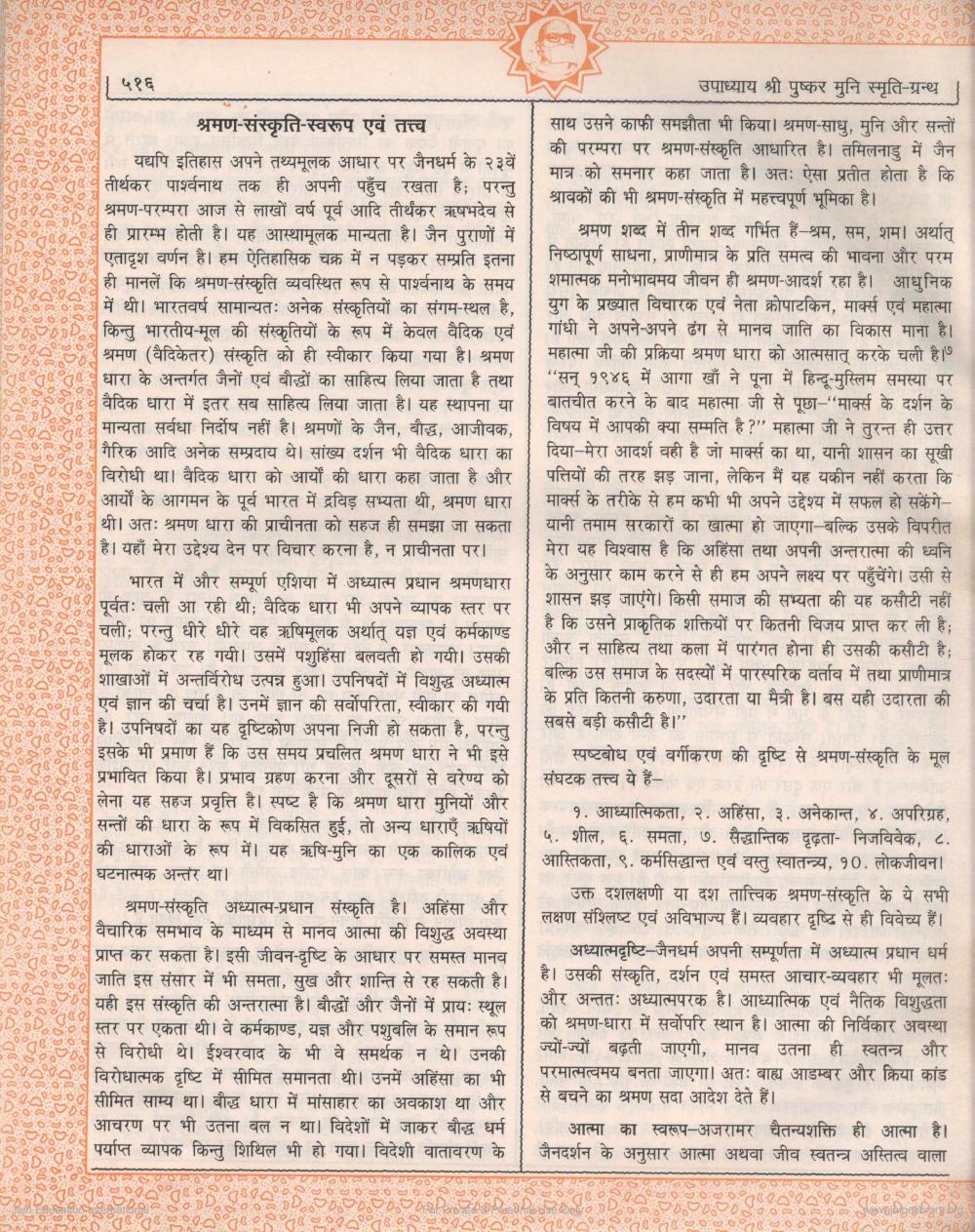Book Title: Manav Sanskruti ke Vikas me Shraman Sanskruti ki Bhoomika Author(s): Ravindra Jain Publisher: Z_Nahta_Bandhu_Abhinandan_Granth_012007.pdf View full book textPage 4
________________ ५१६ श्रमण-संस्कृति-स्वरूप एवं तत्त्व यद्यपि इतिहास अपने तथ्यमूलक आधार पर जैनधर्म के २३वें तीर्थकर पार्श्वनाथ तक ही अपनी पहुँच रखता है, परन्तु श्रमण परम्परा आज से लाखों वर्ष पूर्व आदि तीर्थंकर ऋषभदेव से ही प्रारम्भ होती है। यह आस्थामूलक मान्यता है। जैन पुराणों में एतादृश वर्णन है। हम ऐतिहासिक चक्र में न पड़कर सम्प्रति इतना ही मानलें कि श्रमण संस्कृति व्यवस्थित रूप से पार्श्वनाथ के समय में थी भारतवर्ष सामान्यतः अनेक संस्कृतियों का संगम स्थल है, किन्तु भारतीय मूल की संस्कृतियों के रूप में केवल वैदिक एवं श्रमण (वैदिकेतर) संस्कृति को ही स्वीकार किया गया है श्रमण धारा के अन्तर्गत जैनों एवं बौद्धों का साहित्य लिया जाता है तथा वैदिक धारा में इतर सब साहित्य लिया जाता है। यह स्थापना या मान्यता सर्वथा निर्दोष नहीं है। श्रमणों के जैन, बौद्ध, आजीवक, गैरिक आदि अनेक सम्प्रदाय थे। सांख्य दर्शन भी वैदिक धारा का विरोधी था । वैदिक धारा को आर्यों की धारा कहा जाता है और आर्यों के आगमन के पूर्व भारत में द्रविड़ सभ्यता थी, श्रमण धारा थी। अतः श्रमण धारा की प्राचीनता को सहज ही समझा जा सकता है यहाँ मेरा उद्देश्य देन पर विचार करना है, न प्राचीनता पर । भारत में और सम्पूर्ण एशिया में अध्यात्म प्रधान श्रमणधारा पूर्वतः चली आ रही थी; वैदिक धारा भी अपने व्यापक स्तर पर चली; परन्तु धीरे धीरे वह ऋषिमूलक अर्थात् यज्ञ एवं कर्मकाण्ड मूलक होकर रह गयी। उसमें पशुहिंसा बलवती हो गयी। उसकी शाखाओं में अन्तर्विरोध उत्पन्न हुआ। उपनिषदों में विशुद्ध अध्यात्म एवं ज्ञान की चर्चा है। उनमें ज्ञान की सर्वोपरिता, स्वीकार की गयी है। उपनिषदों का यह दृष्टिकोण अपना निजी हो सकता है, परन्तु इसके भी प्रमाण हैं कि उस समय प्रचलित श्रमण धारा ने भी इसे प्रभावित किया है। प्रभाव ग्रहण करना और दूसरों से वरेण्य को लेना यह सहज प्रवृत्ति है। स्पष्ट है कि श्रमण धारा मुनियों और सन्तों की धारा के रूप में विकसित हुई, तो अन्य धाराएँ ऋषियों की धाराओं के रूप में। यह ऋषि-मुनि का एक कालिक एवं घटनात्मक अन्तर था । श्रमण-संस्कृति अध्यात्म-प्रधान संस्कृति है। अहिंसा और | वैचारिक समभाव के माध्यम से मानव आत्मा की विशुद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। इसी जीवन-दृष्टि के आधार पर समस्त मानव जाति इस संसार में भी समता, सुख और शान्ति से रह सकती है। यही इस संस्कृति की अन्तरात्मा है। बौद्धों और जैनों में प्रायः स्थूल स्तर पर एकता थी। वे कर्मकाण्ड, यज्ञ और पशुबलि के समान रूप से विरोधी थे। ईश्वरवाद के भी वे समर्थक न थे। उनकी विरोधात्मक दृष्टि में सीमित समानता थी। उनमें अहिंसा का भी सीमित साम्य था। बौद्ध धारा में मांसाहार का अवकाश था और आचरण पर भी उतना बल न था। विदेशों में जाकर बौद्ध धर्म पर्याप्त व्यापक किन्तु शिथिल भी हो गया विदेशी वातावरण के 3434 उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि स्मृति ग्रन्थ साथ उसने काफी समझौता भी किया। श्रमण-साधु, मुनि और सन्तों की परम्परा पर श्रमण-संस्कृति आधारित है। तमिलनाडु में जैन मात्र को समनार कहा जाता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि श्रावकों की भी श्रमण संस्कृति में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। श्रमण शब्द में तीन शब्द गर्भित है-श्रम, सम, शम अर्थात् निष्ठापूर्ण साधना, प्राणीमात्र के प्रति समत्व की भावना और परम शमात्मक मनोभावमय जीवन ही श्रमण-आदर्श रहा है। आधुनिक युग के प्रख्यात विचारक एवं नेता क्रोपाटकिन, मार्क्स एवं महात्मा गांधी ने अपने-अपने ढंग से मानव जाति का विकास माना है। महात्मा जी की प्रक्रिया श्रमण धारा को आत्मसात् करके चली है । ७ “सन् १९४६ में आगा खाँ ने पूना में हिन्दू-मुस्लिम समस्या पर बातचीत करने के बाद महात्मा जी से पूछा- "मार्क्स के दर्शन के विषय में आपकी क्या सम्मति है ?" महात्मा जी ने तुरन्त ही उत्तर दिया- मेरा आदर्श वही है जो मार्क्स का था, यानी शासन का सूखी पत्तियों की तरह झड़ जाना, लेकिन मैं यह यकीन नहीं करता कि मार्क्स के तरीके से हम कभी भी अपने उद्देश्य में सफल हो सकेंगेयानी तमाम सरकारों का खात्मा हो जाएगा बल्कि उसके विपरीत मेरा यह विश्वास है कि अहिंसा तथा अपनी अन्तरात्मा की ध्वनि के अनुसार काम करने से ही हम अपने लक्ष्य पर पहुँचेंगे। उसी से शासन झड़ जाएंगे। किसी समाज की सभ्यता की यह कसौटी नहीं है कि उसने प्राकृतिक शक्तियों पर कितनी विजय प्राप्त कर ली है; और न साहित्य तथा कला में पारंगत होना ही उसकी कसौटी है; बल्कि उस समाज के सदस्यों में पारस्परिक बर्ताव में तथा प्राणीमात्र के प्रति कितनी करुणा, उदारता या मैत्री है। बस यही उदारता की सबसे बड़ी कसौटी है।" स्पष्टबोध एवं वर्गीकरण की दृष्टि से श्रमण संस्कृति के मूल संघटक तत्त्व ये हैं १. आध्यात्मिकता, २ अहिंसा, ३. अनेकान्त, ४. अपरिग्रह, ५. शील, ६. समता, ७. सैद्धान्तिक दृढ़ता- निजविवेक, ८. आस्तिकता, ९. कर्मसिद्धान्त एवं वस्तु स्वातन्त्र्य, १०. लोकजीवन । उक्त दशलक्षणी या दश तात्विक श्रमण-संस्कृति के ये सभी लक्षण संश्लिष्ट एवं अविभाज्य है। व्यवहार दृष्टि से ही विवेच्य हैं। 00 अध्यात्मदृष्टि - जैनधर्म अपनी सम्पूर्णता में अध्यात्म प्रधान धर्म है। उसकी संस्कृति, दर्शन एवं समस्त आचार-व्यवहार भी मूलतः और अन्ततः अध्यात्मपरक है। आध्यात्मिक एवं नैतिक विशुद्धता को श्रमण-धारा में सर्वोपरि स्थान है। आत्मा की निर्विकार अवस्था ज्यों-ज्यों बढ़ती जाएगी, मानव उतना ही स्वतन्त्र और परमात्मत्वमय बनता जाएगा। अतः बाह्य आडम्बर और क्रिया कांड से बचने का श्रमण सदा आदेश देते हैं। आत्मा का स्वरूप- अजरामर चैतन्यशक्ति ही आत्मा है। जैनदर्शन के अनुसार आत्मा अथवा जीव स्वतन्त्र अस्तित्व वाला Navajalges 28.001Page Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8