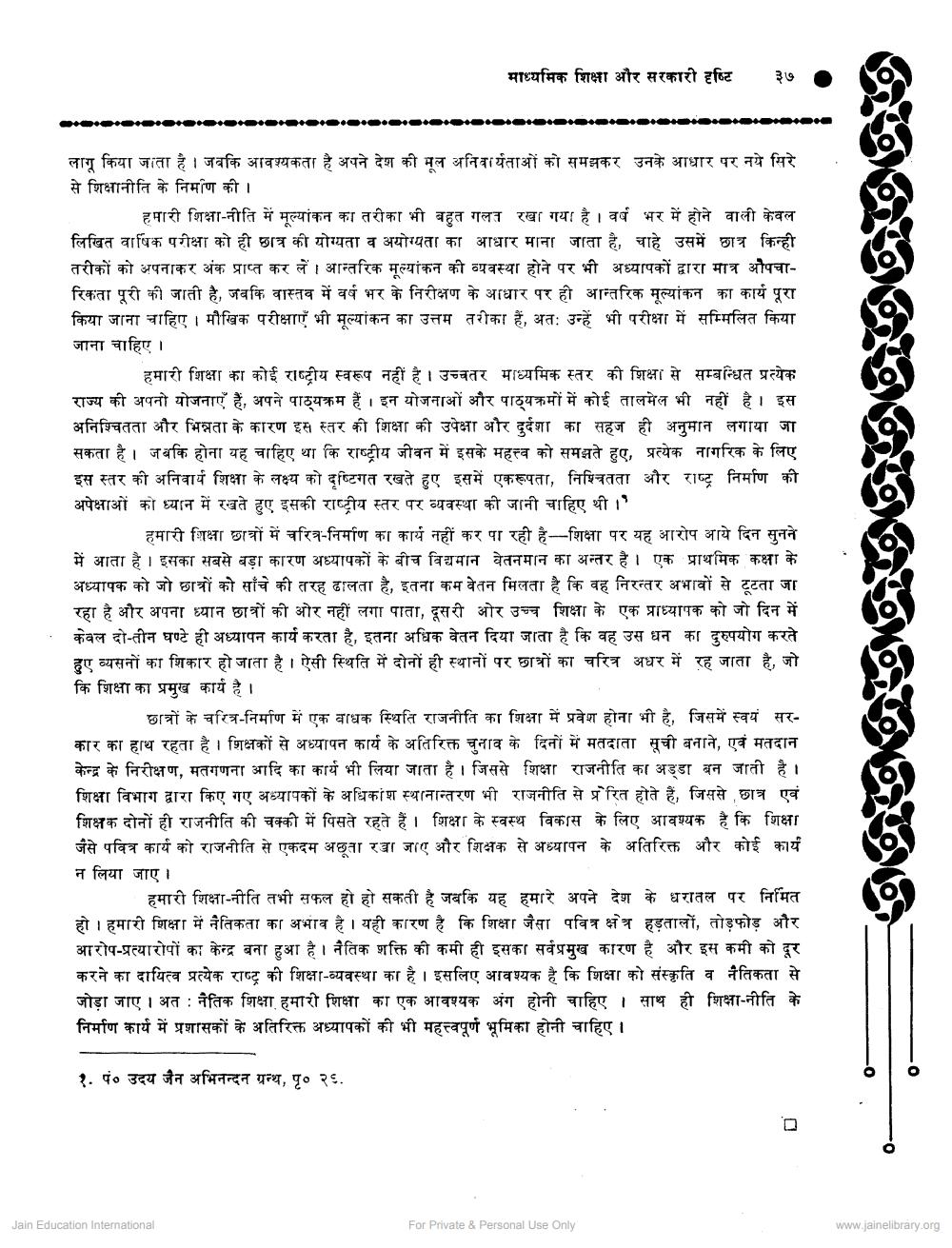Book Title: Madhyamik shiksha aur Sarkar Drushti Author(s): Sushma Arora Publisher: Z_Kesarimalji_Surana_Abhinandan_Granth_012044.pdf View full book textPage 5
________________ माध्यमिक शिक्षा और सरकारी दृष्टि 37 . लागू किया जाता है / जबकि आवश्यकता है अपने देश की मूल अनिवार्यताओं को समझकर उनके आधार पर नये सिरे से शिक्षानीति के निर्माण की। हमारी शिक्षा-नीति में मूल्यांकन का तरीका भी बहुत गलत रखा गया है। वर्ष भर में होने वाली केवल लिखित वार्षिक परीक्षा को ही छात्र की योग्यता व अयोग्यता का आधार माना जाता है, चाहे उसमें छात्र किन्ही तरीकों को अपनाकर अंक प्राप्त कर लें। आन्तरिक मूल्यांकन की व्यवस्था होने पर भी अध्यापकों द्वारा मात्र औपचारिकता पूरी की जाती है, जबकि वास्तव में वर्ष भर के निरीक्षण के आधार पर ही आन्तरिक मूल्यांकन का कार्य पूरा किया जाना चाहिए / मौखिक परीक्षाएँ भी मूल्यांकन का उत्तम तरीका हैं, अत: उन्हें भी परीक्षा में सम्मिलित किया जाना चाहिए। हमारी शिक्षा का कोई राष्ट्रीय स्वरूप नहीं है। उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा से सम्बन्धित प्रत्येक राज्य की अपनो योजनाएँ हैं, अपने पाठ्यक्रम हैं / इन योजनाओं और पाठ्यक्रमों में कोई तालमेल भी नहीं है। इस अनिश्चितता और भिन्नता के कारण इस स्तर की शिक्षा की उपेक्षा और दुर्दशा का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। जबकि होना यह चाहिए था कि राष्ट्रीय जीवन में इसके महत्त्व को समझते हुए, प्रत्येक नागरिक के लिए इस स्तर की अनिवार्य शिक्षा के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए इसमें एकरूपता, निश्चितता और राष्ट्र निर्माण की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसकी राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था की जानी चाहिए थी।' ___ हमारी शिक्षा छात्रों में चरित्र-निर्माण का कार्य नहीं कर पा रही है-शिक्षा पर यह आरोप आये दिन सुनने में आता है / इसका सबसे बड़ा कारण अध्यापकों के बीच विद्यमान वेतनमान का अन्तर है। एक प्राथमिक कक्षा के अध्यापक को जो छात्रों को साँचे की तरह ढालता है, इतना कम वेतन मिलता है कि वह निरन्तर अभावों से टूटता जा रहा है और अपना ध्यान छात्रों की ओर नहीं लगा पाता, दूसरी ओर उच्च शिक्षा के एक प्राध्यापक को जो दिन में केवल दो-तीन घण्टे ही अध्यापन कार्य करता है, इतना अधिक वेतन दिया जाता है कि वह उस धन का दुरुपयोग करते हुए व्यसनों का शिकार हो जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों ही स्थानों पर छात्रों का चरित्र अधर में रह जाता है, जो कि शिक्षा का प्रमुख कार्य है। छात्रों के चरित्र-निर्माण में एक बाधक स्थिति राजनीति का शिक्षा में प्रवेश होना भी है, जिसमें स्वयं सरकार का हाथ रहता है। शिक्षकों से अध्यापन कार्य के अतिरिक्त चुनाव के दिनों में मतदाता सूची बनाने, एवं मतदान केन्द्र के निरीक्षण, मतगणना आदि का कार्य भी लिया जाता है / जिससे शिक्षा राजनीति का अड्डा बन जाती है। शिक्षा विभाग द्वारा किए गए अध्यापकों के अधिकांश स्थानान्तरण भी राजनीति से प्रेरित होते हैं, जिससे छात्र एवं शिक्षक दोनों ही राजनीति की चक्की में पिसते रहते हैं। शिक्षा के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक है कि शिक्षा न लिया जाए। हमारी शिक्षा-नीति तभी सफल हो हो सकती है जबकि यह हमारे अपने देश के धरातल पर निर्मित हो / हमारी शिक्षा में नैतिकता का अभाव है। यही कारण है कि शिक्षा जैसा पवित्र क्षेत्र हड़तालों, तोड़फोड़ और आरोप-प्रत्यारोपों का केन्द्र बना हुआ है। नैतिक शक्ति की कमी ही इसका सर्वप्रमुख कारण है और इस कमी को दूर करने का दायित्व प्रत्येक राष्ट्र की शिक्षा-व्यवस्था का है / इसलिए आवश्यक है कि शिक्षा को संस्कृति व नैतिकता से जोड़ा जाए / अत : नैतिक शिक्षा हमारी शिक्षा का एक आवश्यक अंग होनी चाहिए / साथ ही शिक्षा-नीति के निर्माण कार्य में प्रशासकों के अतिरिक्त अध्यापकों की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। 1. पं० उदय जैन अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० 26. Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 3 4 5