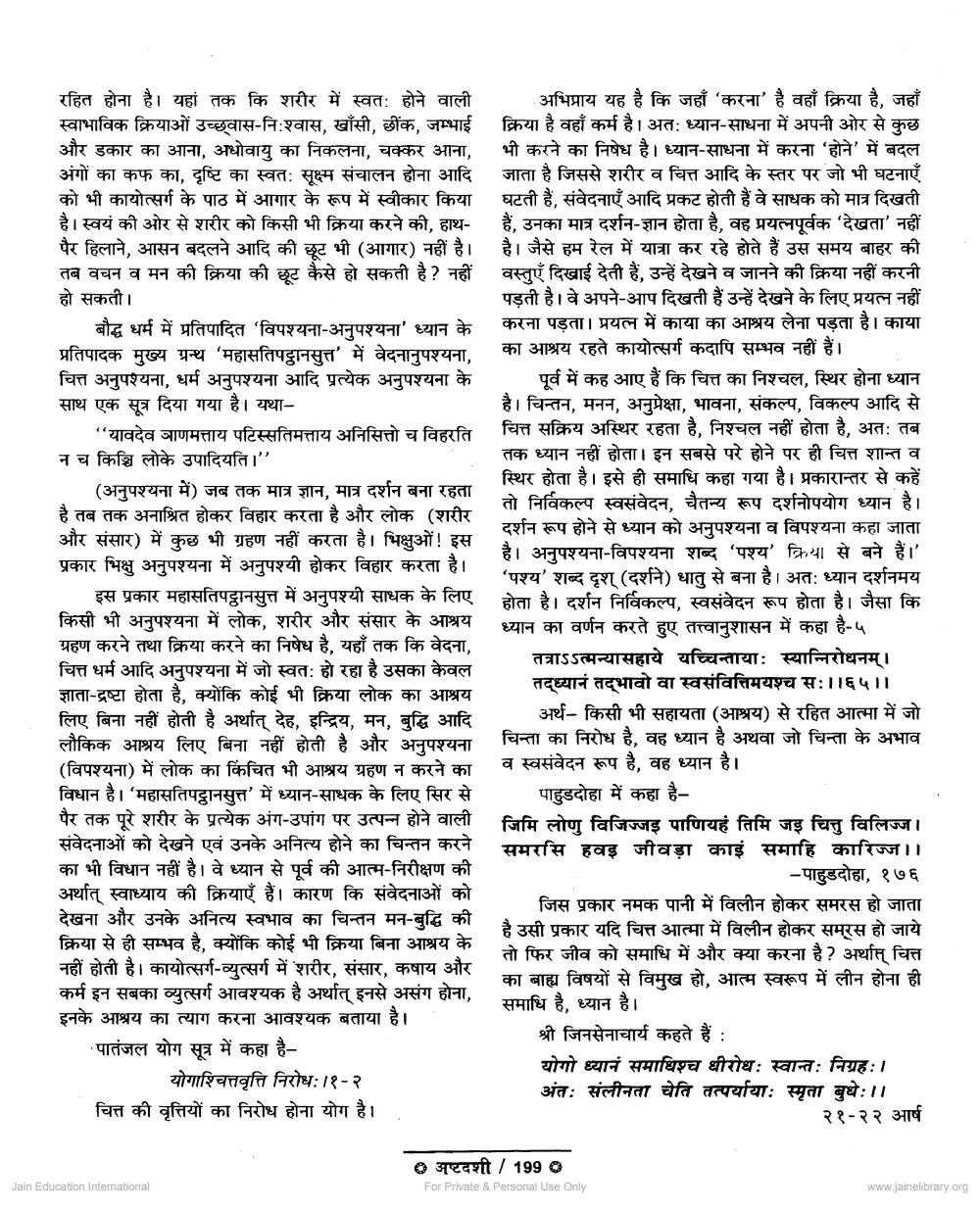Book Title: Kayotsarga Dhyan ki Purnata Author(s): Kanhaiyalal Lodha Publisher: Z_Ashtdashi_012049.pdf View full book textPage 2
________________ रहित होना है। यहां तक कि शरीर में स्वतः होने वाली अभिप्राय यह है कि जहाँ 'करना' है वहाँ क्रिया है, जहाँ स्वाभाविक क्रियाओं उच्छ्वास-नि:श्वास, खाँसी, छींक, जम्भाई क्रिया है वहाँ कर्म है। अत: ध्यान-साधना में अपनी ओर से कुछ और डकार का आना, अधोवायु का निकलना, चक्कर आना, भी करने का निषेध है। ध्यान-साधना में करना होने' में बदल अंगों का कफ का, दृष्टि का स्वत: सूक्ष्म संचालन होना आदि जाता है जिससे शरीर व चित्त आदि के स्तर पर जो भी घटनाएँ को भी कायोत्सर्ग के पाठ में आगार के रूप में स्वीकार किया घटती हैं, संवेदनाएँ आदि प्रकट होती हैं वे साधक को मात्र दिखती है। स्वयं की ओर से शरीर को किसी भी क्रिया करने की, हाथ- हैं, उनका मात्र दर्शन-ज्ञान होता है, वह प्रयत्नपूर्वक 'देखता' नहीं पैर हिलाने, आसन बदलने आदि की छूट भी (आगार) नहीं है। है। जैसे हम रेल में यात्रा कर रहे होते हैं उस समय बाहर की तब वचन व मन की क्रिया की छूट कैसे हो सकती है? नहीं वस्तुएँ दिखाई देती हैं, उन्हें देखने व जानने की क्रिया नहीं करनी हो सकती। पड़ती है। वे अपने-आप दिखती हैं उन्हें देखने के लिए प्रयत्न नहीं बौद्ध धर्म में प्रतिपादित 'विपश्यना-अनुपश्यना' ध्यान के करना पड़ता। प्रयत्न में काया का आश्रय लेना पड़ता है। काया करना पड़ता। प्रयत्न प्रतिपादक मुख्य ग्रन्थ 'महासतिपट्टानसुत्त' में वेदनानुपश्यना, ___ का आश्रय रहते कायोत्सर्ग कदापि सम्भव नहीं हैं। चित्त अनुपश्यना, धर्म अनुपश्यना आदि प्रत्येक अनुपश्यना के पूर्व में कह आए हैं कि चित्त का निश्चल, स्थिर होना ध्यान साथ एक सूत्र दिया गया है। यथा है। चिन्तन, मनन, अनुप्रेक्षा, भावना, संकल्प, विकल्प आदि से "यावदेव जाणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय अनिसित्तो च विहरति चित्त सक्रिय अस्थिर रहता है, निश्चल नहीं होता है, अत: तब न च किञ्चि लोके उपादियति।" तक ध्यान नहीं होता। इन सबसे परे होने पर ही चित्त शान्त व स्थिर होता है। इसे ही समाधि कहा गया है। प्रकारान्तर से कहें (अनुपश्यना में) जब तक मात्र ज्ञान, मात्र दर्शन बना रहता है तब तक अनाश्रित होकर विहार करता है और लोक (शरीर तो निर्विकल्प स्वसंवेदन, चैतन्य रूप दर्शनोपयोग ध्यान है। दर्शन रूप होने से ध्यान को अनुपश्यना व विपश्यना कहा जाता और संसार) में कुछ भी ग्रहण नहीं करता है। भिक्षुओं! इस है। अनुपश्यना-विपश्यना शब्द 'पश्य' क्रिया से बने हैं।' प्रकार भिक्षु अनुपश्यना में अनुपश्यी होकर विहार करता है। 'पश्य' शब्द दृश् (दर्शने) धातु से बना है। अत: ध्यान दर्शनमय ___ इस प्रकार महासतिपट्ठानसुत्त में अनुपश्यी साधक के लिए होता है। दर्शन निर्विकल्प, स्वसंवेदन रूप होता है। जैसा कि किसी भी अनुपश्यना में लोक, शरीर और संसार के आश्रय ध्यान का वर्णन करते हुए तत्त्वानुशासन में कहा है-५ ग्रहण करने तथा क्रिया करने का निषेध है, यहाँ तक कि वेदना, चित्त धर्म आदि अनुपश्यना में जो स्वत: हो रहा है उसका केवल तत्राऽऽत्मन्यासहाये यच्चिन्तायाः स्यान्निरोधनम्। ज्ञाता-द्रष्टा होता है, क्योंकि कोई भी क्रिया लोक का आश्रय तद्ध्यानं तद्भावो वा स्वसंवित्तिमयश्च सः।।५।। लिए बिना नहीं होती है अर्थात् देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि अर्थ- किसी भी सहायता (आश्रय) से रहित आत्मा में जो लौकिक आश्रय लिए बिना नहीं होती है और अनुपश्यना चिन्ता का निरोध है, वह ध्यान है अथवा जो चिन्ता के अभाव (विपश्यना) में लोक का किंचित भी आश्रय ग्रहण न करने का विधान है। 'महासतिपट्टानसुत्त' में ध्यान-साधक के लिए सिर से पाहुडदोहा में कहा हैपैर तक पूरे शरीर के प्रत्येक अंग-उपांग पर उत्पन्न होने वाली जिमि लोणु विजिज्जइ पाणियहं तिमि जइ चित्तु विलिज्ज। संवेदनाओं को देखने एवं उनके अनित्य होने का चिन्तन करने समरसि हवइ जीवड़ा काइं समाहि कारिज्ज।। का भी विधान नहीं है। वे ध्यान से पूर्व की आत्म-निरीक्षण की -पाहुडदोहा, १७६ अर्थात् स्वाध्याय की क्रियाएँ हैं। कारण कि संवेदनाओं को जिस प्रकार नमक पानी में विलीन होकर समरस हो जाता देखना और उनके अनित्य स्वभाव का चिन्तन मन-बुद्धि की है उसी प्रकार यदि चित्त आत्मा में विलीन होकर समरस हो जाये क्रिया से ही सम्भव है, क्योंकि कोई भी क्रिया बिना आश्रय के तो फिर जीव को समाधि में और क्या करना है? अर्थात् चित्त नहीं होती है। कायोत्सर्ग-व्युत्सर्ग में शरीर, संसार, कषाय और का बाह्य विषयों से विमुख हो, आत्म स्वरूप में लीन होना ही कर्म इन सबका व्युत्सर्ग आवश्यक है अर्थात् इनसे असंग होना, समाधि है, ध्यान है। इनके आश्रय का त्याग करना आवश्यक बताया है। श्री जिनसेनाचार्य कहते हैं : पातंजल योग सूत्र में कहा है योगो ध्यानं समाधिश्च धीरोध: स्वान्तः निग्रहः। योगाश्चित्तवृत्ति निरोधः।१-२ अंतः संलीनता चेति तत्पर्यायाः स्मृता बुधेः।। चित्त की वृत्तियों का निरोध होना योग है। २१-२२ आर्ष ० अष्टदशी / 1990 For Private & Personal Use Only Jain Education International www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 2 3 4