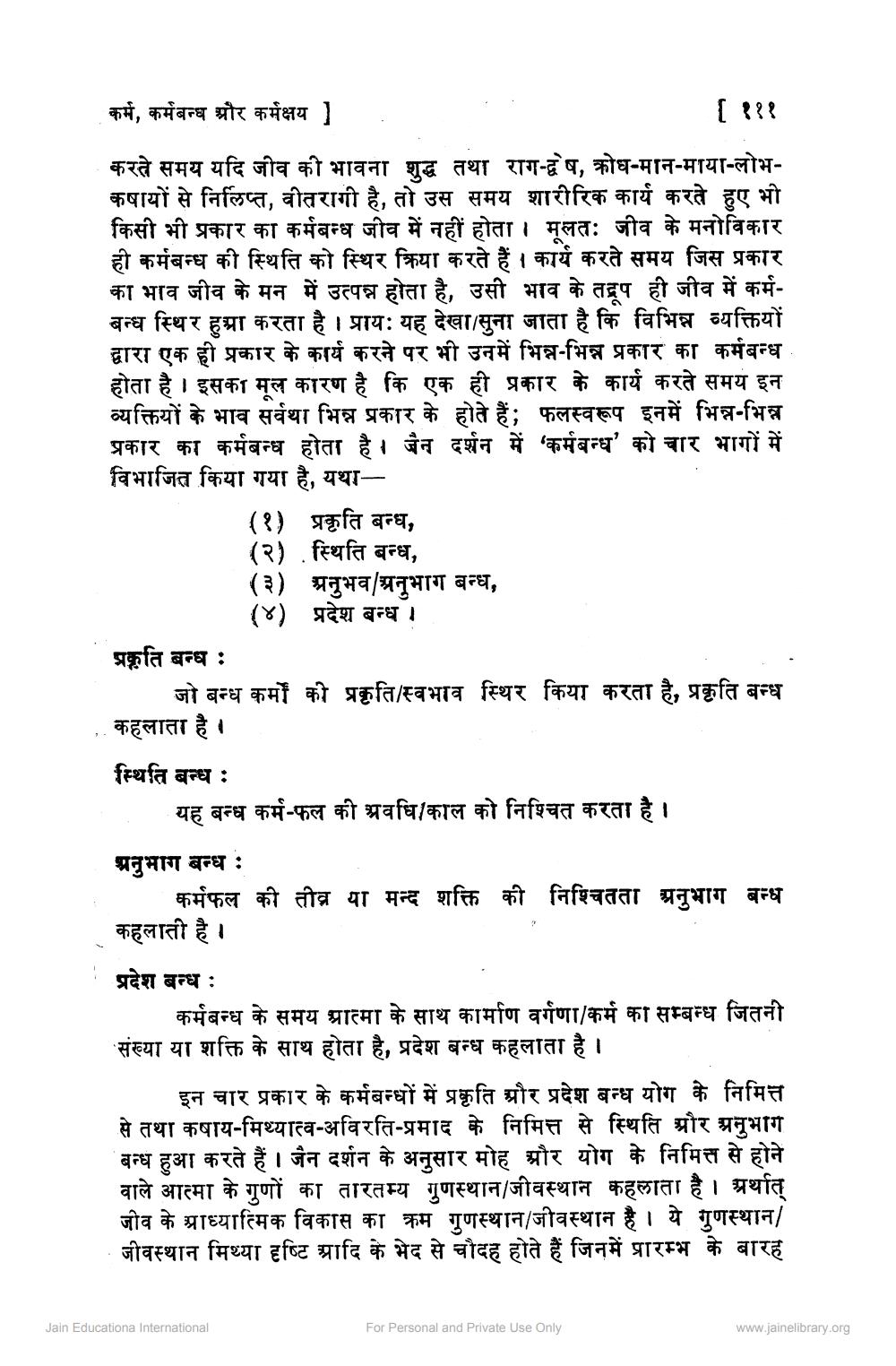Book Title: Karm Karmbandh aur Karmkshay Author(s): Rajiv Prachandiya Publisher: Z_Jinvani_Karmsiddhant_Visheshank_003842.pdf View full book textPage 5
________________ कर्म, कर्मबन्ध और कर्मक्षय ] [ १११ करते समय यदि जीव की भावना शुद्ध तथा राग-द्वेष, क्रोध - मान-माया-लोभकषायों से निर्लिप्त, वीतरागी है, तो उस समय शारीरिक कार्य करते हुए भी किसी भी प्रकार का कर्मबन्ध जीव में नहीं होता । मूलतः जीव के मनोविकार ही कर्मबन्ध की स्थिति को स्थिर क्रिया करते हैं । कार्य करते समय जिस प्रकार का भाव जीव के मन में उत्पन्न होता है, उसी भाव के तद्रूप ही जीव में कर्मबन्ध स्थिर हुआ करता है । प्राय: यह देखा / सुना जाता है कि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा एक ही प्रकार के कार्य करने पर भी उनमें भिन्न-भिन्न प्रकार का कर्मबन्ध होता है । इसका मूल कारण है कि एक ही प्रकार के कार्य करते समय इन व्यक्तियों के भाव सर्वथा भिन्न प्रकार के होते हैं; फलस्वरूप इनमें भिन्न-भिन्न प्रकार का कर्मबन्ध होता है । जैन दर्शन में 'कर्मबन्ध' को चार भागों में विभाजित किया गया है, यथा स्थिति बन्ध : (१) प्रकृति बन्ध, (२) स्थिति बन्ध, (३) (४) प्रकृति बन्ध : जो बन्ध कर्मों की प्रकृति / स्वभाव स्थिर किया करता है, प्रकृति बन्ध कहलाता है । अनुभव / अनुभाग बन्ध, प्रदेश बन्ध । यह बन्ध कर्म - फल की अवधि / काल को निश्चित करता है । अनुभाग बन्ध : कर्मफल की तीव्र या मन्द शक्ति की निश्चितता अनुभाग बन्ध कहलाती है । Jain Educationa International प्रदेश बन्ध : कर्मबन्ध के समय श्रात्मा के साथ कार्माण वर्गणा / कर्म का सम्बन्ध जितनी संख्या या शक्ति के साथ होता है, प्रदेश बन्ध कहलाता है । इन चार प्रकार के कर्मबन्धों में प्रकृति और प्रदेश बन्ध योग के निमित्त से तथा कषाय- मिथ्यात्व - अविरति प्रमाद के निमित्त से स्थिति और अनुभाग बन्ध हुआ करते हैं । जैन दर्शन के अनुसार मोह और योग के निमित्त से होने वाले आत्मा के गुणों का तारतम्य गुणस्थान / जीवस्थान कहलाता है । अर्थात् जीव के प्राध्यात्मिक विकास का क्रम गुणस्थान / जीवस्थान है । ये गुणस्थान / जीवस्थान मिथ्या दृष्टि आदि के भेद से चौदह होते हैं जिनमें प्रारम्भ के बारह For Personal and Private Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 3 4 5 6