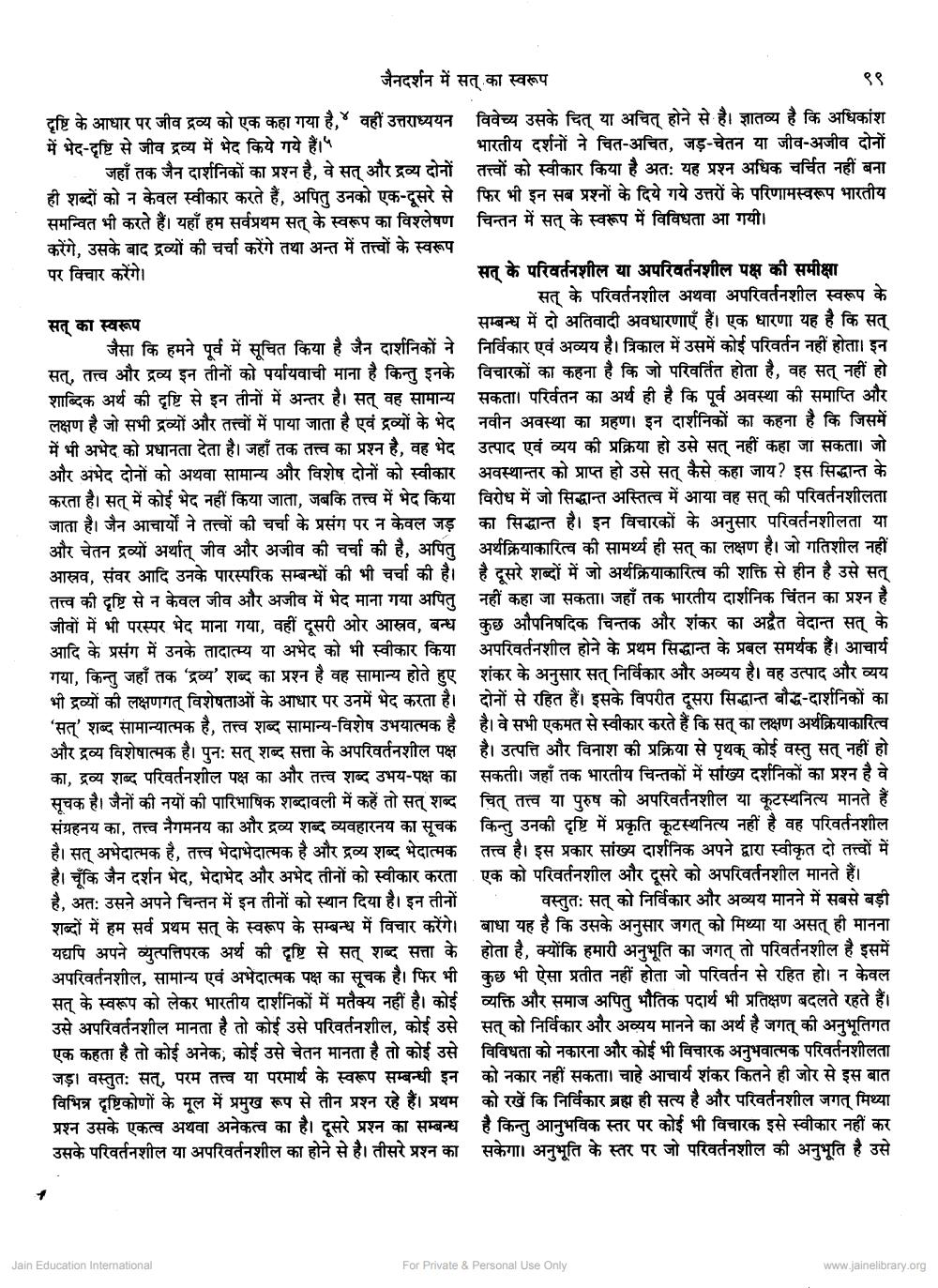Book Title: Jaindarshan me Sat ka Swarup Author(s): Sagarmal Jain Publisher: Z_Shwetambar_Sthanakvasi_Jain_Sabha_Hirak_Jayanti_Granth_012052.pdf View full book textPage 3
________________ दृष्टि के आधार पर जीव द्रव्य को एक कहा गया है, में भेद दृष्टि से जीव द्रव्य में भेद किये गये है। 4 जैनदर्शन में सत् का स्वरूप वहीं उत्तराध्ययन जहाँ तक जैन दार्शनिकों का प्रश्न है, वे सत् और द्रव्य दोनों ही शब्दों को न केवल स्वीकार करते हैं, अपितु उनको एक-दूसरे से समन्वित भी करते हैं। यहाँ हम सर्वप्रथम सत् के स्वरूप का विश्लेषण करेंगे, उसके बाद द्रव्यों की चर्चा करेंगे तथा अन्त में तत्त्वों के स्वरूप पर विचार करेंगे। Jain Education International सत् का स्वरूप जैसा कि हमने पूर्व में सूचित किया है जैन दार्शनिकों ने सत्, तत्त्व और द्रव्य इन तीनों को पर्यायवाची माना है किन्तु इनके शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से इन तीनों में अन्तर है सत् वह सामान्य लक्षण है जो सभी द्रव्यों और तत्त्वों में पाया जाता है एवं द्रव्यों के भेद में भी अभेद को प्रधानता देता है जहाँ तक तत्त्व का प्रश्न है, वह भेद और अभेद दोनों को अथवा सामान्य और विशेष दोनों को स्वीकार करता है। सत् में कोई भेद नहीं किया जाता, जबकि तत्त्व में भेद किया जाता है। जैन आचार्यों ने तत्वों की चर्चा के प्रसंग पर न केवल जड़ और चेतन द्रव्यों अर्थात् जीव और अजीव की चर्चा की है, अपितु आसव, संवर आदि उनके पारस्परिक सम्बन्धों की भी चर्चा की है। तत्त्व की दृष्टि से न केवल जीव और अजीव में भेद माना गया अपितु जीवों में भी परस्पर भेद माना गया, वहीं दूसरी ओर आस्रव, बन्ध आदि के प्रसंग में उनके तादात्म्य या अभेद को भी स्वीकार किया गया, किन्तु जहाँ तक 'द्रव्य' शब्द का प्रश्न है वह सामान्य होते हुए भी द्रव्यों की लक्षणगत् विशेषताओं के आधार पर उनमें भेद करता है। 'सत्' शब्द सामान्यात्मक है, तत्त्व शब्द सामान्य विशेष उभयात्मक है और द्रव्य विशेषात्मक है। पुनः सत् शब्द सत्ता के अपरिवर्तनशील पक्ष का द्रव्य शब्द परिवर्तनशील पक्ष का और तत्त्व शब्द उभय पक्ष का सूचक है। जैनों की नयों की पारिभाषिक शब्दावली में कहें तो सत् शब्द संग्रहनय का, तत्त्व नैगमनय का और द्रव्य शब्द व्यवहारनय का सूचक है। सत् अभेदात्मक है, तत्त्व भेदाभेदात्मक है और द्रव्य शब्द भेदात्मक है। चूँकि जैन दर्शन भेद, भेदाभेद और अभेद तीनों को स्वीकार करता है, अतः उसने अपने चिन्तन में इन तीनों को स्थान दिया है। इन तीनों शब्दों में हम सर्व प्रथम सत् के स्वरूप के सम्बन्ध में विचार करेंगे। यद्यपि अपने व्युत्पत्तिपरक अर्थ की दृष्टि से सत् शब्द सत्ता के अपरिवर्तनशील, सामान्य एवं अभेदात्मक पक्ष का सूचक है। फिर भी सत् के स्वरूप को लेकर भारतीय दार्शनिकों में मतैक्य नहीं है कोई उसे अपरिवर्तनशील मानता है तो कोई उसे परिवर्तनशील, कोई उसे एक कहता है तो कोई अनेक, कोई उसे चेतन मानता है तो कोई उसे जड़। वस्तुतः सत्, परम तत्त्व या परमार्थ के स्वरूप सम्बन्धी इन विभिन्न दृष्टिकोणों के मूल में प्रमुख रूप से तीन प्रश्न रहे हैं। प्रथम प्रश्न उसके एकत्व अथवा अनेकत्व का है। दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध उसके परिवर्तनशील या अपरिवर्तनशील का होने से है। तीसरे प्रश्न का । ९९ विवेच्य उसके चित् या अचित् होने से है। ज्ञातव्य है कि अधिकांश भारतीय दर्शनों ने चित-अचित, जड़-चेतन या जीव-अजीव दोनों तत्वों को स्वीकार किया है अतः यह प्रश्न अधिक चर्चित नहीं बना फिर भी इन सब प्रश्नों के दिये गये उत्तरों के परिणामस्वरूप भारतीय चिन्तन में सत् के स्वरूप में विविधता आ गयी। सत् के परिवर्तनशील या अपरिवर्तनशील पक्ष की समीक्षा । सत् के परिवर्तनशील अथवा अपरिवर्तनशील स्वरूप के सम्बन्ध में दो अतिवादी अवधारणाएं हैं। एक धारणा यह है कि सत् निर्विकार एवं अव्यय है त्रिकाल में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इन विचारकों का कहना है कि जो परिवर्तित होता है, वह सत् नहीं हो सकता परिवर्तन का अर्थ ही है कि पूर्व अवस्था की समाप्ति और नवीन अवस्था का ग्रहण इन दार्शनिकों का कहना है कि जिसमें उत्पाद एवं व्यय की प्रक्रिया हो उसे सत् नहीं कहा जा सकता। जो अवस्थान्तर को प्राप्त हो उसे सत् कैसे कहा जाय ? इस सिद्धान्त के विरोध में जो सिद्धान्त अस्तित्व में आया वह सत् की परिवर्तनशीलता का सिद्धान्त है। इन विचारकों के अनुसार परिवर्तनशीलता या अर्थक्रियाकारित्व की सामर्थ्य ही सत् का लक्षण है जो गतिशील नहीं है दूसरे शब्दों में जो अर्थक्रियाकारित्व की शक्ति से हीन है उसे सत् नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक भारतीय दार्शनिक चिंतन का प्रश्न है कुछ औपनिषदिक चिन्तक और शंकर का अद्वैत वेदान्त सत् के अपरिवर्तनशील होने के प्रथम सिद्धान्त के प्रबल समर्थक हैं। आचार्य शंकर के अनुसार सत् निर्विकार और अव्यय है वह उत्पाद और व्यय दोनों से रहित हैं। इसके विपरीत दूसरा सिद्धान्त बौद्ध दार्शनिकों का है। वे सभी एकमत से स्वीकार करते हैं कि सत् का लक्षण अर्थक्रियाकारित्व है। उत्पत्ति और विनाश की प्रक्रिया से पृथक् कोई वस्तु सत् नहीं हो सकती। जहाँ तक भारतीय चिन्तकों में सांख्य दर्शनिकों का प्रश्न है वे चित् तत्त्व या पुरुष को अपरिवर्तनशील या कूटस्थनित्य मानते हैं किन्तु उनकी दृष्टि में प्रकृति कूटस्थनित्य नहीं है वह परिवर्तनशील तत्व है। इस प्रकार सांख्य दार्शनिक अपने द्वारा स्वीकृत दो तत्त्वों में एक को परिवर्तनशील और दूसरे को अपरिवर्तनशील मानते हैं। वस्तुतः सत् को निर्विकार और अव्यय मानने में सबसे बड़ी बाधा यह है कि उसके अनुसार जगत् को मिथ्या या असत् ही मानना होता है, क्योंकि हमारी अनुभूति का जगत् तो परिवर्तनशील है इसमें कुछ भी ऐसा प्रतीत नहीं होता जो परिवर्तन से रहित हो न केवल व्यक्ति और समाज अपितु भौतिक पदार्थ भी प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। सत् को निर्विकार और अव्यय मानने का अर्थ है जगत् की अनुभूतिगत विविधता को नकारना और कोई भी विचारक अनुभवात्मक परिवर्तनशीलता को नकार नहीं सकता। चाहे आचार्य शंकर कितने ही जोर से इस बात को रखें कि निर्विकार ब्रह्म ही सत्य है और परिवर्तनशील जगत् मिथ्या है किन्तु आनुभविक स्तर पर कोई भी विचारक इसे स्वीकार नहीं कर सकेगा। अनुभूति के स्तर पर जो परिवर्तनशील की अनुभूति है उसे For Private & Personal Use Only - www.jainelibrary.org.Page Navigation
1 2 3 4 5 6 7