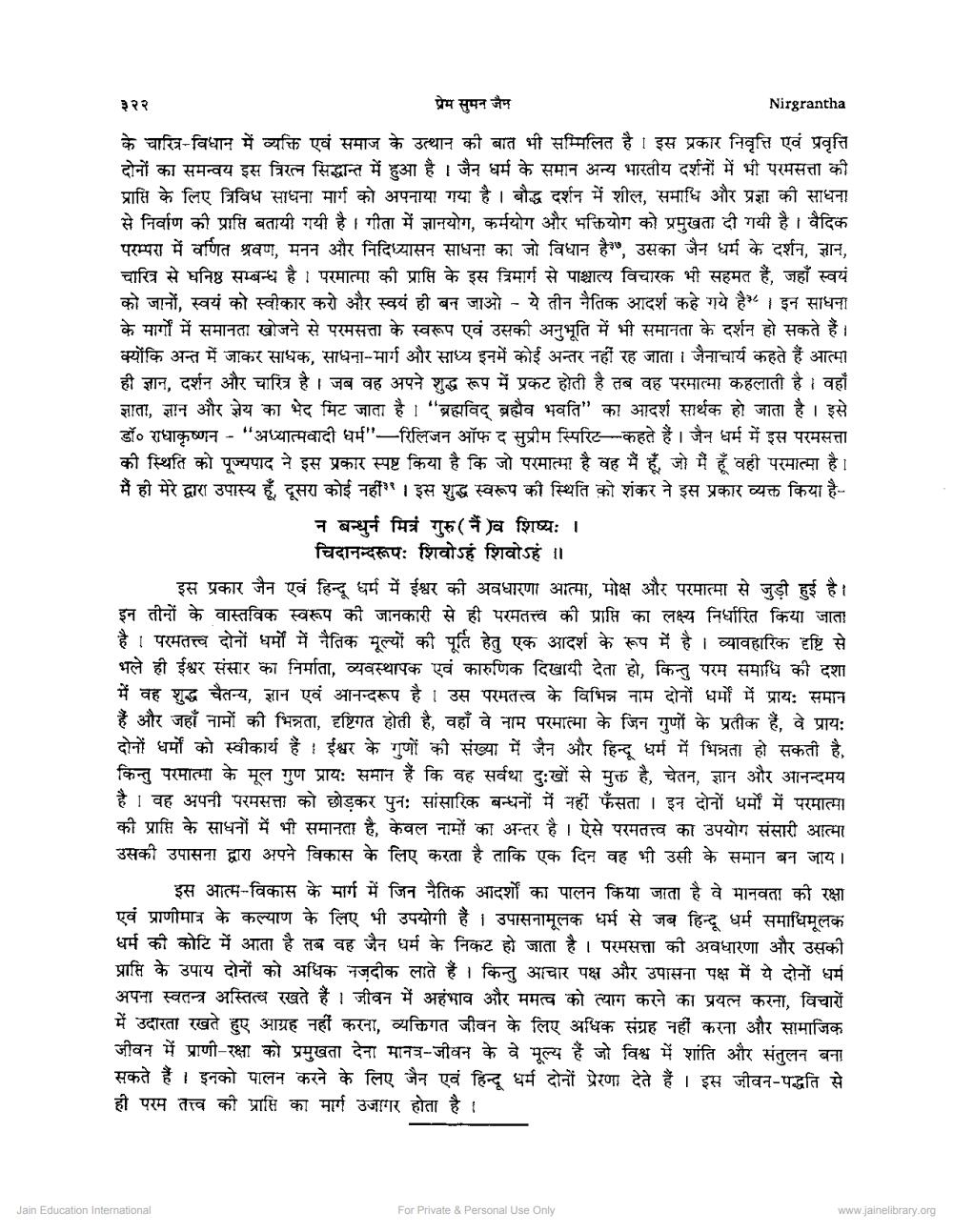Book Title: Jain evam Hindu Dharm me Param Tattva ki Avadharna Author(s): Prem Suman Jain Publisher: Z_Nirgrantha_1_022701.pdf and Nirgrantha_2_022702.pdf and Nirgrantha_3_022703.pdf View full book textPage 7
________________ ३२२ प्रेम सुमन जैन Nirgrantha के चारित्र-विधान में व्यक्ति एवं समाज के उत्थान की बात भी सम्मिलित है। इस प्रकार निवृत्ति एवं प्रवृत्ति दोनों का समन्वय इस त्रिरत्न सिद्धान्त में हुआ है। जैन धर्म के समान अन्य भारतीय दर्शनों में भी परमसत्ता की प्राप्ति के लिए त्रिविध साधना मार्ग को अपनाया गया है। बौद्ध दर्शन में शील, समाधि और प्रज्ञा की साधना से निर्वाण की प्राप्ति बतायी गयी है। गीता में ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग को प्रमुखता दी गयी है। वैदिक परम्परा में वर्णित श्रवण, मनन और निदिध्यासन साधना का जो विधान है, उसका जैन धर्म के दर्शन, ज्ञान, चारित्र से घनिष्ठ सम्बन्ध है। परमात्मा की प्राप्ति के इस त्रिमार्ग से पाश्चात्य विचारक भी सहमत है, जहाँ स्वयं को जानों, स्वयं को स्वीकार करो और स्वयं ही बन जाओ ये तीन नैतिक आदर्श कहे गये है"। इन साधना के मार्गों में समानता खोजने से परमसत्ता के स्वरूप एवं उसकी अनुभूति में भी समानता के दर्शन हो सकते हैं। क्योंकि अन्त में जाकर साधक, साधना मार्ग और साध्य इनमें कोई अन्तर नहीं रह जाता। जैनाचार्य कहते हैं आत्मा ही ज्ञान, दर्शन और चारित्र है। जब वह अपने शुद्ध रूप में प्रकट होती है तब वह परमात्मा कहलाती है। वहाँ ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का भेद मिट जाता है। "ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति" का आदर्श सार्थक हो जाता है। इसे डॉ० राधाकृष्णन "अध्यात्मवादी धर्म" रिलिजन ऑफ द सुप्रीम स्पिरिट — कहते हैं। जैन धर्म में इस परमसत्ता की स्थिति को पूज्यपाद ने इस प्रकार स्पष्ट किया है कि जो परमात्मा है वह मैं हूँ, जो मैं हूँ वही परमात्मा है। मैं ही मेरे द्वारा उपास्य हूँ, दूसरा कोई नहीं"। इस शुद्ध स्वरूप की स्थिति को शंकर ने इस प्रकार व्यक्त किया है - न बन्धुर्न मित्रं गुरु (नैव शिष्यः । चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं ॥ इस प्रकार जैन एवं हिन्दू धर्म में ईश्वर की अवधारणा आत्मा, मोक्ष और परमात्मा से जुड़ी हुई है। इन तीनों के वास्तविक स्वरूप की जानकारी से ही परमतत्त्व की प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है परमतत्त्व दोनों धर्मों में नैतिक मूल्यों की पूर्ति हेतु एक आदर्श के रूप में है। व्यावहारिक दृष्टि से भले ही ईश्वर संसार का निर्माता, व्यवस्थापक एवं कारुणिक दिखायी देता हो, किन्तु परम समाधि की दशा में वह शुद्ध चैतन्य, ज्ञान एवं आनन्दरूप है । उस परमतत्त्व के विभिन्न नाम दोनों धर्मों में प्रायः समान हैं और जहाँ नामों की भिन्नता, दृष्टिगत होती है, वहाँ वे नाम परमात्मा के जिन गुणों के प्रतीक हैं, वे प्रायः दोनों धर्मों को स्वीकार्य है। ईश्वर के गुणों की संख्या में जैन और हिन्दू धर्म में भित्रता हो सकती है. किन्तु परमात्मा के मूल गुण प्रायः समान हैं कि वह सर्वथा दुःखों से मुछ है, चेतन, ज्ञान और आनन्दमय है । वह अपनी परमसत्ता को छोड़कर पुनः सांसारिक बन्धनों में नहीं फँसता । इन दोनों धर्मों में परमात्मा की प्राप्ति के साधनों में भी समानता है. केवल नामों का अन्तर है। ऐसे परमतत्त्व का उपयोग संसारी आत्मा उसकी उपासना द्वारा अपने विकास के लिए करता है ताकि एक दिन वह भी उसी के समान बन जाय । इस आत्म-विकास के मार्ग में जिन नैतिक आदर्शों का पालन किया जाता है वे मानवता की रक्षा एवं प्राणीमात्र के कल्याण के लिए भी उपयोगी हैं । उपासनामूलक धर्म से जब हिन्दू धर्म समाधिमूलक धर्म की कोटि में आता है तब वह जैन धर्म के निकट हो जाता है। परमसत्ता की अवधारणा और उसकी प्राप्ति के उपाय दोनों को अधिक नजदीक लाते हैं। किन्तु आचार पक्ष और उपासना पक्ष में ये दोनों धर्म अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखते हैं। जीवन में अहंभाव और ममत्व को त्याग करने का प्रयत्न करना, विचारों में उदारता रखते हुए आग्रह नहीं करना, व्यक्तिगत जीवन के लिए अधिक संग्रह नहीं करना और सामाजिक जीवन में प्राणी रक्षा को प्रमुखता देना मानव जीवन के वे मूल्य है जो विश्व में शांति और संतुलन बना सकते हैं । इनको पालन करने के लिए जैन एवं हिन्दू धर्म दोनों प्रेरणा देते हैं । इस जीवन-पद्धति से ही परम तत्त्व की प्राप्ति का मार्ग उजागर होता है । Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.orgPage Navigation
1 ... 5 6 7 8 9